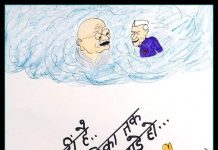प्रो. पार्थनाथ मुखर्जी (3 सितम्बर 1940 – 12 फरवरी 2021) भारतीय समाजशास्त्र की स्वाधीनोत्तर पीढ़ी के यशस्वी नायक थे। साठोत्तरी समाजशास्त्रियों की पहली कतार के प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उनके चिंतन और लेखन में लोकतंत्र, जन-आन्दोलन, और राष्ट्रनिर्माण के बारे में देशज दृष्टि और समाजशास्त्रीय अनुशासन के प्रति सतत सरोकार था। उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र परिषद के लिए 1988-89 में महामंत्री और 2004-05 में अध्यक्ष के रूप में चार बरस का समय दिया। समाज के अध्ययन-अध्यापन में विशिष्ट और बहुआयामी योगदान के लिए भारतीय समाजशास्त्र परिषद ने उन्हें ‘लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड’ से विभूषित किया था।
मैं 1972-74 के तूफानी दौर में उनका 5 सेमेस्टर तक विद्यार्थी रहा। प्रो. जे.एस. गांधी, प्रो.बी.के. नागला, प्रो. जगन्नाथ पाठी और श्री मुकुल दुबे हमारे सहपाठी थे। हम सबसे उनका एक शिक्षक के नाते मर्यादित और मित्रवत व्यवहार था। यह मित्रभाव उनके व्यक्तित्व का मूल गुण था। इसीलिए वह शीघ्र ही ‘प्रो. मुखर्जी’ से ‘पार्थो दा’ बन गए और आजीवन बने रहे। तबसे अगले पांच दशकों तक देश में और विदेश में और अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में भी, अन्य विद्यार्थियों की तरह मुझे भी उनका मार्ग-दर्शन पाने का सौभाग्य रहा।
मैंने इन पचास बरसों में गांधी विद्या संस्थान (वाराणसी) से लेकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (शिमला) के परिसंवादों में और इंडियन सोशियोलाजिकल सोसायटी से लेकर इन्टरनेशनल सोशिओलाजिकल एसोसिएशन के सम्मेलनों में सहभागी रहकर उनको निकट से जाना था। इस दौरान मैं प्रो. पार्थनाथ मुखर्जी के जयप्रकाश नारायण से लेकर किशन पटनायक और गुन्नार मिर्डल से लेकर इमानुएल वालरस्टाइन के संबंधों का भी साक्षी बना।
1940 में गया में जनमे और पटना में उच्च शिक्षा प्राप्त प्रो. पार्थनाथ मुखर्जी एक आदर्शवादी और निर्मल बौद्धिक थे। उनका जीवन यशमय था। उन्होंने अपने निजी और सार्वजनिक जीवन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाने में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, एकनिष्ठ पति, स्नेहिल पिता, विश्वसनीय मित्र, प्रेरणादायक शिक्षक, प्रतिष्ठित समाजशास्त्री, सरोकारी नागरिक और सद्भावपूर्ण मनुष्य के रूप में सबका अपनत्व पाया। वह किशोरावस्था से ही रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के चिंतन के प्रति आकर्षित थे। भारतीय समाजशास्त्र की दुनिया में उनका प्रो. नर्मदेश्वर प्रसाद और प्रो. रामकृष्ण मुखर्जी से गुरु-शिष्य का संबंध था। जेएनयू के एक दशक के कार्यकाल में उन्होंने प्रो. योगेन्द्र सिंह, प्रो. टी.के. ओम्मन, प्रो. एम.एन. पाणिनि, प्रो. के.एल. शर्मा और अनेक अन्य सहकर्मियों से आत्मीय रिश्ता बनाया। उनकी सज्जनता के कारण हर अगले पड़ाव पर कई और मित्र बने।
हर व्यक्ति की तरह उनके व्यक्तिगत और बौद्धिक जीवन में एकाध अप्रिय प्रसंग भी आए। 1988 में अपनी धर्मपत्नी को कैंसर से बचाने में असफलता ने उन्हें बहुत व्यक्तिगत पीड़ा दी। शैक्षणिक संसार में कुछ महत्त्वाकांक्षी सहकर्मियों ने द्वेष और असत्य का जाल बिछाया। लेकिन उन्होंने इस सब के प्रति द्रष्टाभाव रखा। इनकी परछाईं आगे की जिन्दगी पर नहीं पड़ने दी। मन में कटुता नहीं पनपने दी। वह क्षमाशील थे। तभी पटना, कोलकाता और वाराणसी से लेकर दिल्ली और मुंबई तक उनके सहयोगियों और विद्यार्थियों का व्यापक दायरा था।
वैचारिक पूर्वाग्रहों के प्रति सावधानी और तथ्य-आधारित दृष्टिकोण प्रो. मुखर्जी के अध्ययनों की उल्लेखनीय विशेषता थी। ग्रामदान आंदोलन और माओवादी किसान आंदोलन दोनों के अध्ययन में योगदान करनेवाले एकमात्र समाजशास्त्री के रूप में महत्त्वपूर्ण बने।
अपने छह दशक लम्बे सक्रिय बौद्धिक जीवन में आत्म-प्रचार से दूर रहकर प्रो. मुखर्जी ने शोधकर्ता, अध्यापक, संस्था-निदेशक, संगठनकर्ता और सरोकारी बुद्धिजीवी जैसी सभी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का अनुकरणीय तरीके से निर्वाह किया। लेकिन हर दौर में उनका सत्ता-प्रतिष्ठान और निहित स्वार्थों के प्रति एक स्वस्थ आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहा।
पार्थो दा देश के चार उल्लेखनीय उच्च अध्ययन केन्द्रों – पटना वि.वि. (1963-70), दिल्ली वि.वि. (1970-72), जवाहरलाल नेहरू वि.वि. (1972-79) और टाटा समाजविज्ञान संस्थान (1980-96) के लोकप्रिय शिक्षक रहे। उनकी विद्वत्ता और जीवनशैली की समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की चार पीढ़ियों पर अमिट छाप पड़ी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (कोलकाता/ दिल्ली) से अपनी संबद्धता की अवधि में उन्होंने ग्रामीण श्रमजीवियों की जीवन-दशा और सुधार के कई अनदेखे पहलुओं के अध्ययन से अपने को जोड़ा। ‘खालिस्तान’ और सिख अस्मिता के विश्लेषण में योगदान किया। इसके आगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (मुंबई) और कौंसिल ऑफ़ सोशल डेवलपमेंट (दिल्ली) के निदेशक बनकर लोकहितकारी शोधकार्यों को प्रोत्साहन देकर उन्होंने इन राष्ट्रीय संस्थानों का भविष्य प्रकाशमान किया। ओल टॉर्नक्विस्ट और मनोरंजन मोहंती के साथ जन-अधिकार आंदोलनों के बारे में प्रस्तुत शोध बहुचर्चित बना। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (दिल्ली) के मानद प्रोफेसर की भूमिका में ग्रामीण भारत की चुनौतियों को रेखांकित करके भारतीय राष्ट्र-निर्माण के विमर्श में इस संस्थान के लिए नए आयाम जोड़े।
भारतीय समाजशास्त्र परिषद के प्रति उनके मन में एक विशेष प्रतिबद्धता थी। यह तो बराबर याद रहेगा कि उन्होंने इसी परिषद के माध्यम से दक्षिण एशिया में समाजशास्त्रियों की निकटता में बुनियादी योगदान करके इस तनावग्रस्त क्षेत्र में समाजशास्त्रियों के बीच संवाद की जरूरत को महत्त्वपूर्ण बनाया।
इस स्मृतिलेख के अंत में सिर्फ यही दिलासा की बात है कि सभी सृजनशील बुद्धिजीवी देहांत के बाद भी अपनी रचनाओं के जरिये प्रासंगिक बने रहते हैं। प्रो. पार्थनाथ मुखर्जी की रचनाओं में, अनेकों लेखों और व्याख्यानों के साथ ही, ‘फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म टु इलेक्टोरल पोलिटिक्स’ (1983), ‘इंडियन सोशिओलाजी’ (1986), ‘सोशिओलोजी इन साउथ एशिया’ (1997), ‘पीपल्स राइट्स : सोशल मूवमेंट्स इन साउथ एशिया’ (1997), ‘मेथडॉलजी इन सोशल रिसर्च – एसेज इन ऑनर ऑफ़ रामकृष्ण मुखर्जी’ (2000), ‘इंडीजेनेटी एंड युनिवेर्सेलेटी इन सोशल साइंस : ए साउथ एशियन पर्सपेक्टिव’ (2004), और ‘पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटाइजेशन’ (2007) बहुत महत्त्वपूर्ण रही हैं। नि:संदेह यह सब उनकी बहुमूल्य विरासत हैं और इनके जरिये आनेवाली पीढ़ियों के लिए प्रो. पार्थनाथ मुखर्जी के ज्ञान-प्रकाश और मार्ग-दर्शन की निरंतरता बनी रहेगी……