(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में सच्चिदा जी की पुस्तिका आज से समता मार्ग पर धारावाहिक रूप से प्रकाशित होगी। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
हमारा निजी रहन-सहन कैसा होता है, इसके सामाजिक प्रभाव के संबंध में बहुत विचार नहीं किया जाता। ऐसे लोग भी, जो समाज-परिवर्तन करना चाहते हैं, समाज से गरीबी मिटाना चाहते हैं और समता लाना चाहते हैं, खुद कैसे रहते हैं इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमारा रहन-सहन और उपभोग का स्तर वास्तव में एक नितांत निजी मामला नहीं है। यह एक विशेष वातावरण की उपज है और स्वयं एक वातावरण बनाता है। यह वातावरण बहुत हद तक समाज के विकास की दिशा को प्रभावित करता है और इस बात का भी निर्धारण करता है कि उपलब्ध साधनों का कैसे उपयोग होगा। अतः यह एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।
निजी रहन-सहन के संबंध में इस लापरवाही को वामपंथी और मार्क्सवादी पार्टियों में एक तरह की सैद्धांतिक मान्यता प्राप्त हो गयी थी। एक यूरोपीय वामपंथी ने इस संबंध में एक दिलचस्प बात बतायी। उसने बताया कि मार्क्स की स्वयं की आदतें फिजूलखर्ची की थीं हालाँकि उनकी जिंदगी प्रायः अभाव में ही बीती। इस व्यक्ति ने यह भी बताया कि पश्चिम के मार्क्सवादी मार्क्स की इस कमजोरी को अपनी फिजूलखर्ची के समर्थन में उदाहरण की तरह पेश करते हैं। भारत में भी जब किसी वामपंथी नेता के खर्चीले रहन-सहन की आलोचना की जाती है तो झट से यह जवाब मिलता है- ‘हमारा काम श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊपर उठाना है, खुद अपने जीवन-स्तर को नीचे गिराना नहीं।’शुरू में समाजवादियों और गांधीवादियों के बीच अकसर यह एक विवाद का मुद्दा रहता था। यह बात अलग है कि आमतौर पर समाजवादी कार्यकर्ताओं का जीवन बहुत ही सादगी और कभी-कभी तो अत्यंत गरीबी का होता था, क्योंकि ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए दूसरे तरह की जिंदगी संभव नहीं थी। जब सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह हाल था तो आम आदमी में इस विषय पर सोचने की जरूरत कैसे पैदा होती?
इस समस्या को इस तरह नजरअंदाज करने के पीछे एक कारण यह भी था कि आजादी के पहले तक शहरी संस्कृति के तामझाम का प्रभाव बहुत सीमित था और उपभोक्तावादी संस्कृति अपने आप में विचार-विमर्श का विषय नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह संस्कृति जलकुंभी की तरह समाज पर छाती गयी है। जो गरीब हैं वे तो गरीबी के कारण इससे अछूते रह जाते हैं या इसके प्रभाव से और गरीब होते चले जाते हैं, लेकिन मध्यमवर्ग में तो यह महामारी की तरह फैल गयी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के रहन-सहन और इसके प्रति उनकी दृष्टि का भी इस संस्कृति से गहरा संबंध है। अतः इस प्रश्न पर पूरी स्पष्टता की जरूरत है।
एक कारण और था जिससे वामपंथी लोगों में उपभोग की सीमा के सवाल पर कोई विचार नहीं होता था। यह मान लिया जाता था कि औद्योगिक उत्पादन की क्षमता सीमाहीन है और इसके अंधाधुंध प्रसार से कोई सामाजिक समस्या पैदा नहीं होगी। यह विचार भी पश्चिमी देशों से ही हमें मिला था। लेकिन अब पश्चिम के अधिकतर वैज्ञानिक और चिंतक भी यह मानने लगे हैं कि इस उत्पादन की एक सीमा है और हम उस सीमा के काफी करीब आ चुके हैं। इस कारण वहाँ छात्रों तथा बुद्धिजीवियों के बीच एक नया वामपंथ पैदा हो रहा है, जो प्राकृतिक साधनों की सीमाओं, प्रदूषण आदि समस्याओं के साथ वामपंथ को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इन लोगों ने भी यह अनुभव किया है कि मानव विकास की कल्पना प्रकृति द्वारा बाँधी गयी सीमाओं के भीतर ही की जा सकती है। स्पष्ट है कि कोई भी दीर्घकालीन विकास प्राकृतिक साधनों के अपव्यय को रोककर ही संभव है। हमारा उपभोग कितना और किन वस्तुओं का हो वह इससे सीधा जुड़ा हुआ है। इस तरह उपभोक्तावादी संस्कृति एक तरह से समाज के विकास के लिए सबसे प्रमुख अवरोध बन गयी है।
इस सवाल पर साफ दृष्टि की इसलिए भी जरूरत है कि उपभोक्तावाद का दबाव बहुत जबरदस्त होता है। किसी व्यक्ति के इर्द-गिर्द लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं आदि की देखादेखी ही वह अपना रहन-सहन बनाने की कोशिश करता है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी स्तर के उपभोग को सामान्य मान ले तो वह इस दबाव से नहीं बच सकता। इससे वह तभी बचेगा जब उसे यह पता हो कि कौन सी सामाजिक शक्तियाँ इस दबाव के पीछे काम करती हैं और कैसे वे उसके बुनियादी मूल्यों के विपरीत प्रभाव डालती हैं या उन उद्देश्यों को नष्ट करनेवाली हैं जिनको लेकर वह चलता है। आज उपभोक्तावाद पूँजीवादी शोषण व्यवस्था का परिणाम भर नहीं है बल्कि उसे जिंदा रखने का सबसे कारगर हथियार भी है। इसलिए भी संघर्ष को उपभोक्तावाद के खिलाफ केंद्रित करना जरूरी हो जाता है। यह पुस्तिका उपभोक्तावाद के विभिन्न पहलुओं पर इसी दृष्टि से विचार करती है।
जब हम उपभोक्तावादी संस्कृति की बात करते हैं तो उपभोग तथा उपभोक्तावाद में फर्क करते हैं। उपभोग जीवन की बुनियादी जरूरत है। इसके बगैर न जीवन संभव है और न वह सब जिससे हम जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह के उपभोग में हमारा भोजन शामिल है जिसके बिना हम जी नहीं सकते या कपड़े शामिल हैं जो शरीर ढँकने के लिए और हमें गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाने के लिए जरूरी हैं। इसी तरह जीवन की रक्षा करनेवाली या शरीर की तकलीफों को दूर करनेवाली दवाएँ, ऋतुओं के प्रकोप से बचाने के लिए घर, ये सब उपभोग की वस्तुएँ हैं। औरतों और मर्दों द्वारा एक-दूसरे को आकर्षित करने के शृंगार के कुछ साधन भी उपभोग की वस्तुओं में आते हैं। यह बिलकुल प्राकृतिक और स्वाभाविक जरूरत है। मनुष्य में ही नहीं, पशु-पक्षियों और पेड़- पौधों में भी नर और मादा के बीच आकर्षण पैदा करने के लिए सुंदर रंगीन बाल, रोंएँ और पंख, भड़कीले रूप, मीठे संगीतमय स्वर तथा तरह-तरह की गंध प्रकृति की देन हैं। इन सब गुणों की उपयोगिता जीवों में विभिन्न मात्रा में रूप, रंग, गंध, स्वर आदि के प्रति स्वभाव से प्राप्त आकर्षण से आती है। यही स्वाभाविक आकर्षण एक ऊँचाई पर मनुष्यों में सौंदर्य-बोध को जन्म देता है। अपने परिवेश को नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्ति आदि से सजाना या साहित्य और विज्ञान के जरिए अपने वातावरण का प्रतीकात्मक अनुभव करना, मनुष्य को सबसे ऊँचे दर्जे का आनंद देता है। इस प्रक्रिया में निर्मित कलावस्तु, पुस्तक आदि सब मनुष्य के स्वाभाविक उपभोग के क्षेत्र में आते हैं। संक्षेप में उपभोग की वस्तुएँ वे हैं, जिनके अभाव में हम स्वाभाविक रूप से अप्रीतिकर तनाव का अनुभव करते हैं– चाहे वह भोजन के अभाव में भूख की पीड़ा से उत्पन्न हो अथवा संगीत एवं कलाओं के अभाव में नीरसता की पीड़ा से।
इसके विपरीत ऐसी वस्तुएँ, जो वास्तव में मनुष्य की किसी मूल जरूरत या कला और ज्ञान की वृत्तियों की दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से प्रचार के द्वारा उसके लिए जरूरी बना दी गयी हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति की देन हैं। पुराने सामंती या अंधविश्वासी समाज में भी ऐसी वस्तुओं का उपभोग होता था जो उपयोगी नहीं थीं बल्कि कष्टदायक थीं– उदाहरण के लिए चीन में कुलीन महिलाओं के लिए बचपन से पाँव को छोटे जूते में कसकर छोटा रखने का रिवाज, लेकिन यह प्रचलन औरतों की गुलामी और मर्दों की मूर्खता का परिणाम था। अतः शोषण की समाप्ति या चेतना बढ़ने के साथ इसका अंत होना लाजिमी था, लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति ऐसी वस्तुओं को शुद्ध व्यावसायिकता के कारण योजनाबद्ध रूप से लोगों पर आरोपित करती है और मनोविज्ञान की आधुनिकतम खोजों का इसके लिए प्रयोग करती है कि इन वस्तुओं की माया लोगों पर इस हद तक छा जाए कि वे इसके लिए पागल बने रहें।
( जारी )
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



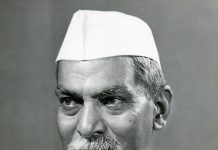














इस पुस्तिका के प्रकाशन केलिए आपका हार्दिक आभार !