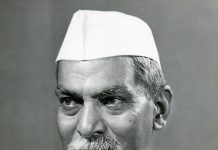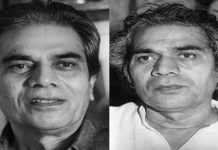(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
औद्योगिक मानसिकता
थोक पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली के विकास और पूँजीवादी व्यवस्था के वर्चस्व के साथ तेजी से बड़ी मात्रा में उत्पादन अब जीवन के हर क्षेत्र का लक्ष्य बन गया। एसेंबली लाइन अब कारखाने की छत के नीचे ही सीमित नहीं रही, सारी दुनिया इसके दायरे में आने लगी। उत्पादन के क्षेत्र में अब पूरे देश से या दुनिया भर के अर्ध तैयार सामान को किसी बड़ी जानी-मानी कंपनी की छत्रछाया में इकट्ठा कर अंतिम रूप दिया जाने लगा। धीरे-धीरे पूँजीवादी उत्पादन की आवश्यकता और इसके मानक पूरे समाज पर हावी होने लगे। खासतौर से शिक्षा व्यवस्था और बौद्धिक क्षेत्र में यह पूरी तरह से हावी हो गया है। अब शिक्षा और शोध संस्थान भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के ढाँचे पर एसेंबली लाइन का रूप ग्रहण करने लगे हैं। शिक्षा का उद्देश्य जीवन और उसकी समस्याओं को समझाना और उनके मानवीय दायित्वों के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करने के बजाय औद्योगिक समाज की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना बन गया है।
औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया की तरह शिक्षा और शोध भी खंडित हो गये हैं जिसका उद्देश्य छोटे-छोटे क्षेत्रों के विशेषज्ञ पैदा करना भर हो गया है। ऐसे विशेषज्ञ अकसर अपने विषय के पूर्ण स्वरूप और समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। हजारों लोगों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किये जा रहे शोध कार्यों के उद्देश्य का ज्ञान सिर्फ उन वृहत् प्रतिष्ठानों को होता है जो उनके शोध का उपयोग किसी खास उद्देश्य के लिए करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में औद्योगिक या सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं। ये प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयों को विशेष तरह की शिक्षा या शोध के लिए अनुदान देते हैं। जिसके बिना बड़े पैमाने पर शिक्षा या शोध का काम नहीं हो सकता। इस तरह शिक्षा-व्यवस्था पर औद्योगिक प्रणाली के मूल्य हावी होते जा रहे हैं।
उद्योगों की मानसिकता अब इस हद तक व्यापक होती जा रही है कि कलाकारों, साहित्यकारों एवं समाजशास्त्रियों के ‘वर्कशाप’ गठित होने लगे हैं जो एक हद तक पूँजीवादी समाज में लोगों की बनती हुई स्थिति का प्रतीक भी है। पूँजीवाद समाज में कला, साहित्य या समाजशास्त्र, सभी का अंतिम मूल्य बाजारू मूल्य बन जाता है, जिसमें महत्त्व इस बात का नहीं है कि किसी कलाकार या साहित्यकार ने कितनी गहरी अनुभूति या मानवीय सत्य को सफल अभिव्यक्ति दी है बल्कि यह है कि उसने एक व्यावसायिक समाज की जरूरत के हिसाब से कितना खपत के लायक माल तैयार किया है। अगर इस दूसरी कसौटी पर उसका माल ठीक उतरता है तो फिर उसकी सफलता निश्चित है। फिर रेडियो, टीवी और अखबारों की सुर्खियों से रँगकर वह ख्यातिप्राप्त लेखक या कलाकार बन जाएगा।
एसेंबली लाइन से जुड़े कलाकार, विचारक और साहित्यकार को बस उस चीज का अधिकार नहीं है जिसको पूर्ववर्ती समाज में उसकी सबसे बड़ी निधि माना जाता था– एक हद का एकांत जीवन और चिंतन, क्योंकि उन्हें सब कुछ औरों के साथ औरों के चिंतन से जुड़कर करना है। एक हद तक कला और साहित्य सदा कलाकार-साहित्यकार समुदाय के भीतर विकसित होते थे। इसमें विचारों के आदान-प्रदान और चयन से मौलिक चीजें निकलती थीं। लेकिन अब कलाकारों-साहित्यकारों का नया समुदाय एक व्यावसायिक समुदाय बन रहा है जिसमें कलाकार या साहित्यकार को विशेष योजना के तहत ‘इकट्ठा’ शब्द के असली अर्थ में एक छत के नीचे इकट्ठा किया जाता है। इस तरह के व्यावसायिक उद्यम में पुस्तक की कल्पना का संयोजन अब लेखक का निजी मामला नहीं। इसके लिए उसे पहले प्रकाशकों की योजना को जानना-समझना होता है और फिर उसके अनुसार लिखना होता है। इसके बाद भी अगर प्रकाशकों के हिसाब से बात ठीक नहीं बन पायी तो आधे दर्जन संपादक उसे काट-छाँट और संवर्धित कर उस रूप में ला देंगे जो बाजार की चाह के मुताबिक है। अगर लेखक को जीना है तो अपना नाम भर इस रचना को दे देना है जो वास्तव में उसकी नहीं रही।
ऐसे समाज में धीरे-धीरे आदमी की संवेदनशीलता और सृजनशीलता नष्ट होती चली जाती है। आदमी का जीवन यांत्रिक होता जाता है और इस तरह आध्यात्मिक रूप से (आध्यात्मिकता धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि इस अर्थ में कि आदमी के जीवन की सार्थकता जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता से ऊपर उठकर चेतना की दुनिया में निवास करने में ही होती है) आदमी खोखला हो जाता है। अगर आदमी का जीवन खोखला हो गया है और उसमें नीरसता और ऊब पैदा हो गयी है तो फिर उसको भरने के लिए कुछ चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति आदमी की इस आध्यात्मिक भूख को कारखाने में निर्मित सामग्रियों से भरकर मिटाने का उपाय है।
इसके अलावा सर्जनात्मकता के अभाव में आदमी का अस्मिता-बोध खतम होता जाता है। इसके विपरीत जब आदमी अपनी भावनाओं के अनुरूप कुछ भी बनाता है तो उसमें उसके अपनेपन की अभिव्यक्ति होती है और इससे निजत्वबोध का जन्म होता है। ऐसा आदमी अपने को निजी मूल्यों की कसौटी पर कसना चाहता है लेकिन सृजन-प्रक्रिया से रिक्त आदमी हमेशा अपने को दूसरों की निगाह से तौलता है। इससे नकलचीपन और फैशनपरस्ती आती है। वह सोचता है कि जो सब रखते हैं उसे रखने से, जो सब खरीदते हैं उसे खरीदने से और जैसा सब सोचते हैं वैसा सोचने से ही समाज में उसकी कोई स्थिति बन पाएगी। ऐसे आदमी का स्वभाव अपने को दूसरे के अनुरूप बनानेवाला हो जाता है और ऐसा आदमी भावनात्मक रूप से दूसरों पर आश्रित होता है। वह अधिनायकवादी व्यवस्था में ज्यादा इत्मीनान महसूस करता है क्योंकि इसमें वह अपने बारे में बहुत सारे निर्णय लेने से मुक्त हो जाता है। या मोटेतौर पर वह यह सोचने लगता है कि जैसा सब सोचते हैं वही ठीक है।
एक तरह से इससे भीड़तंत्र की भूमिका तैयार होती है। यह फटेहालों की भीड़ नहीं होती– नवीनतम परिधानों और क्रीम पाउडर में सजे-धजे बाहर से अति सुसंस्कृत लगने वाले लोगों की भीड़ होती है। लेकिन थोड़ा कुरेदने पर इन परिधानों के भीतर से खोखलापन झाँकने गलता है। हल्की चोट लगते ही सब ढोल की तरह एक-सी आवाज निकालने लगते हैं। इसकी परीक्षा किसी भी फैशनेबल जमात के बीच लीक से हटकर कोई विचार व्यक्त करके तुरंत हो सकती है। ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएँ सुनने लायक होती हैं। लीक से अलग कही गयी बात उन्हें ‘कुफ्र’ जैसी जान पड़ती है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.