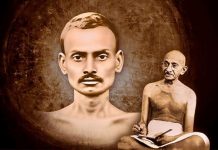चौखम्भा राज के प्रस्ताव में राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण के जरिये आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों के लोकतांत्रिकीकरण का निर्देश है। इसमें राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक शक्ति के स्वामियों, और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत को लोकतंत्र और देशहित का सबसे प्रबल शत्रु के रूप में पहचानते हुए इसे नयी राज्यव्यवस्था की संरचना के जरिये प्रभावहीन बनाने का बीड़ा उठाया गया था। इस योजना में प्रशासनिक व्यवस्था के अविलम्ब जनहित-उन्मुख होने का दबाव था। प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुष के बीच जातिभेद, वर्गभेद और धर्मभेद से ऊपर उठकर परस्पर सहयोग और अधिकतम समत्व की संभावना पर बल था। दूसरे शब्दों में, डॉ. लोहिया की चौखम्भा राज योजना नवस्वाधीन भारत के लिए क्षेत्रीयता, अलगाववाद, अधिनायकवाद, नौकरशाही, और बड़ी मशीन पर आधारित उद्योगीकरण जैसे महाप्रश्नों का एकसाथ समाधान प्रस्तुत करती है।
चौखम्भा राज के प्रस्ताव में गाँव-उन्मुख लोकतंत्र को विकसित करने की एक सुविचारित योजना थी। इसमें गाँव पंचायत और किसानों में सीधा सम्बन्ध, उत्पादकता और संसाधनों की जानकारी, फसलवार खेती की योजना, और गाँव पंचायत, योजना आयोग व भूमि आयोग में समन्वय का सुझाव था। गाँव -पंचायत को अनाज संग्रह और लगान वसूली की जिम्मेदारी का प्रस्ताव भी किया गया। पीने का साफ पानी, गाँव की स्वच्छता, और यातायात सड़क निगरानी के लिए ग्राम-पंचायत को ध्यान रखना था। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय, दवाखाना, प्रसव-सेवा केंद्र और शिशु कल्याण केंद्र की व्यवस्था सँभालनी थी। इसी स्तर पर खेल और सांस्कृतिक कार्यों के प्रोत्साहन का दायित्व दिया गया। गाँव-पंचायत में युवाओं को सक्रिय भूमिका विशेषकर ग्राम कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में योगदान पर जोर दिया गया। निरक्षरता निवारण, ग्रामोद्योग संवर्धन व सहकारी समितियों को प्रोत्साहन भी गाँव स्तर पर ही सँभालने का सुझाव था। खेतों और अन्न-उत्पादन के सुधार के लिए ‘अन्न सेना’ और खेतीयोग्य भूमि के विस्तार के लिए ‘भूमि सेना’ का प्रावधान रखा गया। इसमें ग्रामीण बेरोजगारी का भी समाधान था।
आज भी चौखम्भा राज की कल्पना को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विमर्श में महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन डॉ. लोहिया मानते थे कि चौखम्भा राज की स्थापना से सिर्फ सत्ता का विकेंद्रीकरण ही नहीं बल्कि हमारे नव-स्वाधीन राष्ट्र के लिए अनेकों अन्य हितकारी परिणाम निकलेंगे :
1. विविधता में एकता को बल मिलेगा। हर स्थानीय समुदाय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध लघु योजनाएँ लागू करते हुए अंतत: देश की दुर्दशा के उन्मूलन में योगदान करेगा।
2. भाषा, धर्म और अन्य आधारों पर पैदा बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक विभाजन में निहित अलगाव, असुरक्षा और तनाव का यह रचनात्मक समाधान होगा।
3. भूस्वामित्व से पैदा आर्थिक गैरबराबरी में निहित द्वंद्व और टकराहट के बावजूद अंतर्वर्गीय सहकारिता की प्रगति होगी।
4. राज्यसत्ता का देशीकरण (विउपनिवेशीकरण) होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान गाँव से लेकर जिला, प्रदेश और केंद्र में जमी हुई अफसरशाही पर विधिसम्मत तरीके से लोकशाही का नियंत्रण कायम करने की जरूरत पूरी होगी।
5. अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आमदनी का 1/4 गाँव सरकार और 1/4 हिस्सा जिला सरकार को देने से परस्पर पूरकता स्थापित के जरिये नया प्राणसंचार होगा।
6. चौखम्भा राज छोटी मशीनों के माध्यम से तकनीकी विकेंद्रीकरण संपन्न करेगा और यह लोकतान्त्रिक क्रान्ति का भी आधार बनेगा।
7. गाँव-समाज की उदासीनता दूर होगी; प्रभु जातियों का आलस मिटेगा और वंचित जातियों में आशा का संचार होगा।
8. यह भी निश्चित है कि भारत विभाजन के सदमे से सहमे देश में एकसाथ विभिन्न स्थानीय समुदायों की विविधतामय सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण और सहभागी प्रक्रियाओं से लोकतांत्रिक राष्ट्रीय एकता का संवर्धन हो सकेगा।
9. यह योजना देश की राज्यव्यवस्था में विदेशी शासन से जुडी जनविरोधी प्रवृत्तियों और परम्पराओं के उन्मूलन का भी लक्ष्य जनसाधारण के वोट से चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिये पूरा करेगी।
कुछ निष्कर्ष
इस निबंध के अंत में यह प्रश्न स्वाभाविक होगा कि सहभागी राष्ट्रनिर्माण की यह अनूठी योजना क्यों नहीं स्वीकारी गयी? वस्तुत: चौखम्भा राज की योजना के साथ कई असुविधाजनक तथ्य जुड़े हुए थे जिससे यह देश के लिए आकर्षक नहीं सिद्ध हुई।
एक तो इसमें राज्यव्यवस्था के समूल लोकतांत्रिकीकरण का आवाहन था। जो देश की तत्कालीन शक्ति संरचना में अरसे से सुस्थापित व्यक्तियों, वर्गों और जातियों के लिए खतरे की घंटी थी। दूसरे, इसकी प्रस्तावक जमात अर्थात भारत के समाजवादी नेता और कार्यकर्ता 1946 में संविधान सभा के चुनावों से अलग रहे और भारत विभाजन के प्रस्ताव पर कांग्रेस की पहली कतार के सभी नेताओं के खिलाफ थे। डॉ. लोहिया समेत अधिकांश सोशलिस्ट एक अलग दल के रूप में कांग्रेस के विरुद्ध 1952, ’57 और ’62 के आम चुनावों में आमने सामने हुए। इससे उनको सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा‘बहिष्कृत’ जैसा सलूक मिला और उनके देशहितकारी प्रस्तावों की भी खुली उपेक्षा की गयी।
तीसरे, कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा अपनाये गये राष्ट्रनिर्माण के रास्ते की समस्याओं की पूरी तस्वीर 1962 के चीनी हमले और 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बीच की अवधि में क्रमश: सामने आयी। लेकिन तब तक समूचे राजनीतिक समुदाय में सत्ता के राष्ट्रहितकारी विकेंद्रीकरण की बजाय आत्मरक्षा की प्रवृत्ति प्रबल हो चुकी थी। सहभागी लोकतंत्र के जरिये राष्ट्रनिर्माण की बजाय ‘सरकारीकरण’ और व्यक्ति-केंद्रित सत्ताविमर्श की केन्द्रीयता को महत्त्व दिया जाने लगा।
चौथे, 1974 में जयप्रकाश नारायण के प्रयासों से शुरू ‘सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन’ ने 1. राष्ट्रनिर्माण की समस्याओं, 2. ‘लोक’ पर ‘तंत्र’ के चौतरफा वर्चस्व के हानिकारक परिणाम, 3. देश की सत्ता के बिगड़ते चरित्र और 4. लोकतंत्र के आत्मघाती दोषों की तरफ देश का ध्यान जरूर खींचा। लेकिन जून ’75 और मार्च, ’77 के इमरजेंसी राज के बाद लोकतांत्रिक नव-निर्माण की सभी सकारात्मक संभावनाएँ धूमिल हो चुकी थीं।
इसी के समांतर, समाजविज्ञान की सैद्धांतिक दृष्टि और मौलिक राजनीतिक नव-निर्माण के ताजा इतिहास की मदद से यह भी याद रखना चाहिए कि बिना जनक्रांति के संपन्न हुए राजनीतिक परिवर्तनों में राज्यसत्ता के सन्दर्भ में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती आयी है। पूरे नेहरू-युग में सत्ता-प्रतिष्ठान की तरफ से ‘संकट-वाद’ को ही सभी बुनियादी बदलावों को टालने की आड़ बनाया गया था। इसमें गांधीजी की हत्या, कांग्रेस से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध विच्छेद, देशी रियासतों का आधा-अधूरा विलय, शरणार्थी समस्या, कश्मीर में टकराहट, देशभर में भाषाओं को लेकर आन्दोलन, 1952 और ’57 के आमचुनावों में कांग्रेस की प्रबल विजय और मध्यम वर्ग में यथास्थितिवादी रुझानों का उभार जैसे तथ्यों ने अवरोधक का काम किया।
विकेंद्रीकरण की प्रगति के लिए जनसाधारण में आन्दोलन, राजनीतिक समुदाय में आम सहमति और राजनीतिक नेतृत्व में दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है और 1947-’67 के दौर में इन तीनों का स्पष्ट अभाव था। फिर किसी राजसत्ता के नवनिर्माण में एक ठोस संवैधानिक व्यवस्था और लोकहितकारी न्यायपालिका से सहारा मिलता है लेकिन नवस्वाधीन भारत में यह दोनों सुविधाएँ भी नहीं थीं।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.