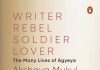आजकल देश में विकल्प की तलाश की बहुत चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का विकल्प। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का विकल्प। मौजूदा चुनाव व्यवस्था का विकल्प। पूँजीवादी वैश्वीकरण और लँगोटिया पूँजीवाद (‘क्रोनी कैपिटलिज्म’) का विकल्प। वित्तीय (‘आवारा’) पूँजी का विकल्प। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के व्यवसायीकरण का विकल्प। मंदिर-मस्जिद ध्रुवीकरण का विकल्प। परिवारवाद और वोट बैंक का विकल्प। प्रभु-जातियों की राजनीति का विकल्प। काले धन और अपराधीकरण का विकल्प। ‘गोदी मीडिया’ का विकल्प….
विकल्प की तलाश के तीन कारण
भारत में विकल्प के लिए बढ़ती इस बेचैनी के तीन बड़े कारण हैं। एक तो, दुनिया में पूँजीवाद सोवियत संघ के विघटन, अमरीका में आर्थिक राष्ट्रवाद के विस्तार और चीन के पूँजीवादी हो जाने के बावजूद पंचर पहिये की गाड़ी की तरह ठहर गया है। जो कसर बाकी थी उसे कोरोना की महामारी ने पूरा कर दिया। पिछले तीस बरस से चल रहे बाजारवादी वैश्वीकरण ने देशों के अंदर और देशों के बीच गैरबराबरी को बढ़ाने के साथ ही धरती के अपार दोहन से सब कुछ तहस-नहस कर रखा है। अब दुनिया के एक प्रतिशत सत्ताधारी तबके (पावर इलीट/रूलिंग क्लासेस), अमीर देश में ‘रंग-भेद’ पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रवाद और गरीब देश में ‘धर्म-भेद’ आधारित राजनीति के जरिये अपने अस्तित्व की रक्षा में जुट गए हैं। इससे पूरी दुनिया में लोकतंत्र ‘बहुमत की मनमानी’ का बहाना बन गया है। सत्ता-प्रतिष्ठान का विरोध नहीं किया जा सकता। चुनाव प्रक्रिया धन-मीडिया-दबंगई के त्रिदोष से अस्वस्थ हो गयी है। नागरिक अधिकारों, गैर-सरकारी मंचों और लोक-संगठनों पर ग्रहण लग गया है। बोलने, लिखने और सामूहिक प्रयासों की आजादी का अधिकांश नव-स्वाधीन देशों की सरकारें सम्मान करना भूल गयी हैं। चुनाव और मीडिया धनशक्ति का धंधा बन रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक दल पूँजीपतियों और प्रभु जातियों की सेवा के लिए सजायी गयी दुकानों जैसे हो गए हैं।
दूसरे, देश में कांग्रेस के विकल्प के रूप में सत्ता में स्थापित भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन अपनी चमक खो रहा है। नरेंद्र मोदी 2019 में दुबारा प्रधानमन्त्री जरूर बने लेकिन कोरोना की महामारी और किसानों की लाचारी के दुहरे प्रकोप के सामने असफल हो चुके हैं। इनके राज में दवाई-कमाई-पढ़ाई-महँगाई-रिहाई के पाँच मोर्चे खुल गए हैं और हर मोर्चे पर मोदी सरकार पीछे हटी है। इस सरकार के कारण हमारी अर्थव्यवस्था दिशाहीन है। राष्ट्र-निर्माण के लिए ‘सबका विश्वास’ अर्जित करने की जगह सरकार द्वारा ‘बाँटो और राज करो’ की नीति ही राजधर्म हो गयी है। सम्प्रदाय (हिन्दू-मुसलमान-सिख-ईसाई), क्षेत्र (असम-मेघालय; मणिपुर-नगालैंड), जाति (अगड़ा-पिछड़ा; ब्राह्मण-राजपूत; पिछड़ा-अतिपिछडा; दलित-महादलित) और जनजातीय समुदायों के झगड़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की सरहदों पर चीन की सेनाओं की मनमानी के आगे सरकार की लाचारी देशभक्त नागरिकों और सैनिकों में चिंता पैदा कर चुकी है। बैंकों से लेकर सरकारी कामों में भ्रष्टाचार बेकाबू है क्योंकि अब सीधे सरकार नाजायज तरीके से ‘प्रधानमन्त्री कोष’ जैसे रहस्यमय उपायों से धन-संचय के धंधे में जुट गयी है।
भारतीय जनता पार्टी सरकार में कायम है और उसका धन-भण्डार बेहद बढ़ा है लेकिन उसकी लोकप्रियता घट चुकी है। कई महत्त्वपूर्ण समर्थक दल हट रहे हैं और अभी भी समर्थक बने हुए दल अपने आप में घट रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गयी। पंजाब में अकाली दल किसान के साथ खड़ा हो गया। बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा की संयुक्त सरकार वेंटीलेटर पर है– यह किसी को नहीं मालूम कि कब और क्यों दम उखड़ जाएगा! बंगाल के चुनाव में मिली हार के बाद से मोदी-शाह-अदानी-अम्बानी सरकार की उलटी गिनती शुरू है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मजबूरी आ गयी। उत्तराखंड में एक के बाद एक कई मुख्यमंत्री बदले गए लेकिन सरकार की धमक नहीं लौटी। केन्द्रीय सरकार में बड़ा फेर-बदल करने के बावजूद सक्षम मंत्रियों और अफसरों का अभाव है। इस सब के कारण उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन पाँच प्रदेशों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के बारे में मतदाताओं के रुझान को देखते हुए मार्च, ’22 में बहुत कुछ बिगड़ने का अनुमान है।
तीसरे, कांग्रेस और प्रमुख प्रादेशिक गैरभाजपाई दल अपने को सर्वगुण संपन्न मानकर सत्तारोहण की तैयारी में हैं और अपने सामंती तौर-तरीकों को सुधारने की कोई फ़िक्र नहीं है। ये देश की खोखली चुनाव-व्यवस्था और लोकतंत्रविरोधी दल-व्यवस्था में सुधार को कोई जरूरी काम नहीं मानते। चुनाव में खर्च की कोई सीमा नहीं रह गयी है और दलों में अपने आय-व्यय को जनता से साझा करने का साहस नहीं है। राजस्थान और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल में शासनतंत्र में जवाबदेही की कोई पहल नहीं है। ‘जिला सरकार’ और ‘पंचायत सरकार’ की व्यवस्था के जरिये सहभागी लोकतंत्र की स्थापना को तैयार नहीं हैं। भाजपा के ‘हम दो (मोदी+शाह) – हमारे दो (अदानी+अम्बानी)’ तक सिमटने की शिकायत करते रहने के बावजूद प्रमुख गैर-भाजपाई दलों में भी एक शिखर पुरुष या महिला की मनमानी है। ये सभी दल चुनाव को ‘पैसे का खेल’ मानकर चुनाव की महँगी मशीन बन चुके हैं। इसलिए भाजपा की दबंगई से मुक्ति पाने के लिए परिवर्तन की राजनीति की संभावना बढ़ रही है लेकिन राजनीति में परिवर्तन की जरूरत के प्रति गैर-भाजपाई दलों में आत्मघाती उदासीनता है।
गठबंधन की राजनीति का सच
देश में 1975-77 की इमरजेंसी के बाद से लोकतांत्रिक राजनीति 1977 से ही गठबंधनों के जरिये संचालित होती आयी है और पिछले दो दशकों से कांग्रेस के नेतृत्व में गठित संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा (यूपीए/ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाएंस) और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (एनडीए/ नेशनल डेमोक्रेटिक एलाएंस) के बीच सत्ता का पेंडुलम झूल रहा है। समाजवादियों का कुनबा इन्हीं दो के बीच अपने को बाँटता रहता है। क्योंकि समाजवादियों द्वारा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग कोई तीसरा राष्ट्रीय मोर्चा बनाने की पहल नहीं रही है। 2024 के लिए भी नहीं है।
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 1989-90 से आन्दोलन और चुनाव के व्याकरण में बहुत अंतर हो गया है। जन आन्दोलन के लिए जनहित के प्रश्न, एक ईमानदार नेतृत्व, पीड़ित हिस्सों का समर्थन और जोखिम उठानेवाले कार्यकर्ताओं का ताना-बाना चाहिए। जबकि चुनाव में प्रत्याशी की छबि, प्रभु जातियों की अनुकूलता, एक बड़ी रकम और चुनाव प्रबंधन में दक्ष व्यक्तियों का कौशल हार-जीत में योगदान करता है। आन्दोलन की क्षमतावाले दल घटे हैं और चुनाव में सक्षम सिद्ध होनेवाले दल अपने को आन्दोलनों से बचाते हैं।
समाजवादी परिवार में चार प्रवृत्तियाँ
इस परिस्थिति में अपने को समाजवादी माननेवाले राजनीतिक व्यक्तियों के बीच कम से कम चार प्रकार की प्रवृत्तियाँ या धाराएँ दिखाई पड़ रही हैं : 1. विभीषण-विदुर परंपरा, 2. गैर-कांग्रेसवाद, 3. निराशा के कर्तव्य, और 4. संसदवाद।
1. विभीषण–विदुर परम्परा : पहली धारा के रूप में राजसत्ता की चमक-गमक-धमक से जुड़े समाजवादियों की गतिविधियाँ चर्चा में हैं। विभीषण और विदुर सत्ता-प्रतिष्ठान और प्रभुवर्ग के ही अंश थे। उदाहरण के लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव कराया है कि भारत सरकार देश की जातिगत जनगणना कराए। यह जाति-विमर्श को समाजवादी धार देने की कोशिश है और इसे सवर्णों को छोड़कर बाकी सभी जातियों का समर्थन है। भाजपा में समाजवादी पृष्ठभूमि वाले एक वरिष्ठ राज्यपाल ने किसानों के साथ अन्याय के लिए प्रधानमंत्री मोदी की खुली भर्त्सना का सिलसिला बना दिया है। सत्ताधारी दल के कुछ सांसद भी सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्नों पर असंतोष जाहिर करने का साहस दिखा रहे हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके लेकिन समाजवादी चंद्रशेखर की उँगली पकड़कर सरकारी बाबू से राष्ट्रीय नेता बने एक व्यक्ति तो बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा से ही इस्तीफ़ा देकर मोदी-शाह विरोधी मोर्चे के नए सूत्रधार हो गए हैं। इन सभी को ‘विवेक आधारित विद्रोह की विभीषण-विदुर परम्परा’ का वारिस माना जाना चाहिए।
2. गैर-कांग्रेसवादी धारा : पिछले दिनों उत्तरप्रदेश में दो वरिष्ठ समाजवादियों ने 70 बरस से भी अधिक की उम्र में अनेकों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करके देश भर के समाजवादियों की आँख नीची करने को मजबूर कर दिया। इसमें से एक व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ी और दूसरे ने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दिया है। दोनों ने अपने दलों में उपेक्षा और अपमान की शिकायत की और ‘गैर-कांग्रेसवाद’ के प्रति प्रतिबद्धता के कारण भाजपा में प्रवेश को सही कदम बताया।
मौजूदा राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन (एनडीए) के कम से कम बीस प्रतिशत सदस्य राजनीतिक दृष्टि से ‘हिंदुत्ववाद’ की बजाय गैर-कांग्रेसवाद के अनुयायी हैं। ‘संघ-परिवार’ से बाहर से लाये गए हैं। लेकिन संघ परिवार के वरिष्ठ नेताओं को भी सिर्फ ‘मार्गदर्शक मंडल’ के लायक माननेवाले भाजपा नेता ऐसे बूढ़े गैरकांग्रेसवादी तोतों को कैसे महत्त्वपूर्ण बना के रखेंगे? इससे पहले शफीक अहमद तातारी, आरिफ बेग, हुकुमदेव यादव, चंद्रमणि त्रिपाठी और नीरज सिंह जैसे लोग समाजवादी जमातों में से भाजपा के सरकस में लाए गए थे और कोई ख़ास अंतर नहीं पैदा हुआ। क्योंकि दल-परिवर्तन के बावजूद दिमाग परिवर्तन नहीं हो पाता है। फिर गांधीवादी समाजवाद से शुरू भाजपा अब गांधीजी के ह्त्यारे का महिमामंडन और गैर-हिन्दुओं का बहिष्कार करनेवालों की ओर बढ़ चुकी है। इसका नारा ‘कांग्रेस हटाओ–देश बचाओ’ की बजाय ‘गैर-हिन्दू हटाओ, हिन्दू बचाओ!’ हो चुका है।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.