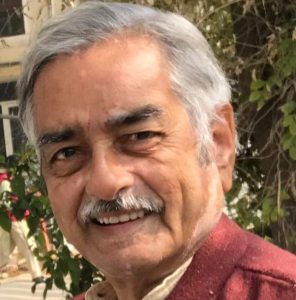
— प्रयाग शुक्ल —
कुछ कृतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ने के साथ ही आपको एक नयेपन का बोध होता है। स्वयं जीवन को भी आप कुछ नयी तरह से देखने-सोचने लगते हैं, और अगर वह कृति आपकी मातृभाषा की ही है तो उसमें भाषा को जिस नयेपन के साथ बरता गया है, वह व्यवहार भी गहरे में स्पर्श करता है। आप रोमांचित भी होते हैं। एक प्रकार की ऊर्जा भी मिलती है। सो, कुछ ऐसे ही नयेपन, ऐसी ही ऊर्जा का अनुभव तब किया था जब 1956-57 में सोलह-सत्रह वर्ष की वय में अज्ञेय का उपन्यास ‘शेखर : एक जीवनी’ पढ़ा था –पहला भाग या जब ‘रेणु’ के ‘मैला आँचल’ और ‘परती : परिकथा’ उपन्यास पढ़े थे। ऐसी ही कोई कृति(याँ) उसके लेखक के बारे में जानने को – और अधिक जानने को प्रेरित भी करती हैं। तब मैं कोलकाता में था, और सूरजमल नागरमल जालान, तथा ‘बड़ा बाजार लाइब्रेरी’ जैसे पुस्तकालयों में जाया करता था। उनका सदस्य भी था। फिर तो ‘शेखर : एक जीवनी’ का दूसरा भाग भी पढ़ा। ‘तार सप्तक’ और ‘दूसरा सप्तक’ भी पढ़े, और ‘अज्ञेय’ की कहानियाँ भी पढ़ीं। क्रमशः उनके कविता संग्रह भी देखने में आए। भाई-बहनों के बीच और अशोक सेकसरिया जैसे मित्र के साथ उनके लेखन पर चर्चा भी होने लगी। यह इच्छा भी जागी कि कभी उनसे परिचय हो सके, उन्हें देख सकूँ और उनसे बातें कर सकूँ तो कितना अच्छा हो। हम नया-पुराना भी कुछ तो पढ़ ही चुके थे, छायावाद के कवियों को भी, प्रेमचन्द को भी और जाहिर है कि उनकी गरिमा-महिमा से अभिभूत थे। पर, अज्ञेय को पढ़ने का अनुभव इस मामले में अलग था कि वह ‘आज’ के, नयेपन के, एक ‘नये’ बोध के प्रतिनिधि सरीखे लगते थे, और तब हम जो लिख-सोच रहे थे उसके बहुत निकट भी। युवा मन को, उनके क्रांतिकारी जीवन ने, और भारत के विभिन्न अंचलों में बीते उनके बचपन, उनकी किशोरावस्था-युवावस्था के ‘अभियानों’ आदि ने कुछ रोमांचित करना भी शुरू किया था। और आज सोचकर देखता हूँ तो इस तथ्य ने तब भी बहुत अपील किया था कि स.ही.वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ जी का बचपन जम्मू में बीता है, किशोरावस्था के दिन कश्मीर-तमिलनाडु में भी, युवावस्था की पढ़ाई लाहौर में हुई है, कोलकाता में ‘विशाल भारत’ में रह चुके हैं। और चालीस वर्ष की वय के आसपास वह सेना में भर्ती होकर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों-पर्वतों-नदियों से निकट परिचय प्राप्त कर चुके हैं। और ‘अरे, यायावर रहेगा याद’ जैसे यात्रा-वृत्तान्त में उन्हें दर्ज भी कर चुके हैं। ‘हीलीबोन की बत्तखें’ कहानी भी इस सिलसिले में याद आती है। और ‘दूर्वादल’ सरीखी कविता भी, जो शिलांग में लिखी गयी थी और जिसकी पंक्तियाँ ‘तमक कर दामिनी बोली क्षितिज ने पलक-सी खोली’ जब भी याद करता हूँ, ‘क्षितिज के पलक खोलने वाले’ बिम्ब पर कुछ ठहर कर सोचने ही नहीं लगता मानो उसके मर्म को ‘देखने’ भी लगता हूँ। ‘पावस प्रात शिलंग’ कविता को भी इसी सन्दर्भ में याद कर ले सकते हैं। उन युवा दिनों में ‘अज्ञेय’ को पढ़ने के अनुभवों को आज तक के पढ़ने के अनुभवों से जोड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि उस रोमांच, आकर्षण और कुछ ‘नया’ पाने के सम्मोहन में कोई कमी नहीं आयी है। उनके साहित्य के, भाषा-व्यवहार के नये अर्थ और मर्म, नयी तरह से खुलते ही जाते हैं।
वर्ष 2005 में जब मैंने ‘कल्पना’ के ‘काशी अंक’ का सम्पादन किया तो उसके‘आरम्भिक’ के लिए ‘अज्ञेय’ की ये पंक्तियाँ सहज ही खोज ली थीं : ‘मृत्यु को / मृत्यु का आलोक / जीवन को / जीवन का / ओ! जीवन! ओ मरण! ओ वृन्द–वाद्य! हम गाते हैं / जहाँ हैं / साथ दो।’
इसे मैं अपने जीवन का एक सुखद संयोग ही मानता हूँ कि कोलकाता के युवा दिनों में अज्ञेय से परिचय की, उनसे मिलने की, जो इच्छा जागी थी, वह जल्दी ही पूरी हुई। 1958 में ‘कल्पना’ में मेरी एक कविता और एक कहानी प्रकाशित हुई। एक कहानी ‘सड़क का दोस्त’, ‘कहानी’ में आयी। ‘कृति’ और ‘युगचेतना’ में भी कुछ चीजें छपीं। और मैंने पाया कि तब हिंदी संसार की जो स्थिति थी उसमें मैं थोड़ा-बहुत जाना जाने लगा हूँ, वरिष्ठ और अग्रज लेखकों-संपादकों का प्रेम भी पाने लगा हूँ। और जब तेईस वर्ष की आयु में‘कल्पना’ के संपादक-मंडल में पहुँचा तो ‘अज्ञेय’ से पत्र-व्यवहार कुछ सहज भाव से ही कर पा रहा हूँ, यह भी कि उनके पत्र मुझे यह बता रहे हैं कि उनका स्नेह भी मुझे सहज ही में उपलब्ध हो गया है।

‘कल्पना’ (हैदराबाद) में कोई एक साल बिताकर जब मैं फ्रीलांसिंग करने के इरादे से दिल्ली पहुँचा तो अज्ञेय, ‘दिनमान’ के सम्पादक नियुक्त हो चुके थे, उनसे भेंट हुई। और ‘दिनमान’ में कला-संस्कृति-नाटक-साहित्य समेत अन्य विषयों पर लिखना भी शुरू हुआ। इसे भी एक सुखद संयोग मानता हूँ कि अज्ञेय ने ही मुझे साठ के दशक में मुकुल डे की एक प्रदर्शनी का कार्ड सौंपकर उसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और इब्राहिम अलकाजी का इंटरव्यू करने के लिए भेजा था। शम्भु मित्र-तृप्ति मित्र ‘बहुरूपी’के नाटकों के साथ-साथ दिल्ली आये तो मुझे वे नाटक देखने के लिए (कुछ यह सोचकर कि मुझे बांग्ला आती थी) कहा, ‘आप कुछ समय इनके साथ बितायें।’ और शंभु मित्र के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मुझे मिला।
इन प्रसंगों ने मेरे जीवन में क्या कुछ जोड़ा है, उसे मैं आज भी अकूत ही मानता हूँ। जब वात्स्यायन जी ने मुझे मुकुल डे की प्रदर्शनी की जिम्मेदारी सौंपी थी तो मैंने संकोचपूर्वक, कुछ अस्फुट-से स्वर में यही कहा था कि मैं बंगाल स्कूल के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, मुकुल डे के काम से भी कोई खास परिचय नहीं है तो उनका उत्तर यही था कि ‘जाकर देखिए तो।’ कुछ पुस्तकें भी उन्होंने लाकर दीं। कुछ सामग्री मैंने एकत्र की। प्रदर्शनी दो-तीन बार देखी। कैटलॉग को मनोयोगपूर्वक पढ़ा और कुछ संभ्रम के साथ ही, कि पता नहीं समीक्षा उन्हें कैसी लगेगी मनोहर श्याम जोशी के हाथ में थमा दी, जो तब ‘दिनमान’ के सहायक संपादक थे, मेरे शुभचिंतक थे, मुझ पर अगाध स्नेह रखते थे, और फ्रीलांसर के नाते मुझे बहुतेरे काम भी सौंपते रहते थे, जिससे कि मेरे अर्थोपार्जन में कुछ इजाफ़ा हो।
वात्स्यायन जी ने वह समीक्षा पढ़ी, जहाँ-तहाँ से कुछ संपादित की, कुछ चीजें जोड़ीं और उनके द्वारा पास की गयी समीक्षा दिखाते हुए मनोहर श्याम जोशी ने कहा, ‘तुम बेकार की दुविधा में पड़े रहते हो। यह देखो, समीक्षा छपने जा रही है।’ मैंने वह हाथ में ली, अज्ञेय के अत्यंत सतर्क संपादन को गौर से देखा- जैसे कि हर बार देखता था- और विस्तृत समीक्षा छपने जा रही है सोचकर मन में एक उछाल-सी महसूस की। हाँ, वे क्षण आज भी याद हैं क्योंकि उन क्षणों ने मेरे जीवन में एक नयी राह खोल दी। अगली ही भेंट में अज्ञेय ने मुझसे कहा कि ‘अब दिनमान का कला-कॉलम आप लिखना शुरू करिए।’ जहाँ तक याद पड़ता है हुआ यह भी था कि ‘दिनमान’ का कला-कॉलम तब श्रीकान्त वर्मा ही प्रायः लिखा करते थे, पर दिनमान के विशेष संवाददाता के नाते उनका कामकाज बढ़ चुका था, सो यह व्यवस्था सोची गयी थी। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे य़ह दायित्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, पर एक बार जो वह कॉलम लिखना शुरू किया तो मैं स्वयं कला की दुनिया में मानो उतरता ही चला गया, आनंद भी बहुत आया, और दस वर्षों तक तो वह कॉलम लिखा। कला को देखने, उस पर लिखने-पढ़ने-सोचने-चर्चा करने का वह सिलसिला आज तक थमा नहीं है।

यह भी याद करता हूँ इस सिलसिले में, कि स्वामीनाथन से आत्मीयता भी मानो अज्ञेय के कारण ही बढ़ी थी- स्वामीनाथन से मेरा तब तक स्वल्प परिचय ही था, पर एक बार अज्ञेय ने मुझे उनसे ‘इक्कीसवीं शती में कला का रूप-स्वरूप क्या होगा’ पर इंटरव्य़ू करने के लिए भेजा था। विविध क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों से इक्कीसवीं शती पर यह परिचर्चा दिनमान ने आयोजित की थी, ‘कला’ पर स्वामीनाथन के विचार चाहिए थे। स्वामी के साथ उस भेंट ने मुझे कला के प्रति और अधिक आकर्षित तो किया ही, मुझे उनके निकट भी ला दिया और आयोजन की उस आत्मीयता ने, कला-चर्चा के सवालों से कुछ इस तरह रूबरू किया कि बहुत कुछ जानने-सोचने को मिलता रहा।
स्मृतियाँ बहुतेरी हैं, कुछ वे भी जब अज्ञेय का पुस्तकालय कई दिनों तक देखा था और जब अज्ञेय-कपिला जी के सत्यमार्ग (चाणक्यपुरी) वाले निवास पर कविता-पाठ के आत्मीय आयोजनों में शामिल हुआ था। वत्सल निधि के मानसर-शिविर की भी भी यादें कई हैं, और उनके केवेंटर्स ईस्ट वाले निवास की भी कई, पर अभी स्मृतियों से विराम लेता हूँ। और यह याद करता हूँ कि अज्ञेय की ‘स्मृतिलेखा’ पुस्तक भी मेरी प्रिय पुस्तकों में है। मैथिलीशरण गुप्त, निराला, प्रेमचंद, रायकृष्ण दास, पन्त, सरोजिनी नायडू आदि पर उऩ स्मृति-लेखों में, संस्मरण भी हैं, और इन व्यक्तित्वों के कामकाज का एक सम्यक् आकलन भी। अज्ञेय ने सभी विधाओं में लिखा- उपन्यास, नाटक, कथा, कविता, यात्रा-वृत्तांत, संस्मरण, डायरी, जर्नल, ललित निबंध और ‘कुट्टिचातन’नाम से व्यंग्य-विनोद की विधा में भी। कलाओं पर भी उनका बहुतेरा लेखन है। और ‘प्रतीक’ और ‘दिनमान’ के माध्यम से कलाओं पर बहुतेरी सामग्री का आयोजन-संपादन भी उन्होंने किया। उनकी जन्मशती पर खजुराहो, एलोरा, बंगाल स्कूल आदि पर लिखे हुए उनके निबंधों के एक संकलन के लिए चीजें इकट्ठा कर रहा हूँ, ललित कला अकादमी के लिए। यह संकलन उनके ऐसे कामकाज की ओर ध्यान दिलाएगा, जिसकी ओर हिन्दी जगत का पूरा फोकस रहा नहीं है- ऐसी उम्मीद करता हूँ। (यह संकलन तो उस वक्त नहीं आ सका, पर कृष्णदत्त पालीवाल के संपादन में, ऐसा एक संकलन सस्ता साहित्य मंडल से आया है।)
भाषा-सजग अज्ञेय, परंपरा-आधुनिकता (समकालीनता) के सम्यक् सुमेल के धनी अज्ञेय और चिंतक अज्ञेय का साहित्य अब ऐसी धरोहर की तरह है, जिससे नयी पीढ़ियाँ भी बहुत कुछ पाती-निकालती रह सकती हैं। वह साहित्य, एक विस्तृत फलक बनाता है, और उसमें पूर्व-पश्चिम का जो भी संवाद है, अपनी शर्तों पर, वह जाँचने-परखने लायक है।
उनकी कविता- वह तो बहुत कुछ कहती-देती है ही। ‘असाध्य वीणा’ की यह एक पंक्ति देखिए : ‘कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित जलपंछी की चाप।’ इसे पढ़ते ही किशोरावस्था में अपने गाँव के निकट की एक झील पर देखे हुए ऐसे ही दृश्य उभर आए थे। उन्हें एक नयी तरह से देखा और अनुभव किया था। एक पंक्ति में यह ‘चित्र’ मुझे आज भी मोहित करता है। और उस शब्द सजगता और लाघव का एक प्रमाण भी है, जो अज्ञेय-काव्य की एक आधारभूत विशिष्टता है। अज्ञेय स्मरण, हमेशा ही, एक स्फूर्ति और ताजगी से भर देता है। (2010)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


















श्रेष्ठ आत्मीय, प्रेरणास्पद संस्मरण; स्वयं अपने आप में एक सौम्य सार्थकता और उत्साह का भाव पैदा कर सकने में समर्थ महत्वपूर्ण लेख।
“तमक कर दामिनी बोली
क्षितिज ने पलक-सी खोली”
जैसी पंक्तियों (जिनसे दो चार होने का अवसर मुझे पहले नहीं मिला था) का उद्धरण मेरे लिए इस लेख से मिलने और याद रह जाने वाली मूल्यवान प्राप्ति है।
आभार!
अमिताभ खरे