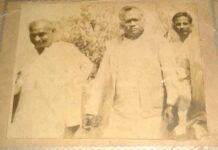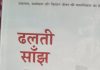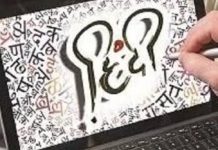ब्रिटेन से लौटने के बाद भी राष्ट्रीय एकता के बारे में मुहम्मद अली जिन्ना ने कुछ वर्ष अपनी राय नहीं बदली थी। अभी भी वे हिंदू और मुसलमानों को एक ही राष्ट्र के नागरिक समझते थे। 7 फरवरी 1935 को केंद्रीय असेंबली में संवैधानिक सुधारों पर बोलते हुए उन्होंने कहा : “विपक्ष के नेता द्वारा अभिव्यक्त की गयी भावना से मैं सहमत हूँ। मेरी भी राय है कि धर्म को राजनीति में नहीं घुसने देना चाहिए, नस्ल या वंश के प्रश्न को भी राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए….धर्म, व्यक्ति और ईश्वर के बीच का मामला है।”
जिन्ना साहब ने आगे कहा…. “मैं अखिल भारतीय संघराज्य के खिलाफ नहीं हूँ। गृहविभाग के सदस्य ने ठीक ही कहा है कि महात्मा गांधी भी संघराज्य के खिलाफ नहीं हैं। मगर इसका क्या मतलब है? इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि आपकी आपत्तिजनक और अस्वीकारणीय योजना को हम कबूल करें….इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप भारतीय लोकमत से सलाह करके यहाँ जवाबदेह सरकार स्थापित करें।” (जमील अहमद द्वारा संपादित जिन्ना के भाषणों का संग्रह, खंड 1, पृ. 4-13)
होते-होते जब 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के संविधान को लागू किया गया तो मुस्लिम लीग ने पाया कि चुनावों में उनको किसी भी राज्य में बहुमत नहीं मिला है। मुस्लिम बहुसंख्यक राज्यों– पंजाब, बंगाल, सिंध, उत्तर-पश्चिम का सीमावर्ती प्रांत- में से किसी भी प्रांत में मुस्लिम सीटों में से बहुसंख्यक स्थान उन्हें नहीं मिल सके। उन्होंने यह भी देखा कि छह राज्यों में कांग्रेस पार्टी को निःसंदेह बहुमत मिला है और कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी बन सकती हैं। इन सरकारों में कांग्रेस पार्टी द्वारा मुस्लिम लीग को कोई साझेदारी नहीं दी गयी। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में भी मुस्लिम लीग को सत्ता नहीं मिल सकी। बम्बई और उत्तरप्रदेश में मुस्लिम लीग को अच्छी सीटें मिली थीं, दोनों राज्यों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान नहीं दिया। बम्बई में एक निर्दलीय सदस्य को मंत्री का तिलक लगाया गया और उत्तरप्रदेश में एक दलबदलू को। नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व बहुत ज्यादा हताश हो गया और उसमें भयंकर आक्रोश उत्पन्न हो गया।
जैसे-जैसे सत्ता के हस्तांतरण की बेला नजदीक आने लगी और स्वराज्य का सगुण रूप सामने आने लगा तो मुस्लिम लीग के नेता निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालिग मताधिकार पर आधारित प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक स्वराज्य में उनको सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलनेवाली है। अतः अलगाववादी, पृथकतावादी प्रवृत्ति मुसलमान नेतृत्व के मन में घर करने लगी और जिस पाकिस्तान की योजना को उस समय कुछ छात्रों का कल्पना-विलास कहकर मुस्लिम नेताओं ने तिरस्कृत किया था, वही पाकिस्तान की कल्पना धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगी।
जहाँ पृथकतावादी और अलगाववादी प्रवृत्ति मुसलमान समुदाय में बड़े पैमाने पर पनप रही थी, वहाँ कांग्रेस के नेताओं में भी सत्ता पर अपना एकाधिपत्य, अपना सर्वाधिकार स्थापित करने की इच्छा जागृत हो रही थी। हाँ, कांग्रेसी नेता यह कहते थे कि कांग्रेस का अपना एक राजनीतिक कार्यक्रम है, आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम है, कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कांग्रेस मतदाताओं के प्रति प्रतिबद्ध है। ऐसी स्थिति में दूसरे दलों के साथ हम लोग कैसे साझेदारी कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं? सत्ता में हम कैसे उन्हें हिस्सा दे सकते हैं जिनका कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम से मेल न खाता हो? इस पर मुस्लिम लीग के नेताओं और जिन्ना साहब तथा खलीकुज्जमां जैसे नेताओं का कहना था कि उत्तरप्रदेश में मुस्लिम लीग के साथ मिलीजुली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने स्वतंत्र कार्यक्रम और नीति की आड़ ले रही है, जबकि जिन दो राज्यों (असम और पश्चिमोत्तर प्रांत) में कांग्रेस को निर्विवाद बहुमत नहीं मिला है, क्या उन राज्यों में कांग्रेस ने अन्य गुटों के साथ मिलकर साझेदारी सरकारें स्थापित नहीं की हैं? अगर इस तरह की मिलीजुली सरकार असम और सीमावर्ती प्रांत में बनाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व को कोई हिचक नहीं है तो उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में इस तरह की सरकारें बनाने में क्या दिक्कत है?उनका यह भी कहना था कि मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव में प्रगतिशील कार्यक्रम स्वीकारा था, जो कि कांग्रेस से मिलता-जुलता था।
कांग्रेसी नेताओं ने अपनी सरकारें बनाने के लिए मुस्लिम लीग के सदस्यों तथा अन्य मुसलमान पार्टियों के सदस्यों को फुसलाकर उन्हें कांग्रेस के सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया था और उनको तरह-तरह का लालच दिखाया था, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनने पर उन्हें मंत्रिमंडलों में ले लिया जाएगा। उन्होंने किया भी यही। उत्तर-प्रदेश में एक दलबदलू को उन्होंने मंत्रिमंड़ल में शामिल कर लिया। इन सारी बातों को लेकर मुस्लिन लीग का नेतृत्व क्रोधित हो उठा और कांग्रेस के प्रति उनमें काफी कटुता पैदा हो गयी। नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों में 1912-13 के बाद लगातार जो राजनीतिक चेतना जगी थी, जिसको 1920 तक एक राष्ट्रीयत्व के आदर्श की ओर जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खां और डॉ. अंसारी जैसे नेताओं ने मोड़ा था, वह चेतना अब सांप्रदायिक रूप लेने लगी। यहीं से मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति एक किस्म का भय, एक किस्म की नफरत पैदा होने लगी।
इस सारे परिप्रेक्ष्य में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्रवादी नेता के मत परिवर्तन का रहस्य जब हम ढूँढ़नें चलें तो उस समय हमें हिंदु-मुसलमान अलगाव का संदर्भ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हिंदुओं के सामाजिक आचरण और व्यवहार के अलावा सत्ता में साझेदारी भी इसका एक महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक राज्यों में कांग्रेस को जितना विशाल समर्थन प्राप्त हुआ, उतना किसी भी मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य में मुस्लिम लीग को प्राप्त नहीं हुआ। पंजाब-सिन्ध में तो लीग का सफाया ही हो गया था। तुलनात्मक दृष्टि से बंगाल में मुस्लिम लीग कुछ अच्छी स्थिति में रही थी। इससे कांग्रेसी नेताओं में अभिमान, अतिरेकी आत्मविश्वास और कुछ हद तक दंभ भी उत्पन्न हो गया। पश्चिमोत्तर सीमावर्ती राज्य के मुस्लिम चुनाव क्षेत्रों में भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। अतः कांग्रेस का रूख मुस्लिम लीग के प्रति कुछ उपेक्षा और उद्दंडता भरा हो गया।
मुस्लिम लीग को बम्बई और उत्तरप्रदेश में उल्लेखनीय यश मिला था। जहाँ बम्बई मुसलमान व्यापारियों और पूंजीपतियों का केंद्र था वहाँ उत्तरप्रदेश मुस्लिम सभ्यता, शिक्षा और साहित्य का केंद्र था। इन दो राज्यों में कांग्रेस यदि गैर-मुस्लिम लीगी मुसलमानों को बिना मतलब तिलक लगाकर मंत्री नहीं बनाती या मुस्लिम लीग से इस्तीफा दिलवाकर लीग के विधायक को मंत्रीपद की शपथ नहीं दिलवाती बल्कि स्वयं मुस्लिम लीग को ही सत्ता में साझेदारी दे देती तो शायद जिन्ना न द्विराष्ट्रवादी बनते और न ही पाकिस्तान का निर्माण होता। इसके दो सबूत हैं। वायसराय लिनलिथगो के पुत्र ने उनकी जो जीवनी लिखी है उसमें 1937-38 में हुई जिन्ना-लिनलिथगो की बातचीत का उल्लेख है।
उस समय तक जिन्ना संघ-राज्य की कल्पना के खिलाफ नहीं थे। उनके सामने स्पष्ट रूप से संयुक्त हिंदुस्तान की तस्वीर थी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और कानजी द्वारकादास जिन्ना साहब के समकालीन थे। खलीकुज्ज्मां उत्तरप्रदेश मुस्लिम लीग के नेता थे। इन तीनों के संस्मरणों से प्रकट होता है कि इन दो राज्यों में जिन्ना और मुस्लिम लीग सरकार में साझेदारी चाहते थे। बंगाल और असम में भी संमिश्र सरकारें संभव थीं और सुभाष बाबू इसके पक्ष में थे। परंतु मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू संमिश्र सरकार के विरोधी थे। जिन्ना ने मई 1937 में बम्बई के विधानसभाई नेता बालासाहेब खेर से बात की थी और गांधीजी को एकता के बारे में अपना संदेश भी भेजा था। मगर गांधीजी ने विशेष दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कुछ रूखा-सा जवाब दे दिया। गांधीजी ने कहा कि एकता में मेरा अटूट विश्वास है, वह जरा भी धूमिल नहीं हुआ है, मगर मैं असहाय हूँ। मुझे अंधकार में कोई प्रकाश की किरण नहीं दिखाई दे रही है। यह उन्होंने अपने 22 मई, 1937 के पत्र में लिखा था।
उत्तरप्रदेश में कांग्रेस ने कैसी अपमानजनक शर्तें रखी थीं, इसकी चर्चा पहले आ चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्ना ने समझ लिया था कि कांग्रेस के साथ साझेदारी संभव नहीं है और कांग्रेस भी मुस्लिम लीग को प्रातिनिधिक संस्था के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। अतः जिन्ना इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक मुसलमान जनता को उसकी भावना को आंदोलित करनेवाले नारे नहीं दिए जाएंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं पूछेगा। उनका यह अनुमान गलत नहीं था। अगले 6-7 वर्षों में स्वतंत्र पाकिस्तान के नारे ने मुस्लिम जनता को इतना उद्वेलित कर दिया कि गांधीजी को भी इस सत्य को कबूल करना पड़ा। हमेशा अन्तरराष्ट्रीयता के ख्याबों में भ्रमण करनेवाले जवाहरलाल नेहरू को भी अपनी ‘जेल डायरी’(1942-45) में इस सत्य को स्वीकारना पड़ा है। सितंबर 1944 के गांधी-जिन्ना वार्तालाप ने इस बात पर मुहर लगा दी। जैसा कि जिन्ना साहब ने जून 1947 में मुस्लिम लीग कौंसिल की बैठक में स्वयं कहा था, सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जब मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत ‘गहरी नींद में डूबे हुए थे,’ उत्तरप्रदेश, बम्बई जैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रांतों ने अतुल कुर्बानी देकर पाकिस्तान की नींव डालकर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। एक राष्ट्रवाद से द्विराष्ट्रवाद तक, महत्त्वाकांक्षा से भरे एक व्यक्ति के सफर की, यह शोक कथा है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.