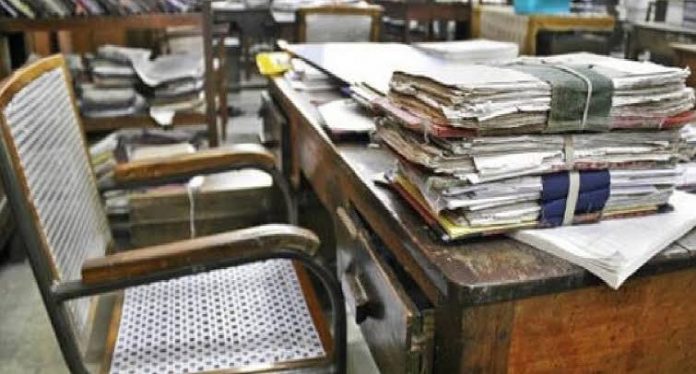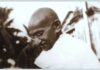— किशन पटनायक —
(कल प्रकाशित लेख ‘प्रशासनिक सुधार की चुनौती’ का दूसरा हिस्सा)
दरअसल, न प्रशासन सही शब्द है, न गवर्नेन्स। पारंपरिक शब्द ‘राजा-प्रजा’संबंध दोनों से बेहतर है। लोकतांत्रिक जमाने में हम उसको कहेंगे राज्य-प्रजा संबंध और यह सटीक भी है। राज्य को आम आदनी अपनी बात कह पाता है या नहीं? किंवदंती के अनुसार सम्राट जहाँगीर के अंतःपुर में एक घंटी होती थी जिसकी जंजीर महल के बाहर सड़क पर टँगी रहती थी। कोई भी उसको खींचकर सम्राट को खिड़की पर बुला सकता था। यह अगर राज्य-प्रजा संबंध की मध्ययुगीन कसौटी थी, तो आधुनिक विकासशील लोकतंत्र में क्यों नहीं हो सकती? अपनी वाजिब बात कहने के लिए या किसी कानूनी प्राप्य को लेने के उद्देश्य से, कलेक्टर को छोड़िए, तहसीलदार या दरोगा के सामने आम नागरिक सहज ढंग से बात कर लेगा, तो उसको लगेगा कि उसे लोकतंत्र मिल गया है। इसी का नाम है ‘सुनवाई’ यानी लोकतंत्र का पहला सोपान। वोट का महत्त्व इसके बाद।
दूसरी बात है विलंब। घूसखोरी और आतंक का सबसे बड़ा कारण है विलंब। सौ रुपए का डाक टिकट खरीदने के लिए डाकघर में और पचास हजार का चेक भुनाने के लिए बैंक में आधे घंटे से कम समय लगता है। अगर इसी ढंग का कोई काम सचिवालय या कलेक्टर कार्यालय से हासिल करना है तो महीनों या सालों लग सकते हैं। अदालत में भी उतना ही समय लगेगा। लोकतंत्र की पाठ्यपुस्तक लिखती है कि अदालत मौलिक अधिकारों तथा अन्य अधिकारों की रक्षक है। भारत का आम आदमी इस रक्षक से जितना डरता है, उतना और किसी से नहीं।
अदालत पुलिस की चाकर है, अपने अधिकारों की माँग करनेवाले किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा इलजाम लगाकर अदालत के द्वारा जेल भिजवा सकती है पुलिस। पुलिस-अदालत की जोड़ी से आंदोलनकारी राजनैतिक कार्यकर्ता भी आतंकित रहता है। फिर अधिकारों की माँग करे कौन?
हम जनांदोलनवाले कहते रहते हैं कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए, और अनेक अधिकार मिलने चाहिए। कभी हम आत्मसमीक्षा करें, पूछें कि बेचारे आम आदमी पर कितने अधिकार लादते जाएंगे। वह क्या करेगा इन अधिकारों को लेकर। अधिकार को कानून बनाने के लिए आंदोलन करना तो समझ में आता है, लेकिन जरा सोचिए हम जनता से कानूनी अधिकार के लिए लड़ने का आह्वान करते हैं। वह तो लड़ नहीं पाएगी, लड़ने के लिए नेता या एन.जी.ओ. या वकील ढूँढ़ना पड़ेगा। इनका धंधा अच्छा चलेगा। अधिकार, अधिकार, अधिकार और अधिकारों के कानून बनने के बाद लड़ो, लड़ो, लड़ो तो लोकतंत्र किसलिए?
कभी विश्वबैंक कह देगा, “साँस लेने का अधिकार होना चाहिए, पहले साँस लेने का कानून बनाओ, बाद में साँस लेने का आंदोलन करो।” हम निश्चित नहीं हैं कि विश्वबैंक के वाशिंगटन स्थित दफ्तर में ‘हवा पर अधिकार’ का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो चुका है!
अधिकार से अधिक महत्त्वपूर्ण है ‘सुनवाई’ और ‘कार्रवाई’। वाजिब बातों की तत्काल सुनवाई और अविलंब कार्रवाई। महत्त्वपूर्ण यह है कि नागरिक को सम्मानित आदमी समझा जाए।
गांधीवादियों ने अधिकारियों को ‘सेवक’ बनाना चाहा था। यह फिजूल बात है। मतदाता सूची में जिसका नाम है अधिकारी उसे मनुष्य समझे, यह काफी है। भारत का दारोगा, मजिस्ट्रेट और सीमांत इलाकों में भेजा गया सेना का अधिकारी आम नागरिक को कुत्ते जैसा समझता है। इस वाक्य में कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
समाज के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित नागरिक मानव अधिकार का मुद्दा उठाते हैं;इराक, कश्मीर, नगालैंड के विद्रोहियों के प्रति पुलिस के बर्बर आचरण के बारे में छानबीन करते हैं। इतने बड़े लोग पारिवारिक और व्यक्तिगत कामों से समय निकालकर विद्रोहियों के ऊपर पुलिस बर्बरता का प्रतिवाद करते हैं तो समाज में विवेक होने का प्रमाण है। लेकिन क्या इस बर्बरता को सज्जनों का यह समूह रोक पाएगा?
जिस देश का प्रशासन और कानून-व्यवस्था रोज कानून के प्रति वफादार लोगों पर शर्मनाक ढंग से ज्यादतियाँ करती रहती है, उसी का अधिकारी गैरकानूनी काम करने वालों के प्रति कैसे सदय हो सकता है? मानवाधिकारों के लिए समर्पित इन भद्र लोगों के समूहों से हमारा अनुरोध है कि मनमोहन सिंह द्वारा गठित प्रशासन-सुधार आयोग पर यह दबाव डालें कि पुलिस, प्रशासन तथा अदालतों की कार्यशैली में ढाँचागत परिवर्तन लाकर वफादार नागरिकों के प्रति सभ्य और लोकतांत्रिक आचरण का नियम बनवाएं। तब इस आचरण का एक अंश विद्रोहियों को भी मिल जाएगा।
भारतीय प्रशासन में राजा है जिला कलेक्टर। वह अपने क्षेत्र का सम्राट होता है। उसके अधीन कितने विभाग हैं, कोई नहीं जानता। जब कोई प्रगतिशील विचार का अच्छा विद्यार्थी आई.ए.एस. होता है, पहले दो साल तक संवेदनशील रहता है। जिला कलेक्टर होने के बाद उसमें औद्धत्य का गुण प्रवेश करता है।
जिला कलेक्टर की संस्था के रहते हुए विकेंद्रीकरण की बात करना बेमानी है। शासन के विकेंद्रीकरण का कोई लक्षण पंचायती राज में नहीं है।
पंचायती राज एक प्रकार की ठेकेदारी है। उसके पास कोई कोष नहीं होता है जिसका खर्च वह अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कर सके। गाँव के लिए अच्छी सड़क चाहिए तो उसके लिए प्रधानमंत्री योजना चाहिए। संसद के सदस्य के पास किसी भी सरपंच से अधिक कोष होता है।
यूरोपीय देशों में शासन का जितना विकेंद्रीकरण है, उतना ही करना है तो भी मौजूदा जिला कलेक्टर व्यवस्था को समाप्त करना होगा। राजनीति-विज्ञान के किसी शिक्षक से यह बात कहेंगे तो वह कहेगा कि देश शासनविहिन हो जाएगा। उसकी मूर्खता पर यह शासन-व्यवस्था टिकी हुई है।
सचिवालय में सबसे पहले किरानी के पास जाना पड़ता है। उसके पास निर्णय की कोई क्षमता नहीं है। पचास रुपए के भुगतान पर भी वह हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। मुहल्ले में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति भी नहीं दे सकता है। उसके लिखे हुए ‘नोट’ पर अधिकारी हस्ताक्षर करता है। बिना संशोधित किए हस्ताक्षर लगाने का अनुपात है अस्सी प्रतिशत। अतः अस्सी प्रतिशत निर्णय का अधिकार किरानियों को सौंप दिया जाए तो उनको आत्मगौरव का बोध होगा।
प्रस्तुत लेख के लिए अंतिम बात है उत्तरदायित्व, यानी जवाबदेही। ब्रिटिश काल में नौकरशाही में जो थोड़ी-बहुत जिम्मेदारी की भावना या जवाबदेही का डर था, वह इसलिए था कि छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी गोरे मालिक से डरता था।
गोरे मालिक चले जाने के बाद भारतीय नौकरशाही ने प्रशासन के सारे नियम-कायदे खुद बनाए तो जवाबदेही का कोई ढाँचा उन्होंने अपने लिए ईजाद नहीं किया। किसी इंजीनियर के तत्वावधान में पुल बन रहा है। बनने के एक-दो साल बाद टूटा दिखाई पड़ता है। इसका उत्तरदायित्व लेने के लिए वह तैयार नहीं है।
किसी जिले में वृद्धावस्था पेंशन दो महीनों से नहीं मिली है, एक पेंशन लेनेवाले गरीब आदमी की मृत्यु भूख से हो जाती है, जिला कलेक्टर को उत्तरदायी नहीं माना जाता है। सेना के सिपाहियों ने मणिपुर में बलात्कार के बाद एक औरत की हत्या कर दी। सेना के स्थानीय अधिकारियों को दोषी नहीं बनाया जाता है। ऐसी है उत्तरदायित्व की शून्यता। इंजीनियर, जिला कलेक्टर और सेनाधिकारी को हत्या करवाने के अपराध में सर्वोच्च सजा मिलनी चाहिए। उत्तरदायित्व का सिलसिला इसी तरह शुरू हो सकता है।
विडंबना यह है कि जब कोई युवा विद्यार्थी आई.ए.एस. होकर प्रशासनिक सेवा के लिए चुना जाता है, उसको सर्वश्रेष्ठ योग्यतासंपन्न समझा जाता है। सर्वश्रेष्ठ योग्यतासंपन्न समूह ने प्रशासन-तंत्र निर्मित किया है, जो पूरी तरह भ्रष्ट, अकुशल और अमानवीय है। उसे सुधारने के लिए एक कठोर इच्छाशक्ति वाले राजनैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.