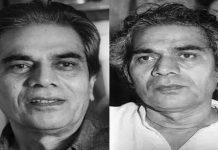हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बड़े चाव से हमें यह बताते रहे हैं कि “दुनिया भारत की ओर देख रही है।” यह बात या इससे मिलती-जुलती बात प्रधानमंत्री के भाषणों में कई दफा आयी। मसलन, मार्च में जब उन्होंने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का पॉवरहाउस कहा, मई में जब कहा कि दुनिया भारत के स्टार्टअप में भविष्य देख रही है, जून में जब कहा कि दुनिया भारत में निहित संभावनाओं की तरफ देख रही है और उसकी उपलब्धियों की प्रशंसा कर रही है और जुलाई में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा जब वह उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस-वे का उदघाटन कर रहे थे।
जरूर दुनिया भारत की तरफ देख रही है- लेकिन सम्मान और प्रशंसा की नजर से नहीं- इसकी पुष्टि आकार पटेल की किताब ‘मोदी-काल की कीमत’ (‘प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स’) पढ़ने से होती है। इस किताब में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हालात के वैश्विक सूचकांकों की सूची दी हुई है जो बताती है कि इन वैश्विक सूचकांकों में हमारा देश किस पायदान पर खड़ा है। लगभग इन सभी सूचकांकों में भारत का काफी निचला स्थान और किसी किसी में एकदम फिसड्डी होना यह बताता है कि दुनिया हममें जो देख रही है उसका प्रधानमंत्री के दावों से कोई मेल नहीं है।
मसलन, आकार पटेल बताते हैं कि हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है (यह सूचकांक बताता है कि किसी देश-विशेष का पासपोर्ट धारक पूर्व वीजा के बगैर कितने देशों की यात्रा कर सकता है, सिंगापुर और जापान इस सूचकांक में शीर्ष पर हैं)। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (वैश्विक भूख सूचकांक) में भारत 94वें स्थान पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स (यह सूचकांक यह दर्शाता है कि कोई देश अपने नागरिकों की आर्थिक और पेशेवर संभावनाओं को मूर्त रूप देने में कहां खड़ा है) में 103वें स्थान पर और संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पर खड़ा है। कई सूचकांकों में भारत की स्थिति में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने (2014) के बाद से गिरावट आयी है।
दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है यह मायने रखता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यह और भी महत्त्वपूर्ण है। जब हम ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजादी मिलने का 75वॉं वर्ष मना रहे हैं, हमें अपने आप से पूछना चाहिए : भारत कहां खड़ा है? क्या भारत के लोग खुश हैं? किस हद तक हमने एक राष्ट्र के तौर पर और नागरिक के रूप में संविधान में वर्णित आदर्शों पर अमल किया है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आशाओं को किस हद तक पूरा किया है?
संस्थाओं का अवमूल्यन
2015 में मैंने भारत को “सिर्फ चुनावी लोकतंत्र” करार दिया था, जिससे मेरा मतलब यह था कि चुनाव भले समय पर हो जाते हैं लेकिन एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में वास्तव में कोई जवाबदेही नहीं है। संसद, मीडिया और तमाम महकमे आदि इतने नाकारा और कर्तव्य-विमुख हैं कि सत्ताधारी दल की ज्यादतियों को रोक नहीं पाते हैं।
लेकिन अब तो लगता है कि भारत को “सिर्फ चुनावी लोकतंत्र” भी ज्यादा दिन नहीं कह पाएंगे। इलेक्टोरल बांड योजना की पर्दादारी, चुनाव आयोग का पक्षपाती रवैया, चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए दबाव डालने तथा रिश्वत का इस्तेमाल के कारण चुनाव भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं, न ही उनके नतीजों का हमेशा सम्मान किया जाता है।
हाल के वर्षों में भारतीय राज्य असहमति को कुचलने में बहुत ही निष्ठुर हो गया है। खुद सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच 24,000 से अधिक भारतीय नागरिक यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किए गए। इनमें से 1 फीसद से भी कम, दोषी साबित हुए। बाकी 99 फीसद लोगों की जिंदगी शक्की और एक खास विचारधारा से परिचालित राज्यतंत्र ने तबाह कर दी। पत्रकारों पर हमले भी और बढ़ गए, अगर आकार पटेल अपनी किताब में नवीनतम आंकड़ों को शामिल करें तो प्रेस की आजादी के वैश्विक सूचकांक में उन्हें भारत को 142वें स्थान के बजाय 150वें स्थान पर रखना पड़ेगा।
दमन के इस दौर में यह बताना काफी निराशाजनक है कि ऊपरी अदालतों ने नागरिक के विरुद्ध शासन का पक्ष लेने के लिए किन आरोपों का सहारा लिया है। जैसा कि प्रताप भानु मेहता ने हाल में लिखा है, “नागरिक अधिकारों का संरक्षक होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट अब नागरिक अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा है।”
संवैधानिक मामलों के विद्वान अनुज भुवानिया “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बहुसंख्यकवादी शासन के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के घुटने टेक देने” के बारे में हमें बता चुके हैं। वह यह भी बताते हैं कि “मोदी-काल में न सिर्फ सरकारी ज्यादतियों को रोकने की अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वाह करने में अदालत नाकाम रही है बल्कि इसने मोदी सरकार के एजेंडे का साथ देते हुए चीयरलीडर का काम किया है। इसने न सिर्फ शासन के स्वेच्छाचार के विरुद्ध नागरिकों के लिए ढाल बनने की अपनी मान्य भूमिका को तिलांजलि दे दी है बल्कि यह एक शक्तिशाली तलवार बन गयी है जिसे शासन के कहने पर लहराया जा सकता है।”
भारत के लोगों के पास बोलने की आजादी राजनैतिक तौर पर बहुत कम बची है, सामाजिक स्तर पर तो और भी कम। यहां से अंग्रेजों के जाने के पचहत्तर साल बाद भी हमारा समाज बहुत गहराई से श्रेणियों में विभाजित है।
1950 में भारत के संविधान ने जातिगत और लैंगिक भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया, फिर भी ये भेदभाव काफी हद तक जारी हैं। हालांकि एफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण दलितों के बीच से एक ऊर्जावान पेशेवर वर्ग तैयार करने में मददगार साबित हुआ है, सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में जातिगत पूर्वाग्रह बने हुए हैं। जाति उन्मूलन के डॉ आंबेडकर के आह्वान के इतने सालों बाद भी मात्र इनेगिने अंतर्जातीय विवाह होना इसी बात को रेखांकित करता है कि हमारा समाज कितना अनुदार और रूढ़िवादी है।
जेंडर के पैमाने पर देखें तो, दो आंकड़े बताते हैं कि हम आदर्श स्थिति से कितना नीचे हैं। पहला है, श्रम शक्ति में भागीदारी की दर, जो कि 25 फीसद के आसपास है, और विएतनाम या चीन को तो छोड़ दीजिए, यह बांग्लादेश से भी काफी कम है। दूसरा है स्त्री-पुरुष विषमता के वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति। हम इस सूचकांक में (जुलाई 2022) सर्वे किए गए कुल 146 देशों में 135वें स्थान पर हैं, और स्वास्थ्य तथा जीवन प्रत्याशा के पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर।
समाज से अब मैं संस्कृति और धर्म की तरफ चलता हूं। तस्वीर यहां भी कुछ अच्छी नहीं है। बंदिशें बढ़ रही हैं, राज्य की तरफ से भी और स्वयंभू निगरानी गिरोहों (विजिलैंट ग्रुप्स) की तरफ से भी, कि भारत के लोग क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, वे कहां रह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और किससे विवाह कर सकते हैं। शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू देश के मुसलमानों का दानवीकरण है, भाषा के स्तर पर भी और सलूक के स्तर पर भी। आज के भारत में राजनीति में और पेशेवर पदों पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, कार्यस्थलों पर और बाजारों में उनके साथ भेदभाव होता है, टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया में उन्हें काफी बुरा-भला कहा जाता है और उनका मखौल उड़ाया जाता है। उन्हें यह सब जो सहना पड़ता है और उन्हें जिस तरह लांछित किया जाता है वह हमारे लिए सामूहिक शर्म का विषय है।
नौकरशाही का नया शिकंजा
संस्कृति से मैं आर्थिकी पर आता हूं। नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को और खुली अर्थव्यवस्था बनाने के वादे पर सत्ता में आए थे। लेकिन वास्तव में वह एक तरह के संरक्षणवाद की तरफ लौट गए हैं, 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने जिसका खात्मा करना चाहा था। भीतर मुड़ने के इस रुख ने देश के अपने उद्यमियों को पक्षपात से मुक्त प्रतिस्पर्धा का मौका तक नहीं दिया है- इसके बजाय बस कुछ चहेते उद्योगपतियों ने ही चॉंदी काटी है, जिसे भारत सरकार के एक पूर्व आर्थिक सलाहकार ने कलंकित पूंजीवाद का ‘2 A मॉडल’ नाम दिया है। टैक्स और कस्टम विभागों में अफसरों को फिर से वे अधिकार दे दिए गए हैं जो उनसे ले लेने थे। लाइसेंस-परमिट राज के इस नए रूप का दंश खासकर छोटे उद्यमी महसूस कर रहे हैं। इस बीच बेरोजगारी की दर काफी ऊंची है और कामगारों की कुशलता का स्तर नीचा है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 तैयार की है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे धनी 1 फीसद लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22 फीसद है जबकि सबसे गरीब 50 फीसद लोगों के पास राष्ट्रीय आय का सिर्फ 13 फीसद। जुलाई 2021 में मुकेश अंबानी 80 अरब डॉलर के मालिक थे, इससे पहले के साल के मुकाबले उनकी आय में 15 अरब डॉलर का जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी अवधि में गौतम अडानी की संपत्ति में आश्चर्यजनक उछाल आया – 13 अरब डॉलर से 55 अरब डॉलर। अडानी की निजी संपत्ति अब 110 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गयी है।
भारत में आय और संपत्ति की विषमता सदियों रही है लेकिन अब यह दिनोदिन और भी अधिक गैरबराबरी वाला समाज बनता जा रहा है।
चाहे मात्रात्मक स्तर पर देखें या गुणात्मक स्तर पर, भारत की आजादी के पचहत्तर वर्षों का प्रगति विवरण निस्संदेह काफी मिश्रित है। निश्चित रूप से नाकामियों का ठीकरा केवल मौजूदा सरकार के सिर पर ही नहीं फोड़ा जा सकता। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भले लोकतांत्रिक संस्थाओं को खड़ा किया और धार्मिक तथा भाषाई बहुलता को मान दिया, लेकिन उसे भारत के उद्यमियों में कहीं अधिक भरोसा जताना चाहिए था, साथ ही उसे निरक्षरता दूर करने और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए और तेजी से काम करना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने युद्ध-काल में अपने को एक काबिल नेता साबित किया लेकिन स्वतंत्र संस्थाओं पर उनके प्रशासन का कब्जा, अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण को मजबूत करना, एक गौरवशाली इतिहास वाली राजनीतिक पार्टी को एक पारिवारिक जागीर में बदल देना, खुद के इर्दगिर्द व्यक्ति पूजा की संस्कृति विकसित करना, इस सब ने हमारे राजनीतिक जीवन और आर्थिक संभावनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया।
नरेन्द्र मोदी पूरी तरह अपने बूते बने हुए और बहुत परिश्रमी राजनेता हैं लेकिन सत्ता के केन्द्रीकरण और समाज तथा आर्थिक पहलुओं पर राज्य के कठोर नियंत्रण में उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। उनकी निरंकुश प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित बहुसंख्यकवाद के साथ मिलकर जो सब किये जा रही है उसके बारे में भविष्य में इतिहासकार जब लिखेंगे तो उनकी राय आज की भक्त ब्रिगेड जैसी नहीं होगी बल्कि काफी कठोर होगी।
किये गये वादों, और जो किया जा सकता था, इन दोनों के बीच के अंतराल का विश्लेषण करने के लिए हमें ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों के तथा जिन सरकारों का उन्होंने नेतृत्व किया उनके कृत्यों (और कुकृत्यों) पर निगाह डालनी चाहिए। या हम इस मसले को समाजशास्त्रीय नजरिए से भी देख सकते हैं, आंबेडकर के उस कथन की रोशनी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र अभी ऊपरी सज धज है क्योंकि यहां की जमीन यानी यहां का सामाजिक ढांचा निहायत अलोकतांत्रिक है। शायद साढ़े सात दशक का समय गुलामी के उन अनगिनत रूपों से छुटकारा दिलाने के लिए काफी कम है, जिनसे भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास आक्रांत रहे हैं।
हमें हमारे नेताओं द्वारा हमारे नाम पर किये जा रहे शेखी-भरे दावों से भुलावे में नहीं आना चाहिए, यह डींग हांकना आनेवाले दिनों में और बढ़ सकता है। दुनिया न तो चमत्कृत है न भारत की तरफ प्रशंसा की नजर से देख रही है। यही बात भारत के उन लोगों के बारे में भी कही जा सकती है जो खुद देख सकते हैं और खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। भारत जहां औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र है वहीं भारत के लोगों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत तौर पर आजादी पाना अभी बाकी है।
(द टेलीग्राफ से साभार)
अनुवाद : राजेन्द्र राजन
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.