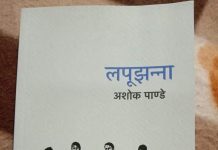— नंदकिशोर आचार्य —
आधुनिक काल में सत्ता का मूल स्रोत नागरिकों का विश्वास और स्वीकृति है तो इसलिए यह आवश्यक है कि राजसत्ता इस मूल आधार से विछिन्न न हो, अन्यथा इसका तात्पर्य सत्ता का निरंतर उत्तरदायित्वहीन और धीरे धीरे मानवीय मूल्यों से उदासीन और आततायी होते जाना होगा। लोकप्रतिनिधियों के सावधि चुनाव और संसदीय लोकतंत्र इसी मूल आधार को बनाए रखने की दिशा में किए जाने वाले प्रयत्न हैं। लेकिन इन संस्थाओं का सारा इतिहास इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता कि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं बल्कि अक्सर ऐसा हुआ कि इन संस्थाओं का स्वरूप और प्रकृति सारी वैधानिक औपचारिकताओं के बावजूद निरंकुशता के करीब आते गए हैं। इसीलिए यह आवश्यक समझा जाने लगा है कि ग्राम स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाय ताकि राज्य से नागरिक का अधिकारिक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो सके और राजनैतिक निर्णयों को वह अधिकाधिक प्रभावित कर सके।
लेकिन यह विकेंद्रीकरण भी तभी सार्थक हो सकता है, जब इसकी संवैधानिक गारंटी हो और देश की सर्वोच्च संस्था को भी इसके बुनियादी ढांचे और अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार न हो। इससे संबंधित व्यवस्थाएं विचार-विमर्श के द्वारा तय की जा सकती हैं।
लेकिन इसकी सफलता भी इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि सावधि चुनाव के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी एक निश्चित अवधि के लिए अबाध अधिकार न दिए जाएं और कोई ऐसी विधि विकसित की जाय जिसके द्वारा उन पर निरंतर प्रभावी नियंत्रण कायम रखा जा सके। स्थानीय स्तर से लेकर प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर तक ऐसी नागरिक समितियों का गठन किया जा सकता है जो स्वयं विधिनिर्माण और कार्यपालिका संबंधी कार्य न करती हों लेकिन किए कार्यों की समीक्षा कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर अपने इलाके के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित निर्देश भी दे सकें।
इस तरह की समितियों का गठन केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर भी होना चाहिए ताकि सभी प्रकार के हितों का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो सके। इन समितियों को अपने इलाके के प्रतिनिधि को वापिस बुलाने का अधिकार भी दिया जा सकता है – इस शर्त के साथ कि यदि पुनः उसी प्रतिनिधि में जनता द्वारा विश्वास प्रकट किया गया तो संबंधित समिति स्वयमेव भंग समझी जाएगी और इसका गठन दोबारा किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था से जहां निर्वार्चित संस्थाओं पर लोक-नियंत्रण बना रह सकेगा, वहीं इस व्यवस्था का दुरुपयोग भी कम से कम हो सकेगा। इस समिति के सदस्यों के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे किसी दल विशेष से सक्रिय रूप से न जुड़े हों। इस समिति के चुनावों के समय कोई दल कोई निर्देश जारी नहीं कर सकेगा, इसकी भी संवैधानिक व्यवस्था की जानी जरूरी होगी।
दरअसल, लोकतंत्र ठीक तरह से काम कर सके, इसके लिए नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों का राजनैतिक दलों से मुक्त होना आवश्यक है। किसी युग में राजनैतिक दलों ने लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाई भी हो तब भी अब वे धीरे-धीरे ही सही उसके क्रियान्वयन में बाधा ही अधिक होते जा रहे हैं।
आधुनिक समाजों का विकास जिस तरह से ही रहा है, उसमें किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह संभव नहीं रह गया है कि वह एक छोटी-सी अवधि में पूरे समाज के लिए सही राजनीतिक निर्णय ले सके। प्रत्येक सरकार एक निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है – इसका एक सीधा मतलब क्या यह नहीं है कि लोकतांत्रिक नैतिकता के अनुसार किसी भी सरकार को ऐसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए जिसका प्रभाव उस निश्चित अवधि से आगे भी पड़ता हो? लेकिन क्या व्यवहारतः ऐसा संभव है?
इसी तरह प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव घोषणापत्र के आधार पर चुना जाता है, लेकिन उनके शासन की अवधि के दौरान ऐसे भी बहुत से मामले आते हैं जिनका कोई उल्लेख चुनाव घोषणापत्र में नहीं किया गया होता है – बल्कि सभी मामलों का उल्लेख किया जाना संभव नहीं है – ऐसी स्थिति में यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसे कहां तक लोकेच्छा को प्रतिबिंबित करने वाला कहना उचित समझा जाएगा? इसी के साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कई दफा बहुत सी सरकारों द्वारा कुछ ऐसे निर्णय ले लिये जाते हैं और कुछ योजनाओं पर इतना अधिक व्यय कर दिया जाता है कि उन्हें बदलना या रोक देना किसी ऐसे दल के लिए भी संभव नहीं रहता जो संबंधित निर्णय या योजना से पूरे तौर पर असहमत हो। इसके लिए आवश्यक है कि महत्वपूर्ण और नीति संबंधी बुनियादी मसलों पर समय-समय पर जनमत संग्रह के द्वारा आम राय जानी जाय और निर्वाचित सरकार उसी के आधार पर अपने निर्णय ले।
एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित सरकार को ऐसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जिनके आधार पर उस सरकार के हटने के बाद भी उसकी नीतियां जारी रह सकें। कुछ बुनियादी और जरूरी बातों के लिए नीति संबंधी निर्णयों का उल्लेख संविधान में ही कर दिया जाना उचित है ताकि उन पर अपने शासन के दौरान कोई भी राजनैतिक संगठन अलग-अलग निर्णय न ले – बल्कि सभी संविधान में निहित नीति का ही सम्मान करें। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जनमत-संग्रह के आधार पर ही किया जाना उचित है।
सवाल उठाया जा सकता है कि इस प्रकार बार-बार जनमत-संग्रह करवाना बहुत व्यय साध्य है। लेकिन यहां यह भूला जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ-साथ ही लागू की जा सकती है क्योंकि तब बहुत से स्थानीय मसलों पर आम राय प्राप्ति करना महंगा नहीं पड़ेगा और न हर आम राय का गोपनीय होना ही जरूरी होगा।
वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दलों की कोई विशेष सार्थकता नहीं रह गई है क्योंकि उनका प्रधान लक्ष्य मानवीय चेतना के विकास में कोई सार्थक राजनीतिक भूमिका अदा कर सकने की बजाय सत्ता पर अधिकार करना अधिक हो गया है। सत्ताकांक्षा के इस खेल के सभी नियमों को मानना प्रत्येक राजनैतिक दल की मजबूरी बनता जा रहा है और उसी का एक परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक राजनीतिक दल की संस्कृति करीब-करीब एक जैसी होती जा रही है। सभी के साधन एक जैसे हैं, अतः साध्य पर भी उनका असर पड़ना स्वाभाविक है।
इसलिए ऐसा लगने लगा है कि राजनीतिक दल किसी मानवीय मूल्य की राजनीतिक स्वीकृति के लिए प्रयत्नरत संगठन होने की बजाय सत्ताकांक्षी लोगों के गिरोह अधिक हो गए हैं। शायद यही कारण है कि अपने समय की प्रतिभा राजनीति की बजाय विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों की ओर अधिक उन्मुख है क्योंकि वर्तमान राजनीतिक संस्कृति का उसके आसाथ कोई रचनात्मक संबंध नहीं बनने पाता। इसलिए जहां एक ओर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और निर्वाचित प्रतिनिधियों पर निरंतर नियंत्रण आवश्यक है, वहीं साथ ही यह भी जरूरी है कि राजनीतिक दलों की इस पतनशील स्थिति को पहचाना जाए और उसका विकल्प दे सकने में समर्थ राजनैतिक व्यवस्था विकसित करने की ओर चेष्टारत हुआ जाए।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.