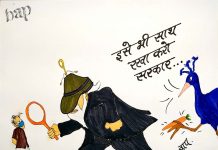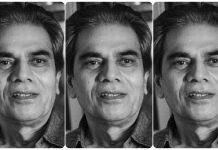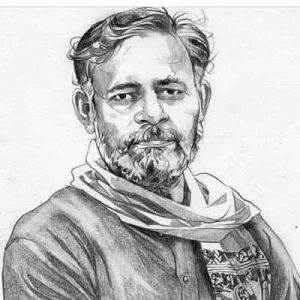
— योगेन्द्र यादव —
सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य श्रेणी के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। पहली नजर में यह फैसला न्यायसंगत और तर्कसंगत प्रतीत होता है। लेकिन जरा बारीकी से देखें तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ द्वारा किए गए इस फैसले से कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। यह निर्णय भविष्य में कई विसंगतियों को जन्म देगा।
इसमें कोई संदेह नहीं कि सवर्ण जातियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीबों की संख्या काफी बड़ी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर लोगों में एक बड़ी संख्या सवर्ण जातियों के मजदूरों की होती है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते अपने गांव में मजदूरी नहीं कर सकते। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि शैक्षणिक और नौकरी के अवसरों को हासिल करने में परिवार की आर्थिक हैसियत की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
आजकल हर परीक्षा ट्यूशन और कोचिंग पर निर्भर करती है। आपकी जाति चाहे जो भी हो, यदि आपके मां-बाप महंगी कोचिंग नहीं खरीद सकते तो आपके उच्च शिक्षा और नौकरी की परीक्षा में सफल होने की संभावना बहुत घट जाती है। जाहिर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा भी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करना जरूरी है।
सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था आरक्षण की शक्ल ले? क्या सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ मिले? क्या गरीबी के आधार पर मिलने वाले इस आरक्षण से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के गरीबों को बाहर रखा जाए?
यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सरकार ने 2019 के चुनाव से पहले 103वें संविधान संशोधन के जरिए सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान आरक्षण के अलावा 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की थी। उस समय सभी पार्टियों ने इसका समर्थन कर दिया था।
इससे पहले नरसिंहा राव की कांग्रेस सरकार भी ऐसी ही एक व्यवस्था कर चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में उसे असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। इस नए संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खण्डपीठ ने इस पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। फैसला एकमत से नहीं हुआ। तीन जजों यानी न्यायमूर्ति माहेश्वरी, त्रिवेदी और पारदी वाला ने इस संविधान संशोधन को सही बताया, तो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति भट्ट ने संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया।
जाहिर है खंडपीठ का पूरा फैसला पढ़ने के बाद इस पर काफी चीरफाड़ होगी, टिप्पणियां और बहस होगी। लेकिन शुरुआती तौर पर कोर्ट द्वारा सुनाए फैसले में दिए गए तर्क के आधार पर कुछ सवाल उठाने जरूरी हैं। फिलहाल कानूनी पेच को छोड़कर दो बड़े सवाल उठाने जरूरी हैं।
पहला सवाल यह है कि क्या गरीबी की बीमारी के लिए आरक्षण सही दवा है? इसमें एक कानूनी पेच है कि क्या संविधान में ‘सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों’ के लिए विशेष व्यवस्था की अनुमति को गरीबों पर लागू किया जा सकता है? लेकिन अगर इस कानूनी पेच को छोड़ भी दिया जाए तब भी सवाल उठता है कि आरक्षण जैसे औजार का प्रयोग किन परिस्थितियों में करना सही होगा? अब तक आरक्षण के पक्ष में दलील यह रही है कि यह एक असाधारण औजार है जिसका इस्तेमाल केवल पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों साल की वर्जनाओं और वंचनाओं को काटने के लिए किया जाना चाहिए।
अगर इसका इस्तेमाल किसी एक परिवार या व्यक्ति की दिक्कत या अवसरों की समानता के लिए किया जाने लगा तो यह आरक्षण जैसे असाधारण औजार का दुरुपयोग होगा। अगर गरीबी के कारण पैदा हुई असमानता को ठीक करना है तो उसके लिए बेहतर स्कूली व्यवस्था, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सुविधाएँ देना बेहतर होगा। अगर सचमुच गरीबों को शिक्षा और नौकरी के बेहतर अवसर देने हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए शिक्षा के निजीकरण को रोकना जिसके चलते गरीब घर के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा लेना दूभर हो गया है। सवाल यह है कि अगड़ी जाति के गरीबों को आरक्षण का लॉलीपॉप इसलिए तो नहीं थमाया जा रहा है कि शिक्षा के महंगे होते जाने पर उनके गुस्से से ध्यान बंटाया जा सके?
दूसरा सवाल यह है कि अगर गरीब परिवार के बच्चों के लिए आरक्षण करना ही है, तो वह केवल सामान्य वर्ग के लिए ही क्यों हो? अपने असहमति के फैसले में न्यायमूर्ति भट्ट और ललित ने सरकार के सर्वेक्षण का हवाला दिया है जो बताता है कि देश के 6 में से 5 गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से आते हैं। ऐसे में गरीबों के आरक्षण का बड़ा हिस्सा भी इस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए।
लेकिन संविधान के 103वें संशोधन के अनुसार गरीबी के आरक्षण का फायदा केवल उन परिवारों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति या ओ.बी.सी. में नहीं आते। तर्क यह है कि उन्हें जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा है इसलिए आर्थिक आधार पर उन्हें दोहरा फायदा नहीं दिया जा सकता। इस तर्क का मतलब यह होगा कि देश की 70 से 75 प्रतिशत बहुसंख्यक आबादी को 50 प्रतिशत नौकरियों तक सीमित कर दिया जाएगा और बाकी 50 फीसदी नौकरियां व्यवहार में देश की 25 से 30 प्रतिशत अगड़ी जातियों के लिए आरक्षित हो जाएँगी।
सवर्ण गरीब किसी भी तरह से देश की आबादी का 5 से 6 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण देना कहा तक न्यायसंगत है? यह तो सामाजिक न्याय के नाम पर अन्याय होगा। यूं भी हमारे देश में जाति का झूठा सर्टिफिकेट बनाना कठिन है लेकिन गरीबी का झूठा प्रमाणपत्र बनाना सबसे आसान है, जो जितना अमीर है वह गरीबी का प्रमाणपत्र उतनी ही आसानी से बनवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन तमाम लोगों को निराश किया है जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को इस देश में चले आ रहे सामाजिक अन्याय की काट के रूप में देखा है। देखना यह है कि इस फैसले को पलटने में अब कितने बरस या दशक लगते हैं।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.