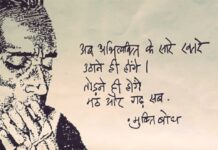— राम जन्म पाठक —
कहीं भी रहना, क्या सिर्फ रहना मात्र होता है! यानी सुबह उठना, खाना खाना, नौकरी पर जाना, शाम को वापस आना, थोड़ा काम-वाम करके फिर निद्रा की गोद में। या इससे कुछ अलग होता है कहीं भी रहना।
क्या रहने और बसने में कुछ अंतर है? गांवों में हम बसते हैं और शहरों में हम रहते हैं। मेरा घर उत्तर प्रदेश के एक बहुत पिछड़े जिले बस्ती के एक गांव में है। एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी से बैलगाड़ी लेकर बस्ती तक गए थे। इस यात्रा संस्मरण को उन्होंने ‘सरयू पार की यात्रा’ नामक पुस्तक में कलमबद्ध किया है। यह पुस्तक हिंदी का पहला यात्रा-संस्मरण मानी जाती है। इसमें उन्होंने बस्ती जिले की दीन-हीन दशा का वर्णन किया है। यहां तक लिख गए ”बस्ती को बस्ती कहूं, तो काको कहूं उजाड़।” तो मैं ऐसे ही जिले का बाशिंदा हूं।
विषयांतर से बचते हुए मैं फिर उसी रहने और बसने के प्रश्न पर डटा रहना चाहता हूं। ज्यादातर छोटे-छोटे शहरों से गुजरते हुए बड़े शहर दिल्ली में रह रहा हूं। तकरीबन सोलह बसंत तो नहीं, हां सोलह जेठ-बैसाख और माघ-पूस और इतने ही कोहरा-धुंध और शोर भरे साल जरूर गुजर गए। इससे पहले फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली और मुरादाबाद जैसे शहरों में जरूर रहा हूं। सोचता हूं हर जगह रहता ही क्यों हूं, बसता क्यों नहीं।
और कमाल यह भी कि रहने, रहने में भी फर्क होता है। हर शहर की अपनी अलग खुशबू और बदबू होती है। अपनी बनावट, अपनी बुनावट। चक्करदार पथ के साथ हर शहर जैसे सुबह को होता है, वैसे शाम को नहीं होता। कुछ उदास शामें और निकम्मे भोर भी होते हैं। आप जैसे फैजाबाद में रहते हैं, वैसे इलाहाबाद में नहीं रहते।
जब मैं इलाहाबाद में रहता था यानी 1984 से लेकर 1996 तक। तो साइकिल उठाकर बहुत कम समय में सारी जगहें छान मारता था और ढेर सारे दोस्तों और दुश्मनों से मिल आता था। मन फूला-फूला रहता था। थोड़ा खुश-खुश। हमारे अवधी में कहते हैं गगन-मगन। गंगा की विशालता और क्षितिज छूते कछार को मैंने गोविंदपुर कालोनी के मकान नं 113 में रहते हुए कितने ही तरीके से कितने ही बार मंत्रमुग्ध होकर निहारा है। गंगा की रेत में लोटने चला जाता था दोस्तों के साथ। कबड्डी खेलकर और धंसकर-हंसकर नहाते हुए लौट आता था। रास्ते में सरसों के फूल लहराकर हमारी अगवानी कर लेते थे।
लेकिन बसना वहां भी नहीं हो पाया। सूकरखेत था हमारा इलाहाबाद। उसकी छाप अंग-अंग पर विराजमान है।
लेकिन सोचता हूं कि बस क्यों नहीं पाया वहां। क्या था जो अपने वश में नहीं था। वीरेन डंगवाल की कविता है, ‘जहां के हो गए, वहीं से कर दिए गए अपरिहार्य बाहर।’ बरेली में भी रहा अल्पकाल के लिए। बस उसी तरह जैसे ट्रेन से उतरकर मुसाफिरख़ाने में रहते हैं थोड़ी देर। बरेली में भला था क्या, सिवा डंगवाल और सिवा डंगवाल के।
मुरादाबाद का पड़ाव लंबा खिंचा। बल्कि यों कहिए कि वहीं फंस गए या यों कहें कि थोड़ा गहरे धंस गए। शायरों की जबान उधार लूं तो कहूंगा कि जहां रहा आबाद रहा, क्योंकि फैजाबाद रहा, इलाहाबाद रहा और मुरादाबाद रहा। मुरादाबाद, इलाहाबाद के रचाव-बसाव से बिल्कुल भिन्न है। इलाहाबाद में कोई कितना ही बड़ा अफलातून हो, सूरमां हो, माफिया हो, ज्ञानी हो, किसी के मन में उनके लिए कोई अतिरिक्त भाव नहीं है। जज हों, कलट्टर हों, कुलपति हों, प्रोफेसर हों, दुकानदार हो, नर्तकी हो, वेश्या हो- जा रहा है तो जाने दो। उस तरफ देखना ही नहीं है। जिस शहर ने चार-चार प्रधानमंत्री दिए हों, उसे किसी को बहुत ज्यादा भाव देने की जरूरत क्या है!
इलाहाबाद बहुत जल्दी किसी का नोटिस नहीं लेता। और मुरादाबाद? यह हर किसी का नोटिस लेता है। मेरे जैसे छुटभैए पत्रकार का भी। मुझे बहुत झेंप लगती थी जब मैं किसी कार्यक्रम वगैरह को कवर करने जाता था तो वीआइपी लोगों में मेरा भी नाम माइक से पुकार दिया जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे प्रतिक्रिया करूं। लेकिन, बहुत बाद में समझ में आया कि यह इस शहर का मिजाज है। जिगर मुरादाबादी का शेर है- अपना पैगाम मुहब्बत है, जहां तक पहुंचे। पता नहीं कैसे इस शहर को लोगों ने सांप्रदायिक कहकर बदनाम किया होगा, यहां के लोग, हिंदू और मुसलमान बहुत मिलनसार हैं। बाहर के लोगों का स्वागत करने को उत्सुक रहने वाला शहर है मुरादाबाद। हर वक्त मदद को तैयार।
लेकिन बसना यहां भी नहीं हो पाया।
सोलह साल से डेरा दिल्ली में है। दिल्ली सपनों का शहर है शायद। नहीं सपनों के टूटने का, नहीं मृगमरीचिका का, नहीं गुजारा करने का। हां, यही सही है, यह गुजारा करने का ही शहर है। यहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर बड़े-बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, कलाकार, अभिनेता और माफिया-अपराधी भी बस गुजारा ही करते हैं। गालिब उकता गए थे इस शहर से। उन्होंने लिखा- है अब इस मामूरे में क़हत-ए-ग़म-ए-उल्फ़त ‘असद’। हम ने ये माना कि दिल्ली में रहें खावेंगे क्या। (यानी दिल्ली में प्रेम के दर्द की कमी है, और जिस शायर का भोजन ही प्रेम का दर्द हो, वह खाएगा क्या।)
गालिब, जिगर के उलट हैं। या यों कहें कि दिल्ली, मुरादाबाद से उलट है।
मुरादाबाद में मोहब्बत की भरमार है और दिल्ली में मोहब्बत का दर्द ही नहीं है। मीर भी दिल्ली से निराश रहे होंगे, लेकिन वे लाचार थे शायद, कुछ मेरी तरह। कुछ रोजी-रोटी फंसी होगी यहां। वही गुजारे वाली बात। तभी बोले- कौन जाए मीर ई दिल्ली की गलियां छोड़कर। सो मैं भी दिल्ली में गुजारा कर रहा हूं। मगर, बसना यहां भी नहीं हो पा रहा है।
आखिर बसना होता क्या है। क्या रचना? यानी जो रचेगा वही बसेगा। ऐसा कुछ, क्या? क्या गांव के लोग रचते हैं, इसीलिए बसते हैं। और शहर के लोग?
तो क्या मुझे बसने के लिए अपनी बस्ती में जाना होगा। क्या अब मैं वहां जा पाऊंगा। जा भी पाया तो बस पाऊंगा। नहीं, पुराने साथी अब वहां नहीं मिलते। नए बच्चों को मैं पहचानता नहीं, वे मुझे भी नहीं पहचानेंगे। जहां मैं सवारी से उतरता था, उस केशवपुर और घघौवा पुल का नक्शा बदल चुका है। सरयू के तट पर है हमारा गांव-घर। सरयू में बहुत पानी बह चुका है। गांव में बाढ़ अब भी आती है, अपनी ऋतुचर्या के हिसाब से। मेरे पिता इतने धार्मिक हैं, बाढ़ जब सब-कुछ, खेत की फसल लील जाती तो कहते- कोई बात नहीं, सरयू मैया के पांव तो पड़े खेत में। यही कहकर संतोष कर लेते थे। क्या यही संतोष है, जो गांवों में लोगों को बसाता है।
इतना संतोष मैं कहां से लाऊंगा?
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.