
— आलोक रंजन —
भारत जैसे बहुभाषी देश में अस्मितावादी राजनीति के हवाले से भाषा के सवाल तो उठते रहते हैं लेकिन उसकी सैद्धान्तिक समझ बनाने संबंधी पहल लगभग न के बराबर होती है। आम भारतीय मानस के लिए भाषा के प्रश्न देश की राजभाषा और कभी-कभी होने वाले हिन्दी विरोधी प्रदर्शनों तक ही सीमित रहते हैं। एक महत्त्वपूर्ण विषय होने के बावजूद इसका स्वतंत्र अध्ययन तो दूर इस पर चर्चा तक नहीं होती है। राजीव रंजन गिरि की पुस्तक परस्पर : भाषा-साहित्य-आंदोलन इस महत्त्वपूर्ण विषय को औपचारिक ज्ञान का हिस्सा मानते हुए एक जरूरी किताब की तरह हमारे सामने आती है।
हिन्दी देश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होने के साथ-साथ देश की राजभाषा भी है। इन सबके अतिरिक्त यह भाषा आम तौर पर देश की भाषा- समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती रही है इसलिए इसके पक्ष से लिखा जाना तार्किक भी है। इस पुस्तक में हिन्दी क्षेत्र की ‘भाषा’ के ‘बोली’ बन जाने और ‘बोली’ का ‘भाषा’ का स्तर पा जाने की बहु-स्तरीय कहानी के साथ साथ संविधानसभा में देश की राजभाषा को लेकर हुई बहसों और प्रतिनिधियों के अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं के महत्त्व और राष्ट्रीय पहचान की जरूरत संबंधी खंडन-मंडन, हिन्दी की ‘लघु-पत्रिकाओं’ के साहित्यिक योगदान और उनकी विकास-यात्रा को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह किताब हिन्दी भाषा और साहित्य की यात्रा को तीन अध्यायों में रखकर विश्लेषित करती है। प्रथम अध्याय ‘उन्नीसवीं सदी में ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली विवाद’, दूसरा अध्याय ‘राष्ट्र-निर्माण, संविधान-सभा और भाषा-विमर्श’ और तीसरा अध्याय ‘बीच बहस में लघुपत्रिकाएँ : आंदोलन, संरचना और प्रासंगिकता’ के नाम से सामने आते हैं; विषय-क्रम किताब की एक झलक हमारे सामने रखता है। लेखक इस पुस्तक की भूमिका में बताते हैं कि ये अध्याय शोध-लेखों के रूप में विभिन्न पत्रिकाओं में पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं, अब ये किताब के रूप में सामने आए हैं। यह किताब हिन्दी की साहित्यिक और संवैधानिक यात्रा का समग्र विश्लेषण है जो इन अध्यायों में क्रमिक रूप से व्यक्त हुआ है।
इस पुस्तक की भूमिका की शुरुआत में ही राजीव लिखते हैं : “किसी समाज का बहुभाषी होना उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक है। इस समृद्धि के साथ कुछ समस्याएँ भी पल्लवित-पुष्पित होती रहती हैं। चाहे समृद्धि हो या समस्या, दोनों भू-राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना से गहरे प्रभावित होती हैं।” ये पंक्तियाँ भारत की बहुभाषिक संरचना के सभी पक्षों को बहुत स्पष्टता के साथ रखती हैं। भारत का बहुभाषी होना एक ओर यदि सकारात्मक है तो दूसरी ओर राजनीतिक और समाजार्थिक अधिरचनाओं के माध्यम से कुछ नए पहलू उजागर होते हैं जिनमें नकारात्मक हिस्से भी हैं। ग्रीनबर्ग विविधता संबंधी सूची जारी करने वाली संस्था है; उसके अनुसार, भारत भाषाई विविधता में दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। ऐसे बहुभाषी देश में हिन्दी का राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेना हिन्दी के महत्त्व को प्रतिबिम्बित करता है। साथ ही यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तविक स्थिति यही है?

लेखक जिन समस्याओं के पल्लवित और पुष्पित होने की बात अपनी भूमिका में करते हैं उसी के मद्देनजर हिन्दी या देश की किसी भी अन्य भाषा की स्थिति वह नहीं है जिसकी वह अधिकारिणी है। यह पुस्तक उन प्रक्रियाओं पर गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत करती है जिसके तहत हिन्दी सहित तमाम अन्य स्थानीय भाषाओं ने अपना महत्त्व हासिल नहीं किया। इस कड़ी में आदिवासी भाषाओं की तो दशा और खराब रह गयी। अपने तीनों अध्यायों के माध्यम से यह किताब हिन्दी भाषा की विकास यात्रा की बात करती है लेकिन इसका फ़लक हिन्दी तक महदूद नहीं रहता। सांप्रदायिक राजनीति, उपनिवेशवादी छाप और भूमंडलीकरण के प्रभाव में भाषाओं की यात्रा कैसे होती है और किस प्रकार यह अपने बोले जाने वाले वर्ग को प्रभावित करते हुए उसकी राजनीतिक और सामाजिक संरचना का निर्माण करती चलती है उसे लेखक ने अपने विश्लेषण में केन्द्रीय तत्त्व के रूप में रखा है। यहाँ यह दोहराना आवश्यक हो जाता है कि इन सबको व्यक्त करने के लिए लेखक ने हिन्दी भाषा साहित्य के विभिन्न पहलुओं का सहारा लिया है।
उन्नीसवीं सदी में ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली विवाद
भाषा का बोली का रूप ग्रहण कर लेना और बोली का भाषा में बदल जाना हिन्दी भाषा साहित्य की दृष्टि से एक रोचक परिघटना है। लेकिन इसके प्रति अब तक की समझ को इस अध्याय ने न सिर्फ झकझोरा है बल्कि नए विश्लेषणों और प्रमाणों के साथ अलग व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है जो ज्यादा तार्किक और समीचीन भी है। आमतौर पर खड़ीबोली हिन्दी को ब्रजभाषा के स्थान पर काव्यभाषा के रूप में स्थापित करवाने का पूरा श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है लेकिन राजीव ने इसे सर्वथा नवीन तथ्यों के आलोक में देखा है। ‘ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली’ की बहस को वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बजाय अयोध्या प्रसाद खत्री के माध्यम से रखते हैं। इसके पीछे का आधार यह है कि जिस प्रक्रिया को द्विवेदी जी का आरंभ किया माना जाता है उसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी।
अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी किताब ‘खड़ी बोली का पद्य’ के माध्यम से एक ऐसी भाषा की काव्यभाषा के रूप में वकालत की जो ब्रज के मुकाबले एक बोली थी। उस समय ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा के रूप में अलग अलग हिस्सों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य कर रही थी। लेकिन खड़ी बोली जो कि महज एक जनपदीय भाषा भर थी उसने संपर्क भाषा के रूप में तेजी से अपना स्थान ग्रहण करना शुरू कर दिया था। खड़ी बोली और ब्रज भाषा के उदाहरण से यह बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि बोली और भाषा का रूपान्तरण भाषा की अपनी क्षमताओं के बजाय बदलती राजनीति व समाजार्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। खड़ी बोली एक ‘बोली’ के रूप में पहले से मौजूद थी लेकिन उसने उस दौर में आधुनिकता के साथ अन्योन्यक्रिया के दौरान भाषा का स्वरूप ग्रहण किया। अपने को बदलते परिवेश में ढाल लेने के कारण ही हिन्दी ने ब्रज के मुकाबले स्वयं को स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। पद्य की भाषा अभी भी ब्रज ही बनी हुई थी।
इसके बाद भी यह वह दौर नहीं था कि ब्रज ने आज की हिन्दी की तरह दूसरी जनपदीय भाषाओं के ऊपर अपना आधिपत्य थोप दिया हो और भाषाओं के बीच वैमनस्य पैदा कर दिया हो। यदि ऐसा होता तो अयोध्या प्रसाद खत्री या उन जैसे लोगों के लिए यह काम बहुत सरल हो जाता जो खड़ीबोली को काव्य की भाषा के रूप में प्रयोग करने के पक्षधर थे। यह पुस्तक खत्री जी के प्रयासों को हिन्दी के पाठकों के सामने रखती है और उन प्रयासों के माध्यम से तत्कालीन प्रतिष्ठित साहित्यकर्मियों के व्यवहारों का विश्लेषण करती है जिससे उनके पूर्वग्रहों का पता चलता है।
राजीव रंजन गिरि एक पुस्तक ‘खड़ी बोली का पद्य’ के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक स्थितियों की जो पड़ताल करते हैं वह अपने आप में आँख खोलने वाली है। इनमें सबसे बड़ा तो यही कि पद्य की भाषा के रूप में खड़ीबोली के विकास के लिए काम करने वालों में अयोध्या प्रसाद खत्री का योगदान स्वीकार नहीं किया जाता। दूसरे, बहुत-से प्रगतिशील चेहरों की कलई भी इसके मार्फत खुलती है। तीसरी सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि भाषाई सांप्रदायिकता के बीजवपन को भी देखा जा सकता है। खत्री जी कविता में जिस भाषा की प्रतिष्ठा चाहते थे उसका संघर्ष आगे चलकर ‘ब्रज बनाम खड़ीबोली’ तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि ‘हिन्दी बनाम उर्दू’ का भी हो गया।
अपने विश्लेषण में राजीव लिखते हैं “… विडम्बना यह है कि आचार्य शुक्ल भाषा को आधुनिकता का एक मुख्य नियामक मानते हैं लेकिन उस दौर में आधुनिक भाषा को लेकर आंदोलन करने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री को इसका वाजिब श्रेय नहीं देते ! इसकी वजह क्या है? दरअसल, खत्री की बात प्रमुखता से दर्ज करने पर ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में मीर एवं नज़ीर को भी शामिल करना पड़ता क्योंकि लिपि अलग होने के बावजूद मीर, नज़ीर जैसे रचनाकारों की भाषा सहज एवं स्वाभाविक हिन्दी के ज्यादा करीब थी।”
लेखक खत्री की सहज भाषा के माध्यम से जो बात उठा रहे हैं वह उस समय की सच्चाई थी। बहुत-से ऐसे रचनाकार जो हिन्दी को काव्यभाषा बनाने के पक्ष में थे वे भी इसके सहज रूप के पक्षधर नहीं थे। इसीलिए अयोध्या प्रसाद खत्री को न तो उस समय समर्थन मिला न ही आचार्य शुक्ल के बाद के साहित्य-इतिहासकारों, आलोचकों ने इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। “परस्पर : भाषा–साहित्य–आंदोलन” किताब का यह अध्याय अपने चार उपशीर्षकों ‘राधाचरण गोस्वामी और खड़ीबोली पद्य का आंदोलन’, ‘राजा शिवप्रसाद और खड़ीबोली का पद्य’ , ‘बालकृष्ण भट्ट और खड़ीबोली का पद्य आंदोलन’ के सहारे खड़ीबोली को पद्य की भाषा बनाने के विभिन्न पक्षों की सम्यक विवेचना प्रस्तुत करता है। इनके जरिये साहित्य और उससे बाहर के सम्पूर्ण परिवेश के बहस-मुबाहिसे को विस्तारपूर्वक उभारते हुए, हिन्दी क्षेत्र की बोलियों के आपसी संघर्ष, विचार परंपरा आदि के माध्यम से स्वनामधान्य साहित्यिक और गैरसाहित्यिक व्यक्तित्वों को नए सिरे समझने का प्रयास किया है। इससे निश्चित रूप से कुछ मूर्तियाँ टूटती हैं और पाठकों तक जरूरी बातें पूरी प्रामाणिकता के साथ पहुँचती हैं।
राष्ट्र-निर्माण, संविधान-सभा और भाषा-विमर्श
राजीव रंजन गिरि की किताब का एक हिस्सा हिन्दी के उस संघर्ष का किस्सा है जो उसने राजभाषा बनने के लिए किया। यह अध्याय भारत की बहुभाषिकता से उपजी पहली और अबतक की सबसे बड़ी समस्या राजभाषा की समस्या से हमारे देश के शुरुआती नीति निर्माताओं के जूझने का विस्तृत विवेचन है। संविधान सभा की बहसों में देश की भाषा के प्रश्न पर जो बहसें हुईं, सदस्यों ने जो अपनी बातें रखीं और उन सबका जो परिणाम सामने आया उनका गहरा विश्लेषण पुस्तक के इस अध्याय में किया गया है। हिन्दी को बड़े ही गहरे संघर्ष के बाद राजभाषा का दर्जा मिला। बहुभाषी देश में अन्य भाषाओं के बरक्स ही राजभाषा की स्थिति होनी थी और इस पुस्तक में प्रस्तुत संविधान सभा की बहसों को देखकर लगता है कि यह स्थिति आनी ही थी। बोलने वालों की बड़ी संख्या के कारण हिन्दी की स्थिति बहुत मजबूत थी। इसके बरक्स देश का ऐसा एक बड़ा भूगोल था जहाँ की अपनी भाषाओं के पिछड़ जाने का खतरा था। एक लोकतान्त्रिक देश के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति थी। संविधान सभा के सामने देश की एक भाषा हो यह भाषा संबंधी समस्या के रूप में सामने आया। इस समस्या के बहुत-से निहितार्थ थे।
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषाई विविधता के हिसाब से भारत काफी संपन्न और देश के नागरिकों की चेतना के लिए या एक नेमत की तरह है लेकिन इस विविधता से राष्ट्र की एकता प्रभावित होती है। अपने क्षेत्र की भाषाओं का प्रश्न उठाना उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी जरूरी भूमिका थी और इसका निर्वाह उन्होंने बखूबी किया भी। इसके तहत वे यह स्थापित करने में सफल हो गए कि ‘हिन्दी उन पर थोपी जा रही है’ और ‘हिन्दी भाषाई साम्राज्यवाद’ का प्रसार कर रही है। अपनी बोलियों और भाषाओं को लेकर उनके जो तर्क और डर थे उनसे इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन इसने हिन्दी को लेकर एक अलग तरह की घृणा का प्रसार किया जिसने आगे चलकर इस देश की एकमात्र राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्थापना पर लगभग स्थायी ग्रहण लगा दिया।
संविधान सभा ने हिन्दी को अधिकारी भाषा अर्थात राजभाषा का स्थान दिया और यह स्थापना भी दी कि आने वाले पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा होगी। संविधान में भाषाओं की स्थिति को लेकर देश के बहुभाषी चरित्र का ध्यान रखा गया। संविधान सभा में हुई बहसों से यह बात उभरकर आई कि हमारे जैसे बेहद बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश के लिए किसी भी एक भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करना अव्यावहारिक कदम होगा। आज देखें तो यह राष्ट्र के संस्थापकों की परपक्वता लगती है कि उन्होंने कोई राष्ट्रभाषा नहीं घोषित की। लेकिन यह किताब इन बातों का जो गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है उसे देखते हुए यह एक ऐसे फार्मूले को स्वीकार कर लेना लगता है जिसमें ज्यादा विवाद की संभावना नहीं थी। तत्कालीन संविधान सभा की बहसों में हिन्दी को बढ़ावा दिए जाने को एक संवैधानिक दायित्व की जगह भाषाई वर्चस्व के एजेंडे के रूप में पेश किया गया। ऐसा दिखाया गया कि इस तरह की नीति से भारत की विविधता पर खतरा आ जाएगा और यह एक नवनिर्मित देश की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस पुस्तक को पढ़ते हुए यह दिलचस्प बात भी सामने आती है कि हिन्दी का समर्थन करने वाले सदस्य भी अपने भाषणों में इस बात की पूरी संभावना छोड़ रहे थे जो हिन्दी के खिलाफ काम कर रही थी।
इन सब स्थितियों के मद्देनज़र यह अध्याय एक अलग स्थापना करने में सफल रहता है। दक्षिण या भारत के किसी और हिस्से के प्रतिनिधि हिन्दी को अपने ऊपर थोपे जाने और हिन्दी के साम्राज्यवाद की बात करते हैं यह कितना भी तार्किक लगे सही नहीं है। हिन्दी का विरोध करने वाले हिन्दी के बजाय अंग्रेजी के पक्ष में खड़े होते हैं। जबकि अंग्रेजी भी कोई ऐसी भाषा नहीं कि उसे सब बोलते हों या फिर वह ज्यादातर लोगों द्वारा समझी जाती थी। राजीव इस अध्याय में इसे हिन्दी विरोध का सबसे रोचक पहलू मानते हैं। दक्षिण भारत के लोग जिनकी स्वाभाविक भाषा अंग्रेजी नहीं थी वे अंग्रेजी के लिए तो सहमत हो रहे थे लेकिन हिन्दी पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे जो संभव है सही नहीं भी होते। संविधान सभा के सदस्यों का अंग्रेजी प्रेम एक दूसरी स्थिति की ओर इशारा करता है। इसकी जड़ें संविधान सभा के गठन में थीं।
हिन्दी का भारत देश की राष्ट्रभाषा न बनकर आधे-अधूरे तरीके से देश की राजभाषा बनने और उसमें भी अंग्रेजी की उच्चता के बने रहने के पीछे औपनिवेशिक विरासत काम कर रही थी। उस सभा के सदस्य औपनिवेशिक भारत के कुलीन परिवारों में अंग्रेजी में प्रशिक्षण प्राप्त लोग थे जिनके लिए अपने को अंग्रेजी में अभिव्यक्त करना ज्यादा सरल था। इसी वजह ने हिन्दी के खिलाफ काम किया। बहुसंख्यक की भाषा होने के बावजूद यह वर्चस्व की भाषा नहीं थी। राजीव उचित ही लिखते हैं : “राष्ट्रभाषा से राजभाषा तक की यात्रा में न तो हिन्दी समर्थकों की सभी बातें मानी गयीं और न विरोधियों की। असफल हिंदुस्तानी के पक्षधर भी हुए। सफल हुआ, तत्कालीन अंग्रेजीदां तबका। इस वर्ग की कामनाएँ बड़ी हद तक पूरी हो गयीं।”
बीच बहस में लघुपत्रिकाएँ : आंदोलन, संरचना और प्रासंगिकता
इस पुस्तक का तीसरा अध्याय सूचना क्रांति और भूमंडलीकरण के दौर से पहले हिन्दी प्रदेशों में सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण को मजबूत बनाने में महती भूमिका निभाने वाली लघुपत्रिकाओं को समर्पित है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि आजादी के बाद के भारत में हिन्दी भाषाविमर्श में साहित्यिक लघुपत्रिकाओं का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। ये भले ही छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत प्रयासों से अनियमित तौर पर ही छपती रही हों लेकिन इनका उद्देश्य और इनकी मंशा सदैव सरहनीय रहे। यह अध्याय इस बात की स्थापना भी करता है कि छोटे शहरों और कस्बों से प्रकाशित होने वाली इन पत्रिकाओं ने रचनाकारों की एक बड़ी जमात पैदा की जिसने हिन्दी भाषा साहित्य को इसका समृद्ध समकाल देने के साथ-साथ रचनात्मक स्तर पर प्रखरता और मजबूती दी है।
यह पुस्तक बताती है कि लघु पत्रिकाएँ देश की आज़ादी के बाद की बदली हुई परिस्थितियों में साहित्यिक हलचलों और गतिविधियों की संवाहक रहीं। साठ और सत्तर के दशक में इन साहित्यिक पत्रिकाओं के विभिन्न रूपों का पता चलता है वहीं नब्बे के दशक में ये पत्रिकाएँ विभिन्न सांस्कृतिक आंदोलनों के उभार को गति प्रदान करने और उनके सैद्धांतिकरण में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही थीं।
यह अध्याय हिन्दी की लघुपत्रिकाओं की वर्तमान अवस्थिति की सम्यक आलोचना भी करता चलता है। ये पत्रिकाएँ सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक मोर्चों पर आ रहे नवीन बदलावों के साथ सामंजस्य बिठाने में नाकाम रही हैं। लघु पत्रिकाओं के संपादकों के वास्तविक संघर्ष और सच्चे प्रयासों की सीमाएँ भी इस आंदोलन की संरचना में दृष्टिगत हो जाती हैं। यही इनके दायरे को निरंतर सीमित करती जा रही हैं।
राजीव रंजन गिरि की यह पुस्तक ‘परस्पर : भाषा–साहित्य–आंदोलन’ हिन्दी भाषा के सम्यक विमर्श को पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। यह शोधपरक पुस्तक कितने श्रम से तैयार हुई होगी इसका अंदाजा इसके साथ दिए गए परिशिष्ट से हो जाता है जिसमें संदर्भ ग्रन्थों , पत्र-पत्रिकाओं की लंबी सूची है। यह परिशिष्ट हिन्दी भाषा के गंभीर अध्येताओं और भाषा पर शोध करने वालों के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। अक्सर शोधलेखों वाली किताब को लेकर पठनीयता में कमी होने की बात कही जाती है लेकिन यह पुस्तक पठनीयता के लिहाज से भी खरी उतरती है। लेखक ने बड़े ही सरल और सहज तरीके से गंभीर बहसों और मुद्दों को प्रस्तुत किया है। रज़ा पुस्तकमाला के तहत प्रकाशित यह पुस्तक हिन्दी भाषा साहित्य के विकास को देखने की नई दृष्टि देती है।
किताब : परस्पर : भाषा-साहित्य-आंदोलन
लेखक : राजीव रंजन गिरि
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन; दिल्ली
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

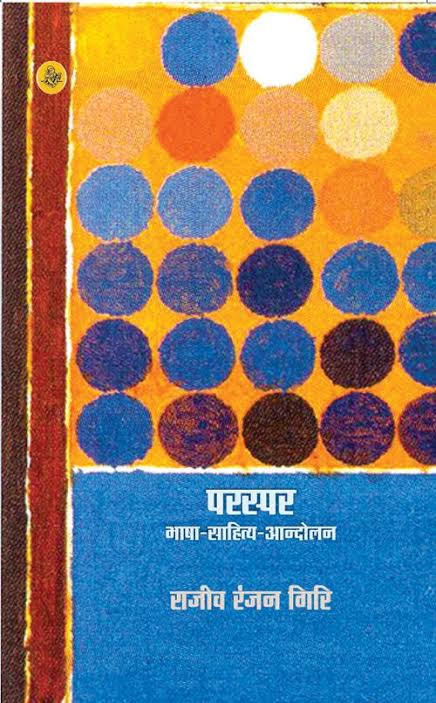


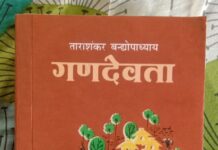













राजीव रंजन गिरि श्रेष्ठ आलोचक हैं! इनके लेखन में अध्येता आलोचक की दृष्टि और प्रामाणिक संदर्भ पाठक को प्रभावित करता है।
राजीव रंजन गिरि जी की पुस्तक ‘परस्पर : भाषा-साहित्य-आंदोलन’ की आलोक रंजन जी द्वारा की गई समीक्षा पठनीय है,जो मूल कृति को पढ़ने का आमंत्रण देती है!
‘परस्पर : भाषा-साहित्य-आंदोलन’ के लेखक और समीक्षक, दोनों के लिए शुभकामनाएँ!
Thanks
बहुत अच्छी टिप्पणी की आलोक रंजन जी ने। बधाई राजीव जी ।