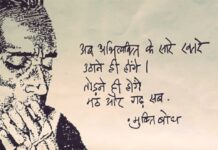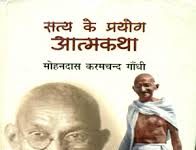— ध्रुव शुक्ल —
1. मतान्धता जीवन को मुश्किल में डाल रही है। संवाद और असहमति का सम्मान घट रहा है। संविधान पर शरीयतों और पुरानी संहिताओं का दबाव बनाया जा रहा है। देश का जीवन अधकचरी आधुनिकता और रूढ़िग्रस्त पुरानेपन में ज़िद बांधकर फंसा है। ऐसी हालत का सामना कैसे किया जाए?
2. बैर और घृणा को बढ़ावा मिल रहा है जिसमें सबकी परवाह किये बिना अपनी-अपनी सत्ता बचाये रखने की बड़ी भूमिका है। प्रेम और सौहार्द का सार्वभौमिक मूल्य घट रहा है। प्रतिनिधि राजनीतिक जन-समर्थन पाकर उसका स्वार्थपूर्ण धंधा कर रहे हैं और देश में फैले मानस रोगों का इलाज नहीं मिल रहा है। यह इलाज कैसे खोजा जाए?
3. पाखण्ड के कई रूप प्रकट हो रहे हैं। वैश्विक चैतन्य और प्रकृति की दार्शनिक समझ का घोर अभाव है। संसद, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और हाट-बाजार में जीने की कोई कला दिखायी नहीं देती। सारे ठिकाने केवल अपनी दुकान चला रहे हैं और लोग भटक रहे हैं। इस भटकन से निजात पाने का रास्ता क्या है?
4. सामाजिक जड़ता का अंधेरा इतना बढ़ रहा है कि जैसे कोई कुछ करने की स्थिति में ही नहीं हो। केवल राजनीतिक अधिकार पा जाना ही काफी नहीं है। कोई भी समाज अपने पांवों पर खड़े रहकर अपने देश के साधनों को बचाये बिना जीवन को साध नहीं सकता। अपनी पराधीनता का सामना ख़ुद कैसे किया जाए?
5. अधिनायक बढ़ रहे हैं। चाहे वे राजनीतिक हों, मज़हबी हों और चाहे अराजकता फैलाने वाले गिरोहों को चलाने वाले लोग हों। आपसी सहमति से लोकहित को साधना कठिन होता जा रहा है और गैरज़रूरी काबिज लोगों के एकतरफ़ा और अविवेकी फैसले पूरे जीवन को घेरते जा रहे हैं। तब आपसी सहमति पर आधारित लोकतंत्र को बचाये रखने का उपाय क्या होगा?
6. राष्ट्रवाद का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा। कोई समझने को तैयार नहीं लगता कि राष्ट्र तो वह होता है जिसमें सभी बहुविश्वासी आबादियां एकसाथ स्वास्थ्य, शिक्षा और समृद्धि के साथ न्यायपूर्ण जीवनयापन कर सकें और उन्हें अपने पीछे छूटते जा रहे उन गांवों की चिंता भी हो, जिनके बिना शहरी आबादियों का पालन-पोषण संभव ही नहीं। यह अवरुद्ध होता जा रहा रास्ता फिर कैसे खोला जाए?
हमें साथ बैठकर इन प्रश्नों पर गहन विचार के साथ कोई व्यावहारिक कार्ययोजना बनाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह इक्कीसवीं सदी हमें चैन से बैठकर सोचने का समय ही नहीं दे रही। कभी-कभी लगता है कि यह सदी तकनीक के बल पर एक ऐसा कर्महीन जीवन रच रही है जिसमें मानवीय कर्मकुशल जीवन की संभावना ही नहीं बचेगी।
ऐसी हालात पर विमर्श और कार्यात्मक उपायों के प्रति जन-जागरण अनिवार्य हो गया है। यह काम कभी-कभार मंच सजाकर भाषण करने से न हो पाएगा। इसके लिए तो बचे हुए घने बरगदों की छाया में नियमित चौपालें लगाकर सबको एक-दूसरे के करीब लाना होगा।

झूठी हैं खबरें अखबार की
अरे झूठी हैं खबरेंअखबार की
धूम मची लूट-मार की
रैयत मंहगाई की मारी
गांव-गांव छायी लाचारी
कीसें कहें बिपत अति भारी
पाग गिर गई है पूरी सरकार की
धूम मची लूट-मार की
घर-बखरी भई दो कौड़ी की
चिंता है मौड़ा-मौड़ी की
जिंदगानी रै गयी थोरी-सी
बात कैसें बनें रुजगार की
धूम मची लूट-मार की
नेता भये स्वारथ की हंडी
भर दई मुस्तंडों सें मंडी
घर-घर जनम लयें पाखंडी
राजनीति है चोर-लबार की
धूम मची लूट-मार की
कोऊ काऊ के काम नें आये
खेवैया खुद नाव डुबाये
परदेसी खों गरे लगाये
करे बातें चुनाव परचार की
धूम मची लूट-मार की
अरे झूठी हैं खबरें अखबार की
धूम मची लूट-मार की
(बुन्देलखण्डी गारी गायन पर आधारित)
—–
रहनुमा पहले भी थे पर बदजुबां तो न थे
पहले इतने इंतज़ाम न थे
बहुत-से किस्से इतने आम न थे
कुछ जज़्बात दिल में दबे रहते थे
कुछ साथ चले जाते थे
इतनी गूॅंगी इबारतें न थीं
इतनी ऊबी इबादतें न थीं
दुश्मनी थी तो दुआ भी थी
इतनी दरिंदगी तो न थी
ग़र्द था ग़ुबार भी थे
हम इतने दरकिनार न थे
दोस्ती इतनी गुमराह न थी
इतनी अकेली किसी की आह न थी
ज़िन्दगी इतनी झुकी-झुकी तो न थी
बंदगी इतनी बुझी-बुझी तो न थी
उम्मीद इतनी तो थी
बेदखल होंगे तो कहीं और चले जाएंगे
कोई हमराह भी मिल जाएंगे
बियाबाॅं इतने पहले तो न थे
दाग़ पहले भी दामन पे लगा करते थे
इतने बदनिशां तो न थे
रहनुमाॅं पहले भी थे
इतने बदगुमाॅं तो न थे
इतने बदज़ुबाॅं तो न थे
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.