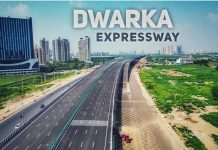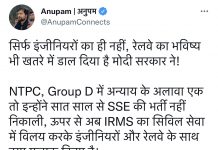— परिचय दास —
विजयदेव नारायण साही हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक और चिंतक थे, जिनकी आलोचना-शैली तर्कपूर्ण, गहराई से विश्लेषणात्मक और मौलिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। अमीर खुसरो पर उनकी असहमतियाँ विशेष रूप से खुसरो के काव्य और व्यक्तित्व को लेकर समकालीन और पारंपरिक दृष्टिकोण के आलोचनात्मक विश्लेषण में दिखाई देती हैं।
साही की असहमतियाँ:
अमीर खुसरो का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण:
पारंपरिक दृष्टिकोण: खुसरो को सूफी परंपरा के महान कवि और भक्त माना जाता है, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया।
साही की आलोचना: साही ने खुसरो की इस छवि को अति-रोमांटिक और अतिरंजित माना। उनके अनुसार, खुसरो का व्यक्तित्व एक तरफ सूफी विचारधारा से प्रेरित था, लेकिन दूसरी ओर उनके लेखन में दरबारी संस्कृति और सत्ता के प्रति झुकाव भी स्पष्ट है। साही ने इसे उनके “लोकप्रिय कवि” होने की छवि के विपरीत माना।
खुसरो और लोक संस्कृति:
पारंपरिक धारणा: खुसरो को लोकभाषा (खड़ीबोली, ब्रज, और अवधी) के प्रवर्तक और लोककाव्य के जनक के रूप में देखा जाता है।
साही का मत: साही ने कहा कि खुसरो का लोककाव्य केवल आंशिक रूप से लोकसंस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। खुसरो का काव्य आम जनता की बजाय शाही दरबार और विशिष्ट वर्ग के लिए अधिक था। उनका “लोक” से जुड़ाव सतही और सांस्कृतिक प्रयोग मात्र था।
अमीर खुसरो का काव्यगत योगदान:
साही ने खुसरो की कविता में विचार और गहराई की कमी बताई। उनके अनुसार, खुसरो की रचनाएँ शैली और शिल्प में तो उत्कृष्ट हैं, लेकिन वे गहन मानवीय समस्याओं और उनके समाधान पर केंद्रित नहीं हैं। खुसरो का काव्य अधिकतर मनोरंजन और दरबारी संस्कृति की सेवा के लिए है।
उन्होंने खुसरो की पहेलियों, मुकरियों, और दोहे को रचनात्मकता का उत्कृष्ट नमूना माना, लेकिन इसे साहित्यिक गहराई से वंचित भी बताया।
दरबारी कवि के रूप में खुसरो:
साही ने खुसरो के दरबारी कवि होने के पहलू पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, खुसरो सत्ता और दरबार के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे, जिससे उनका काव्य स्वायत्तता और स्वतंत्रता खो बैठा। साही ने इसे खुसरो के सूफी व्यक्तित्व के साथ एक विरोधाभास बताया।
खुसरो की बहुभाषिकता:
पारंपरिक दृष्टिकोण: खुसरो को बहुभाषिक साहित्य के प्रतिनिधि के रूप में आदर्श माना गया है।
साही का मत: उन्होंने कहा कि खुसरो की बहुभाषिकता उनकी प्रतिभा का प्रमाण तो है, लेकिन यह उस समय के सांस्कृतिक संदर्भों का दबाव भी था। खुसरो की भाषाओं का चयन अधिकतर राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता के कारण था, न कि केवल साहित्यिक उद्देश्य से।
विजयदेव नारायण साही ने अमीर खुसरो की आलोचना में उन्हें नकारने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का पुनर्मूल्यांकन किया। उन्होंने खुसरो को उनकी सीमाओं के साथ देखने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि खुसरो को उनके यथार्थ और संदर्भ में समझा जाए, न कि केवल आदर्शीकृत दृष्टिकोण से।
साही के ये तर्क खुसरो के काव्य और उनकी सांस्कृतिक भूमिका को नए सिरे से देखने का दृष्टिकोण देते हैं, जो साहित्य और संस्कृति के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करते हैं।
विजयदेव नारायण साही ने अमीर खुसरो के साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर गहन आलोचना की है, जिसमें धर्म और कट्टरता से संबंधित पहलू पर भी उनकी असहमतियाँ शामिल हैं। खुसरो को पारंपरिक रूप से धार्मिक सहिष्णुता, सूफी परंपरा, और हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन साही ने इस छवि पर कई सवाल उठाए।
साही की असहमति:
धार्मिक सहिष्णुता का आदर्शीकृत स्वरूप:
पारंपरिक दृष्टिकोण: खुसरो को धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना गया है। उन्हें हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
साही का मत: साही ने इस धारणा को आंशिक और सतही बताया। उनके अनुसार, खुसरो का धार्मिक दृष्टिकोण उनके सूफी जुड़ाव और दरबारी जीवन के दबाव के बीच संतुलन का प्रयास था। यह सहिष्णुता किसी गहन दार्शनिक समझ की बजाय राजनैतिक और सांस्कृतिक अनुकूलन का परिणाम थी।
खुसरो और इस्लामिक कट्टरता:
पारंपरिक धारणा: खुसरो को कट्टरपंथ से परे एक समावेशी कवि माना जाता है।
साही की आलोचना: साही ने कहा कि खुसरो के लेखन में इस्लामी सत्ता और उनके धार्मिक झुकाव के स्पष्ट प्रमाण हैं। खुसरो अपने संरक्षक सुल्तानों की कट्टर इस्लामी नीतियों का प्रतिरोध नहीं करते। उनके कुछ लेखन, जैसे फारसी में लिखी गई शाही प्रशस्तियाँ, कट्टर इस्लामी सत्ता के प्रति उनका झुकाव दिखाती हैं।
साही ने यह भी तर्क दिया कि खुसरो की सहिष्णुता व्यक्तिपरक थी, जबकि उनके संरक्षक सुल्तानों की नीतियाँ कट्टर और एकांगी थीं। खुसरो ने इन नीतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि नहीं डाली।
धर्म के प्रति खुसरो का यथार्थवादी दृष्टिकोण:
साही का दृष्टिकोण: साही के अनुसार, खुसरो का धर्म के प्रति दृष्टिकोण व्यावहारिक था, न कि आदर्शवादी। उन्होंने धर्म को सत्ता और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का साधन माना।
साही ने खुसरो की रचनाओं में धार्मिक तत्वों की चर्चा को अधिकतर सांस्कृतिक दिखावे और दरबारी राजनीति का हिस्सा बताया। उनके अनुसार, खुसरो ने धर्म का उपयोग सामूहिक पहचान और सत्ता के प्रति निष्ठा को मजबूत करने के लिए किया।
हिंदू-मुस्लिम संस्कृति का मेल:
पारंपरिक दृष्टिकोण: खुसरो को भारतीय संगीत, भाषा, और काव्य में हिंदू-मुस्लिम संस्कृति के सम्मिलन का प्रतिनिधि माना गया है।
साही का तर्क: साही ने कहा कि खुसरो की यह भूमिका केवल सांस्कृतिक अनुकूलन थी, न कि सच्ची धार्मिक या सांप्रदायिक एकता। उनके अनुसार, खुसरो ने दरबारी आवश्यकताओं के तहत संस्कृतियों को जोड़ा, लेकिन उनकी रचनाओं में धार्मिक आत्मालोचना या कट्टरता के प्रतिरोध का अभाव है।
सूफीवाद और धार्मिक सहिष्णुता:
पारंपरिक दृष्टिकोण: खुसरो को सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य के रूप में धार्मिक सहिष्णुता का आदर्श माना गया है।
साही की असहमति: साही ने कहा कि खुसरो का सूफीवाद भी उनके दरबारी व्यक्तित्व से प्रभावित था। उन्होंने सूफी विचारधारा को गहराई से आत्मसात करने की बजाय उसे सांस्कृतिक प्रभाव और लोकप्रियता के लिए प्रयोग किया।
विजयदेव नारायण साही के अनुसार, अमीर खुसरो की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समावेशिता को अतिरंजित रूप से महिमामंडित किया गया है। खुसरो का दृष्टिकोण अधिकतर दरबारी आवश्यकताओं और सत्ता के प्रति वफादारी से प्रेरित था। साही ने इस बात पर जोर दिया कि खुसरो को उनके यथार्थवादी संदर्भ और सीमाओं के भीतर देखा जाना चाहिए, न कि केवल आदर्शीकृत छवि के रूप में।
यह दृष्टिकोण खुसरो की ऐतिहासिक और साहित्यिक भूमिका को समझने में एक नया और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.