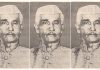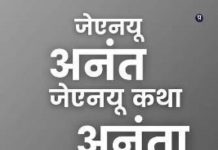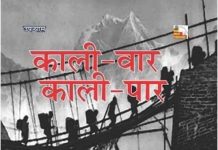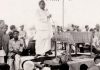अष्टावक्र की परंपरा में भारतीय विचार सागर में दो ऐसे जाजल्वमान सन्त हुए हैं जिन्होने गुरूडम को न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी खारिज किया। कृष्णमूर्ति का कथन है कि – ” सत्य का कोई मार्ग नही होता, सत्य तक पंहुचने के अनेक रास्ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना रास्ता स्वंय चुनना है, सत्य गतिशील होता है। यदि वह स्थिर रहता तो किसी मार्ग से उस तक पंहुचा जा सकता था किन्तु चूंकि वह गतिमान है, अतः कोई मंत्र, कोई गुरू, मुमुक्षु को सत्य तक नही पंहुचा सकता है। ” कृष्णमूर्ति ने कोई शिष्य नही बनाया।
स्वामी सहजानन्द के साथ भी, राहुल सांकृत्यायन, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, यदुनंदन शर्मा, सुभाषचंद्र बोस, मुजफ्फर अहमद, राजेश्वर राव जैसे बडे नामचिन लोगो ने काम किया परन्तु स्वामी सहजानंद ने उनके साथ सहयोगी का व्यवहार किया। राहुल सांकृत्यायन से स्वामी जी की अत्यन्त घनिष्ठता रही। 20 अप्रैल सन 1940 को सुभाषचंद्र बोस ने ” फारवर्ड ” पत्रिका मे अग्रलेख लिखकर स्वामी जी को अपना गुरू माना, यह उनका बडप्पन था। सन 1929 – 1939 तक जयप्रकाश स्वामी जी के साथ किसान सभा में काम किए । सन 1941 ई. के डुमराव अधिवेशन से दोनो एक-दूसरे से सदा के लिए अलग हो गए । जयप्रकाश नारायण ने अपनी अलग किसान सभा बनाई जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र देव और उपाध्यक्ष रामवृक्ष बेनीपुरी थे। जयप्रकाश नारायण ने सन 1975 ई. के पटना सभा मे स्वामी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि – ” राजनीति के आरम्भिक दौर में स्वामी जी हमलोगों के गुरू थे। ”
कृष्णमूर्ति और स्वामी सहजानंद में गुरूडम के विरोध पर सहमति थी परन्तु उनकी सोच में वैभिन्य भी था। कृष्णमूर्ति, अष्टावक्र की तरह यह विश्वास करते थे कि जीव सदा सर्वदा मुक्त रहता है, वह क्रिया कांड के बंधनो में स्वंय को बाध लेता है । स्वतंत्रता सदा आरंभ मे होती है न कि अंत में । कृष्णमूर्ति का विश्वास था कि यदि प्रेम को अस्तित्व में आना है तो बौद्धिकता को विसर्जित होना पड़ेगा। सत्य को बुद्धि द्वारा अनुकरण के माध्यम से जानना, समझना एक तरह की मूर्ति पूजा है। हम सत्य को तभी पा सकते हैं जब स्व की समस्त संरचना को तिलांजलि दे देते हैं।
स्वामी सहजानंद अस्मिता की तलाश स्वयं के अस्तित्व में करते हैं परन्तु वे इसे आशिक तौर पर ही स्वीकार करते हैं। वे व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के अधीन थोडे-बहुत अपवाद के साथ रखना चाहते हैं। इसीलिए वे संगठन में विश्वास करते हैं, परन्तु पार्टियों की पंडागिरी उन्हे नापसंद है। संगठन के साथ पूर्ण रूप से कार्यरत रहते हुए कुछ अंश मे वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के भी पक्षधर हैं। स्वामी जी हृदय और मस्तिष्क, श्रद्धा और तर्क, दिल और दिमाग दोनो को अधूरा मानते हैं। वे श्रद्धा पर बुद्धि का और बुद्धि पर श्रद्धा का पहरा चाहते हैं ताकि दोनो एक दूसरे के अभाव को पूर्ण कर सके। महज हृदय पर विश्वास करना पोंगापंथ को बढावा दे सकता है तथा बुद्धि पर विश्वास करना बेलगाम हो सकता है।
स्वामी जी के इस वैचारिकी से वेदान्ती जो सिर्फ हृदय पर विश्वास करना जानते थे और मार्क्सवादी जो हृदय को अनसुना कर सिर्फ तर्क के भरोसे अपनी नैया पार लगाना चाहते थे, दोनो नाराज हो गए और स्वामी जी के विचारो को चुप्पी के द्वारा अभी तक अंधकार में रखे हुए हैं।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.