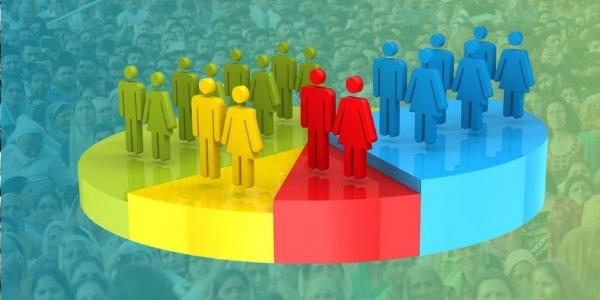– परिचय दास —
।। एक ।।
जातीय जनगणना, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय सामाजिक संरचना के भीतर एक गूढ़ और बहुस्तरीय विमर्श का द्वार खोलती है। यह विमर्श मात्र आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों की परतें भी उजागर होती हैं। भारत की सामाजिक बनावट में जाति एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सच्चाई है, जो आज भी जीवन के अनेक स्तरों को प्रभावित करती है। यद्यपि भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्श स्थापित किए किंतु यथार्थ में सामाजिक समता अब भी एक अधूरी परियोजना बनी हुई है। जातीय जनगणना इस असमानता की पारदर्शी पड़ताल करने का उपकरण बन सकती है।
राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने का सबसे प्रमुख निहितार्थ यह है कि इससे देश में जाति आधारित संरचनाओं की सही स्थिति सामने लाई जा सकती है। जाति की वर्तमान संख्या, जातिगत समूहों का प्रतिशत, उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि स्वामित्व, रोजगार आदि से संबंधित आँकड़े सामने आने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि अब तक जिन वर्गों को ‘पिछड़ा’, ‘अति पिछड़ा’, ‘दलित’ या ‘आदिवासी’ कहा जाता रहा है, उनकी यथास्थिति क्या है और उन पर सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है। यह आंकड़े न केवल नीति निर्माण को वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाएँगे, बल्कि सामाजिक न्याय की परियोजना को और अधिक धार देंगे।
जातीय जनगणना के आलोचक अकसर यह तर्क देते हैं कि जाति को पुनः सार्वजनिक विमर्श में लाकर हम समाज को और अधिक विभाजित कर देंगे किन्तु जब तक जातिगत असमानताएँ यथार्थ में मौजूद हैं तब तक उनका दस्तावेज़ीकरण ही उन पर नीति-आधारित हस्तक्षेप का आधार बन सकता है। इससे न केवल वंचित तबकों को उचित प्रतिनिधित्व और संसाधनों में हिस्सेदारी मिल सकेगी बल्कि एक उत्तरदायी और जवाबदेह लोकतंत्र की संकल्पना भी साकार होगी।
वर्तमान समय में भारत के अनेक राज्यों में, विशेषकर बिहार में, जातीय जनगणना का एक सफल प्रयोग देखा गया है। इसने यह सिद्ध किया कि जनसंख्या के भीतर कौन-कौन से सामाजिक समूह किस अनुपात में हैं और किन वर्गों को सरकारी योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति केवल क्षेत्रीय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होती है। जब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर समूचे भारत की जातीय स्थिति को नहीं जानते, तब तक सामाजिक न्याय की योजनाएँ एक तरह की अंधी राजनीति ही रह जाएँगी। आंकड़ों की पारदर्शिता ही न्यायसंगत आरक्षण, समावेशी विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की पूर्वशर्त है।
जातीय जनगणना का आर्थिक पक्ष भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। जब हम यह जानते हैं कि किस जाति या समुदाय के पास कितनी भूमि है, किसके पास कितनी शिक्षा है और किस वर्ग की आमदनी किन स्तरों पर है, तब ही सरकारें सही तरीके से बजट वितरण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास योजनाएँ बना सकती हैं। इससे यह भ्रांति भी समाप्त होगी कि आरक्षण या अन्य सकारात्मक भेदभाव की नीतियाँ बिना तथ्य के चलाई जा रही हैं। आंकड़ों पर आधारित योजनाओं से न केवल नीति निर्माण में वैज्ञानिकता आएगी बल्कि उसमें नैतिक वैधता भी जुड़ जाएगी।
भारत में जाति कोई केवल धार्मिक या सामाजिक संकल्पना नहीं है; वह एक आर्थिक श्रेणी भी है। अधिकांश जातियाँ परंपरागत पेशों और संसाधन संपन्नता के हिसाब से बनी थीं, और अब भी उनमें वही प्रवृत्तियाँ दिखती हैं। उच्च जातियाँ अधिकतर संसाधन-संपन्न हैं, जबकि निम्न जातियाँ अब भी रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। राष्ट्रीय जातीय जनगणना इस आर्थिक विषमता का वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत कर सकती है। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन से समुदाय आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी समान अवसरों से कोसों दूर हैं और किसे किन स्तरों पर कितनी सहायता की ज़रूरत है।
राजनीतिक दृष्टि से भी जातीय जनगणना के गहरे निहितार्थ हैं। भारत में राजनीति और जाति का संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ रहा है। किंतु जातीय जनगणना इस संबंध को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। जब यह पता चलेगा कि किसी जाति या समुदाय की जनसंख्या कितनी है, और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि कितने हैं, तब प्रतिनिधित्व की वास्तविकता सामने आएगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या लोकतंत्र वास्तव में समावेशी बना है, या उसमें कुछ वर्गों का ही प्रभुत्व बना हुआ है।
जातीय जनगणना न केवल सामाजिक न्याय की योजनाओं को समुचित आधार देती है, बल्कि वह नागरिकों को यह अधिकार भी देती है कि वे यह जान सकें कि उनके समुदाय की स्थिति क्या है, और राज्य उनके लिए क्या कर रहा है। यह एक उत्तरदायी लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है। आंकड़ों की गैरमौजूदगी में हम केवल नारे और अनुमान के सहारे नीतियाँ बनाते हैं, जो अक्सर केवल राजनीतिक स्वार्थ का साधन बन जाती हैं। जातीय जनगणना से नीतिगत विमर्श का आधार मजबूत होता है, और उसमें लोकहित की प्रामाणिकता बढ़ती है।
इसका एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि जातीय जनगणना भारतीय समाज की बहुलता और विविधता को आंकड़ों के स्तर पर रेखांकित करती है। जब हम यह जान पाएँगे कि भारत में कितनी जातियाँ हैं, उनके उपवर्ग कौन-कौन से हैं, और उनका वितरण किस प्रकार का है, तब हम भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को एक सम्यक् परिप्रेक्ष्य में देख पाएँगे। इससे न केवल सामाजिक विज्ञानों के शोधों को बल मिलेगा, बल्कि यह इतिहास, नृविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों में नई दृष्टियों का मार्ग प्रशस्त करेगा।
हालाँकि जातीय जनगणना के समक्ष कुछ व्यावहारिक और वैचारिक चुनौतियाँ भी हैं। जैसे कि जातियों की परिभाषा, उनकी बदलती पहचान, उपजातियों की स्थिति, और स्वघोषणा के आधार पर पहचान की प्रामाणिकता किंतु ये सभी चुनौतियाँ किसी भी बड़े सामाजिक-सांख्यिकीय अभियान का हिस्सा होती हैं, जिन्हें सही प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और प्रशासनिक सतर्कता से हल किया जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक समर्थन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक हैं।
जातीय जनगणना को केवल राजनीतिक लाभ या नुकसान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह सामाजिक विषमता के सत्य को स्वीकार करने और उसे बदलने की एक नैतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इससे प्राप्त आंकड़े भारत को एक अधिक समावेशी, समानतामूलक और लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदलने की प्रक्रिया को गति देंगे। आज जब दुनिया भर में डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक असमानताएँ गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, जातीय जनगणना एक आवश्यक और अनिवार्य कदम बन जाती है।
।। दो ।।
जातीय जनगणना की आवश्यकता को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम जाति और आंकड़ों के अंतःसंबंध को इतिहास की दृष्टि से देखें। 1931 की जनगणना आखिरी बार थी, जब भारत में जातियों का विस्तृत विवरण दर्ज किया गया था। स्वतंत्र भारत में यह अभ्यास समाप्त कर दिया गया, यह मानते हुए कि जाति आधारित गणना सामाजिक समरसता के विरुद्ध है। परंतु इस निर्णय के पीछे जो आदर्श थे, वे धरातल पर कभी भी समाज को एकरस या समतामूलक नहीं बना सके। इसके उलट, जाति की अनुपस्थिति ने उन असमानताओं को अदृश्य बना दिया, जिन पर आधारित समाज की संपूर्ण संरचना खड़ी थी। ऐसे में जातीय आंकड़ों की अनुपलब्धता अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की निगरानी को कठिन बना देती है।
जातीय जनगणना का एक गहरा लोकतांत्रिक पहलू यह है कि यह समाज के हाशिये पर खड़े व्यक्ति की पहचान को वैधता देता है। जब एक व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि उसकी सामाजिक स्थिति, उसके समुदाय की कठिनाइयाँ और उसके संघर्ष राज्य की निगरानी में हैं तो उसमें लोकतांत्रिक विश्वास गहराता है। यह विश्वास एक निष्क्रिय नागरिकता को सक्रिय नागरिकता में रूपांतरित कर सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए जातीय जनगणना उनका अस्तित्व दर्ज कराने का माध्यम बन सकती है।
सामाजिक न्याय का आधार मात्र प्रतिनिधित्व नहीं होता बल्कि उस प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और अधिकार भी उसमें निहित होते हैं। यदि किसी समुदाय की जनसंख्या पर्याप्त है लेकिन उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नगण्य है और आर्थिक-सामाजिक स्थिति बदहाल है, तो यह लोकतंत्र की विफलता मानी जाएगी। इस विफलता की पहचान केवल आंकड़ों से ही संभव है जो जातीय जनगणना से उपलब्ध हो सकते हैं। इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आरक्षण और अन्य नीतियाँ कितनी प्रभावशाली रही हैं और किन समूहों को अब भी विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।
जातीय जनगणना सामाजिक नीति के उन पहलुओं को भी स्पष्ट करती है जो अब तक अस्पष्ट या अनुपस्थित रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, शहरीकरण, तकनीकी शिक्षा, सरकारी नौकरियों और उद्यमिता में विभिन्न जातीय समूहों की भागीदारी का तुलनात्मक अध्ययन केवल तब संभव होगा जब हमारे पास जाति आधारित समग्र आंकड़े हों। इससे यह देखा जा सकता है कि कौन-से समूह तेजी से सामाजिक गतिशीलता की ओर बढ़ रहे हैं और कौन-से अब भी जड़ता में फँसे हुए हैं। इससे सामाजिक नीति में प्राथमिकता निर्धारण अधिक सटीक और कारगर हो सकेगा।
जातीय जनगणना से संबंधित एक बड़ा विमर्श यह भी है कि इससे ‘अतिपिछड़े’ और ‘अत्यंत वंचित’ समुदायों की पहचान सरल होगी। अभी तक आरक्षण नीतियाँ अपेक्षाकृत व्यापक वर्गों के लिए लागू हैं, जिनमें भीतर ही भीतर असमानताएँ हैं। जैसे ओबीसी वर्ग एक समरूप इकाई नहीं है—उसमें कुर्मी, यादव जैसे सामाजिक रूप से मजबूत समूह हैं तो मुसहर, बिंद, नाई, तेली, लोहार जैसे समूह भी हैं जो अभावग्रस्त हैं। बिना आंकड़ों के हम यह भेद नहीं समझ सकते। जातीय जनगणना यह स्पष्ट करने में मदद करेगी कि कौन-से समूह नीतियों का लाभ उठा पा रहे हैं और कौन-से नहीं। इससे आरक्षण की आंतरिक पुनर्संरचना की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
जातीय जनगणना का संबंध केवल सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों तक सीमित नहीं है। यह सांस्कृतिक आत्मबोध की पुनर्परिभाषा का भी अवसर बन सकती है। लंबे समय तक जातियों की पहचान केवल उनके परंपरागत पेशों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी रही किंतु आधुनिक संदर्भों में जातियों का सांस्कृतिक स्वरूप परिवर्तित हो रहा है—शिक्षा, भाषिक पहचान, भोजन, वेशभूषा और विवाह संबंधों में व्यापक बदलाव आ रहे हैं। जातीय जनगणना इस सांस्कृतिक रूपांतरण को दर्ज करने का भी एक उपकरण बन सकती है। इससे यह समझना संभव होगा कि सामाजिक परिवर्तन किस गति और दिशा में हो रहा है और उसमें कौन-से वर्ग आगे या पीछे हैं।
इसके अतिरिक्त, भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से जाति एक चुनावी औजार बन चुकी है, उसमें जातीय जनगणना का प्रयोग एक औचित्यपूर्ण और पारदर्शी विमर्श खड़ा कर सकता है। अभी तक जाति केवल चुनावी जातिनामा बनकर रह गई है, जहाँ नेता अपने प्रत्याशी की जाति से लेकर मतदाताओं की जाति तक की गणना ‘अनधिकारिक’ तौर पर करते हैं। यह गणना बिना किसी वैज्ञानिक आधार के केवल चुनावी हितों के लिए की जाती है। जबकि जातीय जनगणना इसे एक आधिकारिक स्वरूप दे सकती है, जो आंकड़ों के सहारे राजनीतिक निर्णयों की विवेकशीलता को मजबूती प्रदान करेगा।
जातीय जनगणना को लेकर जो भय और आशंकाएँ हैं, वे प्रायः यह मानकर खड़ी की जाती हैं कि इससे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यह विभाजन वास्तविक नहीं बल्कि केवल दृष्टिगत है। यथार्थ यह है कि सामाजिक विभाजन पहले से मौजूद हैं—केवल वे दस्तावेज़ीकृत नहीं हैं। जातीय जनगणना का काम इस अदृश्य असमानता को दृश्य में लाना है। इससे समाज को आत्मावलोकन का अवसर मिलेगा और यह समीक्षा की जा सकेगी कि देश की सामाजिक परियोजनाएँ कितनी सफल रही हैं।
सांख्यिकी और नीति निर्माण का संबंध अंतर्संबंधी है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ भिन्न सामाजिक वर्ग, आर्थिक स्तर और भौगोलिक स्थिति वाले समुदाय रहते हैं, वहाँ एकरूप नीतियाँ अक्सर प्रभावहीन होती हैं। जातीय जनगणना क्षेत्रीय विषमताओं को भी समझने में मदद करेगी। जैसे उत्तर भारत की जातीय संरचना दक्षिण भारत से भिन्न है, और वहाँ के सामाजिक आंदोलन भी। इन क्षेत्रीय अंतरों की समझ के बिना नीति निर्माण में न्याय और सटीकता संभव नहीं है। राष्ट्रीय जातीय जनगणना एक ऐसा उपकरण है जो क्षेत्रीय, वर्गीय और जातीय आंकड़ों के समेकन के माध्यम से समावेशी नीतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
बाजार की भाषा में कहें तो जातीय जनगणना सामाजिक डाटा की वह विस्तृत रिपोर्ट है जो उपभोक्ता (नागरिक) और प्रदाता (राज्य) के संबंध को अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाती है। इससे यह भी ज्ञात होगा कि किन जातीय समुदायों का कितना उपभोग है, किसके पास बाजार तक पहुँच है और कौन-से वर्ग इसके बाहर हैं। इससे सामाजिक-आर्थिक सुधारों को लक्ष्यबद्ध करना आसान होगा। निजी क्षेत्र की कंपनियाँ भी इस डाटा का उपयोग सामाजिक दायित्व (CSR) योजनाओं के निर्धारण में कर सकती हैं।
जातीय जनगणना उस अस्मिता की पुनर्व्याख्या का भी औजार है जिसे भारतीय लोकतंत्र ने कभी ‘तिरस्कार’, ‘अनदेखी’ और ‘बदनाम’ श्रेणियों में डाल दिया था। यह उन समुदायों के लिए आत्मगौरव का स्रोत बन सकती है जिन्हें अब तक ‘सिर्फ जाति’ कहकर हाशिये पर रखा गया। यह जनगणना उन्हें ‘सिर्फ आंकड़ा’ नहीं बल्कि ‘राज्य की दृष्टि में मान्यता प्राप्त इकाई’ बना सकती है। यही इसकी सबसे बड़ी नैतिक विजय होगी—कि जाति को मिटाने के पहले उसे पूरी तरह से समझा जाए, स्वीकार किया जाए और उसके आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाए।
।। तीन ।।
जातीय जनगणना की संकल्पना जब राज्य की नीतिगत मशीनरी में प्रवेश करती है तब यह एक मात्र सांख्यिकी उपकरण नहीं रह जाती बल्कि एक विमर्श बन जाती है—एक ऐसा विमर्श, जो समाज की जटिल परतों को उद् घाटित करता है, उसकी परछाइयों तक पहुँचता है और उस आलोक की माँग करता है जो अब तक केवल कुछ वर्गों तक सीमित थी। यह विमर्श उन सूक्ष्म विभाजनों को उघाड़ता है जो भारतीय समाज की चेतना में गहराई तक समाए हुए हैं—जहाँ ‘नाम’ मात्र सामाजिक स्थिति का पर्याय बन जाता है और ‘उपस्थिति’ एक वर्ग विशेष की ही नियति बनकर रह जाती है।
भारत में जाति एक सांस्कृतिक संयोग नहीं बल्कि ऐतिहासिक रणनीति रही है—एक ऐसी संरचना जिसमें सामाजिक श्रम का वर्गीकरण नहीं, बल्कि श्रमिकों का मूल्यांकन और तिरस्कार निहित रहा है। जातीय जनगणना इस दीर्घकालिक चुप्पी को तोड़ती है—यह न केवल सामाजिक मानचित्र को अद्यतन करती है बल्कि यह भी बताती है कि किस श्रेणी को इतिहास में किस प्रकार का स्थान मिला, किसे किनारे कर दिया गया और किसे व्यवस्था के केंद्र में स्थापित कर दिया गया। जब कोई समुदाय यह कहता है कि वह संख्या में अधिक है पर व्यवस्था में नगण्य, तो वह संख्या की राजनीति नहीं कर रहा बल्कि प्रतिनिधित्व की माँग कर रहा है।
वर्तमान भारत में, जहाँ लोकतंत्र बहुसंख्यक आकांक्षाओं के प्रबंधन की प्रणाली है, वहाँ जातीय जनगणना इन आकांक्षाओं को तर्क और तथ्य का धरातल देती है। यह बताती है कि लोकतंत्र की आत्मा केवल मतदान में नहीं, बल्कि उस मतदान के पीछे छिपी सामाजिक अवस्थिति की समझ में है। जातीय जनगणना यह स्पष्ट करती है कि ‘वोट देने का अधिकार’ और ‘राजनीति में उपस्थित रहने का अवसर’ दो अलग-अलग बातें हैं। यह उस खाई को भरने का यत्न है जो दिखने में अदृश्य है लेकिन सामाजिक अनुभवों में तीव्र है।
जातीय जनगणना का एक अघोषित कार्य यह भी होता है कि यह राष्ट्रीयता के विचार को विस्तृत करती है। जब देश की विभिन्न जातियों, समुदायों और उपजातियों का यथार्थ दस्तावेज़ित होता है, तब ‘राष्ट्र’ कोई अमूर्त, निर्गुण सत्ता नहीं रह जाता बल्कि वह बहुरंगी, बहुस्तरीय और बहुजनमुखी इकाई बन जाता है। इसका यह भी अर्थ है कि राष्ट्र अब केवल ‘एकता’ के बिंब से परिभाषित नहीं होगा बल्कि ‘विविधता की गहराई’ के माध्यम से भी पहचाना जाएगा। इस प्रकार जातीय जनगणना राष्ट्रीय चेतना को समरसता से नहीं, समावेशिता से जोड़ने का कार्य करती है।
आर्थिक नीति-निर्माण के क्षेत्र में भी जातीय जनगणना क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावनाएँ रखती है। अभी तक हमारी योजनाएँ वर्ग आधारित गरीबी-रेखाओं, ग्रामीण-शहरी विभाजनों और क्षेत्रीय असंतुलनों को ध्यान में रखकर बनती रही हैं परंतु जातीय आंकड़े यह दिखा सकते हैं कि एक ही आर्थिक श्रेणी में भी जातीय विविधता किस प्रकार भिन्न प्रकार के वंचनाओं को जन्म देती है। उदाहरणतः एक दलित श्रमिक और एक ओबीसी श्रमिक, भले ही एक समान आय-वर्ग में हों परंतु उनकी सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा तक पहुँच, आवास की गुणवत्ता, और पुलिस-प्रशासन से अनुभव—इन सभी में भिन्नता हो सकती है। ऐसी बारीकियाँ योजनाओं को अधिक संवेदनशील और लक्षित बना सकती हैं।
यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि जातीय जनगणना केवल पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है—बल्कि सवर्ण समाज के भीतर की विविधताओं को भी समझने का माध्यम है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ जैसे समूहों को एकरूप मानना उनके अंदर मौजूद आर्थिक-सामाजिक असमानताओं की अनदेखी करना है। जातीय जनगणना उन जातियों के अंदर के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को भी प्रकाश में लाएगी जो अब तक अपने समूह की सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण नीति-निर्माण से उपेक्षित रहे हैं। इससे समाज में यह बोध भी पनपेगा कि ‘सामाजिक सम्मान’ और ‘आर्थिक यथार्थ’ दो भिन्न धाराएँ हैं और दोनों के लिए अलग हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
जातीय जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वर्चस्व की संरचनाओं को सार्वजनिक करती है। यह स्पष्ट कर देती है कि किन जातियों के पास शैक्षिक संस्थानों का नेतृत्व है, किनके पास न्यायपालिका, प्रशासन, मीडिया और कॉरपोरेट जगत की भागीदारी है। जब यह ज्ञात होगा कि देश की सर्वोच्च संस्थाओं में चंद जातियाँ ही बार-बार प्रतिनिधित्व पा रही हैं तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ वास्तव में समावेशी हैं या केवल दिखावटी? इससे नीति-निर्माताओं पर यह नैतिक दबाव पड़ेगा कि वे ‘सार्थक प्रतिनिधित्व’ की अवधारणा को स्वीकारें।
जातीय जनगणना एक प्रतीकात्मक क्रांति भी है। यह सत्ता को यह याद दिलाने का यंत्र है कि वह ‘न्याय’ केवल भाषणों में नहीं, आँकड़ों के आधार पर भी स्थापित करे। यह जनगणना न केवल आंकड़ों की माँग करती है बल्कि राज्य से यह अपेक्षा करती है कि वह उन आंकड़ों के आलोक में निर्णय करे। जब सामाजिक सत्य सामने होगा, तब उसे नकारना कठिन होगा और यही वह क्षण होगा जब भारत अपने ‘लोकतंत्र’ को मात्र एक प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवनदृष्टि के रूप में देखने लगेगा।
कुछ आलोचकों का कहना है कि जातीय जनगणना से ‘जाति’ का बोलबाला और बढ़ेगा, सामाजिक एकता को क्षति पहुँचेगी और इससे नई तरह की राजनैतिक माँगें जन्म लेंगी परंतु यह तर्क उस दृष्टिकोण से आता है जो जाति को केवल समस्या मानता है, समाधान नहीं। यथार्थ यह है कि जाति तब तक मिट नहीं सकती, जब तक उसे न्याय से गुज़ारकर समता में रूपांतरित न किया जाए। जातीय जनगणना इस प्रक्रिया की शुरुआत है। यह जातियों को केवल गिनने का काम नहीं करती बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के विमर्श में उपस्थित करती है।
एक दिलचस्प आयाम यह भी है कि जातीय जनगणना भाषा, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं को भी उजागर करती है। जब कोई जनगणना अपने उत्तरदाता से उसकी जाति पूछती है, तो वह व्यक्ति अपने इतिहास से जुड़ता है। उसे यह अवसर मिलता है कि वह स्वयं को पहचान सके—न केवल एक श्रेणी के रूप में बल्कि एक जीवित सामाजिक इकाई के रूप में। यही वह क्षण होता है, जब व्यक्ति ‘गणना’ का विषय नहीं, बल्कि इतिहास का भाग बनता है।
राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना एक तरह से भारत की आत्मा की पुनर्परिभाषा है। यह उसे उसकी परंपराओं, विडंबनाओं और संभावनाओं के साथ जोड़ती है। यह एक राष्ट्र को कहती है कि उसे अपने नागरिकों को न केवल अधिकार देना है, बल्कि उन्हें ‘देखना’ भी है—उनकी उपस्थिति, उनकी जाति, उनके कष्ट और उनकी आकांक्षाओं को ‘दर्ज करना’ है। जब तक यह दर्ज नहीं होता, तब तक ‘राष्ट्रीय एकता’ केवल एक अधूरी कल्पना बनी रहती है।
जातीय जनगणना न केवल एक प्रशासनिक अभ्यास है, न केवल एक आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रिया—बल्कि यह भारत के लोकतंत्र की पुनर्रचना की नींव है। यह हमें हमारे सामाजिक यथार्थ से जोड़ती है, उन मौन आवाज़ों को सामने लाती है जिन्हें इतिहास और सत्ता ने लंबे समय तक अनसुना किया और यह सुनिश्चित करती है कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक न्यायिक, समावेशी और जागरूक सामाजिक तंत्र बने।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.