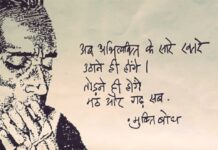— परिचय दास —
वह स्त्री जो चुपचाप घर की दीवारों पर वर्षों से टँगी रही, तस्वीर नहीं बनी — साया बनती रही। वह स्त्री, जिसे उसके ही नाम से कम, संबोधन से अधिक पुकारा गया — मिसेज़ (श्रीमती) । उसके भीतर जो कुछ भी स्त्री था, वह धीरे-धीरे लुप्त होता गया और एक लय, एक रीति, एक रस्म में समाहित होता गया — जो समाज ने, जो विवाह ने और जो पुरुष की महत्त्वाकांक्षाओं ने रचा था। “मिसेज़” नामक यह फ़िल्म इसी विलुप्त होती पहचान को पुनः खोजने की कथा है। यह एक स्त्री के पुनराविष्कार की गाथा है, जो अपने मौन के भीतर से निकलकर बोलती है — अस्फुट नहीं, स्पष्ट और असंदिग्ध।
फिल्म के आरंभिक दृश्य में ही कैमरा बहुत कुछ कह जाता है। मध्यमवर्गीय गृहस्थी की उन आदतों को, जो सुलझी हुई दिखती हैं पर भीतर से गाँठ-गाँठ भरी हैं — कैमरा उन्हें टटोलता है, सहलाता है और उजागर करता है। किरदारों की बातचीत, कपड़े, बैठने का ढंग, मोबाइल की स्क्रीन पर जमी धूल — सब कुछ मिलकर एक अदृश्य कविता रचते हैं, जो शहर की अनकही स्त्रियों की आवाज़ बनती है। यह फिल्म संवादों की नहीं, दृश्यों की भाषा बोलती है। उसकी नायिका — मिसेज़ ( श्रीमती) — अपने मौन में जितना कहती है, शायद बोलकर उतना कभी न कह पाती।
‘मिसेज़’ ( श्रीमती ) एक साधारण नाम, पर वह साधारण नहीं है। वह पत्नी है पर सबसे अधिक — वह एक स्त्री है, जो भूल गई थी कि वह अपने लिए भी कुछ सोच सकती है। जो अपने पति के करियर में, रसोई के सिलसिले में बिखरते-बिखरते स्वयं को भूल बैठी थी और यही विस्मृति, फ़िल्म का मूल है — वह क्षण जब वह स्वयं को दोबारा याद करती है। याद करती है कि उसके भी कुछ स्वप्न थे — अधबुने, अधपके, अधूरे। लेकिन वे उसकी थीं और अब वे फिर से उसके पास लौटते हैं।
फ़िल्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह किसी बड़े नारे, किसी उग्र स्त्रीवाद, किसी विद्रोह के शोर के बिना भी स्त्री की आज़ादी की बात करती है। वह उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसके भीतर से निकालकर नया बनाती है। यह सृजनात्मक विद्रोह है — जो रसोई से उठकर नृत्य की ओर बढ़ता है। मिसेज़ कोई क्रांति नहीं करती, वह बस याद दिलाती है कि स्त्री होना एक भाव है — और उस भाव को मरने नहीं देना चाहिए।
सान्या मल्होत्रा का अभिनय — जैसे कोई पुरानी कविता हो, जिसे अब तक किसी ने ध्यान से न पढ़ा हो, और अब वह पहली बार पूरी संवेदना के साथ पढ़ी जा रही हो। उनके चेहरे पर जो भाव आते हैं, वे संवादों के शब्दकोश से नहीं, आत्मा के लहजे से निकलते हैं। उनकी आँखों में जो थकान है, वह किसी एक दिन की नहीं, वर्षों के त्याग की थकान है — और जब वही आंखें चमकने लगती हैं, तो दर्शक भी भीतर से उजास से भर उठता है।
फिल्म में नायिका का नृत्य से जुड़ना — एक सांकेतिक दृश्य है। नृत्य यहाँ प्रतीक बन जाता है उस जीवन का, जिसमें सिर्फ़ नर्तन नहीं, आत्म-साक्षात्कार है। वह अपने संवाद नहीं रटती, वह उन्हें जीती है। जैसे अपने ही जीवन के अधूरे पन्नों को मंच पर खुलकर पढ़ती है। और जब वह मंच से नीचे उतरती है, तो वही स्त्री होती है, पर बदली हुई — आत्मविश्वास से भरी, अपने ही नाम से पुकारने योग्य।
यह फिल्म पति-पत्नी के रिश्ते को भी नये सिरे से देखती है। पति को कोई खलनायक नहीं बनाया गया, न ही किसी कठोर स्त्री के उदय का आलंबन रखा गया है। संबंधों की संश्लिष्टता, परस्पर निर्भरता और मनुष्य की आत्म-भूल — यह सब कुछ बहुत ही सूक्ष्मता से, एक सजग दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह दृष्टि आलोचना की नहीं, करुणा की है। निर्देशक का कैमरा किसी के भी पक्ष में नहीं, केवल सत्य के पक्ष में है — वह जो घर की दीवारों में दफ़न होता आया है।
संवादों की मितव्ययिता, संगीत की गहराई, दृश्यों की आत्मीयता — सब कुछ मिलकर एक ललित काव्य की रचना करते हैं। यह फ़िल्म दृश्य-कविता बन जाती है — जिसमें शब्द कम हैं, पर अनुभूति भरपूर है। यह फ़िल्म आँखों से देखी नहीं जाती — यह हृदय से महसूस की जाती है।
यह कहानी उन असंख्य ‘मिसेज़’ की है, जो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमारे आसपास हैं। वे जो नाम के पहले ‘श्रीमती’ लगाकर गुमनाम हो गईं, और जिनके भीतर अब भी कोई सपना साँस ले रहा है। यह फिल्म उनके लिए है — एक लौ की तरह, एक राह की तरह।
शांत नृत्य की मुद्रा में जमी हुई ऋचा जब रसोई में खड़ी होती है, तो लगता है जैसे वह भारतीय स्त्री के हज़ार वर्षों के मौन को ओढ़े कोई प्रतिमा हो—कठोर, निष्कंप, पर भीतर ही भीतर चटकती हुई। मिसेज़ केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि वह थरथराता हुआ अनुभव है जो हर उस स्त्री की आँखों में बसता है, जो घर की देहरी लांघकर अपने सपनों को भीतर ही समेट लेती है। यह फ़िल्म नायक की नहीं, नायिका की कथा है; लेकिन यह कथा भी कथा नहीं, वह कसमसाती चुप्पी है जो हर सुबह साड़ी की चिटकिनी में बंधती है, हर रात थाली में परोसकर परोसी जाती है, और हर दिन चाय में उबाल की तरह पकती है।
यह फिल्म दर्शक को सतह पर बहकाती नहीं है; वह भीतर तक उतरती है—उस रसोई तक, जहाँ स्त्रियाँ सिर्फ खाना नहीं पकातीं, बल्कि अपने सपनों को सेंकती हैं, ख्वाहिशों को आंच में डालकर धीमी आँच पर जीती हैं। ऋचा की भूमिका में सान्या मल्होत्रा ने वह अंडरटोन, वह सूक्ष्म कम्पन पकड़ा है जो एक शिक्षित, संवेदनशील और आत्माभिमानी स्त्री के भीतर उपजते विद्रोह का पूर्वगान है। जब वह पति के स्पर्श को झटकती है, तो वह केवल असहमति नहीं, वह अपने शरीर और आत्मा की अस्मिता की पुनःस्थापना है।
फ़िल्म की कथा हमारे उस समाज का आइना है जहाँ विवाह एक संस्थान नहीं, स्त्री की नियति बना दिया गया है। दिवाकर का सधा हुआ, परंपरावादी चेहरा आधुनिकता की वेशभूषा में छुपे पितृसत्ता का चरित्र है। उसके ‘आई लव योर किचन स्मेल’ जैसे वाक्य स्त्री की भूमिका को सुगंध और स्वाद तक सीमित करने की कुटिल अभिव्यक्ति हैं। वह प्यार नहीं करता, वह उपभोग करता है—और जब वह उपभोग से परे जा कर स्त्री की चेतना से टकराता है, तो टूटता है।
फिल्म में सास की भूमिका कोई परंपरा की पोषक नहीं, बल्कि वही संरक्षक है जो पुरुष वर्चस्व को हर रोज़ नियमित बनाती है। वह टूथब्रश थमाती है, वह ऋचा को आदेश देती है, वह रसोई को ही स्त्री का धर्मशास्त्र मानती है लेकिन सबसे मारक दृश्य तब आता है जब ऋचा अपनी ‘माहवारी’ के दौरान रसोई से दूर रहने का “अनुग्रह” पाती है, और उसमें ही वह अपनी पहली राहत महसूस करती है। यह कैसा विडंबनापूर्ण सौंदर्य है कि स्त्री को समाज द्वारा ‘अशुद्ध’ कहे जाने पर ही थोड़ी देर को स्वतंत्रता मिलती है।
पर यह फिल्म केवल प्रतिरोध की कथा नहीं है। यह उस धीमे उफान की रचना है, जहाँ स्त्री पहले समझती है, फिर सहेजती है, फिर सहती है और अंततः उठ खड़ी होती है। ऋचा का वह नृत्य, जहाँ वह अपने भीतर के आक्रोश और अस्वीकार को पांव की थाप में बदलती है—वह दृश्य भारतीय स्त्री विमर्श का सबसे शुद्ध, सबसे मार्मिक बिंब बन जाता है। वह नृत्य केवल अभिव्यक्ति नहीं, वह शपथ है; वह घोषणा है कि स्त्री अब रसोई से नहीं, अपने भीतर से बोलेगी।
कथ्य की दृष्टि से यह फिल्म जितनी सरल है, शिल्प की दृष्टि से उतनी ही सघन। कैमरा बहुत कुछ नहीं कहता लेकिन वह सब दिखाता है जो कहा नहीं जा सकता—रसोई की गंदगी, नल की टपकन, ससुर के हाथ में ब्रश और पति की शुष्कता—ये सभी दृश्य शब्दों से परे जाकर दृश्य-काव्य बन जाते हैं। प्रथम मेहता का छायांकन जैसे हर कट में स्त्री की सांस की गति को पकड़ लेता है। कहीं अंधकार, कहीं धूप, कहीं चूल्हे की आँच—हर तत्त्व एक प्रतीक बनकर उभरता है।
संगीत भी इस फिल्म में पारंपरिक भूमिका नहीं निभाता, वह हस्तक्षेप नहीं करता। वह मौन में से जन्म लेता है, मौन में विलीन हो जाता है। यह मौन ही इस फिल्म का सबसे बड़ा संवाद है और यही कारण है कि यह फिल्म कहीं भी ऊँचे स्वरों में चीखती नहीं, वह धीमे-धीमे एक हाहाकार को जन्म देती है, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में नहीं कह सकते।
मिसेज़ एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्त्री-केंद्रित फिल्म है, लेकिन वह ‘स्त्री विमर्श’ की नारेबाज़ी नहीं करती। वह सहज है, सहज में तीखी है और तीखेपन में करुणामयी है। जब रिचा एक बाल्टी गंदे पानी को पति पर उँडेलती है, तो वह केवल अपमान नहीं, वह एक युग का अंत है। और जब वह चुपचाप घर छोड़ देती है—बिना किसी को कुछ बताए—तब वह स्त्री की नई यात्रा की शुरुआत है, जो अब किसी गृहस्थी में नहीं, बल्कि स्वयं में बसती है।
इस फिल्म को देखते हुए दर्शक केवल स्त्री के दुख से नहीं, अपनी चुप्पियों से भी साक्षात्कार करता है। हर पुरुष को यह फिल्म एक आईना देती है और हर स्त्री को एक राह। शायद इसीलिए ‘मिसेज़’ केवल एक फिल्म नहीं—एक चुपचाप उगता हुआ विद्रोह है, एक कविता है जो आँच में पकी है, एक नृत्य है जो आँसुओं की छाया में जन्मा है।
जहाँ ‘मिसेज़’ फिल्म स्त्री की अंतर्यात्रा, उसके अवरोधों और उस मौन की अभिव्यक्ति है जो रसोई में जन्म लेती है, वहीं वह उस सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था की पड़ताल भी है जो इन सबका कारण बनती है। यह फिल्म भारतीय समाज के उस अंत:संस्कार की भी आलोचना है जिसमें विवाह, परंपरा और गृहस्थ जीवन एक शास्त्रीय अनिवार्यता की तरह चित्रित होते हैं। ऋचा के माध्यम से यह फिल्म पूछती है—क्या विवाह केवल एक संस्था है या एक आदिम अनुशासन?
ऋचा की शिक्षा, उसका नृत्य, उसका आत्मसम्मान—ये सब उस घर में अनुत्तरित प्रश्न की तरह पड़े रहते हैं। उन्हें कोई पढ़ता नहीं, कोई सुनता नहीं। लेकिन फिल्म यह बात बहुत बारीकी से पकड़ती है कि पितृसत्ता केवल पुरुषों द्वारा नहीं, बल्कि एक समूची सांस्कृतिक परंपरा के सहचर्यों द्वारा पोषित होती है—और उसमें स्त्रियाँ भी भागीदार होती हैं। ऋचा की सास का चरित्र इस यथार्थ को उजागर करता है। वह स्वयं कभी विद्रोह नहीं कर सकी, इसलिए अब वह व्यवस्था की रक्षक बन गई है।
यह फिल्म स्त्री और पुरुष के संबंध को केवल एक नैतिक समस्या की तरह नहीं, बल्कि सौंदर्यबोध और संवेदनशीलता की भी समस्या बनाकर प्रस्तुत करती है। दिवाकर केवल अत्याचारी नहीं है, वह भावशून्य है। वह ऋचा के नृत्य को देखता है, लेकिन उसमें कोई अनुभूति नहीं करता। वह उसे चाहता है, लेकिन उसके चाहने में कोई आत्मीयता नहीं। उसका प्रेम भी आवश्यकता का विस्तार है—और यहीं से उसका पतन आरम्भ होता है।
एक विशेष दृश्य में, जब ऋचा अकेली रसोई में थके हुए हाथों से सब्ज़ी काट रही होती है और कोई संगीत नहीं बज रहा होता—वहाँ मौन का जो आलाप है, वह भारतीय गृहिणी के जीवन का सबसे प्रभावी कोरस बन जाता है। फिल्म का यही मौन भारतीय सिनेमा की उस परंपरा से अलग खड़ा होता है जहाँ संवादों के द्वारा विद्रोह किया जाता था। यहाँ संवाद मौन में हैं, और मौन का प्रतिरोध उससे कहीं अधिक मारक है।
फिल्म का अंतिम दृश्य—जहाँ ऋचा नृत्य के माध्यम से अपने अनुभवों को दृश्यबद्ध करती है—सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि उस संपूर्ण मानसिक यातना का कलात्मक निष्कर्ष है। यह दृश्य ‘दृश्य-काव्य’ की परंपरा में एक नयी ऊँचाई रचता है। उसका प्रत्येक हाथ का उठना, प्रत्येक पाँव की थाप, उसके भीतर पनपे उस क्रोध, घुटन और मुक्ति की यात्रा है जिसे वह शब्दों में कभी कह नहीं पाई।
दूसरी ओर, फिल्म यह भी दिखाती है कि सामाजिक संरचनाएँ कितनी आसानी से पुनरावृत्त होती हैं। दिवाकर दूसरी शादी कर लेता है, और उसकी दूसरी पत्नी उसी व्यवस्था में प्रसन्न दिखाई जाती है—एक दारुण बिंब की तरह। यह दृश्य किसी भव्य क्लाइमेक्स से अधिक भयावह है, क्योंकि यह बताता है कि एक स्त्री के विद्रोह के बावजूद व्यवस्था अपना स्वरूप नहीं बदलती, वह केवल पात्र बदलती है। परिवर्तन की जिम्मेदारी केवल स्त्री की नहीं होनी चाहिए, यह फिल्म अपने पूरे कथ्य में यह माँग रखती है।
मिसेज़ का सिने-शिल्प भी उसी काव्यात्मकता का अनुकरण करता है जो उसके कथ्य में है। कोई बैकग्राउंड स्कोर अधिक हावी नहीं होता, कोई संवाद नाटकीय नहीं होता, और कोई कैमरा मूवमेंट दर्शक को चौंकाने के लिए नहीं रचा गया। सब कुछ धीरे-धीरे घटता है, जैसे सुबह की रोशनी एक गहरे अंधेरे में रिस रही हो। और इस अंधेरे में जो उजास दिखती है, वह केवल रिचा की मुक्ति में नहीं, बल्कि दर्शक के आत्मबोध में भी है।
यह फ़िल्म हमें दो बातें सिखाती नहीं, बल्कि दिखाती है—एक, कि स्त्री के भीतर जो असहमति जन्म लेती है, वह समय के साथ विस्फोट में बदल सकती है। और दो, कि यदि समाज नहीं बदलेगा तो हर ऋचा के बाद एक नई स्त्री उसी जाल में फँसेगी, और वही कथा फिर से घटेगी—बस पात्र बदल जाएँगे।
मिसेज़ कोई उपदेशात्मक आख्यान नहीं है; यह एक अत्यंत कलात्मक, संतुलित और मर्मस्पर्शी कृति है, जो भारतीय सिनेमा में स्त्री-विमर्श को एक नई भाषा, एक नई संवेदना और एक नई गरिमा प्रदान करती है। यह फिल्म देखने के बाद दर्शक भीतर से बदलता है—और यही किसी भी कला की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
मिसेज़ एक ऐसी फिल्म है जो रसोई की दीवारों से उठकर दर्शक की अंतरात्मा तक पहुँचती है। यह कोई नारा नहीं लगाती, कोई प्रत्यक्ष क्रांति नहीं दिखाती, बल्कि उस स्त्री की चुप क्रांति को स्वर देती है जो अक्सर घरेलू दीवारों के भीतर दम तोड़ देती है। ऋचा के माध्यम से यह फिल्म न केवल पितृसत्ता के सांचे को तोड़ती है, बल्कि स्त्री की स्वतंत्र चेतना, उसकी कलात्मक अस्मिता और उसकी मौन प्रतिरोध-शक्ति को एक नया विमर्श भी देती है।
इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने दर्शकों को बाँधती नहीं, उन्हें खोलती है। यह स्त्री-पुरुष दोनों के लिए आत्मदर्शन का दर्पण है—जहाँ एक ओर पुरुष अपने भीतर गढ़ी पितृसत्तात्मकताओं से मुठभेड़ करता है, वहीं स्त्री अपनी चुप्पियों से बाहर आकर एक नई पहचान की यात्रा पर निकलती है।
यह फिल्म एक स्वरहीन संगीत है, एक शब्दहीन कविता, जो दृश्य माध्यम की सीमाओं को पार कर जाती है। इसके अंत में जब ऋचा एक स्वतंत्र नृत्य शिक्षिका बनकर अपने दुःख को कला में रूपांतरित करती है तो वह केवल मुक्त नहीं होती—वह समाज के लिए एक उदाहरण बन जाती है, एक प्रतिरोध की जीवंत आकृति।
फिल्म-संबंधी विवरण इस प्रकार है – निर्देशक: आरती कदव; पटकथा: हरमन बावेजा, अनु सिंह चौधरी; ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ पर आधारित फिल्म; उत्पादन: हरमन बावेजा, पम्मी बावेजा, स्मिता बालिगा, अब्दुल अज़ीज़ मकानी, ज्योति देशपांडे; अभिनय: सान्या मल्होत्रा, निशांत दहिया, कंवलजीत सिंह; छायांकन: प्रथम मेहता; संपादन: प्रेरणा सहगल; संगीत: सागर देसाई, फैजान हुसैन।
‘मिसेज़’ फिल्म भारतीय सिनेमा के स्त्री-विमर्श में एक मील का पत्थर है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि क्रांति केवल नारों से नहीं बल्कि रसोई के कोनों, नल की टपकती बूंदों और स्त्री की आँखों में उगते मौन से भी उपजती है और जब वह मौन एक बाल्टी पानी में बदलकर फूटता है तो वह केवल पति पर नहीं गिरता—वह पूरी व्यवस्था पर एक तीखा, करुण और आत्मगौरवपूर्ण प्रहार बन जाता है। यह फिल्म देखना मात्र एक कलात्मक अनुभव नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.