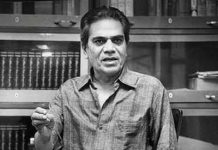— कनक तिवारी —
प्रभाष जोशी से मैं इतना इतना बेतकल्लुफ रिश्ता बना नहीं पाया कि उन्हें यार कह सकूं। अंतरंग रिश्ते के कारण दोस्त एक दूसरे के सामने ‘दैहिक दैविक भौतिक‘ रूप से अनावृत्त होते हैं। मैं उनसे तीन वर्ष छोटा हूं लेकिन अंगरेजी कैलेन्डर के हिसाब से हमारी राशियां एक हैं। उन्हें बड़े भाई की तरह भी नहीं देख पाया क्योंकि हम दोनों अनौपचारिक रिश्ते से छिटकना नहीं चाहते थे। महाभारत में कृष्ण ने कृष्णा को बहन या भाभी मानने के हर ज्ञात रिश्ते के बदले उससे सखा-सखी या बन्धु-बांधवी जैसा रिश्ता ईजाद किया था। प्रभाष जोशी और मैं एक दूसरे के मित्र, बन्धु या और हर किसी परिभाषा के अनुसार आत्मीय थे। ‘हमारी राजनैतिक, सामाजिक और गांधीवादी विचारधाराओं में टकराव नहीं है‘-ऐसा जब मैं उनसे कहता तो वे कहते ‘टकराव नहीं, ठहराव शब्द का इस्तेमाल करो।‘ मुस्कराने तथा ठहाका लगाने के बीच बोलते बोलते हंसते और हंसते हंसते बोलते रहते।
उग्र हिन्दुत्व का नुकीलापन मुझे बहुत गड़ता रहता है। मैंने उनसे अपने दंभ में कहा कि मध्यप्रदेश के ज्ञात और विख्यात बुद्धिजीवियों से कहीं ज्यादा यह अल्पज्ञात लेखक जो राजनीति और वकालत में एक के बाद एक अस्तव्यस्त रहा है, उग्र हिन्दुत्व के खिलाफ लिखता रहता है। प्रभाष जी ने कहा लगी शर्त और हम दोनों के हाथ एक दूसरे के साथ हो गए। उनके आग्रह पर एक रविवार की सुबह जनसत्ता के कार्यालय जब मैं पहुंचा तो उन्होंने अपने हिन्दुत्व संबंधी लेखों का पुलिन्दा थमा दिया। मैं उन्हें देखता और विस्मित तथा पराजित होता रहा। उस दिन प्रभाष जी की मुस्कान मुझे कुटिल लगी थी-नहीं नहीं छेड़ती हुई स्नेहिल-कुटिल। पता नहीं क्रिश्चियन काॅलेज, इंदौर के इस विद्यार्थी को छात्र जीवन में ऐसी व्यंग्य भरी निश्छल मुस्कराहट का पेटेन्ट कराने का अवसर मिला होगा अथवा नहीं। फिर भी अपने बचाव में मैंने कहा ‘प्रभाष जी, मैं अब भी कहता हूं कि मुझसे ज्यादा और तीखा लेखन दक्षिण पंथी हिन्दुत्व को लेकर मध्यप्रदेश में किसी ने नहीं किया है। हालांकि मैं उन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें दैनिक आधार पर यह सब लिखने की नौकरी करनी पड़ती है। ‘उन्होंने कहा, ‘बंधु, इस पुलिन्दे में स्वतंत्र लेखों की ही भरमार है।‘ मैंने फिर कहा ‘इसके बावजूद मैं ही सही हूं क्योंकि आप मध्यप्रदेश के लेखक कहां रहे। आप तो राष्ट्रीय लेखक हैं।‘ वे झेंपते हुए से बोले। ‘इससे क्या मैं मध्यप्रदेशीय नहीं रहा?‘ बिहारी उच्चारण में उनको महारत हासिल थी। उसी ध्वनि मुद्रा में वे बोले ‘का हो, लालू यादव राष्ट्रीय नेता हो जाने से बिहारी नहीं रहेगा?‘ ‘हिन्दू होने का धर्म‘ जब उनके संकलित लेखों का कलेवर बनकर छपा तब एक बहुप्रतीक्षित, बहुचर्चित, बहुआयामी किताब साहित्य के हाथ में आई। एक नार्मदीय ब्राम्हण ने हिन्दुत्व के हिंसक, संकीर्ण और काल तिरस्कृत मुद्दों को जिस प्रभविष्णुता, वाक्वैदग्ध्य और तार्किकता के साथ निपटाया है, उसके मुकाबले संस्कृति, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के शास्त्रीय अंगरेजी ग्रंथों को भी पसीना आ जाता है। प्रभाष जोशी में हिन्दुत्व एक अंतर्भूत प्रक्रिया की तरह उनके वृहत्तर व्यक्तित्व से फूटता था। वह समावेशी, सर्वप्रदेशीय और जाति रहित था। दक्षिण पंथ की विजय होने पर उन्हें कोफ्त होती थी। वे उसके पराजय पर्व के भविष्य वाचक थे। हालांकि कांग्रेस जैसी मध्यमार्गी संस्था के बदमिजाज, भ्रष्ट और सत्ता लोलुप होने को लेकर प्रभाष जोशी ने उसे नहीं बख्शा।
प्रभाश जोशी मनुष्यता का मौसम थे। बातचीत में वे अपरिचित व्यक्तियों के लिए भी सहज हो जाते थे और उन्हें अपने स्नेह से नहलाते रहते थे। जीवन जिन मुफलिसों में सर्द अहसास की तरह समा गया है, उनके लिए प्रभाष जोशी की कलम से ऊष्मा के स्फुलिंग लगातार झरते रहे हैं। उन्होंने समाजवादी होने के बावजूद अपने लेखन में नारेबाजी के शोशे नहीं छोड़े और न ही अकिंचनों के लिए केवल गाल बजाए। समाजवाद और धर्म के सांस्कृतिक पक्ष की जितनी जनतांत्रिक पैरवी उन्होंने की है, वैसे उदाहरण हिन्दी पत्रकारिता और वैचारिक लेखन में बहुत अधिक देखने को नहीं मिलते। वे जिंदादिल इंसान थे। उनकी सोहबत में बैठने वालों को ही नहीं पूरे माहौल को अपने दिलों की धड़कन के बारे में आश्वस्ति मिलती थी। मनुष्य कुल मिलाकर एक ऐसा स्वार्थी प्राणी भी है जो बहुत दिनों तक किसी रिश्ते को कायम नहीं रखता है। हममें से बहुत लोग हैं जो अपने निकट रिश्तेदारों और मित्रों के दुख के क्षणों में कई बार व्यस्तता, बीमारी या उदासीनता के कारण नहीं जाते हैं। पता नहीं वक्त के चलते ऐसे रिश्ते रूढ़ क्यों हो जाते हैं। दुष्यंत कुमार और नवीन सागर दो ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनमें अपने खास मित्रों से मिलने की इतनी गहरी तड़प रही है कि यदि वे उपेक्षित महसूस करते तो मरने मारने की हद तक लड़ पड़ते। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मन में यह खबर मिलते ही कि प्रभाष जी नगर में हैं उनसे मिलने की तड़प उठने लगती। कभी नहीं लगा कि मनुष्य प्रभाष जी के लिए अवांछित निर्मिति है। उनके जेहन में एक तरह का मानव-संगीत गूंजता रहता था। टूटते रिश्तों की दुनिया में प्रभाष जोशी एक फेविकोल थे। फिर लगने लगा है कि एक दूसरे से मिलने से बचने वाले मनुष्यों को कौन समझाएगा कि प्रभाष जोशी के निधन के कारण उनके अमानवीकृत हो जाने का कितना खतरा बढ़ गया है!
‘हिन्दू होने का धर्म‘ मेरी दृष्टि में हिन्दुत्व का एक छोटा मोटा आधुनिक एनसाइक्लोपीडिया है। उसमें अंतर्निहित दार्शनिक बहस का स्तरीय विमर्श है। उसमें केवल तर्क नहीं हैं। उससे ज्यादा सच्ची समझ का आत्मविश्वास है। उसकी भाषा लेखक के अहसासों को इस तरह परोसती है कि पाठक उसमें डूबता चला जाता है। हिंदुत्व की कठिन उपपत्तियों को कलम ने इतना सरल कर दिया है कि उसे पढ़ लेने भर से संकीर्ण राष्ट्रवाद से बहस करने का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठक को प्रभाष जोशी के हस्ताक्षर से हर निबंध में मिलता जाता है। वे एक निष्णात हिन्दू थे-मन वचन और कर्म से। इसलिए एक निखालिस भारतीय भी। धर्म से ज्यादा संस्कृति प्रभाष जोशी के चिंतन का आयाम रही है। धर्म संस्कृति का ही तो प्रतिफलन है। संस्कृति को भला धर्म पर क्यों अवलंबित रखा जाए। धर्म यदि निजी विश्वास का विश्वविद्यालय, अनाथालय या संग्रहालय कुछ भी हो तो संस्कृति एक सामाजिक समास है। वह श्वास या गंध की तरह मनुष्य और मनुष्येतर जीवन में हवा या नदी की तरह प्रवाहित है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.