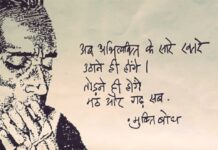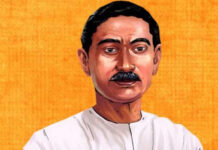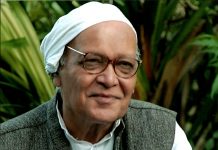— परिचय दास —
आ गया कालीधर — जैसे कोई पुरानी पुकार लौट आई हो गूंजती हुई स्मृति के गलियारे में। कालीधर लापता नहीं हुआ, वो तो हमारे भीतर का एक भूला-बिसरा छोर है, जो अक्सर अनसुना रह जाता है। ज़ी5 पर आई यह फिल्म महज एक कहानी नहीं, बल्कि समय, भूलने और याद रखने की कविता है। अभिषेक बच्चन के अभिनय ने उस कविता में जीवन की लय भर दी है, एक ऐसा संगीत जो धीमा है लेकिन भीतर तक उतर जाता है।
कालीधर अकेला है लेकिन उसकी तन्हाई किसी पत्थर जैसी भारी नहीं, किसी सूखे पत्ते की तरह है—जो उड़ता है, भटकता है, पर हर जगह से कुछ लेकर लौटता है। अल्ज़ाइमर से जूझता यह व्यक्ति समाज की उस ग़ैर-मरहमजद रवैये का आईना है, जो बीमारियों से नहीं, बीमार इंसानों से डरता है। हरिद्वार के कुंभ में उसे छोड़ जाना कोई साधारण परित्याग नहीं है—यह एक युग का अपने ही अनुभव से मुँह फेर लेना है। कालीधर से छुटकारा पाना, किसी बोझ से नहीं, आत्मीयता से पलायन है।
फिर आता है बल्लू—एक बालक, जिसमें कोई अकादमिक भाषण नहीं पर प्रेम का सहज व्याकरण है। दैविक बाघेला की मासूम आँखों में उम्मीद की रेखा कांपती है, जैसे किसी अंधेरी रात में चुपके से जुगनू ने जगह बना ली हो। कालीधर और बल्लू की यह दोस्ती ‘रिश्ते’ शब्द से कहीं आगे जाकर ‘बंध’ बन जाती है—ऐसा बंध, जो उम्र, अनुभव और पीड़ा के आर-पार हो जाता है।
फिल्म बिना किसी घोषणात्मक संवाद के, हमें खोया-पाया विभाग में ले जाती है। जीशान अय्यूब का सुबोध, जैसे खुद व्यवस्था का एक संवेदनशील किनारा हो, जो खोजता है और हर खोज में थोड़ा खुद को भी पा लेता है। निम्रत कौर की उपस्थिति भी किसी स्मृति की तरह है—कम, पर गूंजती हुई। मीरा का किरदार, प्रेम के एक ऐसे रेखाचित्र की तरह उभरता है, जिसे रंगने की कोशिश नहीं की गई—उसकी पीली उदासी में भी एक सौंदर्य है।
मधुमिता सुंदररामन ने इस फिल्म को रचा नहीं, जिया है। उन्होंने एक ऐसे समाज का नक्शा खींचा है, जहां बुज़ुर्ग होना कोई उपलब्धि नहीं, अपराध बन गया है। फिल्म हमें कई मोड़ों पर खुद से मिला देती है—जब हम बल्लू होते हैं, जब हम सुबोध होते हैं, और कभी-कभी खुद कालीधर।
‘कालीधर लापता’ तमिल फिल्म KD का रीमेक जरूर है, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण केवल भाषा का नहीं, संवेदना का भी रूपांतरण है। KD में जहां 80 वर्ष की उम्र अनुभव का लिबास पहनकर आती है, वहीं कालीधर लापता में मिडिल एज की खामोश घुटन है। KD शायद जीवन के अंतिम मोड़ की टोह थी, पर ‘कालीधर लापता’ उस मोड़ के पहले की बेचैनी है।
ये फिल्म हमें बताती है कि लापता होना सिर्फ किसी जगह से ग़ायब होना नहीं होता—कभी-कभी हम रिश्तों, स्मृतियों, या खुद अपने वजूद से भी लापता हो जाते हैं। और फिर, एक बल्लू आता है, जो हमें हमारी ही छाया से मिलवाता है।
‘कालीधर लापता’ एक चुपचाप बहती नदी है—जिसमें दुःख की मछलियाँ भी हैं, उम्मीद की जलधार भी। अभिषेक बच्चन ने इस बार अभिनय नहीं किया, आत्मा रख दी परदे पर। और इस आत्मा में दर्शक अपनी परछाइयाँ पहचानते हैं। तभी तो लोग कह रहे हैं—“आपने दिल जीत लिया, आप तो जादूगर हो भइया।”
कालीधर की यात्रा कोई जियॉग्राफिकल सफर नहीं है—यह एक आंतरिक विस्थापन है। हर कदम पर वह थोड़ा और खोता है, थोड़ा और पाता है। जब वह कुंभ मेले की भीड़ में खोता है, तो वह उस भीड़ की प्रतीकात्मकता से बाहर निकल आता है—यह एक समाज है जो अपनी संतान को, अपने वृद्ध को, अपने बीमार को, और अपनी संवेदना को छोड़ आता है एक तीर्थ में, जहाँ मोक्ष की तलाश करने वाले खुद मोक्ष से भागते हैं।
बल्लू, उस भीड़ में से निकली एक आवाज़ है—एक खोया हुआ बच्चा, जो कालीधर के खोने में अपने पा जाने की संभावना ढूँढ़ता है। वे दोनों मिलकर जैसे कोई नई भाषा गढ़ते हैं—जिसमें ‘पिता’, ‘पुत्र’, ‘दोस्त’, ‘अजनबी’ जैसे पारंपरिक रिश्तों के नाम नहीं होते, बस अपनापन होता है। वे खाना चुराते हैं, हँसी बाँटते हैं, और एक-दूसरे की चुप्पियों में घर बना लेते हैं।
कालीधर जब बल्लू के साथ खेतों में सोता है, किसी गाँव की मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है, या सस्ते ढाबों में बची-खुची रोटियाँ खाता है, तो वह सिर्फ जीवन जी नहीं रहा होता—वह जीवन को फिर से देख रहा होता है। उस बीमार स्मृति में जो कुछ बचा है, वह हीरे की तरह चमकता है—मीरा की याद, माँ की ममता, और अब बल्लू की मुस्कान।
यह फिल्म हमें स्मृति की राजनीति पर भी सोचने पर मजबूर करती है। अल्ज़ाइमर एक जैविक विघटन नहीं मात्र—it is also a metaphor. कालीधर वह आदमी है जिसे उसका समाज, उसका परिवार, और उसकी सभ्यता भूलना चाहती है। वह व्यक्ति जो कभी प्रेम करता था, नौकरी करता था, आशाएँ रखता था—आज वह यादों के बोझ से छूटा हुआ सिर्फ एक नाम है, जिसे उसके अपने भी सुनना नहीं चाहते। पर फिल्म बताती है कि स्मृति से भागना, अपने इतिहास से भागना है। और जो समाज अपने अतीत से भागता है, वो बार-बार खोता है—कभी कालीधर के रूप में, कभी बल्लू के।
निर्देशिका मधुमिता सुंदररामन का काम यहाँ विशेष रूप से सराहनीय है। उन्होंने पटकथा को लाउड नहीं होने दिया, संवादों को घोषणापरक नहीं बनाया। उनका कैमरा उन पलों पर रुकता है, जहाँ ज़्यादातर फिल्मकार हड़बड़ा कर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जब बल्लू और कालीधर एक ट्रेन की छत पर बैठे हैं—आकाश उनके सिर के ऊपर है, ज़िंदगी उनके पाँवों के नीचे, और कोई भी स्टेशन उनका नहीं, फिर भी हर स्टेशन पर उनकी उम्मीद उतरती है।
ज़ीशान अय्यूब का सुबोध उस व्यवस्था का प्रतिनिधि है जो बहुत कम मौकों पर मानवीय बन पाती है, लेकिन जब बनती है, तब चमत्कार होता है। सुबोध के किरदार में गहराई है—वो सिर्फ खोया-पाया अधिकारी नहीं है, वह उन लोगों का प्रतीक है जो संस्थानों के भीतर रहकर भी व्यक्तिगत तौर पर लड़ते हैं, ढूँढ़ते हैं, उम्मीद लगाते हैं।
मीरा के किरदार में निम्रत कौर की वापसी जैसे एक स्मृति का पुनरागमन है। वह कहीं दूर नहीं गई थीं, बस भूल गई थीं। उनके दृश्य कम हैं, पर जब वे आती हैं, तो जैसे किसी पुराने प्रेमपत्र की स्याही फिर से नीली हो जाती है।
‘कालीधर लापता’ की सबसे बड़ी ताक़त उसका संगीत और ध्वनि-संयोजन है—जो कहीं भी ज़्यादा नहीं होता, और न ही इतना कम कि शून्य लगे। वह पीछे से हमारी आँखों में उतरता है, और संवादों से पहले ही दृश्य के अर्थ खोलने लगता है।
यह फिल्म एक जादू की तरह है—धीमी, कोमल, और थोड़ी-सी उदास। यह ऐसी कविता है, जिसे पढ़ते हुए आँखों में पानी आ जाए और होंठों पर मुस्कान भी रहे।
कालीधर की यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, वह खुद एक काव्यात्मक संरचना में ढलने लगती है—जैसे कविता कोई रास्ता हो और मनुष्य उसका यात्री। वह हर नए दृश्य में कोई नया प्रतीक बनकर उभरता है। जब वह बल्लू के साथ खेतों में पत्तों की ओट में सोता है, तो वह दृश्य महज़ गरीबी का चित्र नहीं, बल्कि प्रेम की सहजता का प्रतीक बन जाता है। वे दोनों, जिनके पास न छत है, न घर, पर जिनके पास एक-दूसरे की ऊष्मा है, विश्वास है, और साथ जीने की चाह है।
यहाँ फिल्म हमें बार-बार रुलाती नहीं—बल्कि अपनी लय में हमें भावुकता की उस सतह पर ले जाती है, जहाँ आँसू जरूरी नहीं होते, लेकिन भीतर बहुत कुछ भीग जाता है। एक दृश्य में जब कालीधर बल्लू को गोदी में लेकर पुराने किसी lullaby की तरह कुछ बुदबुदाता है, तो वह कोई नाटकीय क्षण नहीं होता—वह जीवन की वही धुन होती है जो माँ ने कभी सुनाई थी और जिसे अब वह खुद किसी और को सुना रहा है।
फिल्म के संवाद कविता जैसे हैं—कम शब्दों में बहुत कुछ कहने वाले। जैसे कालीधर का कहना: “कुछ याद नहीं रहता… पर ये बच्चा हर सुबह याद दिला देता है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ।” यह संवाद मात्र एक वाक्य नहीं, बल्कि उन हज़ारों बुज़ुर्गों की आवाज़ है जो अपने परिवारों से नहीं, बल्कि अपनत्व से कटे हुए हैं। ये फिल्म उस चुप्पी की व्याख्या करती है, जो बूढ़े हो चुके चेहरों में हमेशा गूंजती रहती है।
बल्लू का किरदार, फिल्म की आत्मा है। वह न तो दया माँगता है, न किसी बड़े सपने का बोझ उठाता है। उसका जीवन बस इतना भर है कि वह आज किसी के साथ चल सके, आज कहीं बैठकर खाना खा सके, और आज की रात डर के बिना सो सके। दैविक बाघेला की सहजता इतनी असाधारण है कि वह अभिनय और वास्तविकता की सीमाओं को मिटा देती है। उसके चेहरे पर जो उम्मीद है, वह किसी क्रांतिकारी घोषणापत्र से बड़ी लगती है।
‘कालीधर लापता’ का हर दृश्य ठहरा हुआ है, पर उसमें गति की आंतरिक छाया है। जैसे नदी थमती नहीं, लेकिन किनारों को चुपचाप छूती जाती है। यह फिल्म भी अपने दर्शकों को कहीं छू जाती है—बिना शोर किए, बिना आक्रोश के।
इस फिल्म में एक गहरा सामाजिक संदर्भ भी है—हम कैसे अपने बुज़ुर्गों के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं, कैसे वृद्धाश्रम और कुंभ मेले हमारी सामूहिक स्मृति से छूटे हुए नामों की कब्रगाह बनते जा रहे हैं। ‘कालीधर लापता’ सिर्फ एक आदमी के लापता होने की दास्तान नहीं है, यह हमारी करुणा, हमारी संवेदना, और हमारे पारिवारिक मूल्यों के धीरे-धीरे ग़ायब होते जाने का शोकगीत है।
लेकिन फिल्म केवल करुणा का आख्यान नहीं बनती। वह जीवन का उत्सव भी है। कालीधर की उस मुस्कान में जब वह बल्लू को देखता है—एक नई सुबह की संभावना है। उसमें यह विश्वास है कि जीवन चाहे कितना भी टूटा हुआ हो, उसमें जुगनुओं की रोशनी बची रहती है।
यह फिल्म अपने दर्शक से समय माँगती है, धैर्य माँगती है, और फिर उसे एक ऐसी सौगात देती है जिसे वो अपने भीतर लंबे समय तक सँजो कर रख सके।
जब ‘कालीधर लापता’ अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, तो यह किसी रहस्य का समाधान नहीं, बल्कि एक आत्मिक पुनर्मिलन की ओर अग्रसर होती है—नायक का अपने अतीत से, दर्शक का अपनी स्मृति से, और समाज का अपनी अनदेखी संवेदना से। यह फिल्म अंत की ओर भागती नहीं, वह थमती है, रुकती है, और धीरे-धीरे अपने दर्शकों के भीतर उतरती है, जैसे पुराना कोई सपना जिसे ठीक-ठीक याद नहीं, पर जिसकी छाया दिल में अब भी है।
जब कालीधर का सामना दोबारा अपने घरवालों से होता है—यह एक सामाजिक क्षमा या पुनर्मिलन का क्षण नहीं है, यह एक अंतर्संघर्ष की कड़ी है। क्या वे अब उसे स्वीकारेंगे? क्या अब वह स्वीकार करना चाहेगा? फिल्म यहाँ निर्णय नहीं देती, वह दर्शक पर छोड़ती है—क्या परिवार वह होता है जो जन्म देता है, या वह जो साथ निभाता है? बल्लू और कालीधर की दोस्ती इस प्रश्न का एक नया उत्तर बनकर उभरती है—संबंध वह होता है जो प्रेम और समर्पण से बना हो, चाहे वह खून का न हो।
सुबोध की यात्रा भी पूरी होती है—एक खोया-पाया अफसर की भूमिका निभाते-निभाते वह खुद बहुत कुछ पा चुका होता है। वह सिर्फ लोगों को नहीं ढूँढता, बल्कि अपने भीतर की खोई करुणा को, अपने पेशे की थकी हुई आत्मा को फिर से पा लेता है। ज़ीशान अय्यूब का अभिनय इस मोड़ पर गहराता है—कम बोलकर भी बहुत कह देना, यही इस किरदार की खूबी बनती है।
मीरा की स्मृति में लौटना—फिल्म को एक भावुक रेखा देता है। उसका आना फिल्म में कहीं ‘प्रेम के अधूरे हिस्से’ की पूर्ति नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि स्मृति, जब भी लौटती है, कोई आंसू या पीड़ा साथ नहीं लाती—वह सिर्फ एक मौन उपस्थिति होती है, जो बताती है कि बीते हुए समय की गरिमा बची हुई है।
फिल्म का अंतिम दृश्य—जहाँ कालीधर और बल्लू किसी बस की छत पर बैठे हैं, और नीचे फैला है रास्ता, दोनों तरफ़ खेत, दूर किसी स्टेशन की सीटी, और आसमान में पंछियों की एक कतार—यह दृश्य किसी फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं, एक गीत की अंतिम पंक्ति जैसा है। कोई तर्क नहीं, कोई नैतिकता नहीं—बस जीवन का एक ठहरा हुआ चित्र, जो बहुत कुछ कहता है बिना बोले।
‘कालीधर लापता’ हमें सिखाती नहीं, दिखाती है। वह संदेश नहीं देती, अनुभव कराती है। उसमें कोई उपदेश नहीं, पर अनुभवों की ऐसी बुनावट है जो लंबे समय तक भीतर बनी रहती है। यह फिल्म उस मौन की तरह है, जो किसी कविता के बाद होता है—जहाँ कोई ताली नहीं बजती, लेकिन हृदय से कोई स्पंदन उठता है।
और अभिषेक बच्चन—उन्होंने इस भूमिका में अपने अभिनय का नहीं, बल्कि अपने भीतर के जीवन अनुभवों का रंग डाला है। उन्होंने इस चरित्र को निभाया नहीं, इसे जिया है। कालीधर के थके हुए कंधे, उसकी बहकी हुई नज़रें, और कभी-कभी एकदम स्पष्ट हो उठती उसकी मासूमियत—ये सब किसी बड़ी अभिनय पाठशाला का हिस्सा नहीं, बल्कि एक गहरे आत्म-अन्वेषण का परिणाम लगते हैं। यह उनकी अभिनय यात्रा का सबसे आत्मीय, सबसे सघन और शायद सबसे सच्चा मोड़ है।
‘कालीधर लापता’ देखने के बाद आप बदलते नहीं, आप थोड़े और सहृदय हो जाते हैं। थोड़ा और ठहरने लगते हैं। आपको याद आता है—कभी किसी मोड़ पर आपने भी किसी को खो दिया था, या शायद… खुद को। और तब, कहीं भीतर से कोई आवाज़ आती है—”मैं लापता नहीं हूँ… बस थोड़ा ठहर गया हूँ… और तुमने मुझे फिर से ढूँढ़ लिया।”
‘कालीधर लापता’ कोई सिनेमा नहीं, वह एक धड़कती हुई कथा है—जिसके हृदय में अकेलापन, स्मृति, त्याग और करुणा की गहरी लहरें हैं। यह फिल्म न तो मनोरंजन के परंपरागत पैमानों पर चलती है, न ही कोई सस्ते भावुक क्षण रचती है। यह हमें भीतर से जगा देने वाली चुप्पी देती है—वह चुप्पी जो किसी बूढ़े पिता की आँखों में बसती है, जिसे उसकी ही संतान मंदिर या मेले में छोड़ आई है।
यह फ़िल्म दरअसल हमसे हमारा ही चेहरा माँगती है—एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में। हम कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि प्रेम की ज़रूरत उम्र नहीं देखती, और कि किसी की याददाश्त खो जाना उतना भयावह नहीं, जितना किसी को जानबूझकर भुला देना।
अभिषेक बच्चन का अभिनय, दैविक बाघेला की मासूमियत, ज़ीशान अय्यूब की संवेदनशीलता और मधुमिता सुंदररामन का निर्देशकीय कौशल—इन सबका सम्मिलित प्रभाव इतना मौन और प्रभावी है कि फिल्म देखने के बहुत देर बाद तक वह मन में बजती रहती है, जैसे दूर कहीं से आती एक धीमी बाँसुरी की तान।
‘कालीधर लापता’ हमें यह सिखाती है कि खो जाना भी कभी-कभी एक राह होती है—खुद तक पहुँचने की, किसी दूसरे का साथ पाने की, और यह जानने की कि सबसे पुख्ता रिश्ते वे होते हैं, जो रक्त से नहीं, दया और सहानुभूति से बने होते हैं।
इस फिल्म को देखा जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि आवश्यक है—आज के इस समय में, जब हम तेजी से अपने भीतर के कालीधर को खोते जा रहे हैं, और भूलते जा रहे हैं कि हमें एक बल्लू की ज़रूरत है—जो हमारी उँगली थामकर कह सके—”चलो, फिर से जीते हैं।”
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.