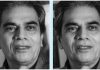— कुमार शुभमूर्ति —
हम गांधीवादी लोग नेहरू की कुछ बातों के कटु आलोचक रहे हैं। खासकर उनकी जो औद्योगिक-आर्थिक नीति थी उसे हम गांधी विरोधी बताते थे और वह आलोचना ठीक ही थी।
लेकिन लोकतंत्र के प्रति उनका लगाव सर्वस्पर्शी था। जनता उन्हें जितना प्यार करती थी वह भारत की जनता को उससे ज्यादा प्यार करते थे।
उन्हें ठीक ही गांधी का राजनैतिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। राज्य के प्रभाव की सीमाएं उनके सामने स्पष्ट थीं। लोक शक्ति का महत्त्व वे समझते थे और इस शक्ति को सशक्त बनाने का काम कितना कठिन है यह भी जानते थे। इसलिए उनका पूरा सहयोग विनोबा और जयप्रकाश जी को मिला था।
कानून की संगठित हिंसा के बल पर चलनेवाली राज्यसत्ता को कैसे अहिंसा की दिशा में ले जाएं उनकी यह एक खोज हमेशा रही। लोकतंत्र तो इसका एक बना-बनाया रास्ता था ही ,परंतु इसे और चौड़ा बनाने के लिए उन्होंने अनेक जोखिम उठाए।
कश्मीर की जनता को बिना मांगे अहिंसा और लोकतन्त्र की दृष्टि से जनमत संग्रह का वायदा करना, श्यामाप्रसाद मुखर्जी को हिंदुत्ववादी होने के बावजूद मंत्रिमंडल में शामिल करना आदि कुछ जोखिम भरे कदम तो थे ही लेकिन सबसे बड़ा जोखिम नेहरू जी ने चीन के संदर्भ में उठाया।
तिब्बत और चीन के ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए तिब्बत पर चीन के कब्जे को उन्होंने ज्यादा महत्त्व नहीं दिया। बौद्ध मठों का आम तिब्बतियों के प्रति मठवादी व्यवहार और माओ की जनवादी सर्वप्रिय नेता की छवि ने भी तिब्बत की समस्या के प्रति उनके मत को प्रभावित किया होगा।
तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद चीन भारत के लिए भी एक खतरा बन सकता है यह स्पष्ट था। उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल ने चेतावनी भी दी थी। चीन ने स्वयं भी इस ओर इशारा कर दिया था कि तिब्बत और भारत की सीमा चीन को मान्य नहीं है। अब क्या करें? क्या फौजी तैयारी?
आर्थिक रूप से बर्बाद होकर सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुए देश का उस वक्त फौजी तैयारी में लगना क्या ठीक था? ऐसा होता तो इसके दो ही अर्थ थे।
एक तो यह कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फौजी ताकत की दृष्टि से, दो गुटों में बंटी दुनिया के किसी एक गुट में शामिल हो जाना और दूसरा यह कि शस्त्रों की दौड़ में कूद पड़ना। दोनों रास्ते मूलतः एक ही थे, और गांधी के राजनैतिक उत्तराधिकारी नेहरू को स्वीकार्य नहीं थे।
गांधी से ही सीखा था एक सपना देखना कि हिंसा से अलग जो शक्तियां हैं उनकी दुनिया में कैसे चले।
यही सपना व्यावहारिक भी था। शस्त्रों की दौड़ न सिर्फ बहुत सारा पैसा खा जाती है, दिमाग ही बदल देती है। योजनाओं की प्राथमिकता बदल जाती है।
देश के वास्तविक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचों का बनना जरूरी था। देश की भूखी-नंगी जनता की बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा होना जरूरी था। आधुनिक जमाने के नए तीर्थों का बनना जरूरी था।
नेहरू ने युद्ध नहीं संवाद की रणनीति अपनायी। चीन को इसमें बांधना चाहा ।1955 के बांडुंग सम्मेलन में “पंचशील करार” पर चीन समेत सभी प्रमुख एशियाई देशों के हस्ताक्षर हुए। चीन भी सामूहिक रूप से वचनबद्ध हुआ, कि सीमा विवाद युद्ध से नहीं बल्कि वार्ता से ही सुलझाया जाएगा।
दुनिया के सामने चीन ने दिए गए वायदे को तोड़ दिया। भारतीय फौज लगभग नि:शस्त्र थी। भारत युद्ध हार गया। नेहरू धोखा खा गए। कहते हैं इसी सदमे से उनकी मृत्यु हो गयी।
अधिकांश लोग इस प्रकरण का जिक्र आते ही चीन की फजीहत करने के बदले नेहरू की फजीहत करने में लग जाते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में, यह नेहरू का अंतरराष्ट्रीय सत्ता और शस्त्रों की होड़ में अहिंसा को दाखिल करने का स्वर्णिम प्रयोग था। यह प्रयोग यदि सफल हो जाता तो आज दुनिया युद्ध से ही नहीं आतंकवाद से भी मुक्त हो गयी होती।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.