
यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है कि देश की दशा और दिशा के मूल्यांकन और आगे का रास्ता अपनाने के लिए सरोकारी व्यक्तियों के बीच चारों तरफ महत्त्वपूर्ण संवाद हो रहे हैं। इस प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देते हुए यह याद दिलाने की जरूरत है कि हम किसी एक व्यक्ति, गिरोह, दल या गठबंधन से ही त्रस्त नहीं हैं बल्कि ‘उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण’ के भयंकर नतीजों का सामना रहे हैं। हमारी मुख्य समस्याओं का बीजारोपण और अंकुरण पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ है। आजकल के सताधीशों द्वारा इसे ज्यादा खाद-पानी दिया जा रहा है और ज्यादा जहरीले फल सामने आ रहे हैं।
लेकिन इसको समझने में देर क्यों हुई है? इसके तीन कारण तो स्पष्ट हैं। एक तो 1990-2010 के बीस बरसों में हमारे मध्यम वर्ग का तात्कालिक विस्तार हुआ और उसे भोगवाद के वैश्विक मायामृग ने देशहित से दूर भटका दिया। लेकिन वैश्विक पूंजीवाद की नाव की आर्थिक राष्ट्रीयता से टकराहट के कारण मध्यम वर्ग को अपनी भौगोलिक सीमाओं में बने रहने की विवशता की समझ हो रही है। इसीलिए वह ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ से लेकर ‘धार्मिक एकरूपता’ जैसे नारों से नया सामाजिक आधार बनाने की प्रवृत्ति को बल देने में जुट गया है।
दूसरे, भारत में संसदवाद और चुनाववाद की आड़ में ‘अस्मिता’ की राजनीति के बहाने नागरिक हितों की बजाय जाति-गठबंधनों और धार्मिक भेदभाव की धुंध को बढ़ाया गया है। 1974 से ही बताये जा रहे जरूरी चुनाव सुधार और राजनीतिक दल-व्यवस्था में सुधार को न करने के पाप ने इस भयानक रोग को फैला दिया है। बिना बुनियादी सुधारों के हम एक बीमार लोकतंत्र की भ्रष्ट चुनाव व्यवस्था और अलोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था के साथ जीने के अभ्यस्त हो रहे हैं।
अब बिना चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों के सुधार के हम इस दलदल में लंबे समय के लिए फँसे रहने को अभिशप्त राष्ट्र और समाज हो गए हैं। इसे हमारे पिछले पांच सौ साल के इतिहास की बुरी यादों और भारत-विभाजन के जिंदा सवाल से बल मिल रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान के बुनियादी मुद्दों को ‘पाकिस्तान-रमजान-कब्रिस्तान- मुसलमान’ के शोर में दबाने में सफलता पाए राजनीतिक गिरोह को सत्ताच्युत करने के लिए तात्कालिक दलीय गठबंधनों से ज्यादा हमारी ऐतिहासिक स्मृतियों, सामाजिक व्याकरण और आर्थिक दिशा के बारे में नई राष्ट्रीय सहमति की रचना की जरूरत है।
तीसरे, चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना संकट ने हमारे बाजार केन्द्रित पूंजी-संचय के आर्थिक आधार की कच्ची नींव का सच दिखाया है। उत्पादन, प्रबंधन और खपत के लिए नगरों और उद्योगों की गाँवों पर निर्भरता का उपेक्षित सच ‘नई आर्थिक नीतियों’ के क्षणभंगुर परिणामों से मोह खतम कर चुका है। यह साफ कहने का समय आ गया है कि भारत के टिकाऊ नव-निर्माण का रास्ता देश के साढ़े पांच लाख गाँवों और सात सौ जिलों से गुजरता है। इन तीन पाठों के प्रकाश में नई राह अपनाने की जरूरत है। सब मिलकर ‘दवाई – कमाई – पढ़ाई – सफाई’ के संकट से जूझ रहे करोड़ों स्त्री-पुरुषों के सहयोगी बनने की राह अपनाएंगे। इन सवालों पर आगे आने के लिए जेलों में बिना मुकदमों के गिरफ्तार हजारों लोकतंत्र रक्षक देशवासियों की ‘रिहाई’ में भी मददगार बनेंगे।
यह निर्विवाद सत्य है कि हमारा देश एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। लेकिन फुटकरिया प्रतिरोध के अलावा किसी तरफ से नीति आधारित कार्यक्रमों से लैस लोकतांत्रिक राजनैतिक विकल्प की दावेदारी नहीं है। देश के पास 1973-74 वाले जयप्रकाश नारायण नहीं हैं। कांग्रेस के पास 1963-65 वाले लालबहादुर शास्त्री या फिर 1969-71 की इंदिरा गांधी नहीं हैं। समाजवादियों के पास 1963-67 वाले लोहिया नहीं हैं। वामपंथियों के पास 1972-77 वाले ज्योति बसु, नम्बूदरीपाद, इंद्रजीत गुप्ता और त्रिदिब चौधरी नहीं हैं। क्षेत्रीय दलों के पास 1974-77 वाले बीजू पटनायक, एन. टी. रामाराव, चौधरी देवीलाल, और गोलप बरबोरा नहीं हैं।
इस तरह हमारे मौजूदा संकट के कई चेहरे हैं।
फिर भी (क) गहरा आर्थिक गतिरोध, (ख) सामाजिक बिखराव, (ग) राजनीतिक टकराहटें, (घ) चीन से लेकर पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के साथ सीमाओं की सुरक्षा का संकट, और (च) विद्यार्थियों-नौजवानों से लेकर किसानों तक चौतरफा असंतोष इसके पांच बहुचर्चित लक्षण हैं। बैंक और नियोजन व्यवस्था से लेकर सेनासंगठन और शिक्षा और शोध के केंद्रों को अस्त-व्यस्त करने के बाद प्रधानमंत्री किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए हैं। दिल्ली से लेकर नागपुर और लखनऊ तक बेहतर विकल्प की तलाश की अफवाह का बाजार गरम है। गृहमंत्री नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता कानून से खिलवाड़ के बाद पस्त हैं। वित्तमंत्री और रेलमंत्री पूंजीपतियों के मान-मनौवल में व्यस्त हैं। विदेशमंत्री और रक्षामंत्री एक दूसरे की समझदारी के प्रति आशंकित हैं। कृषिमंत्री और व्यापार मंत्री एक दूसरे की आड़ ले चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय में छह साल में तीन मंत्रियों को लाया-हटाया गया और दिल्ली विश्वविद्यालय समेत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ‘राग-दरबारी’ न गाने के कारण अपमानित-लांछित किया जा चुका है।
इस संकट से देश में बेचैनी का ज्वार आ गया है। मनचले अरबपतियों के दबाव और राष्ट्रहितकारी दूरदृष्टि के अभाव में केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन बिखर रहा है। पहले महाराष्ट्र में शिवसेना छिटकी फिर पंजाब में अकाली दल हटा। असम का गठबंधन टूट गया है। बिहार का जनता दल (यू) से गठबंधन मरणासन्न है। उत्तराखंड में तो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के उलझने से मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। लेकिन इससे विकल्प निर्माण की प्रक्रिया को बल नहीं मिल रहा है।
विपक्ष में कांग्रेस मुख्य और एकमात्र राष्ट्रव्यापी दल होने के बावजूद दिशाहीन है। मां–बेटे और भाई-बहन के बीच की घटती निकटता और बढ़ती दूरी के किस्सों के बीच शिखर-राजनीति के कम से कम तेईस दिग्गजों को संदेह के घेरे में मान लिया गया है। मध्यप्रदेश में चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेसजन देखते देखते सरकार से हटाए गए। हरियाणा में अंदरूनी विवाद के कारण पराजय का शिकार हुए और अब पराजित कांग्रेस के भीतर से ही एक क्षेत्रीय दल भी पैदा हो गया है। कांग्रेस ने बंगाल में वामपंथी मोर्चे के साथ गठबंधन किया है और केरल के चुनाव में वामपंथी गठबंधन के खिलाफ गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में है। बाकी दलों ने एकाध परिवारों, एकाध जातियों और भाषाई समुदायों की पूंछ पकड़ने में ही भलाई मान ली है।
इधर दुनिया देख रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र, सबसे युवा देश, दूसरी सबसे बड़ी मानव संसाधन लैस आर्थिकी और तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था और तीसरी बड़ी सेना के दावों के बीच समग्र मानवीय विकास अर्थात स्वास्थ्य-शिक्षा-आजीविका की दृष्टि से 193 देशों में बाजार-आधारित वैश्वीकरण के तीन दशकों के बाद भी भारत अभी तक 129वें स्थान पर ही पहुँच पाया है। यह बहुचर्चित रहा है कि चीन हमसे 39 सीढ़ी ऊपर 90वें स्थान पर है। लेकिन अब बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है।
हमारे सत्ता-प्रतिष्ठान के तुगलकी तौर-तरीकों को देखते हुए दुनिया हमें अब लोकतांत्रिक देशों की बिरादरी में मानने से इनकार करने लगी है। वैसे भी ‘सूचना क्रांति’ के युग में मीडिया की आजादी की दृष्टि से हम दुनिया में 116वां देश हैं। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के मामले में हमारा देश 113वें पायदान पर है तभी देश में कम से कम पांच करोड़ बच्चे विद्यालयों में विद्यार्थी होने की बजाय खेतों-कारखानों में श्रमिक बने हुए हैं। स्त्रियों के साथ हिंसा और भेदभाव के पैमाने पर हम 112वें पायदान पर हैं। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद स्त्री-सशक्तीकरण के लिए निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी की जरूरत उपेक्षित है। भूख की व्यापकता के पैमाने पर भारत 94वें स्थान पर है और भ्रष्टाचार के फैलाव में हम 80वें स्थान पर पहुँच गए हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों और जन आंदोलनों की उपेक्षा बढ़ने से जल-जंगल-जमीन-जैव विविधता की रक्षा के मोर्चे पर हमारा देश दुनिया में 168वें स्थान पर चला गया है।
इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि देश को तीन दशकों से जारी ‘नई आर्थिक नीतियों’ की आड़ में वैश्विक वित्तीय पूंजी के स्वामियों की मनमर्जी पर छोड़ने का सिलसिला बढ़ गया है। इसके दुष्परिणामों से परेशान जनसाधारण के आक्रोश से बचने के लिए सांप्रदायिक आधार पर बाँट कर चुनावी शतरंज की चालबाजियों के जरिये वित्तीय पूंजी का राज चलाने का दुस्साहस हो रहा है। हमारा देश 1. न्यायपूर्ण नव-निर्माण, 2. सुशासन, 3. सहभागी लोकतंत्र, 4. पर्यावरण संवर्धन, 5. बंधुत्व आधारित नागरिकता, 6. लोकतांत्रिक राष्ट्रनिर्माण और 7. स्वच्छ राजनीतिक व्यवस्था के संविधान-सम्मत लक्ष्यों से भटकाया जा चुका है।
(लेख का बाकी हिस्सा कल)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.











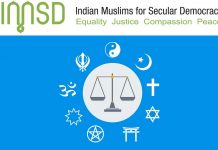






आनंद कुमार जी का यह आलेख एक सजग समाज शास्त्री की सजग सोच का सजग दस्तावेज हैं ।
इस अपूर्व सजग विश्लेषणात्मक दस्तावेज को सभी सजग जन अधिकतम प्रसारण में योगदान कर सजग नागरिक धर्म का सजग निर्वाह करें; यही अभ्यर्थना.
आनंद कुमार जी व ‘समता मार्ग ‘ का अत्यंत आभार.
आलेख के द्वितीय भाग की प्रतीक्षा है.
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ.
🌷📖🙏