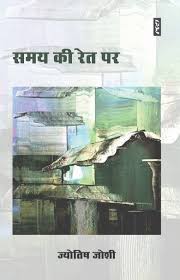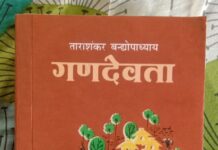— शर्मिला जालान —
प्रख्यात लेखक, आलोचक ज्योतिष जोशी ने लगभग दो दशक पहले ‘सोनबरसा’ उपन्यास लिखा था। तेईस साल के बाद उनका दूसरा उपन्यास समय की रेत पर प्रकाशित हुआ है। यह जिज्ञासा थी कि आखिर कौन सी छटपटाहट और बेचैनी लेखक के अंदर होती है जो उसे दो दशक बाद फिर से उपन्यास लिखवा लेती है? इस जिज्ञासा में ‘समय की रेत पर’ उपन्यास पढ़ गई। उपन्यास पढ़ते हुए यह बात भी मन में थी कि ज्योतिष जोशी जी का बहुत सारा काम समीक्षा, आलोचना के क्षेत्र में है, देखना चाहिए कि उनकी भाषा उपन्यास का निर्वाह किस तरह से करती है। उपन्यास पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगा कि किसी आलोचक, समीक्षक अकादमिक विद्वान की पुस्तक है। सहज सुंदर संवेदनशील पठनीय भाषा में किसी लेखक, उपन्यासकार का उपन्यास पढ़ने का सुखद अनुभव हुआ। ‘समय की रेत पर’ का गद्य पढ़ते हुए कोई व्यवधान पैदा नहीं होता है, लेखक की भाषा अकादमिक बोझ नहीं डालती। बीच-बीच में आए भोजपुरी शब्द और वाक्य आंचलिक पृष्ठभूमि को बतातेहैं। भाषा सधी हुई है जिसमें संतुलन है, स्वाभाविक लगती है, सहज प्रवाह है। मित्रता-प्रेम साहचर्य प्रसंग में भाषा का तरंगित रूप देखते हैं।
उपन्यास का ‘आरम्भिक’ कृति में दिलचस्पी पैदा करता है और यह शिल्प शरत बाबू के उपन्यास की याद दिलाता है। कथा विगत की स्मृति में चलती है- फ्लैशबैक टेकनीक।
यह कहानी पूर्वांचल प्रदेश के प्रवासी प्रभाकर तिवारी के जीवन संघर्ष की महागाथा है। जिसके पिता गरीब माँ-बाप की संतान थे। दादा को बँटवारे में मिली जमीन देसी रियासत के कर्ज में नीलाम हो गयी थी। ग्यारह साल की उम्र में पिता 1940-1945 के समय कलकत्ता न जाकर आसाम कमाने के लिए गए थे। आसाम और बंगाल पूरबियों के लिए जीने का आसरा थे। दादा के मरने के बाद पिता ने खेती और गृहस्थी में खुद को लगाया। फिर अपने बेटे प्रभाकर तिवारी की ग्यारह साल की उम्र में शादी कर दी। घर में पैसों का टोटा हो गया।
यह कथा प्रभाकर तिवारी के माध्यम से एक परिवार की कहानी है। यह रोजनामचा नहीं है बल्कि जिस ग्राम में जन्म लिया वहाँ का सहारा छूटने और दिल्ली में काम खोजने, अपमानित होने, गिर कर सॅंभलने की अथक तलाश है।
“यह बीसवीं सदी के नवें दशक का हाल था जब दिल्ली को पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी जागीर समझते थे और ‘बिहारी’ का संबोधन गाली की तरह उनकी जबान पर हरदम चिपका रहता था। उन दिनों की दिल्ली शोर-शराबे और भीड़ से भले कमतर थी, पर बड़ी बेदिल लगा करती थी। अपमान, उपालंभ और गालियां खाते पूरबिये यहाँ खून का घूँट पीकर जीते। लड़ते तो जाते कहाँ और फिर उनका क्या होता। चाहे बस हो या फैक्ट्री, कॉलेज हो या स्कूल, दुकान हो या ढाबा, कोई ऐसी जगह न बची थी जहाँ बिहारी का जुमला आम न हो और सरेआम गलियाँ न मिलती हों। किसी से अगर कहासुनी हो भी जाए तो कथित भद्रलोक बीच-बचाव कर चुप करा देते पर गाली देने वाले को कुछ न। यह दिल्ली है, यही दिल्ली है जिसके सपने देखता वह यहाँ आया है।”
इसके समानांतर 90 के दशक के हिंदुस्तान का राजनीतिक और सामाजिक जीवन भी हमारे सामने आता है। घर के अंदर का कलह, तनाव, अवसाद और राजधानी दिल्ली का डराने वाला रूप, पग-पग पर साँस लेती हुई कई जिंदगियों से हम रू-ब-रू होते हैं।
यह कृति प्रभाकर तिवारी के दिल्ली प्रवास के लगभग पांच-छह वर्षों के जीवन की माइक्रो स्टडी है। प्रभाकर तिवारी अंदर से प्रौढ़ है। उसकी परिपक्वता ने उसे जीवन जीने, सॅंभालने का साहस दिया है। उपन्यास में आते हुए छोटे-छोटे कई प्रसंग, दिल्ली में आकर, रहने की कोशिश करने वाले युवकों की टूट-बिखर कर फिर से बसने की करुण कथा कहते हैं। बाहर से ठीक-ठाक दिखाई देने वाले जीवन के अंदर का ॲंधेरा हमें दिखाई पड़ता है। 20 वर्ग गज पर खड़े मकान के जीवन, वहाँ रहने-बसने वालों की इच्छाओं-आकांक्षाओं और उसके सच को हम देख पाते हैं।
“रात को जब तीनों जुटते तो दुख एक ग्रंथ की तरह खुल जाता जिसे कोई एक भी पढ़ता तो सब की कथाएँ दृश्य की तरफ खुलती जातीं। दुख फटे कपड़ों में था। औंधे पड़े एल्युमीनियम के बर्तनों में, तेज आवाज़ से भभक उठने वाले पुराने स्टोर में था। बीस गज के प्लॉट पर खड़े इस कमरे की जर्जर दीवारों में था, तो उस फोल्डिंग चारपाई में भी था जिसका एक कोना जाने कैसे तिरछा खड़ा हो गया था कि वह चारों पायों पर बैठती न थी। दुख था तो उसको भेदने के ये तीन बांकुड़े भी थे जो उसे खुशी-खुशी जी कर उसका स्वागत कर रहे थे।”
इस उपन्यास को पढ़ते हुए राजेंद्र यादव का उपन्यास ‘सारा आकाश’ याद आता है। उस उपन्यास में मुख्य पात्र समर की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। विवाह के बाद नौकरी और पढ़ाई की जद्दोजहद में उसका जीवन लहूलुहान होता रहता है। यह उपन्यास कभी-कभी मुझे ‘सारा आकाश’ के समर जैसे युवकों का परवर्ती जीवन लगता है। समर परिवार से दूर दिल्ली नहीं गया लेकिन जो दिल्ली चले जाते हैं वहाँ वह अपने लिए क्या कर पाते हैं, अपने को कैसे खड़ा करते हैं, कैसे बिखरते-अकेले पड़ते हैं, उसकी व्यथा ‘समय की रेत पर’ में करुण कथा बनकर बहती दिखाई देती है |
उपन्यास अपने दम पर अपने जीवन को बनाने, सॅंभालने की अथक कोशिश की कहानी है। यहाँ पर एक के बाद एक नौकरी पाने और उसे छोड़ने का सिलसिला दिखाई देता है। प्रभाकर किसी भी काम में ज्यादा महीने तक नहीं टिकता। नौकरी का छल, पाखंड, सतहीपन उसे जैसे ही दिखता है उसका स्वतंत्र मन उस काम को छोड़कर दूसरे काम की तलाश में लग जाता है। इस प्रक्रिया में दिल्ली में रहने, एम.ए. , एम.फिल. पीएचडी करने दो रोटी कमाने, परिवार को पैसा भेजने की जद्दोजहद में लगे युवकों के जीवन संघर्ष को हम बारीकी से देख पाते हैं। प्रभाकर तिवारी बाईस वर्ष की अवस्था में माँ की मउनी में रखे तीन सौ रुपये लेकर निकल गया था और दिल्ली में वह लहूलुहान होने लगा। राजधानी में उसे कई तरह के अनुभव होते हैं। सिवान के मैरवा का रमेश विश्वकर्मा जो पूरे हैदरपुर गाँव में ‘रमेश अंडा’ नाम से जाना जाता है, अंडे की रेहड़ी लगाता है जैसे युवकों से मिलता है।
वहाँ रहने, पढ़ने वाले युवक उनके प्रेम और वैवाहिक जीवन की झंझट, असफल प्रेम विवाह की परिणतियाँ, प्रभाकर तिवारी के साथ कुमुद का प्रसंग यह ऐसी कथाएँ हैं जो दिल्ली के कई चेहरे दिखाता है। यहाँ मंडल-कमंडल की बात है। देश की राजनीति में उदारीकरण ने किस तरह से मध्यवर्गीय जीवन को ऊपर-ऊपर से क्या और कितना बदल डाला है उस नकली जीवन की सच्चाई है। प्रभाकर के व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन, ग्रामीण जीवन और महानगर के जीवन का द्वंद्व यहाँ पर दिखाई देता है। एक नट जिस प्रकार पतली रस्सी पर सॅंभल-सॅंभल कर चलता है वैसे ही प्रभाकर तिवारी दिल्ली में अपने जीवन को सॅंभालते, बचाते हुए चल रहा है।
सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के निदेशक की अवैध कारगुजारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के कारण बीमार होने के बावजूद उसका गलत तबादला कर दिया जाता है। उसकी स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता है। उसे क्या रोग है पता नहीं पर वह बार-बार अचेत हो जाता है। कभी माँ को पुकारता है, कभी कुमुद को याद करता है, कभी पत्नी की स्मृति हो आती है। एकसाथ कई मोर्चों पर लड़ता हुआ चालीस वर्ष की अवस्था में अकेला है।
उपन्यास पढ़ते हुए जैसे-जैसे हम अंत की तरफ जाते हैं अचानक उपन्यास का समापन हो जाता है। सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के घपले के बारे में बहुत संक्षेप में लेखक ने लिख कर छोड़ दिया। ऐसा पहली बार में लगता है दूसरी बार लगता है लेखक का उद्देश्य प्रभाकर तिवारी के शुरुआती संघर्ष की माइक्रो स्टडी करना है, राजधानी दिल्ली के दहला देने वाले संघर्ष को लिखना है।
पाठक के मन में यह प्रश्न भी आता है कि बचपन की शादी जो बिना सोचे-समझे कर दी जाती है उसकी क्या परिणति है? विवाह और परिवार संस्था, पर प्रश्न पैदा होता है? अभिभावक संतान से अतिरिक्त उम्मीद करते हैं। वह बालक जो पूरी तरह से शिक्षित और आत्मनिर्भर भी नहीं बना वह संतान परिवार को कैसे देखेगी? प्रभाकर तिवारी परिवार से मुँह नहीं मोड़ता। वह लगातार परिवार की चिट्ठियों का इंतजार करता है। अपनी पत्नी और बच्चों को दिल्ली लाना चाहता है। इस तरह प्रभाकर तिवारी एक ऐसे चरित्र के रूप में उभरता है जो धीरज, संयम, विवेक के साथ अपने जीवन में आई हर चुनौती का सामना करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। हर संकट पर विचार करता है, चाहे वह उसके जीवन में आया हुआ कुमुद का प्रेम प्रसंग ही क्यों ना हो वह एक ऐसे आदर्श चरित्र के रूप में इस उपन्यास में आता है जिसकी जीत हुई है या हार, पता नहीं, पर जो अंत में अकेला है।
किताब : समय की रेत पर (उपन्यास)
लेखक : ज्योतिष जोशी
प्रकाशन : सेतु प्रकाशन; सी-21, सेक्टर 65, नोएडा-201301
[email protected]
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.