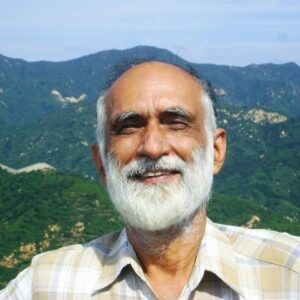
आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भी भारत का विचार समस्याग्रस्त बना हुआ है क्योंकि यह राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़ा है, वह राष्ट्र जो हम बनना चाहते हैं. चूँकि राष्ट्रवाद के कई मॉडल मौजूद हैं, इसलिए यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है कि किसका अनुकरण किया जाए. समकालीन समय में हम राष्ट्रवाद के दो प्रतिस्पर्धी मॉडलों के बीच संघर्ष का सामना कर रहे हैं- सावरकर का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गांधी का नागरिक राष्ट्रवाद.
ध्रुवीकृत सांप्रदायिक पहचानों के तनावपूर्ण माहौल में इन दोनों मॉडलों को गहराई से समझना ज़रूरी है ताकि हम एक समझदारी भरा चुनाव कर सकें. इस लेख का उद्देश्य यही है. इसलिए पहले खंड में, हम आधुनिक राष्ट्रवाद की विचारधारा और पश्चिम में इसके दो प्राथमिक रूपों के विकास की ऐतिहासिक समीक्षा से शुरुआत करेंगे और उन्हें भारत में राष्ट्रवाद के विकास से जोड़ेंगे.
दूसरे खंड में धर्म, राजनीति, हिंसा, भारतीय पहचान और सभ्यता के बारे में सावरकर और गांधी के अलग-अलग विचारों पर प्रकाश डालेंगे.
तीसरे खंड में, हम यह समझने पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे उनके अलग-अलग विचारों ने उन्हें राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों को अपनाने के लिए प्रेरित किया.
अंतिम खंड में, हम बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक समाज के भारतीय संदर्भ में गांधीवादी और सावरकर मॉडल का मूल्यांकन करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा मॉडल शांतिपूर्ण भविष्य की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है.
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राष्ट्रवाद आधुनिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक के रूप में उभरा है. लेकिन पूर्व और पश्चिम के विचारकों के बीच इसकी परिभाषा को लेकर कोई आम सहमति नहीं है. हालाँकि इसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के यूरोप में देखी जा सकती है, लेकिन राष्ट्रवाद ने जो रूप धारण किए हैं, वे इतने विविध हैं कि उन्हें एक ही वैचारिक योजना के अंतर्गत लाना बहुत मुश्किल है. यहाँ तक कि ‘राष्ट्र’ की अवधारणा भी परस्पर प्रतिरोधी परिभाषाओं से भरी है.
राष्ट्र के राजनीतिक घटकों के विपरीत, इच्छाशक्ति और स्मृति जैसे व्यक्तिपरक तत्वों और क्षेत्र व भाषा जैसे अधिक वस्तुनिष्ठ तत्वों के बीच जातीयता की भूमिका को लेकर बहुत कम सहमति है. जब हम दूसरी प्रमुख अवधारणा, ‘राष्ट्रवाद’ पर विचार करते हैं, तो स्थिति में बहुत सुधार नहीं होता है. फिर, उन लोगों के बीच भी मतभेद है जो राष्ट्रवाद के राजनीतिक पहलुओं की बजाय सांस्कृतिक पहलू पर जोर देते हैं. कुछ लोग इसे ‘राष्ट्रीय भावना’ से जोड़ते हैं तो कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा और भाषा के साथ, और कुछ राष्ट्रवादी आंदोलनों के साथ. कुछ के द्वारा सुझाया गया कि दोनों तत्वों को शामिल करते हुए एक संश्लेषण भी संभव है. हालांकि, विभिन्न विद्वानों की विभिन्न परिभाषाओं से कुछ सामान्य विषयों को निकाला जा सकता है.
स्वायत्तता, एकता और पहचान/अस्मिता ऐसे विषय और आदर्श हैं जिनका राष्ट्रवादियों ने हर जगह अनुसरण किया है. राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और संप्रभुता का सिद्धांत है; लोगों को बाहरी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए ताकि वे अपने भाग्य के स्वामी स्वयं बन सकें. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लोगों को सभी आंतरिक विभाजनों को मिटाकर एकजुट होना होगा और एक ऐतिहासिक क्षेत्र में रहना होगा जो उनकी पवित्र मातृभूमि बन जाए, जहाँ एक ही सार्वजनिक संस्कृति पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक बहुमूल्य और पोषित विरासत के रूप में, उनकी प्रामाणिक पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में हस्तांतरित हो. रक्त, जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म और रीति-रिवाज, सभी इसमें भूमिका निभाते हैं.
जैसा कि हमारी उपरोक्त चर्चा से अनुमान लगाया जा सकता है, राष्ट्रवाद की दो मुख्य पर बिल्कुल अलग श्रेणियाँ हैं- सांस्कृतिक और राजनीतिक. ये राष्ट्र की प्रतिस्पर्धी अवधारणाओं पर आधारित हैं और इनके अपने विशिष्ट संगठन हैं, जो अपनी अलग-अलग राजनीतिक रणनीतियाँ अपनाते हैं.
राजनीतिक राष्ट्रवादी का आदर्श शिक्षित नागरिकों की एक ऐसी नागरिक व्यवस्था है जो समान कानून और नागरिकता से एकजुट हों. राष्ट्र की उनकी अवधारणा तर्कवादी है, और वे अंततः सांस्कृतिक मतभेदों से परे एक सामान्य मानवता की कामना करते हैं. इस प्रकार उनका उद्देश्य मूलतः आधुनिकतावादी है, जिसका लक्ष्य अपने समुदाय के लिए एक प्रतिनिधि राज्य सुनिश्चित करना है जहाँ सभी नागरिक एक महानगरीय, तर्कवादी सभ्यता के साथ खुद को फिर से जोड़ने में समान रूप से भागीदार हों.
राजनीतिक राष्ट्रवादियों के विपरीत, सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों के लिए राज्य एक संयोग मात्र होता है. उनके लिए, किसी राष्ट्र का मूल सार उसकी विशिष्ट सभ्यता है, जो उसके विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और भूगोल का परिणाम है. इस प्रकार, राष्ट्र जीवित व्यक्तियों, जैविक प्राणियों की तरह होते हैं, ना कि केवल राजनैतिक इकाइयों की तरह. उनकी विशिष्टता को संजोया जाना चाहिए और इसलिए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक विभाजनों के पक्ष में सार्वभौमिक नागरिकता के अधिकारों को अस्वीकार किया जाना चाहिए. वास्तव में, सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों का उद्देश्य एक विशिष्ट राष्ट्रीय सभ्यता के पुनर्निर्माण के लिए ऐतिहासिक समुदाय का नैतिक पुनरुत्थान करना है. इस उद्देश्य के लिए वे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी जातीय अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता का उत्सव मनाने और विदेशी प्रथाओं को अस्वीकार करने में विश्वास करते हैं.
इस प्रकार वे इस पहचान को अन्य समुदायों से अलग करते हुए अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करते हैं. इसलिए, वे अपने समुदाय को विकास के किसी भी सार्वभौमिक मॉडल, चाहे वह उदारवादी हो या समाजवादी, में समाहित करने का कड़ा विरोध करते हैं.
राजनीतिक राष्ट्रवाद ‘पश्चिम’ में उभरा, जहाँ पुनर्जागरण के बाद से एक परिष्कृत शहरी मध्यवर्गीय संस्कृति पहले ही विकसित हो चुकी थी, और राष्ट्र-राज्य की प्रभावी सीमाएँ या तो मौजूद थीं या बनने वाली थीं. तब राष्ट्रवाद ने एक संवैधानिक रूप धारण कर लिया. पूर्व में स्थिति अलग थी. यहाँ राष्ट्रवाद पश्चिम की तर्कवादी संस्कृति की अनुकरणात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा. चूँकि यहाँ कोई धर्मनिरपेक्ष मध्यवर्ग मौजूद नहीं था और समाज मुख्यतः कृषि प्रधान था, जिस पर प्रतिक्रियावादी अभिजात्य वर्ग का प्रभुत्व था, इसलिए राष्ट्रवादियों ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मृतियों और विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित एक दूरदर्शी राष्ट्र बनाने का प्रयास किया.
उन्होंने पश्चिम के तर्कवादी नागरिकता मॉडल के विरुद्ध किसानों, भूमि और समुदायों के बीच एक श्रेष्ठ, रहस्यमय, जैविक बंधन का दावा किया. इसके लिए कोई भी ‘कोहन’ और ‘गुलनर’ से सहमत हो सकता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा मौजूदा वैचारिक आधुनिकता से उत्पन्न संकट और बहिर्जात आधुनिकीकरण के प्रभाव के प्रति एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया है और इसके परिणामस्वरूप समुदाय के परंपरावादी मूल्यों की पुनः स्थापना हो सकती है, जैसा कि समकालीन मध्य पूर्व और एशिया में देखा जा रहा है. (1)
उपरोक्त चर्चा हमारी समस्या के लिए एक सैद्धांतिक ढाँचा प्रदान करने का एक प्रयास है. लेकिन उसपर विचार करने से पहले, हमें भारतीय राष्ट्रवाद के अर्थ और दिशा को समझना होगा. इरफ़ान हबीब जैसे विद्वान कहते हैं-
“यह वास्तव में शोषित देशों में औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन है, जिसने उत्पीड़ित देशों को राष्ट्रों में परिवर्तित करके राष्ट्रों की सबसे बड़ी श्रेणी का निर्माण किया है. भारत इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है.” (2)
एक समय में भारत को एक देश के रूप में देखा जाता था, जैसे तीसरी शताब्दी ई.पू. अशोक के शिलालेखों में जम्बूद्वीप, पहली शताब्दी ई.पू., खारवेल के हाथीगुम्फा शिलालेख में ‘भारत’ और अमीर खुसरों के भारत के देशभक्तिपूर्ण वर्णन ‘हिंद’ में भी, लेकिन उन्होंने इसे एक राष्ट्र नहीं कहा. ब्रिटिश विजय के बाद, पूरे भारत में समान पीड़ा और समान प्रतिरोध की धारणा बनी. पर यह केवल शुरुआत थी. इससे पहले कि लोग एकता की भावना को महसूस करें, भारतीयों में अपनी जातियों के प्रति प्राथमिक निष्ठा के कारण देशभक्ति की भावना की कमी को दूर करना आवश्यक था. और इरफ़ान हबीब मानते हैं कि
“यह तभी संभव था जब आम जनता इसमें शामिल हो, और यहाँ गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए.”(3)
भारतीय राष्ट्र के विकास में हम तीन जटिल प्रक्रियाएँ देख सकते हैं-
पहला, किसी प्रकार के देश की ऐतिहासिक मान्यता कि एक भौगोलिक क्षेत्र किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है.
दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पश्चिम से उधार लिया गया यह विचार कि राष्ट्र कैसा हो. तीसरा, औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष.
इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी. स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्यधारा का नेतृत्व कर रहे गांधी, पटेल, नेहरू और अन्य नेताओं ने स्पष्ट रूप से यह माना कि एक राष्ट्र के रूप में भारत किसी एक धार्मिक समुदाय का नहीं होगा, बल्कि सभी समुदायों के लोगों को एकता से रहने के लिए एकीकृत करेगा. एक धर्मनिरपेक्ष कल्याणकारी राज्य की स्थापना लोगों के वास्तविक कल्याण के लिए की गयी थी.
हालाँकि, मुख्यधारा के नागरिक राष्ट्रवाद के साथ-साथ, जातीय राष्ट्रवाद का एक और रूप उभरा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य समूह की सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना था. यूरोपीय आधुनिकता से भयभीत होकर, अपने आत्म-सम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने ‘स्वर्णिम अतीत’ की ऐतिहासिक रचना शुरू की जिसमें उसके द्वारा स्वीकृत नयी परम्पराएँ शामिल थीं. इस दृष्टिकोण में एक अस्पष्टता मौजूद थी क्योंकि इसने राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए, औपनिवेशिक आक्रांताओं के मज़बूत पक्ष को हथियाने का प्रयास किया.
एक विचारधारा के रूप में, हिंदू राष्ट्रवाद का निर्माण 1870 और 1920 के बीच हुआ था. यह आर्य समाज से संबंधित उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों से प्रेरित था. बाद में 1920 के दशक में, खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों की लामबंदी से खतरा महसूस करते हुए, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठन उभरे और उन्होंने “एक गढ़ी गयी परंपरा के संदर्भ में दूसरे को कलंकित करने और उसका अनुकरण करने की रणनीति” को अपनाकर हिंदू राष्ट्रवाद को मजबूत किया. (4)
जैसा कि हम वीडी सावरकर और एमएस गोलवलकर के लेखन में देख सकते हैं. चूंकि इस पत्र में हमारा उद्देश्य केवल गांधी और सावरकर के राष्ट्रवाद के विचारों की तुलना करना है, इसलिए हम अपनी चर्चा इन दोनों तक सीमित रखेंगे. बेशक, हिंदू राष्ट्रवाद के समानांतर, विभाजन-पूर्व के दिनों में मुस्लिम राष्ट्रवाद का आंदोलन भी विकसित हुआ.
सावरकर का हिंदुत्व
वी.डी सावरकर ने पहली बार 1920 के दशक में मुस्लिम उग्रवाद, तैयारियों और संगठन की धारणा के एक नए और खतरनाक स्तर के संदर्भ में हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को संहिताबद्ध किया. उनकी पुस्तक, ‘हिंदुत्व: हिंदू कौन है?’, जो पहली बार 1923 में प्रकाशित हुई थी,को हिंदू राष्ट्रवाद का एक बुनियादी और आवश्यक ग्रंथ माना जाता है. यह पुस्तक इस धारणा पर टिकी है कि हिंदू,पैन-इस्लामवाद की तुलना में कमजोर है और नस्ल और भूमि की रक्षा में हिंदू राष्ट्रीयता को मजबूत और संगठित करने का आह्वान करती हैं ताकि अन्य लोग हमला करने का साहस न कर सकें.
सावरकर ने 1906 में इंग्लैंड में मैजिनी और गैरीबाल्डी के अपने अध्ययन के माध्यम से ‘दूसरों को धमकाने’ के बारे में सीखा. उन्होंने मैजिनी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया और भूमिका में गैरीबाल्डी की तुलना शिवाजी से और मैजिनी की तुलना शिवाजी के गुरु रामदास से की. इससे पता चलता है कि सावरकर का राष्ट्रवाद एक आयातित पश्चिमी अवधारणा थी, जिसे उन्होंने परंपरा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया द्वारा अपने देश में लागू करने की कोशिश की थी. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सावरकर स्वयं आस्तिक नहीं थे. उनकी योजना एक समरूप समुदाय बनाने की थी, जिसे हिंदू समाज के भीतर अत्यधिक भेदभाव की अनुमति नहीं थी. इसलिए, हिंदू कौन है, यह परिभाषित करने में वे धर्म के महत्व को कम करते हैं और दावा करते हैं कि हिंदू धर्म ‘हिंदूपन’ के गुणों में से केवल एक है. उनके अनुसार हिंदुत्व तीन स्तंभों पर टिका है-
भौगोलिक एकता, नस्लीय विशेषताएँ और एक साझा संस्कृति, जो वैदिक ‘स्वर्ण युग’ के पौराणिक पुनर्निर्माण से उपजी है.
सावरकर के लिए, भू-भाग की अवधारणा राष्ट्रवाद की सार्वभौमिक अवधारणा से भिन्न थी क्योंकि इसे हिंदू संस्कृति और हिंदू लोगों से अलग नहीं किया जा सकता. उनके लिए, हिंदू मुख्यतः आर्यों के वंशज थे जो सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर बसे और नदियों, समुद्रों और हिमालय के बीच के क्षेत्र के निवासी थे. वैदिक युग के प्रथम आर्यों ने ‘जनता की एकता की भावना’ यहाँ तक कि ‘राष्ट्रीयता की भावना’ विकसित की. उनका ज़ोर भौगोलिक एकता पर था, न कि राष्ट्रवाद की क्षेत्रीय अवधारणाओं पर. उनके विपरीत, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र के जातीय और नस्लीय पहलुओं पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा:
“हिंदू केवल भारतीय राज्य के नागरिक नहीं हैं क्योंकि वे न केवल एक मातृभूमि के प्रति प्रेम के बंधन से, बल्कि समान रक्त के बंधन से भी एक हैं. वे न केवल एक राष्ट्र हैं, बल्कि एक नस्ल-जाति भी हैं.”(5)
इस प्रकार, रक्त को एक प्रबल संयोजक कारक मानकर, सावरकर का नस्लीय मानदंड हिंदू समाज में आंतरिक विभाजनों के महत्व को कम करता है. हालाँकि, नस्लीय शुद्धता की धारणा सावरकर की विचारधारा में अनुपस्थित है और इसलिए यह ‘अन्य’ को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करती. निस्संदेह, सावरकर के लिए मुसलमान और ईसाई खतरनाक ‘अन्य’ हैं, लेकिन उन्हें नस्ल के आधार पर हिंदू के रूप में परिभाषित करते हुए, जो कुछ ही पीढ़ियों पहले धर्मांतरित हुए थे, वे सुझाव देते हैं कि उन्हें हिंदू समाज में पुनः शामिल किया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ नागरिकों के रूप में.
इसके अलावा, सावरकर हिंदुत्व विचारधारा के लिए हिंदू धर्म के बजाय ‘एक समान संस्कृति’ की कसौटी का इस्तेमाल करते हैं . वे हिंदू धर्म में रीति-रिवाजों, सामाजिक भूमिकाओं और भाषा को अत्यंत महत्व देते हैं. वे कहते हैं-
“हिंदू न केवल उस प्रेम बंधन से बंधे हैं जो हम अपनी समान मातृभूमि और समान रक्त के प्रति रखते हैं, जो हमारी रगों में बहता है और हमारे हृदयों को धड़काता है तथा हमें स्नेहिल बनाये रखता है, बल्कि उस सामान्य श्रद्धा के बंधन से भी बंधे हैं जो हम अपनी महान सभ्यता- हमारी हिंदू संस्कृति के प्रति रखते हैं, जिसे “संस्कृति” शब्द के अलावा बेहतर ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो उस भाषा-संस्कृत का सूचक है, जो उस संस्कृति की अभिव्यक्ति और संरक्षण का चुना हुआ माध्यम रही है, जो हमारी जाति के इतिहास में सर्वोत्तम और संरक्षण योग्य थी.”(6)
इसलिए, क्रिस्टोफ़ जैफ्रेलोट से सहमत हुआ जा सकता है कि-
“सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा नस्लीय सिद्धांत के बजाय सांस्कृतिक मानदंडों पर आधारित है और तदनुसार पारंपरिक ब्राह्मणवादी विश्व दृष्टि के अनुरूप है; लेकिन साथ ही, यह जातीय राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है, जो पश्चिमी सिद्धांतों से बहुत कुछ उधार लेता है.” (7)
यह सच है कि सावरकर के हिंदुत्व ने हिंदू राष्ट्रवाद में एक गुणात्मक परिवर्तन लाया और उसे अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया. हिंदू महासभा, जिसके अध्यक्ष सावरकर थे, के पतन के बाद, हेडगेवार, जिन्होंने हिंदुत्व का अध्ययन किया था, के नेतृत्व में आरएसएस ने हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को और विकसित किया. लेकिन हिंदुत्व में सावरकर के आधारभूत योगदान को नकारा नहीं जा सकता. हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच स्पष्ट अंतर करके और हिंदुत्व की एक व्यापक परिभाषा देकर, जिसमें धार्मिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भाषाई क्षेत्र भी शामिल हैं, सावरकर एक व्यापक एकता स्थापित करने में सफल रहे, जो ‘हिंदू कौन है?’ प्रश्न के उनके उत्तर में स्पष्ट है.
“प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है जो इस भारत भूमि को, सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली इस भूमि को अपनी पितृभूमि, अपनी धार्मिक आस्था के उद्गम और पालने की पवित्र भूमि मानता है और इसका स्वामी है.”(8)
एक ही झटके में इस परिभाषा में वेद, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों को हिंदुओं के घटक के रूप में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को इससे बाहर रखा गया है. इसके अलावा, सभी हिंदुओं को ‘हिन्दू सभ्यता’ के प्रति प्रेम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
“‘हिन्दू सभ्यता’ की विशेषता है एक साझा इतिहास, एक साझा नायक, एक साझा साहित्य, एक साझा कला, एक साझा कानून और एक साझा न्यायशास्त्र, एक साझा मेले और त्यौहार, एक साझा रीति-रिवाज, एक समारोह और संस्कार.”(9)
इस प्रकार हिंदू धर्म पर आधारित होने के बजाय, एक व्यापक हिंदू सांस्कृतिक पहचान का निर्माण होता है, जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आसानी से एक भारतीय पहचान का काम कर सकती है. इसलिए, यह कहा जा सकता है कि ‘ हिंदुत्व ‘ सावरकर की प्रमुख अवधारणा है, जो हिंदू राष्ट्रवाद का आधार है. आइए अब देखें कि यह गांधी की हिंदू धर्म की अवधारणा से कैसे भिन्न है.
गांधी का हिंदू धर्म
एक धार्मिक परंपरा के रूप में हिंदू धर्म को परिभाषित करना कठिन है. गांधी के लिए “हिंदू धर्म कोई विशिष्ट धर्म नहीं है. इसमें दुनिया के सभी पैगम्बरों की पूजा के लिए जगह है. यह सामान्य अर्थ में कोई मिशनरी धर्म नहीं है.”(10)
उनके लिए हिंदू धर्म का सार सत्य और अहिंसा है और मोक्ष इसका केंद्रीय सिद्धांत है. यद्यपि वे वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे शास्त्रों में विश्वास करते हैं और भगवद्गीता के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, फिर भी वे शास्त्रों में ऐसी किसी भी आज्ञा को अस्वीकार करते हैं जो तर्क, सत्य और अहिंसा के विपरीत हो. इस प्रकार, वे दलितों और महिलाओं के विरुद्ध अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथाओं का आसानी से विरोध कर सके, जिसे शास्त्रों ने मंजूरी दी थी . यद्यपि वे स्वयं को मुख्यधारा के हिंदू धर्म के भीतरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और स्वयं को सनातन हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म की उनकी गहन और मौलिक व्याख्या, हिंदू धर्म के तीन पारंपरिक मार्गों (ज्ञान, कर्म और भक्ति) के अतिरिक्त, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सेवा मार्ग के रूप में इसमें नए आयाम जोड़ती है.
धर्म पर गांधी के विचार धर्म की पारंपरिक समझ से कोसों दूर प्रतीत होते हैं जब वे तर्क देते हैं कि धार्मिक प्रथाओं, विचारों और विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए. एक ओर, उन्हें सभी धर्मों की सच्चाई पर गहरी आस्था और स्वीकृति है, लेकिन दूसरी ओर, वे सभी मौजूदा धर्मों की अपूर्णताओं से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं क्योंकि वे अपूर्ण मनुष्यों की व्याख्याओं की मध्यस्थता से हम तक आते हैं. इस प्रकार, एक अपूर्ण मानव संस्था विकास और पुनर्व्याख्या की प्रक्रिया के अधीन होती है. इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी धर्म की दो अवधारणाएँ रखते थे: एक आदर्श और दूसरी एक प्रथागत संस्थागत धर्म.
उन्होंने सच्चे धर्म की तुलना एक पेड़ के तने और औपचारिक धर्मों की उसकी शाखाओं से भी की. सच्चा और पूर्ण धर्म केवल वैचारिक रूप से ही अस्तित्व में था. संगठित धर्मों में आमतौर पर मौजूद हठधर्मिता, कर्मकांड, अंधविश्वास और कट्टरता से इसका बहुत कम साम्य था. उनके लिए, धर्म और नैतिकता अविभाज्य हैं. जब वे कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति का कोई मूल्य नहीं है, तो वे एक सार्वभौमिक नैतिक धर्म की बात कर रहे होते हैं, संगठित धर्म की नहीं. वह कभी-कभी आदर्श धर्म और संस्थागत धर्म के बीच झूलते रहते हैं, लेकिन वह धर्म और उसके व्यवहार की एक नई समझ सामने ला सके, जिसमें सामाजिक बुराइयों, असमानताओं और अन्याय के खिलाफ लड़ना व्यक्ति के अपने धार्मिक कर्तव्यों का अभिन्न अंग है.
धर्म के बारे में गांधी की उपरोक्त समझ ने हिंदू धर्म की उनकी अवधारणा को परिभाषित किया, जो रूढ़िवादी हिंदुओं के आचरण से बिल्कुल अलग थी. उन्होंने कभी ज्योतिषियों से परामर्श नहीं लिया और न ही उनके पास विस्तृत पूजा-पाठ और अनुष्ठानों के लिए समय था.
उनका हिंदू धर्म सर्वसमावेशी है, सांप्रदायिक नहीं, घृणा से मुक्त है और अन्य मनुष्यों और सभी जीवन रूपों के साथ ऐक्य भाव रखता है. हालाँकि उन्होंने स्वयं को एक सनातनी हिंदू घोषित किया, लेकिन उन्होंने किसी भी एक धर्म को दूसरे पर, यहाँ तक कि अपने धर्म को भी, विशेषाधिकार नहीं दिया. इस प्रकार, उनका ज़ोर कई अन्य धर्मों के टकरावपूर्ण रवैये के विरुद्ध उन्हें समान सम्मान देने पर है.
हिंसा/अहिंसा
गांधी और सावरकर हिंसा के बारे में अलग-अलग विचार रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय इतिहास की उनकी समझ और भारतीय राष्ट्र के भविष्य के बारे में उनकी दृष्टि अलग-अलग थी. सावरकर ने हिंसा को उचित ठहराया और बौद्धों की अहिंसा की आलोचना यह कहकर की, कि इसने हिंदुओं को कमज़ोर बनाया और उन्हें अतीत में अपमानित करने वालों से बदला लेने में असमर्थ कर दिया. इस प्रकार, हिंसक इतिहास का उनका वर्णन गांधी के शांतिवादी आख्यान और अहिंसा की अवधारणा के समर्थन से बिल्कुल अलग है. उन्होंने गांधी की अहिंसा की तीखी आलोचना की और स्पष्ट शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए.
सावरकर द्वारा हिंसा को महिमामंडित करने के विपरीत, गांधी ने हिंसा का सहारा लेने के अधिकार का खंडन किया, यहाँ तक कि अन्याय के विरुद्ध भी. उनके लिए, हिंसा हमेशा गलत थी और उसकी निंदा की जानी चाहिए. हालाँकि हिंसा का उनका निषेध पूर्ण प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता क्योंकि उनके अपने जीवन में और भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम में कई अपवाद भी दिखाई देते हैं. यहाँ तक कि उनके सत्याग्रह की व्याख्या ‘न्यूनतम हिंसा के प्रयोग’ के प्रचार के रूप में भी की जा सकती है. उन्होंने स्वयं कहा था:
“मैं मानता हूँ कि जहाँ कायरता और हिंसा के बीच ही विकल्प हो, वहाँ मैं हिंसा की सलाह दूंगा.”(11)
इसीलिए गांधीजी ने युद्ध का भी पक्ष लिया. एक व्यावहारिक आदर्शवादी के रूप में, गांधीजी समझते थे कि हिंसा को मानव समाज से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता. उनके लिए, जब तक हम जीवित हैं, कुछ न्यूनतम हिंसा आवश्यक है. जैनों और बौद्धों की अहिंसा में उनका कोई विश्वास नहीं था. हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि उनका मुख्य योगदान अहिंसा को सामाजिक क्रिया के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करके दूसरों की हिंसा के विरुद्ध अहिंसा से लड़ने में था.
सावरकर पूर्ण अहिंसा के विचार के कट्टर आलोचक थे, जो उनके अनुसार, विदेशियों के हाथों भारतीयों की हार का एक कारण था. इसलिए, उन्होंने अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत का प्रचार करने के कारण राजा अशोक को अपनी राष्ट्रीय नायकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया. पूर्ण अहिंसा की तरह, उन्होंने अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति पूर्ण सहिष्णुता को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे राष्ट्र को नुकसान हो सकता था. सहिष्णुता का उनका विचार प्रकृति के सापेक्ष था और उन्होंने भारतीयों के न्यायोचित प्रतिशोध के रूप में जवाबी कार्रवाई करने के वैध अधिकार की वकालत की. उनके लिए, सामूहिक हिंसा, नरसंहार और निर्दोषों के खिलाफ अत्याचार और प्रतिशोध की भावना के स्वाभाविक परिणाम मात्र थे.
इस प्रकार, उन्होंने ईसाइयों पर मराठा सेना द्वारा की गई लूटपाट और हिंसा को उचित ठहराया, और ऐसी घटनाओं को ‘पारिस्थितिक बहाने’ करार दिया. वह हिंदू जाति को ‘सैन्य मानसिकता वाला, उत्साही और वीर बनाना चाहते थे और सभी प्रकार की राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू धर्म का सैन्यीकरण करना चाहते थे’.
दूसरी ओर, गांधीजी ने हिंदू उग्रवाद की आलोचना की, उसके दोषों को उजागर किया और क्रांतिकारी आतंकवाद का यह कह कर खंडन किया:
“क्या आपको हत्या करके भारत को आज़ाद कराने के बारे में सोचकर भी डर नहीं लगता? हमें खुद को मारना होगा. दूसरों को मारने का यह कायरतापूर्ण विचार है. जो लोग हत्या करके सत्ता में आते हैं, वे निश्चित रूप से देश को खुश नहीं कर सकते.”(12)
गांधीजी के लिए, अपनाए गए साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना कि अंतिम उद्देश्य.
हमारी उपरोक्त चर्चा धर्म, हिंसा, इतिहास और सभ्यता जैसे मूलभूत मुद्दों पर गांधी और सावरकर के विचारों के बीच के अपूरणीय मतभेदों की गवाही देती है. यह आगे चलकर, राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्र के भविष्य के अलग-अलग दृष्टिकोण के बारे में उनकी भिन्न अवधारणाओं में विकसित होता है. सावरकर की समझ उन्हें हिन्दू राष्ट्रवाद की ओर ले जाती है, जो उनकी अपनी परिभाषा ‘हिंदू कौन है’ के आधार पर हिन्दुओं के अलावा सभी गैर-हिंदुओं को बाहर करता है. मुसलमानों और ईसाईयों को बाहर रखा गया है क्योंकि उनकी पवित्र भूमि भारत के बाहर थी.
उन्होंने मुसलामानों को ‘संदिग्ध मित्र’ कहा है, अगर वे शत्रु नहीं हैं तो. यद्यपि वे स्वतंत्रता के राजनीतिक संघर्ष के दौरान मुसलमानों के साथ मित्रता के विरोधी नहीं थे, जैसा कि उनकी लोकप्रिय पुस्तक ‘1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम’ (1909) में कहा गया है. हिंदू-मुस्लिम एकता का यह प्रारंभिक प्रक्षेपण बाद में पूरी तरह से उलट गया जब उन्होंने संस्कृति और नस्ल को शामिल करने के लिए हिंदुत्व को जातीय-धार्मिक राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा के रूप में व्यक्त किया. इसका उद्देश्य हिंदुओं में पदानुक्रमित जातियों को एक सांप्रदायिक झंडे तले एकजुट और संगठित करना और इसे एक प्रभावशाली बहुमत बनाना था, जिसके अधीन गैर-हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएँ. इस तरह उन्होंने ‘हिंदू’ और भारत को एक दूसरे के बराबर या पूरक माना.
उनके लिए, राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता परस्पर विरोधी विचार नहीं हैं, क्योंकि हर प्रकार की देशभक्ति कमोबेश सांप्रदायिक और संकीर्ण होती है. इस मानदंड पर, केवल हिंदू ही भारत के प्रति सच्चे देशभक्त होने का दावा कर सकते हैं. उनके लिए हिन्दू स्वयं में एक राष्ट्र हैं, इसलिए हिन्दू धर्म को राष्ट्र के समान माना जाता है. अतः हिन्दू और भारत पर्यायवाची बन जाते हैं. और इस प्रकार,
15 अगस्त 1943 को नागपुर में अपने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को जोरदार ढंग से प्रतिपादित करते हुए कहा कि-
“मुझे श्री जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत से कोई विवाद नहीं है. हम हिंदू स्वयं में एक राष्ट्र हैं और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं.”
सावरकर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के विपरीत, गांधी भारत के लिए अलग विचार रखते थे जिसके अनुसार
“ऐसा नहीं है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के एक साथ रहने से भारत एक राष्ट्र नहीं हो सकता. विदेशियों के आने से राष्ट्र का विनाश नहीं होता क्योंकि वे इसमें विलीन हो जाते हैं. भारत हमेशा से ऐसा ही देश रहा है.”(13)
गांधी के लिए, भारत की धार्मिक और भाषाई विविधता एक संपत्ति थी, न कि एक बोझ. इसलिए, गांधी के भारत के विचार में सभी धर्मों, जातियों और जनजातियों का समावेश है. हिंद स्वराज में, उन्होंने अहिंसक तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग बताया जो सावरकर के उग्र राष्ट्रवाद के विपरीत थी, जहाँ हिंसा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी.
सावरकर के धर्म और संस्कृति के मिश्रण के विपरीत, गांधी ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध अपने तर्कों में दोनों को अलग-अलग रखा. उनके विचारों में धार्मिक मतभेद निरपेक्ष नहीं थे; सभी धर्मों में इतनी समानताएँ हैं, जिन्हें धर्म नकार नहीं सकता. क्षेत्रीय समानताएं और सामंजस्य धार्मिक मतभेदों को कमजोर करते हैं. इस प्रकार, सावरकर का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत गांधी के समावेशी राष्ट्रवाद के विपरीत है. गांधी ने राष्ट्रवाद को गैर-धार्मिक शब्दों में परिभाषित किया और अपनी भारतीय पहचान को अन्य सभी पहचानों से ऊपर रखा. उन्होंने कहा- “हम पहले भारतीय हैं और उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई हैं.” (14) इसके अलावा, उन्होंने हिंदुओं को आगाह किया कि यदि वे सोचते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत केवल हिंदुओं का होगा, तो वे गलत हैं.
यद्यपि गांधी ने स्वतंत्रता के बाद संसदीय लोकतंत्र को अपनाने का समर्थन किया, फिर भी भविष्य के लिए उनकी परिकल्पना केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं बल्कि स्वराज या स्वशासन थी. इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने अपने ‘रचनात्मक कार्यक्रम’ के लिए उन मुद्दों की रूपरेखा तैयार की, जिसे लोकतंत्र के पूरक के रूप में एक संसदीय साधन के अलावा अन्य साधनों के रूप में अपनाया जाना था. हिंद स्वराज में वर्णित गांधी का जीवन मिशन भारतीयों का नैतिक पुनरुत्थान था जिसे वे शारीरिक सुखों और भौतिक सुविधाओं पर आधारित पश्चिमी सभ्यता की तुलना में भारतीय सभ्यता की सच्ची पहचान मानते थे.
इस प्रकार, उन्होंने न केवल आधुनिकता की कड़ी आलोचना की बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टि और इसे वास्तव में प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया. सावरकर के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं थी सिवाय एक काल्पनिक अतीत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने के; एक मजबूत हिन्दू राष्ट्र के रूप में जो राष्ट्रों के बीच भयावह जीवन संघर्ष के रूप में बना रह सके. हालाँकि, एक हिन्दू समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया और जाति व्यवस्था को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने की बात कही. इस प्रकार, दोनों की तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि गांधी का राष्ट्र-निर्माण का दृष्टिकोण सावरकर की तुलना में कहीं अधिक गहरा और व्यापक था.
देशभक्ति से गांधी का तात्पर्य समस्त जन कल्याण से था जो कि एक ऐसी भूमि की यात्रा है जहाँ स्वतंत्रता और शांति हो. वे एक अंतर्राष्ट्रीयतावादी और देशभक्त थे, न कि सावरकर के जैसे संकीर्ण राष्ट्रवादी और कट्टरपंथी. यही कारण है कि वे मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे अनेक नेताओं के साथ-साथ विश्व स्तर पर मुक्ति आंदोलनों को भी प्रेरित कर सके. लेकिन यह प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए कि गांधी की शहादत के 75 वर्षों बाद, जिसने सावरकर के हिंदू राष्ट्रवाद को हाशिये पर धकेल दिया था, समकालीन भारतीय समाज हिंदुत्व की विचारधारा की गिरफ्त में क्यों दिखाई देता है.
इस गिरफ्ती की सफलता के पीछे क्या ताकत काम कर रही है, और भविष्य में भारतीय समाज पर इस गिरफ्ती की सफलता के क्या प्रभाव होंगे?
यद्यपि इस आलेख का उद्देश्य हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ के विवरण में जाना नहीं है, फिर भी यह इंगित करना आवश्यक है कि उन्होंने सफलता पाने के लिए क्या रणनीति अपनाई. जैसा कि पहले बताया गया है, यह ‘दूसरों को धमकाने और अनुकरण करने’ की रणनीति थी जिसमें सबसे पहले, दूसरों की अतिरंजित प्रभुत्वशाली उपस्थिति का इस्तेमाल बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यक बोध के साथ-साथ असुरक्षा की प्रबल भावना पैदा करने के लिए किया गया.
इसके अलावा, हिंदू समाज में जातियों और संप्रदायों में अत्यधिक विभेदीकरण ने इस भावना को और भी प्रबल बना दिया. दूसरे, हिंदू समाज में सुधार के प्रयास किए गए जिसमें चुनिंदा रूप से दूसरों की उन सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुकरण किया गया जिनके बारे में माना जाता था कि उन्होंने दूसरों को शक्ति और श्रेष्ठता प्रदान की थी. यह उधार खुले तौर पर नहीं, बल्कि हिंदू परंपराओं की पुनर्व्याख्या के बहाने किया गया. आत्म-सम्मान पुनः प्राप्त करने और संकटग्रस्त पहचान की रक्षा के लिए ‘वैदिक स्वर्ण युग’ के एक मिथक का वैचारिक रूप से निर्माण किया गया. एक सुसंगठित हिंदू समाज को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वर्ण व्यवस्था की पुनर्व्याख्या की गई.
इस प्रकार, पहचान-निर्माण की हिंदू राष्ट्रवादी रणनीति विरोधाभासी रूप से दूसरे को कलंकित करने और उसका अनुकरण करने पर निर्भर करती है ताकि एक ऐसी हिंदू राष्ट्रवादी पहचान का निर्माण किया जा सके जिसका हिंदू धर्म से बहुत कम संबंध है. लेकिन दोनों में एक समान विशेषता है, वे लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणवादी संस्कृति को साझा करते हैं. भारत के विभाजन और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण, साथ ही, भारत की सीमाओं में हुए बदलाव ने हिंदू राष्ट्रवाद को उपर्युक्त रणनीति अपनाने में मदद की.
हालाँकि विभाजन ने हिन्दू राष्ट्रवाद के विस्तार के लिए अवसर और अनुकूल परिस्थितियां पैदा कीं लेकिन गांधी की हत्या के बाद देश का मिजाज़ और नेहरु की यह क्षमता कि वे उन्हें संवेदनशील मुद्दों पर आन्दोलन शुरू न करने दें, ने उनकी प्रगति को धीमा कर दिया. हालाँकि, नेहरू के बाद स्थिति बदल गयी. कई घटनाओं जैसे पकिस्तान के साथ दो युद्ध, जेपी आन्दोलन, शाह बानो काण्ड, आडवाणी की रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस और 2002 के गुजरात दंगे आदि ने धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से सामूहिक चेतना को हिंदुत्ववादी विचारधारा के पक्ष में बदल दिया.
इसके अलावा निचली जाति और ओबीसी वोटों और समर्थन के चतुर हेरफेर ने आरएसएस-भाजपा को 2014 में सत्ता में पहुँचाया. इस प्रकार अनुच्छेद 370 के उन्मूलन और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ हिंदुत्व एजेंडा को पूरी तरह आगे बढ़ाने के लिए सारी बाधाएं दूर हो गयी. संक्षेप में, यह गांधी के नागरिक राष्ट्रवाद पर सावरकर के हिंदू राष्ट्रवाद की विजय की कहानी है. लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अब हम आगे कहाँ जाएँ? क्या भारत में गांधीवादी समावेशी नागरिक राष्ट्रवाद के पुनरुद्धार की कोई संभावना बची है?
भारत में भाजपा के पिछले 10 वर्षों के शासन से हमें हिंदू राष्ट्रवाद के क्रियान्वयन और भविष्य में क्या होने की संभावना है, इसका अंदाजा लग सकता है. हिंदू बहुसंख्यकवाद ने धर्मनिरपेक्षता की जगह ले ली है, सार्वजनिक स्थानों का हिंदूकरण किया जा रहा है और मुसलमान, ईसाइयों और उदारवादियों को निशाना बनाया जा रहा है. हिंदू गौ रक्षक अल्पसंख्यकों की हत्या/उत्पीड़न कर रहे हैं. प्रशासन, न्यायपालिका, आरबीआई और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है. सीबीआई और ईडी जैसी सरकारी एजेंसियां भी विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है.
संक्षेप में, चुनावी वैधता प्राप्त एक सत्तावादी राज्य का निर्माण किया जा रहा है जो लोकतंत्र एवं सहमति की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करता. नायक पूजा के लिए एक शक्तिशाली नेता की छवि बनाने हेतु प्रचार पर भारी धन खर्च किया जा रहा है.
मुगल काल के अधिकांश भाग को हटाने के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखा जा रहा है. हमारे राष्ट्रीय नेताओं विशेष रूप से गांधी और नेहरू के विरुद्ध झूठा प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया सेल बनाए गए हैं. बुलडोजर न्याय के नाम पर मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई के एक नए तरीके को वैधता प्रदान की जा रही है.
कुछ लोगों ने इसे वास्तविक हिंदू राष्ट्र की सेवा में ‘जातीय लोकतंत्र’ कहा है. इसमें बहुसंख्यक समुदाय राष्ट्र के समान है और अल्पसंख्यकों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया गया है. हिंदुत्व विचारधारा की वैचारिक नींव बरकरार है लेकिन अब इसमें राष्ट्रीय लोकलुभावनावाद जुड़ गया है, जिसका प्रतिनिधित्व मोदी ने चुनाव में सफलता के लिए किया जिससे निम्न जाति के नागरिकों की एक बड़ी संख्या को लुभाया जा रहा है. इन सभी सफलताओं के बावजूद भारतीय समाज में हिंदुत्व की विचारधारा को ठोस रूप देने के लिए आरएसएस द्वारा लगभग 100 वर्षों से किए गए मौन आधारभूत कार्यों को कम नहीं आंका जाना चाहिए.
निष्कर्ष
आज हम जो देख रहे हैं वह बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है जिसके साथ घृणा और हिंसा भी व्याप्त है. उपाय क्या है? ऐसी स्थिति में धार्मिक आस्था और रीति-रिवाज के प्रति शत्रुतापूर्ण पुरानी शैली की धर्मनिरपेक्षता जड़ नहीं पकड़ सकती. केवल गांधी का सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण ही सही विकल्प हो सकता है. इसका अर्थ अपने धर्म में आस्था का त्याग करना नहीं है बल्कि सभी धर्म के प्रति समान सम्मान की मांग करना है. इसमें अपने धर्म की श्रेष्ठता का कोई स्थान नहीं है. लेकिन क्या हम इसे अपनाने के लिए तैयार और इच्छुक हैं?
हमारी पिछली चर्चा से ऐसा प्रतीत नहीं होता. पिछले कुछ दशकों में हमने दुनिया के कई हिस्सों में आक्रामक धार्मिक राष्ट्रवाद के रूप में धार्मिक पुनरुत्थानवाद और कट्टरपंथ का पुनरुत्थान देखा है. धार्मिक/पहचान की राजनीति ने आर्थिक पुनर्वितरण की पुरानी राजनीति की जगह ले ली है जिसे भविष्य के समाजवादी दृष्टिकोण का समर्थन प्राप्त था. इसके अलावा जैसा कि हमने चर्चा की है भारत में यह राष्ट्रवाद औपनिवेशिक आकाओं के विरुद्ध संघर्ष में विकसित हुआ. स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम का पुराना केंद्र बिंदु समाप्त हो गया. राष्ट्र निर्माण के लिए सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम को साथ लेकर पूर्ण स्वराज का गांधीवादी दृष्टिकोण स्वतंत्रता के बाद सत्ता में आई कांग्रेसी सरकार द्वारा कभी गंभीरता से नहीं लिया गया. शेष गांधीवादी भी कुछ खास नहीं कर सके.
गांधी का अहिंसक समाज का आदर्श केवल एक आदर्श ही रह गया. अधिकांश कांग्रेसी नेताओं ने अहिंसा को एक राजनीति के रूप में माना ना कि एक सार्वभौमिक आदर्श के रूप में. परिणाम हमारे सामने है. ऐसा लगता है कि हम गांधी और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं द्वारा प्रचारित समावेशी नागरिक राष्ट्रवाद की लड़ाई लगभग हार चुके हैं. जैसा कि हम जानते हैं सावरकर का हिन्दू राष्ट्रवाद यूरोप की दक्षिणपंथी राजनीति से प्रभावित था.
हम जर्मनी और यूरोप में इस प्रकार के राष्ट्रवाद द्वारा मचाई गई तबाही से भी अवगत हैं. खतरा यह है कि हम भी कहीं उसी रास्ते पर न चल दें. इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव को बचाने के लिए हमें ऐसी सोच का विरोध करना आवश्यक है. एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि जैसा कि गांधी ने सिखाया था-
“बुराई राष्ट्रवाद में नहीं बल्कि संकीर्ण, स्वार्थी और अलगाववादी सोच में है जो आधुनिक राष्ट्रों के लिए अभिशाप है.“(15)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















