टूटता है एकांत
कई दिनों से महज टहनियाँ बनी
जी रही थी गिलोय की बेल।
फूटीं पत्तियाँ
ताजगी भरी
तो लगा कि नहीं जगती उम्मीद भर,
जगती है
द्वंदों में जकड़ी मनुष्यता भी
मनुष्य की,
टूटता है एकांत भी।
चोंच भर
पानी पायी चिड़िया को देखकर
जैसे जाग उठता है सागर का सागर
लहरों के संगीत में
भीतर से भीतर तक
मनुष्य के।
या फैलाव धरती का
जैसे ले जाता है ठेलकर
बनाकर पूरा मनुष्य
वहाँ तक
जहाँ रह रहा होता है कोई अकेला
जूझता
अपनी वंचनाओं से।
महज संयोग नहीं होता
ऐसे में याद हो आना
संगवाई धोती से झांकती टांगों का
पिता की
लगाते खेत में पानी।
कई दिनों से
सिहराने रखी किताब की
खुद को पढ़वाने की
जगी उत्सुकता भी
तो अंतत: तोड़ती है अकेलापन ही।
असहमति के लिए प्रार्थना
नहीं प्रभु
नहीं छीनना असहमति को इस हद तक
कि दरिद्र हो जाऊँ उससे ।
हो जाऊँ अहंकारी
निरी सहमतियों के जंगल में विचरते
अव्वल दर्जे के
हिंस्र पशु-सा।
नहीं प्रभु
नहीं करना वंचित असहमति से भूलकर भी।
जानता हूँ
रहते असहमति के
जुटा पाता हूँ बहुत कुछ सहमति के पक्ष में,
रहता हूँ कितना तो सावधान!
नहीं प्रभु
मत लील लेना असहमति को
कोरोना के प्रकोप-सा!
नहीं जानते क्या आप
बहुत बार राह मिलती है
असहमतियों की ही गली से
सहमतियों को।
मिलता है बहुत आनंद प्रभु
और एक अलग पहचान भी।
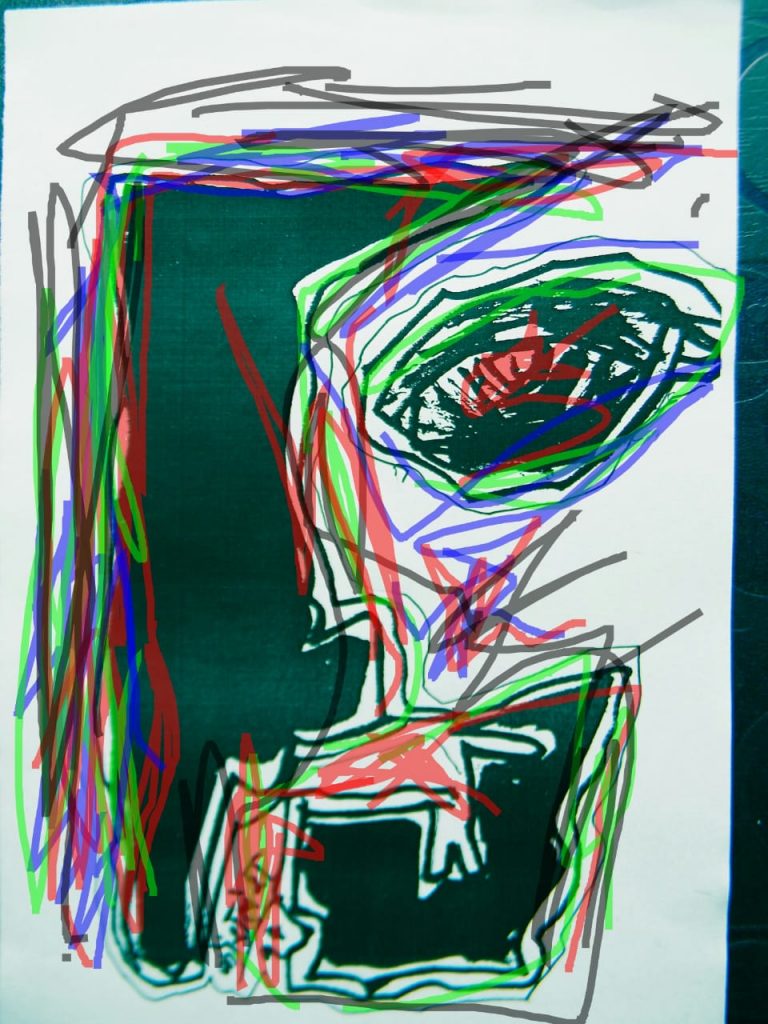
लो किया विसर्जन
अब काहे की लड़ाई
जब आप ही चल दिए
और वह भी
कभी न लौटने के लिए।
यूँ लड़ाई तो पहले भी आपसे नहीं थी
हाँ झगड़ा था आपकी मानसिकता से,
कुछ हरकतों से आपकी।
आपके कहे
अथवा लिखे पर तो
महज पसंद/नापसंद का रौळा था,
था कुछ सहमति-असहमति का जरूरी झोंका।
लो किया विसर्जन
आपके संदर्भ में।
पर मुझे अगर जीना है
तो जीना ही होगा न
जीने की तरह,
जैसे आया हूँ जीता-
इंसान की इंसानियत को समझते,
गोद में उठाए उसे
उसके लिए मरते,
झगड़ते।
एक दलित आदत के खिलाफ
माँ की मौत हो
या बेटी का ब्याह
या फिर जन्म ही किसी का परिवार में
उसकी निगाह में हर ऐसी घटना
जरिया होती है कुछ न कुछ ऐंठने का।
मिनट भी नहीं लगता उसे
भिखमंगा बनने में
उतारने में चालाकी आँखों में।
मानो सीख लिया हो सब
वक्त पड़ने पर
अपना ही खून सोखने वाले
गधे को भी बाप बनाने वालों से।
एक क्षण नहीं लगाता उसे
एक हल्की सी भी गुर्राहट के
चरण थामने में,
करबद्ध दुहाई देने में
क्रूर से क्रूर को भी दाता बना देने में।
तीज त्योहार को भी
पहुँच जाता है वह
अनचाहा, कितने ही द्वारों पर।
नजर नहीं आतीं उसे वे हिकारतें, दुत्कारें
जो उसकी जिद्दी मिन्नतों के बदले
उड़ेल दी जाती हैं उसके कटोरे में।
मानो खड़ा हो कोई नेता अगले चुनाव के लिए।
समझ नहीं आता
कैसे बैठा लेता है संतुलन
गाली और कटोरे में!
क्या सचमुच
नहीं मर सकता वह
अपने उन सपनों के लिए
जो फहरा रहे हैं उसके ही भीतर
जाने कब से।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



















बहुत सुंदर कविताएं👏👏👏
Hindi Bal Sahitya : दिविक रमेश का हिंदी बाल साहित्य संसार – Divik Ramesh
https://www.drmullaadamali.com/2022/06/hindi-bal-sahitya-divik-ramesh.html