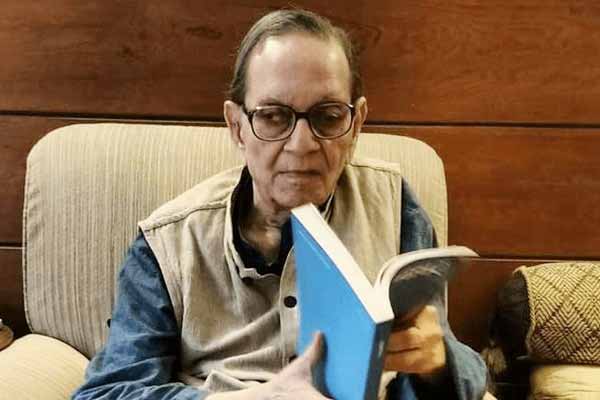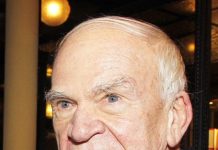— सच्चिदानंद सिन्हा —
सन 1942 के ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन का सोशलिस्टों के लिए असाधारण महत्त्व था। इस आंदोलन के अनुभव से उन्होंने यह निर्णय किया कि उन्हें कम्युनिस्टों से अलग अपना रास्ता तय करना है और इस रास्ते पर चलने में उन्हें बहुत-से मामलों में कम्युनिस्टों के बुनियादी सिद्धांतों का विरोध करना होगा। यहां यह बात ध्यान में रहे कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के वर्षों में दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन अभूतपूर्व तेजी से बढ़ा था।
रूसी सेना के पीछे-पीछे यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कम्युनिस्टों का सत्ता पर कब्जा हो गया। चीन में 1948 में एक लंबी लड़ाई के बाद कम्युनिस्टों ने सत्ता प्राप्त की। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में उनकी ताकत महसूस की जा सकती थी। ईरान में भी वे शक्तिशाली थे। कबायली अफ्रीका तक में उनके छोटे-छोटे प्रभाव क्षेत्र बन रहे थे। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस और इटली में कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत ताकतवर थीं। सारी कम्युनिस्ट पार्टियां कामिन फार्म के माध्यम से सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में थीं और सर्वसत्तावादी शासन का समर्थन करती थीं। सर्वसत्तावादी शासन को वे अलबत्ता सर्वहारा और किसानों की तानाशाही की संज्ञा से अभिहित करती थीं जबकि असलियत में इस प्रकार के शासन में मजदूरों और किसानों को किसी भी प्रकार की स्वाधीनता नहीं थी और ना ही शासन के संचालन में उनकी कोई स्वतंत्र भूमिका। ‘कम्युनिज्म’ की इस बढ़ती तेज लहर के आगे इस बात पर जोर देना कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की स्थापना संभव ही नहीं है, सचमुच ही एक साहसिक बात थी। यह साहस लोकतंत्र के प्रति दृढ़ आस्था से ही आ सकता था।
इस समय कामिन फार्म से संकेत ग्रहण कर भारतीय कम्युनिस्टों ने बी.टी. रणदिवे के नेतृत्व में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्ता हथियाने की मुहिम छेड़ी और चीन की तर्ज पर तेलंगाना (आंध्र) को किसान-शक्ति का गढ़ बनाया। इस तरह किसान-शक्ति के गढ़ बनाकर आखिर में सारे देश में सत्ता पर कब्जा करना कम्युनिस्टों का लक्ष्य था। सोशलिस्टों ने सशस्त्र संघर्ष के रास्ते की मुखालफत की और लोकतंत्र के रास्ते पर चलने का निर्णय किया। यह कहने की जरूरत नहीं कि अपने इस निर्णय के कारण सोशलिस्टों को कम्युनिस्टों की कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा।
जेपी के नेतृत्व में 1948 में जब कांग्रेस के बाहर सोशलिस्ट पार्टी का पुनः गठन हुआ तो उसने लोकतांत्रिक समाजवाद और सर्वसत्तावादी (टोटैलिटेरियन) कम्युनिज्म के बीच भेद को स्पष्ट रूप से चिह्नित और व्याख्यायित किया। सोशलिस्ट पार्टी के नीति-वक्तव्य में जोर देकर यह कहा गया कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। नीति-वक्तव्य के इस वाक्य कि “यह मार्क्सवाद का स्वतःसिद्ध सार्वभौम सिद्धांत है कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद हो ही नहीं सकता ’’ के पीछे जेपी की प्रेरणा साफ दिखाई पड़ती है। यह कहा जा सकता है कि गरीब और अल्पविकसित देशों की प्रभावशाली सोशलिस्ट पार्टियों के बीच भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ही एकमात्र पार्टी थी, जो बिना किसी लाग-लपेट के लोकतंत्र की प्रबल पक्षधर थी।
इस वक्त के राजनैतिक वातावरण में प्रचलित वामपंथी मत के खिलाफ जाकर भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ने अपना यह मत प्रतिपादित किया कि मार्क्सवाद, लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। यह प्रतिपादन मार्क्सवाद सहित समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों को झुठलाने और उन्हें विकृत रूप में पेश करने के प्रयत्नों के खिलाफ उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। इन्हीं दिनों पार्टी को सामाजिक परिवर्तन का एक उपयुक्त माध्यम बनाने के लिए यह सोचा गया कि पार्टी के संगठन को नया रूप प्रदान किया जाना चाहिए।
जेपी दुनिया के समाजवादी आंदोलन के अनुभवों से हमेशा सीखना चाहते थे। पार्टी को ज्यादा व्यापक बनाने की दृष्टि से उन्होंने संगठन का एक नया ढांचा प्रस्तुत किया। इसके पीछे ब्रिटिश लेबर (मजदूर) पार्टी का मॉडल था जो ब्रिटेन में अपने बलबूते पर चुनाव जीतकर सत्तारूढ़ हुई थी। सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में कुछ बड़े कदम उठाये और इसके साथ ही सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम भी शुरू किये। हम ऊपर इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि जेपी अकसर एक प्रकार के युवासुलभ उत्साह से परिचालित होते थे, उन्होंने ब्रिटेन और भारत की परिस्थितियों की भिन्नता को नजरअंदाज किया। उनकी पहल पर 1949 में सोशलिस्ट पार्टी सक्रिय कार्यकर्ताओं की पार्टी के स्थान पर आम (मास) पार्टी बना दी गयी। ब्रिटिश लेबर पार्टी की तर्ज पर उसमें दो प्रकार की सदस्यता का प्रावधान रखा गया। एक तरफ लोगों को बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत सदस्यता प्रदान की गयी तो दूसरी तरफ मजदूर संघों, किसान संगठनों और सहकारी समितियों को संबद्ध (एफिलिएटेड) सदस्यता।
भारत और ब्रिटेन की परिस्थितियों की भिन्नता के चलते यह सांगठनिक व्यवस्था चल नहीं पाई। लेकिन इसके प्रयोग का सोशलिस्ट पार्टी पर गहरा असर पड़ा। असर का सकारात्मक पक्ष यह था कि वह अपना आधार ज्यादा विस्तृत कर पायी और नये इलाकों में उसका प्रवेश हुआ। नकारात्मक पक्ष यह था कि इससे पार्टी का अनुशासन ढीला पड़ गया और उसमें व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा के लिए पार्टी का इस्तेमाल करने और गुटबाजी करने जैसी कांग्रेसी बुराइयां घुस आयीं। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुरू का आदर्शवाद मंद और नष्ट होने लगा। यह बात शायद बहस-तलब बनी रहेगी कि नयी सांगठनिक व्यवस्था पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुई या नुकसानदेह। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इसने सोशलिस्ट पार्टी को एक बृहद चुनावी (इलेक्टोरल) मशीन बना डाला और उसका संगठन सुदूर इलाकों तक पहुंच गया।
पार्टी के इस एकाएक फैलाव ने बड़ी-बड़ी आशाएं जगायीं और जेपी व अन्य नेतागण यह सोचने लगे कि देश ब्रिटेन की तर्ज पर चुनावी राजनीति की एक द्वि-दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें सोशलिस्ट पार्टी खासी ताकत के साथ कांग्रेस की प्रधान विरोधी पार्टी के रूप में उभरेगी और इससे एक टिकाऊ लोकतांत्रिक राज्य-व्यवस्था (पॉलिटी) कायम हो सकेगी। सोशलिस्ट पार्टी द्वारा और उससे संबद्ध संगठनों- हिंद मजदूर सभा और हिंद किसान पंचायत- द्वारा आयोजित सार्वजनिक रैलियों में विशाल भीड़ होने पर जेपी और अन्य नेताओं के इस भ्रम को यथेष्ट बल मिला कि सोशलिस्ट पार्टी आम चुनाव में कांग्रेस की प्रधान विरोधी पार्टी के रूप में उभरकर आएगी। लेकिन भीड़ का मतलब वोट मिलना नहीं होता। पार्टी को रैलियों में भीड़ होने के कारण जो अपार समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता था, वह ऊपर-ऊपर के फेन सरीखा था और विडंबना यह थी कि पार्टी के संगठन को जन-मानस में अपनी पैठ गहरी करने के लिए फुरसत नहीं थी।
दूसरी तरफ महात्मा गांधी, नेहरू और अन्य हस्तियों के नेतृत्व में कांग्रेस की देश के हर गांव तक पहुंच थी और जन-मानस पर उसका गहरा प्रभाव था। यहां तक कि कम्युनिस्टों ने भी अपनी उपस्थिति जताये बिना दीर्घकाल तक काम कर देश के बहुत से हिस्सों में अपना सांगठनिक आधार खड़ा किया था। कुछेक विरल मौकों पर जन-लहर की विशेष परिस्थितियों की बात छोड़ दें, तो चुनावी राजनीति में मतदाताओं को मतदान केंद्रों में जाकर अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रेरित करना सबसे जरूरी सांगठनिक कार्य होता है। मजबूत संगठन न होने पर समर्थन वोट में परिणत नहीं होता। संगठनात्मक शक्ति के अभाव में 1952 के पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की भारी पराजय हुई। उसकी अपेक्षा तो कम्युनिस्ट ज्यादा कामयाब रहे। द्वि-दलीय राज्य-व्यवस्था के प्रति सम्मोहन के कारण सोशलिस्ट नेताओं में गहरी निराशा पैदा हुई। इस वक्त जेपी पार्टी के प्रधान सिद्धांतकार थे। पराजय से वही सबसे अधिक आहत हुए। चुनाव परिणामों का धैर्यपूर्वक संयत विश्लषण करने की जरूरत थी – आखिर इतनी भारी पराजय क्यों और कैसे हुई।
लेकिन जेपी की अपनी प्रवृत्ति हमेशा भावावेगात्मक प्रतिक्रिया करने की रही है। चुनाव में पराजय ने पार्टी के भीतर व्यक्तिगत झगड़ों और कलह का सिलसिला भी शुरू कर दिया। नेताओं के बीच मतभेद उभरने लगे। यह दलीय राजनीति से जेपी के मोहभंग का प्रारंभ था।
( जारी )
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.