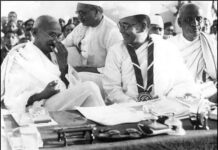(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
समाजवादी कल्पना पर कुठाराघात
इस उपभोक्तावादी दबाव ने मानव भविष्य की समाजवादी कल्पना की जड़ ही खत्म कर दी है। मार्क्स तथा कई अन्य समाजवादियों की यह अवधारणा थी कि भविष्य में समाज में उत्पादन का स्तर इतना ऊँचा उठ जाएगा कि मानव-आवश्यकता की वस्तुएँ उसी तरह उपलब्ध हो सकेंगी जैसे हवा या पानी उपलब्ध है। इससे आवश्यक वस्तुओं के अभाव से होनेवाली छीना-झपटी खत्म हो जाएगी और नया आदमी अपना अधिकांश समय मानवीय-बोध के विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे कला तथा दर्शन के विकास में लगाएगा। कई लोगों ने यह कल्पना की कि जैसे प्राचीन यूनान के कुछ नगर-राज्यों में गुलाम सारे शारीरिक श्रम का काम करते थे और नागरिक राजनीति, कला, दर्शन आदि विषयों में अपना समय लगाते थे, उसी तरह भविष्य में मशीनें वैसे सारे काम जो आदमी को अरुचिकर लगते हैं, करने लगेंगी और आदमी का सारा समय बौद्धिक विकास मे लगेगा। यह बहुत ही मोहक कल्पना थी। लेकिन इस कल्पना के पीछे यह मान्यता जरूर थी कि आदमी की जरूरतें सीमित हैं और एक समतामूलक समाज में मशीनों की मदद से थोड़े श्रम से इन जरूरतों की पूर्ति सब लोगों के लिए हो सकेगी। लेकिन उपभोक्तावाद ने आदमी की जरूरतों को एक ऐसा मोड़ दिया है कि वे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई असीमित होती जा रही हैं और बौद्धिक चिंतन के बजाय मनुष्य की सारी चिंता, सारा श्रम और सारे साधन इन नई जरूरतों की पूर्ति के लिए अनंतकाल तक लगे रहेंगे, हालाँकि प्राकृतिक साधनों के क्षय, प्रदूषण आदि से अपनी वर्तमान गति से आदमी की यह यात्रा अल्पकाल में ही समाप्त हो जाएगी।
इस विकास का एक प्रभाव यह पड़ा है कि विकसित पश्चिमी देशों में धीरे-धीरे यह अवधारणा बढ़ रही है कि मानव-बोध के वे सारे क्षेत्र जिनमें कल्पना का संबंध किसी प्रयोग से नहीं बन पाता, कला का संबंध किसी निजी या सामूहिक सजावट या उत्तेजना से नहीं बन पाता, वे सब अप्रासंगिक हैं। एक उपभोक्तावादी समाज हर वस्तु को उपभोग की कसौटी पर कसता है। ऐसा चिंतन जो प्रयोग के दायरे में नहीं आता कभी उपभोग के दायरे में भी नहीं आ सकता भले ही संप्रेषित होकर वह दूसरे मानव मस्तिष्क में एक नया बोध या सपनों का एक सिलसिला उत्प्रेरित करे, उपभोक्तावादी समाज के लिए निरर्थक हैं क्योंकि वह सपनों या कल्पना स बचना चाहता है। उसके लिए कल्पना की सीमा वे ठोस वस्तुएँ हैं जिन्हें वह छू सकता है, खरीद सकता है और जिनसे अपने घरों को सजा सकता है। इस तरह उपभोक्तावादी संस्कृति धीरे-धीरे मानव-बोध की उस विशिष्टता को नष्ट कर देती है जो मनुष्यों को अन्य जीवों से अलग करती है – यानी ठोस वस्तुओं से ऊपर उठकर कल्पना, अनुमान, प्रतीक आदि के स्तरों पर जीने की विशिष्टता। इस तरह उपभोक्तावादी संस्कृति एक तरफ थोक मशीनी उत्पादन के जरिए वस्तुओं से सृजन का तत्व निकाल देती है तो दूसरी ओर मानव-बोध से कल्पना की संभावना को।
लेकिन कोई भी मानव-भविष्य के समाजवादी या गैर-समाजवादी युटोपिया (कल्पनिक आदर्श) का उद्देश्य मनुष्य को उस स्थिति से मुक्त करने का रहा है जिसमें उसके व्यक्तित्व का चतुर्दिक विकास अवरुद्ध होता है। यही कारण है कि समाजवादी आंदोलन के पीछे वही मानवता काम कर रही है जो किसी बड़े धार्मिक उत्थान के पीछे होती है। इसी से हजारों लोगों को अपने उद्देश्यों के लिए अपने आप के बलि कर देने की प्रेरणा मिलती रही है। इसी कारण अपने विशुद्ध अर्थ में समाजवाद की राजनीति अन्य तरह की राजनीति से अलग रही है। मोटेतौर से राजनीति का केंद्रबिंदु संपत्ति का एक या दूसरी तरह से बँटवारा रहा है। राजनीति के मुद्दे होते हैं- कौन संपत्ति का हकदार होगा, किस व्यक्ति या समूह को किस भूमि या भूभाग पर अधिकार मिलेगा, किसकी क्या आमदनी होगी? और इन्हीं से जुड़ा यह सवाल कि किस व्यक्ति या समूह की क्या सामाजिक राजनीतिक हैसियत होगी। जब मार्क्स ने यही बात कही थी तो उस समय यह कुछ चौकानेंवाली बात लगी थी। लेकिन आज सभी लोग इस सच्चाई को मानने लगे हैं। इस कारण उन लोगों के सामने जिन्होंने नए तरह के समाज के निर्माण की कल्पना की थी, नक्शा ऐसे ‘आर्थिक-मनुष्यों’ का समाज बनाने का नहीं था। इस निरंतर चलनेवाले संपत्ति के बँटवारे की ऊहापोह को लेकर कोई मनीषी क्यों अपना पूरा जीवन लगाता? समाजवाद की कल्पना के पीछे असली भावना आदमी के जीवन को संपत्ति और उसके उन प्रतीकों से मुक्त करना था, जो उसे गुलाम बनाते हैं तथा उसके समुदायभाव को नष्ट करते हैं। इससे एक पूर्ण उन्मुक्त मानव की कल्पना जुड़ी थी। उपभोक्तावाद असंख्य नई कड़ियाँ जोड़कर मनुष्य पर संपत्ति की जकड़न को मजबूत करता है और इसीलिए हमारे युग में समाजवाद के सीधे प्रतिरोधी के रूप में उभरता है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.