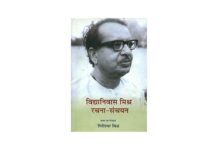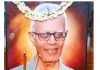— नन्दकिशोर आचार्य —
किसी भी व्यक्ति या समाज के सुसंस्कृत माने जाने की एक अनिवार्य परिणति यह है कि उसमें मानवाधिकारों के प्रति गहरे सम्मान का भाव हो और यह भाव उसके कार्य-व्यापार और आचरण में भी प्रतिफलित होता हो। यही कारण है कि विश्व के लगभग सभी राज्यों ने मानवाधिकारों के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने को उनके सम्मान और व्यवहार में उनके अनुकूल चलने से अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है, जिनमें भारत भी सम्मिलित है। इसी प्रतिबद्धता के चलते भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उसके राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के इन मानवाधिकार आयोगों का काम इस बात की निगरानी करना है कि उनके क्षेत्र में कहीं मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। साथ ही, कोई भी नागरिक अपनी ओर से भी इन आयोगों का ध्यान मानवाधिकार हनन के मामलों की ओर आकर्षित कर सकता है और उस मामले की जाँच करके आयोग उस पर उचित कार्रवाई करते हैं।
सामान्यतः, इतना पर्याप्त होना चाहिए था। लेकिन, यह विडंबनापूर्ण है कि स्वयं इन आयोगों की कार्यप्रणाली से भी कई बार मानवाधिकारों का हनन होता लगता है और शिकायतकर्ता के मन में असंतोष और बेचारगी का भाव पैदा होता है। किसी मनुष्य में बेचारगी और असहायता का भाव पैदा होना तो उसके मानवत्व का ही अपमान है- अधिकार की बात तो और भी आगे की बात हो जाती है। मानवाधिकार आयोगों को की जानेवाली शिकायतों को लेकर कोई कार्रवाई तो ऐसी स्थिति में बहुत दूर की बात लगती है, जब संबंधित शिकायत का संज्ञान लेने और उसकी प्राथमिक जाँच में ही महीनों लग जाना सामान्य बात है। सामूहिक महत्त्व के मामलों में तो मानवाधिकार आयोग फिर भी कुछ त्वरित कार्रवाई करते हैं- जैसे कि गुजरात काण्ड के मामलों में– जिसके लिए निश्चय ही वे प्रशंसा के हकदार हैं, लेकिन व्यक्तिगत मामलों की उचित सुनवाई या तो हो ही नहीं पाती और यदि होती है तो इतनी देर से कि तब तक संबंधित मामले के बहुत से सबूत धूमिल पड़ चुके होते या मिटा दिये जा सकते हैं।
यह मानना शायद ज्यादती होगी कि मानवाधिकार आयोगों द्वारा ऐसा जान-बूझ कर या किसी लापरवाही के कारण किया जाता है।
दरअस्ल, मानवाधिकार आयोगों के पास जिस संख्या में शिकायतें आती हैं, उन सबके प्राथमिक परीक्षण के लिए भी उनके पास पर्याप्त साधन और कर्मचारी नहीं हैं। इसी के चलते यह भी होता है कि जब किसी मामले को हाथ में लिया भी जाता है तो उसकी जाँच सरकारी विभागों के मामले में उन्हीं विभागों के अधिकारियों आदि से करवायी जाती है, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी होती है- जैसे कि पुलिस विभाग के खिलाफ शिकायत की जाँच संबंधित इलाके के एसपी और प्रशासनिक विभागों के खिलाफ शिकायत की जाँच जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्रशासनिक अधिकारी के सुपुर्द की जाती है।
ऐसी स्थिति में उस जाँच की अपनी प्रामाणिकता ही संदिग्ध बनी रहती है- बल्कि किसी भी जाँच के निष्पक्ष होने के बावजूद इस आशंका को निराधार नहीं बनाया जा सकता कि जाँच अधिकारियों ने सरकारी विभागों को बचाने की कोशिश की होगी- क्योंकि अधिकांश मामलों में सरकारी जाँच में इस प्रकार की लीपापोती की जाती रही है।
इसका कारण भी यही बताया जाता है कि राष्ट्रीय अथवा राज्य मानवाधिकार आयोगों के पास स्वतंत्र जाँच के अपने संसाधन नहीं हैं और ऐसी हालत में उन्हें सरकारी अधिकारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। स्मरणीय है कि यह सब तो ऐसी स्थिति में हो रहा है जबकि मानवाधिकार आयोगों के सम्मुख प्रस्तुत की गयी शिकायतें मानवाधिकार हनन के वास्तविक मामलों की तुलना में बहुत कम होती हैं। अधिकांश मामलों में तो भाग्य समझ कर चुप्पी साध ली जाती है क्योंकि पीड़ित पक्ष को अमूमन तो यह जानकारी ही नहीं होती कि वह कहाँ और किस तरह शिकायत कर सकता है तथा शिकायत की प्रक्रिया का उच्चावच क्रम क्या है। यदि यह जानकारी हो भी तो उसे यह प्रक्रिया इतनी लंबी और ऊबाऊ जान पड़ती है कि उसे ऐसा करने का उत्साह ही नहीं होता और कभी प्रारंभिक स्तर पर उत्तेजनावश कोई उत्साह होता भी है तो एक-दो बार के अनुभव से ध्वस्त हो जाता है। बहुत कम मामलों ऐसे होते हैं जिनमें शिकायतकर्ता में आखिर तक दम बचा रहता है- और ऐसा भी अक्सर तभी हो पाता है जब कोई गैर-सरकारी संगठन या मानवाधिकारों के लिए काम करनेवाला कोई स्वैच्छिक संगठन उस मामले में रुचि लेने लगे। लेकिन, ऐसे संगठन भी सब जगह उपलब्ध नहीं होते और उनके कार्यकर्ताओं की अपनी सीमाएँ भी बहुत स्पष्ट हैं। ऐसी स्थिति में किसी पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के लिए लंबे समय तक इस संघर्ष को चलाये रखना संभव नहीं होता। अपने जीवन को चलाये रखने की उसकी आवश्यकता उसे इस संघर्ष से धीरे-धीरे उदासीन कर देती है।
लेकिन, इस सब के बावजूद किसी मानवाधिकार आयोग की इस स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने लायक संसाधन उस के पास नहीं हैं। यदि संसाधन थोड़े-बहुत बढ़ा भी दिए जायें तो भी स्थिति में बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कि मानवाधिकार-चेतना बढ़ते जाने के साथ-साथ शिकायतों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होते जाना अपरिहार्य है। इसलिए, इस स्थिति से निपटने के लिए मानवाधिकार आयोगों की संगठनात्मक संरचना और कार्य-प्रणाली में ही कुछ प्रभावी परिवर्तन करने लाजिमी होंगे।
मानवाधिकार आयोगों की प्रमुख बड़ी समस्या तो यही है कि वे केंद्रीकरण के शिकार हैं। यदि पूरे देश से संबंधित मामलों की शिकायत एक ही जगह की जानी हो और उसकी जाँच आदि की प्रक्रिया एक ही केंद्र से नियंत्रित-निर्देशित की जानी हो तो यह स्वाभाविक ही है कि अधिकांश शिकायतें ठंडे बस्ते में पड़ी रहेंगी। यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा राज्यों के अपने मानवाधिकार आयोग भी हैं और उनसे संबंधित शिकायतें वहाँ की जा सकती हैं। लेकिन, भारत के राज्य यूरोप के कई बड़े राष्ट्रों से भी बड़े हैं और उनमें आनेवाली शिकायतों का निपटारा भी राज्यों की राजधानियों में बैठे आयोगों द्वारा त्वरित प्रभाव से किया जा सकना संभव नहीं है।
दरअस्ल, मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के उद्देश्य को तभी व्यवहार में लागू किया जा सकता है जब इन आयोगों का भी कम से कम जिला स्तर तक विकेन्द्रीकरण हो। राज्य मानवाधिकार आय़ोग की तर्ज पर ही जिला या जनपद मानवाधिकार आयोग बनाने की जरूरत से अब इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह लोक-अदालतें और उपभोक्ता-अदालतें जिला स्तर पर सक्रिय रहती हैं, उसी प्रकार मानवाधिकार आयोग गठन भी जिस्ला स्तर पर होना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि उस जिले में हो रही मानवाधिकार हनन की घटनाओं की ओर न केवल कोई भी नागरिक आसानी से उनका ध्यान आकर्षित कर सकेगा, बल्कि जिला आयोग और उसके सदस्य अखबारों आदि के आधार पर स्वयं भी उन घटनाओं का संज्ञान ले सकेंगे। स्थानीय स्तर के ऐसे संगठन भी इन मामलों को आगे बढ़ाने में अधिक प्रभावी हो सकेंगे जिनके पास वित्तीय अथवा अन्य प्रकार के ऐसे साधन उपलब्ध नहीं हैं जिनसे वे राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों को ले जाने में समर्थ हो सकेंगे।
इन जिला आयोगों में जिला स्तर के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधिकारी को आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है और जिले की स्वैच्छिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से आयोग अन्य सदस्य लिये जा सकते हैं। सदस्यों के चयन में यह ध्यान रखा जा सकता है कि उनमें प्रत्येक तहसील या ब्लाक के साथ स्त्रियों और दलित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो क्योंकि मानवाधिकार हनन की अधिकांश घटनाएँ इन्हीं वर्गों के साथ होती हैं।
जिला स्तर के ये आयोग राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के आयोगों की जाँच एजेन्सियों के रूप में भी काम कर सकते हैं और उनकी जाँच की निष्पक्षता और प्रामाणिकता भी उस तरह संदिग्ध नहीं समझी जा सकती जैसे सरकारी एजेन्सियों की मान ली जाती है। जिस प्रकार राजनीतिक-आर्थिक मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा राजनीतिक-आर्थिक विकेन्द्रीकरण के बिना संभव नहीं है, उसी तरह मानवाधिकारों की प्रभावी निगरानी भी निगरानी की प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के बिना मुमकिन नहीं हो सकती।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.