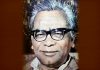— अरुण कुमार त्रिपाठी —
जेपी को इस बात का दोष दिया जाता है कि आज अगर देश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में हिंदुत्ववादी ताकतें हावी हैं और फासीवादी आचरण कर रही हैं तो इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा कहना एक ऐसे नायक के साथ अन्याय होगा जिसने अपने लिए कुछ चाहा नहीं। उसने सिर्फ एक स्वतंत्र, समृद्ध और समतामूलक देश बनाने के लिए ही आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी।
जेपी स्वाधीनता संग्राम के उन नेताओं में थे जिनके समक्ष युवावस्था में कैबिनेट मंत्री, फिर राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री बनने का खुला प्रस्ताव था। लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता से ठुकरा दिया। सत्ता का रंचमात्र लोभ उन्हें छू नहीं गया था लेकिन सत्तर साल की उम्र पार करने के बाद भी उनके भीतर संघर्ष करने और अन्याय को हराने का जज्बा था।
जब जेपी चंडीगढ़ में नजरबंद थे तो वहां के डीएम एम.जी. देवसहायम उनके संपर्क में आए। वे जेपी से प्रभावित होते गए और जेपी की निराशा को उम्मीद में बदलने और उनके आमरण अनशन के फैसले को वापस करवाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। जेपी जब लगातार बीमार होते चले गए और उनके गुर्दे खराब होने लगे तो उन्हें बंबई के जसलोक अस्पताल ले जाया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर उन्होंने देवसहायम से कहा, “देवसहायम तुम मेरे बेटे जैसे हो। हालांकि मेरा अपना कोई बेटा नहीं है। मेरी सेहत जरूरी नहीं है। देश और लोकतंत्र की सेहत महत्त्वपूर्ण है। मैं उस औरत को हराऊंगा और लोकतंत्र की सेहत ठीक करूंगा।”
उन्हीं देवसहायम ने जेपी और आपातकाल पर तीन पुस्तकें लिखी हैं। पहली है इंडियाज सेकेंड फ्रीडम- एन अनटोल्ड स्टोरी। दूसरी है जेपी इन जेल— एन अनसेंसर्ड अकाउंट । तीसरी है— जेपी मूवमेंट—इमरजंसी एंड इंडिया सेकेंड फ्रीडम। देवसहायम का चंडीगढ़ में जेपी से जो परिचय हुआ वह आखिर तक बना रहा। वे उनसे कदमकुआं (पटना) में भी जाकर मिलते रहते थे।
देवसहायम ने अपने वर्णन में लिखा है कि जेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली से दुखी थे। बल्कि जनता पार्टी टूटने और एक वैकल्पिक सरकार के प्रयोग को विफल होने में संघ की भूमिका मानते थे। जेपी एक तरह से संघ से छला हुआ महसूस कर रहे थे।
जेपी और संघ की सोच का अंतर उनके और सरसंघचालक बाला साहेब देवरस के इंदिरा गांधी को लिखे पत्र के फर्क से भी महसूस किया जा सकता है। देवरस ने 22 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर उनके लाल किले वाले भाषण की तारीफ की थी। फिर जो माफीनामा सरकार की ओर से लिखवाया गया उसमें यह भी कहा गया था कि “बाहर निकलने के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो। न ही वे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रोकेंगे और न ही किसी गैरकानूनी गतिविधि में हिस्सा लेंगे। न ही वे आपातकाल की आलोचना करनेवाली किसी गतिविधि का हिस्सा बनेंगे।”
दरअसल जेपी से संघ और जनसंघ के बड़े नेताओं ने वादा किया था कि वे दोहरी सदस्यता का मुद्दा नहीं आने देंगे। लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिरी दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर ही।
इस बात को जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी माना। उन्होंने कहा, “मैं उम्मीद करता था कि बाला साहेब देवरस अपना वादा निभाएंगे। पर मुझे हैरानी नहीं हुई जब आरएसएस ने दूसरा रुख अपनाया। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई।” दरअसल जनता पार्टी संसदीय बोर्ड का प्रस्ताव था कि जनता पार्टी के सदस्य शाखा में न जाएं। चंद्रशेखर यह प्रस्ताव जेपी के कहने पर ही लाए थे। लेकिन उसे लागू नहीं करवा सके और आखिरकार पार्टी टूटी और सरकार गिर गई।
जहां तक हिंदू राष्ट्र, गोरक्षा और हिंदू इतिहास का सवाल है तो उसपर जेपी के विचार स्पष्ट थे और उन्हें किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। उन्होंने कहा था, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह के कुछ लोग खुले तौर पर भारतीय राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। कुछ लोग उसे ज्यादा परोक्ष रूप से पेश कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की पहचान के भीतर राष्ट्रीय विखंडन छुपा हुआ है क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और दूसरे दर्जे के नागरिक बनने को तैयार नहीं होंगे। इस तरह की स्थिति अपने भीतर स्थायी रूप से विवाद रखे हुए है और आखिरकार इसका परिणाम बिखराव में ही होगा।”
जेपी ने कहा था कि जब हम भारत के इतिहास को हिंदू इतिहास के रूप में देखने की कोशिश करते हैं तो हम भारत के महान इतिहास और सभ्यता को छोटा करके आंकते हैं।
गोरक्षा के बारे में वे कहते हैं, “मैं नहीं समझता कि हिंदू धर्म ने कभी ऐसा सोचा था कि कोई भी जानवर कितना भी पवित्र हो लेकिन उसका जीवन मनुष्य के जीवन से ज्यादा पवित्र है। यह प्रभाव तो दरअसल बौद्धों और जैनियों से प्रेरित होकर आया है जिन्होंने मांसाहार और जीव हत्या पर रोक लगाने की कोशिश की। उसी के बाद गायों को ज्यादा पवित्रता प्रदान की गई।”
जेपी की संपूर्ण क्रांति की विरासत में न तो हिंदुत्व है और न ही बहुसंख्यकवाद। उसमें सांप्रदायिक वैमनस्य तो हो ही नहीं सकता।
यह सही है कि जेपी के कई शिष्य बहुत भ्रष्ट निकले पर यह नहीं भूलना चाहिए कि जेपी की लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही थी। उन्हें युवाओं के रोजगार की चिंता थी और चिंता थी भारत से जातिवाद और सांप्रदायिकता मिटाने की।
जेपी रोटी और स्वाधीनता के बीच कोई टकराव नहीं देखते थे। उनकी संपूर्ण क्रांति की विरासत में नागरिक अधिकारों के लिए महत्त्वपूर्ण जगह है।
आज जिस तरह राष्ट्र, सरकार, बहुसंख्यक समाज के लिए नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है ऐसे में जेपी का वह कथन बहुत प्रासंगिक है जो उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती देते हुए कहा था, “मेरे लिए स्वाधीनता मेरे जीवन के आकाशदीप की तरह से है। यह हमेशा से ऐसे ही रही है। इसका मतलब है कि मानव व्यक्तित्व, मानव मस्तिष्क, मानवीय आत्मा की स्वतंत्रता मेरे जीवन का राग है। मैं नहीं चाहूंगा कि भोजन, सुरक्षा, समृद्धि, राज्य की गरिमा या किसी भी अन्य चीज के लिए इसके साथ समझौता किया जाए।’’
भला ऐसे जेपी की संपूर्ण क्रांति की विरासत को कैसे फासिस्ट विरासत कहा जा सकता है? क्योंकि फासीवाद तो राष्ट्र और नस्ल के गौरव के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुर्बान करने को तैयार रहता है। जेपी वास्तव में एक क्रांतिकारी लोकतंत्र के स्वप्नद्रष्टा थे जिसमें गांधी के भारतीय लोकतंत्र की कल्पना भी शामिल थी और यूरोपीय लोकतंत्र के तत्त्व भी थे।

संपूर्ण क्रांति की अवधारणा
जेपी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को अपने स्वास्थ्य और राजनीतिक संघर्ष के कारण बहुत विस्तार नहीं दे सके लेकिन परवर्ती काल में उनके मित्रों और अनुयायियों ने इसपर लिखा है। जेपी के निजी सचिव सच्चिदानंद सिन्हा उर्फ सच्चिदा बाबू ने चार खंडों में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को विस्तार दिया है। इसी तरह लखनऊ मेडिकल कालेज के प्राचार्य रहे डॉ एम. एल. गुजराल ने भी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को विस्तार देने का प्रयास किया है। गांधीवादी संस्थाओं से जुड़े सुभाष मेहता भी ‘ए हैंडबुक आफ सर्वोदय’ शीर्षक से लिखी पुस्तक के दो खंडों में गांधी, विनोबा और जयप्रकाश नारायण के विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं।
जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति मनुष्य और उसके समाज में भीतर और बाहर अहिंसक तरीके से किए जानेवाले बुनियादी परिवर्तन का नाम है। इसके मूल में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के मूल्य हैं।
जेपी ने 1959 में ‘भारतीय राजनीति की पुनर्रचना की अपील’ और 1961 में ‘जनता के लिए स्वराज’ शीर्षक से दो महत्त्वपूर्ण लेख लिखे थे। उसमें उनके संपूर्ण क्रांति के विचार मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने 1969 में एक लेख लिखा जिसमें सबसे पहले संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग किया। यह विचार जयप्रकाश नारायण की एक निस्वार्थी और बलिदानी बौद्धिक और राजनीतिक यात्रा का मानवता और विशेषकर भारत के लिए निचोड़ है।
जेपी के विचार देखने पर टेढ़े-मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए लगते हैं लेकिन वह एक ईमानदार क्रांतिकारी का सत्य और स्वतंत्रता के साथ प्रयोग है।
जेपी शुरू में राष्ट्रवादी थे, आगे चलकर मार्क्सवादी हुए और फिर लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से गांधीवाद के करीब आए और फिर सर्वोदय से होते हुए संपूर्ण क्रांति के मुकाम तक गए। हालांकि जेपी अपनी व्याख्या में सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति में ज्यादा अंतर नहीं देखते और वे सर्वोद्य को साध्य और संपूर्ण क्रांति को साधन मानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि संपूर्ण क्रांति, सर्वोदय आंदोलन की तरह से ठहरा हुआ विचार या व्यवहार नहीं है बल्कि एक प्रतिरोधी गतिशीलता और नवनिर्माण का विचार है।
जेपी समाजशास्त्र के गंभीर विद्यार्थी थे और मार्क्सवाद का उनका अध्ययन भारत में उनके समकालीन किसी भी मार्क्सवादी से कम नहीं था। इसलिए जब 1974 में पहली बार उन्होंने व्यवहार के तौर पर युवाओं के समक्ष संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो यह अचानक प्रकट होनेवाली धारणा नहीं थी। इसकी एक मार्क्सवादी परंपरा है और जेपी से ज्यादा इस बात को कौन समझ सकता है। टोटल रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1847 में कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘पावर्टी आफ फिलासफी’ में दिया था। जेपी ने 127 साल बाद उस अवधारणा को भारत में उतारने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स ने कहा था, “इस बीच सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच का अंतर्विरोध एक वर्ग का दूसरे वर्ग से संघर्ष है। यह संघर्ष अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति संपूर्ण क्रांति में प्रकट करता है।”
जेपी मार्क्सवादी दर्शन में वर्णित क्रांति की अवधारणा और उसके साथ ही सर्वहारा की तानाशाही की अनिवार्यता को त्याग चुके थे। यही वजह है कि वे सर्वोदयी विचारों के साथ जुड़े। लेकिन वर्ग की उपस्थिति और उनके बीच टकराव की वास्तविकता को वे आखिर तक स्वीकार करते रहे।
सन 1977 में जेपी ने छात्र संघर्ष वाहिनी के युवाओं को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि संपूर्ण क्रांति जीवन के सभी पक्षों में परिवर्तन करना चाहती है और वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की एक जीवन शैली विकसित करना चाहती है। उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए वर्ग संघर्ष को एक तकनीक के रूप में स्वीकार किया था।
जब जेपी के इस इंटरव्यू पर उनके सर्वोदयी साथी आपत्ति करने लगे और यह भी कहने लगे कि अब वे फिर मार्क्सवाद की ओर जा रहे हैं तो उनका कहना था कि वर्ग संघर्ष कोई पैदा नहीं करता। वास्तव में समाज में शक्तिशाली और कमजोर दो किस्म के तबके रहते हैं। सवाल इस बात का है कि आप किस वर्ग के साथ खड़े होते हैं।
जेपी ने लंबे समय तक सर्वोदय आंदोलन में भूदान और ग्रामदान के लिए काम करते हुए यह जान लिया था कि वह तरीका ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। उनका यह यकीन कमजोर हो गया कि शक्तिशाली तबका स्वयं उदारता दिखाते हुए कमजोर वर्ग की जिम्मेदारी लेगा। यही वजह थी कि उन्होंने कमजोर वर्ग को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए दावा करने आह्वान किया। उनका संदेश लड़ाई लड़ने का नहीं था लेकिन खामोश बैठने का भी नहीं था। वे चाहते थे कि कमजोर तबका कार्रवाई करे। उसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध और असहयोग का रास्ता सुझाया। कुल मिलाकर वे सत्याग्रह के माध्यम से अपनी संपूर्ण क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे।
उनकी संपूर्ण क्रांति में जिन सात क्रांतियों को शामिल किया गया था वे थीं – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधारात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक।
जेपी की इस क्रांति की अवधारणा में खास बात राजशक्ति पर लोकशक्ति का नियंत्रण कायम करना था।
यही कारण है कि जेपी जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को दिए जाने के पक्ष में थे। इन सबसे ऊपर जेपी के भीतर एक उच्च नैतिकता बोध था और उसी से जुड़ा हुआ सेवा भाव था। यही कारण है वे विभिन्न राजनीतिक दलों की छल कपट की भाषा और कार्रवाई को नापसंद करते थे। इसी बात को आगे ले जाते हुए उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की बात की थी।
जेपी की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा आकर्षक है और समय की मांग भी है लेकिन वह एक प्रकार से आदर्शवादी और यूटोपिया वाली भी है। मधु लिमये ने उनके पार्टी-विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया था। इसी प्रकार जेपी ने छात्रों को क्रांति की मशाल थमाने की कोशिश की थी लेकिन न तो वह कोई स्थायी तबका है और न ही उसकी वर्गीय निष्ठाएं स्पष्ट हैं। इसलिए उनकी क्रांति शायद परवान नहीं चढ़ सकी।
जेपी के अनुसार आज का औद्योगिक मजदूर वर्ग पेटी बुर्जुआ हो गया है इसलिए उससे क्रांतिकारी कामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसकी तुलना में वे ग्रामीणों पर कुछ भरोसा करने की बात करते थे और सामूहिक खेती की पैरवी करते थे। आज देश में किसान आंदोलन चल रहा है और खेती- किसानी पर नए किस्म का संकट है। दूसरी ओर देश में असमानता बढ़ रही है और स्वतंत्रता और भाईचारे पर नए किस्म के खतरे उपस्थित हैं तब जेपी की संपूर्ण क्रांति पर चर्चा की बहुत जरूरत है। ऐसे में जेपी को फासिस्ट या फासिस्टों का साथी कहना हमें भटकाने के अलावा कहीं नहीं ले जाएगा।
जेपी की पूरी सोच के केंद्र में मनुष्य है, राष्ट्र या नस्ल नहीं। वे नागरिक अधिकारों के हिमायती हैं।
ध्यान रहे कि उन्होंने जो कहा था वह अपने अनुभव और समय के लिहाज से कहा था। आज सैंतालीस साल बाद देश को नैतिक पतन से निकालने और मानवीय गरिमा के मूल उद्देश्य को जाग्रत करने के लिए उसकी नई व्याख्या की आवश्यकता है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.