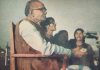— राकेश सिन्हा —
— राकेश सिन्हा —
अगर भूमिहीन मजदूरों को उपज का हिस्सा नहीं दिया जाता तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कृषि और संबंधित उद्योगों में रोजगार को मिलाकर किसी भी परिवार की आमदनी 20 हजार रु. प्रतिमाह से कम न हो। इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए कानूनों में किस तरह का बदलाव करना पड़ेगा उसपर शोध और विचार करने की जरूरत है। अगर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा, मान लीजिए, पंद्रह प्रतिशत ही है तो यह देश के श्रमिक परिवारों के पंद्रह प्रतिशत के लिए ही काफी है। लेकिन कृषि में अगर श्रमिक परिवारों का 45 प्रतिशत हिस्सा लगा है तो कृषि से उनकी आय उनकी कुल आय का एक तिहाई ही होना चाहिए और दो तिहाई आय के लिए अन्य स्रोत होने चाहिए। पंजाब और हरियाणा में इस तरह के उपाय सिर्फ छोटी जोत वाले किसानों के लिए करने की जरूरत होगी।
खेती की जमीन के इस तरह के बँटवारे के साथ कुछ और उपाय भी करने होंगे। इन उपायों के लिए जीरो बजट खेती के मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरफ तो अच्छी किस्मों के बीजों का प्रबंध करना होगा जहां सभी किसानों के लिए सभी फसलों के बीज तैयार किए जाएं। साथ ही खेती की पूरी जमीन के लिए स्थानीय जरूरत के हिसाब से देसी खाद और कीटनाशक तैयार किया जाए। बीज, खाद और कीटनाशक का एक केंद्र पूरी पंचायत के लिए काम कर सकता है। इसके लिए जमीन आदि की व्यवस्था पंचायत में करनी होगी और इसमें भी हर पंचायत में कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता है।
अभी जो खाद और कीटनाशक इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें धीरे-धीरे घटाते हुए देसी खाद और कीटनाशक का प्रयोग बढ़ाना होगा ताकि उत्पादकता पर तुरंत बदलाव का कोई असर न पड़े और जमीन तथा फसल में भरे रासायनिक जहर को धीरे-धीरे खत्म किया जा सके। इस तरह कुछ ही वर्षों में किसान बीज, खाद और कीटनाशक के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे और देसी तरीके से तीनों की गुणवत्ता बढ़ाते रह सकेंगे और खेती की उत्पादकता भी। खेती की लागत में इससे एक बड़ी कटौती होगी।
इसके साथ ही छोटी-छोटी जोत की खेती की जरूरतों के अनुकूल छोटी मशीनें विकसित और विनिर्मित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाना होगा। अगर 10 हार्स पावर से कम की एक ट्रैक्टर जैसी मशीन उपलब्ध कराई जा सके जिसमें पुर्जे बदल-बदल कर खेती के सभी काम, जब जैसी जरूरत पड़े, किए जा सकें तो खेती के काम को काफी सस्ता और आसान बनाते हुए उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है और समय की बचत भी की जा सकती है। इस प्रकार के कृषि उपकरण दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो इस तरह की मशीन डिजाइन भी कर सकते हैं और प्रोत्साहन तथा समर्थन मिलने पर इसका उत्पादन भी कर सकते हैं। बहुत-से लोग इस तरह की मशीनें बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। लेकिन यह बहुत छोटे स्तर पर हो रहा है। अगर सही सरकारी नीतियां बनें तो इस प्रकार के कृषियंत्रों की मांग करोड़ों में हो सकती है। इसके लिए हर जिले के नहीं तो कम से कम मंडल स्तर पर एक विनिर्माण इकाई की जरूरत हो सकती है। अगर एक मशीन बीस साल तक काम कर सकती है तो औसतन हर पंचायत में पच्चीस से तीस मशीनों की जरूरत हर साल पड़ेगी। हर ब्लाक में एक बिक्री केंद्र हो सकता है और हर पंचायत के लिए मशीनों की मरम्मत तथा रखरखाव में प्रशिक्षित मैकेनिकों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें अन्य मशीनों की मरम्मत और रखरखाव में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है।
कृषि के लिए एक बहुत जरूरी पहलू सिंचाई का है। हमारी ज्यादातर खेती वर्षा के भरोसे रहती है। इसकी वजह से हमारी कृषि सूखा, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि और बाढ़, सभी से प्रभावित होती है। इसके लिए हमें एक तरफ तो सूखा और बाढ़ के चक्र को सँभालना होगा तो दूसरी तरफ सिंचाई के साधन और वर्षा के इस्तेमाल को तर्कसंगत बनाना होगा। वर्षा के नियंत्रण में जंगल की भूमिका बहुत अहम है। हमें लगभग एक तिहाई जमीन पर पेड़ों की जरूरत होती है और ये पूरे देश में एक व्यवस्थित तरीके से फैले होने चाहिए। उनका कुछ हिस्सा फलों के बगीचों का हो सकता है तो कुछ हिस्सा इमारती लकड़ी आदि के काम आनेवाला और बाकी पर हर तरह के पेड़ होने चाहिए।
कुछ खास इलाकों को छोड़ कर हमारे देश में कम से कम इतनी तो वर्षा होती है कि पीने और सिंचाई के पानी की कमी न पड़े। हमें जल प्रबंधन के ऐसे तरीके अपनाने होंगे कि भूजल का स्तर बना रहे और हमारी सभी जरूरतें भी पूरी होती रहें। इसके लिए हमें एक तरफ तो नदियों की सफाई कर उन्हें औद्योगिक तथा शहरी प्रदूषण से बचाना होगा तो दूसरी ओर चेकडैम जैसे उपाय कर सतह के ऊपर के जल-स्तर को भी बहुत कम न होने देने की व्यवस्था करनी होगी। तालाबों और कुओं की सफाई कर पारंपरिक जल प्रबंधन की संस्कृति को फिर से नया जीवन देना होगा। सिंचाई और पीने के लिए केवल सतह के ऊपर के और सतह के समीप भूजल का इस्तेमाल करने तक अपने को सीमित करना होगा।
भूजल का उतना ही दोहन किया जाना चाहिए जितना हर साल उसमें भरा जा सके। गहरे ट्यूबवेल, मोटर पम्प का इस्तेमाल बंद होना चाहिए लेकिन तालाब और सिंचाई वाले कुओं से छोटे पम्पों का इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाए। सूखे और बाढ़ के चक्र पर नियंत्रण करना और देश की जरूरत के अनुरूप सिंचाई तथा पेयजल की व्यवस्था करना देश के युवा इंजीनियरों के लिए एक अहम चुनौती है जिसे उन्हें स्वीकार करना होगा।
खाद, बीज, कीटनाशक और सिंचाई के तर्कसंगत प्रबंधन को छोटी मशीनों के इस्तेमाल के साथ जोड़कर और खेती में मेहनत कर फसल तैयार करनेवाले वर्ग को फसल का बड़ा हिस्सा देकर हम उनमें कृषि के सारे परंपरागत ज्ञान को फिर से नया करते हुए कृषि की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने के लिए सही माहौल दे सकते हैं। यदि उत्पादकता दो गुनी भी हो जाती है, जैसा कि चीन में दिखाई दे रहा है, जबकि हमारी कृषिभूमि उनसे ज्यादा अच्छी और उर्वर है, तो जमीन पर मालिकाना हक वाले वर्ग को मिलनेवाला फसल का तीस प्रतिशत हिस्सा भी आज अधिया पर खेती कराने से मिलनेवाले पचास प्रतिशत हिस्से से ज्यादा हो जाएगा।
सरकार को इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि कोई भी कृषिभूमि परती नहीं छोड़ी जाएगी और जो लोग खुद अपनी जमीन पर खेती नहीं करते हैं उन्हें अपनी जमीन अनिवार्य रूप से, फसल के तीस प्रतिशत हिस्से के आधार पर पंचायत के भूमि भंडार के लिए देनी होगी। भूमि पर श्रम करनेवालों को भी ज्यादा हिस्सा मिलने के साथ श्रम और समय की बचत होगी और उनके पास अन्य स्रोतों से बेहतर आमदनी का भी अवसर होगा।
हर पंचायत में, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से एक एकड़ से लेकर पांच एकड़ तक के कुछ तालाब होने चाहिए और पंचायत की जरूरत के हिसाब से स्थित होने चाहिए। इनकी सफाई और रखरखाव का नियमित इंतजाम होना चाहिए। इन तालाबों के चारों तरफ फलों के बगीचे लगाए जा सकते हैं और तालाब का इस्तेमाल मछली पालन के लिए भी होना चाहिए। पूरी पंचायत में एक जगह पर पशुपालन की सामूहिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें देसी नस्ल की गायों का इस्तेमाल हो और दुग्ध तधा दुग्ध उत्पादों का उचित प्रबंधन किया जा सके। हर पंचायत में कुक्कुट पालन का भी सामूहिक प्रबंध किया जा सकता है।
हमारे देश में चरागाह बहुत कम हैं इसलिए देश की आबादी के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत चौपाये जानवरों का मांस न होकर दूध, दही, पनीर आदि के साथ मुर्गी, अंडा और मछली ही हो सकता है। सेहत के लिए भी यह ज्यादा मुफीद है और हमारे देश की जलवायु के ज्यादा अनुकूल भी। पंचायतों में होनेवाले हर प्रकार के उत्पादन, अनाज, सब्जी, फल, दुग्ध उत्पादों, मछली और कुक्कुट की सत्तर प्रतिशत खपत तो गांवों में ही हो जानी चाहिए क्योंकि देश की सत्तर प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में ही रहती है। जो भी उत्पाद पंचायत के बाहर भेजे जाने हैं उसमें अधिक से अधिक संभव मूल्य-वर्धन पंचायत के अंदर ही हो जाना चाहिए। जैसे गेहूं की जगह आटा, सूजी, मैदा और दलिया आदि गांवों में ही तैयार कर लिये जाने चाहिए। इन उत्पादों के विनिर्माण और विक्रय के लिए एक या एक से अधिक छोटी कंपनी पंचायत स्तर पर बनाई जानी चाहिए, जिनका प्रबंधन सामुदायिक स्तर पर ही हो सके या कृषि का प्रबंधन करनेवाली कंपनी ही इसे भी करे।