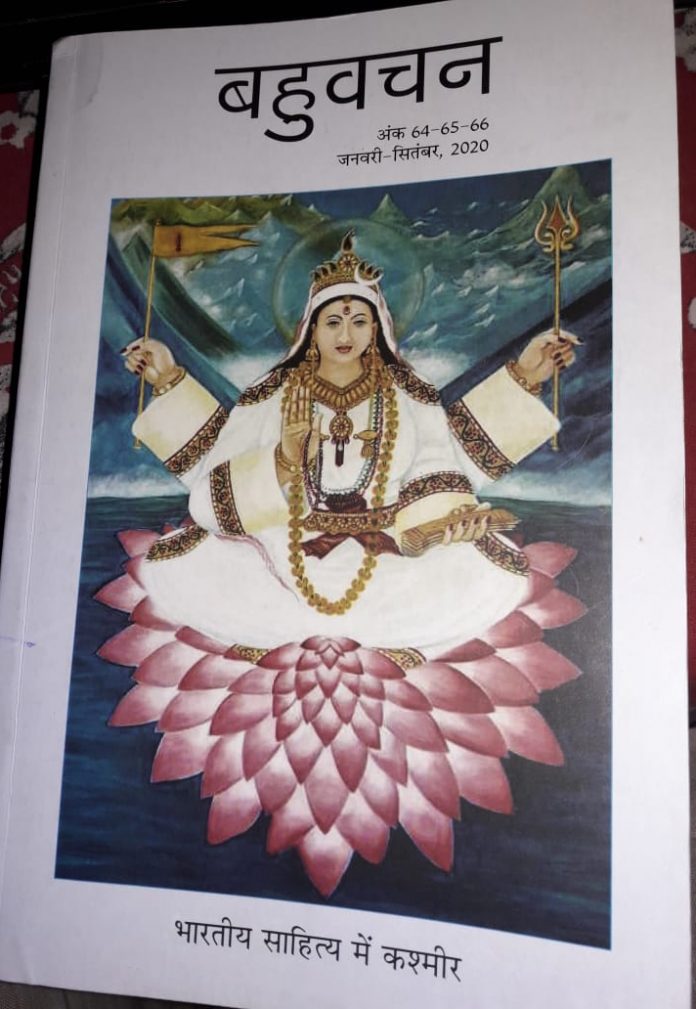— अरुण कुमार त्रिपाठी —
सरकारी सीमाओं की मजबूरियों के बावजूद महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की पत्रिका ‘बहुवचन’ ने भारतीय साहित्य में कश्मीर पर केंद्रित एक समृद्ध अंक निकाला है। कोरोना काल में यह काम कठिन था लेकिन कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल के कुशल नेतृत्व में और प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे के दृष्टि संपन्न संपादकीय समन्वय में जनवरी से सितंबर 2020 तक के तीन अंकों को समाहित करके 508 पृष्ठों का भारी-भरकम अंक पाठकों के समक्ष आ ही गया। ऐसा तो नहीं कह जा सकता कि इस अंक में वह सब कुछ है जिसकी आप अपेक्षा कर सकते हैं लेकिन इसमें विषयों और सामग्री की इतनी विविधता है कि पत्रिका बहुवचन अपना नाम सार्थक करती हुई लगती है। कहते हैं कि जब विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अशोक वाजपेयी ने यह पत्रिका निकाली थी तो इसका नाम यही कहते हुए रखा था कि इस देश में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो एकवचन में हो इसलिए इसका नाम बहुवचन ही रखा जाना चाहिए।
निश्चित तौर पर पत्रिका में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जिसे कुछ लोग हिंदू परंपरा भी कहते हैं के साहित्य और दर्शन से संबंधित बहुत सारी और प्रामाणिक सामग्री है। उग्रवाद और अलगाववाद से ग्रसित कश्मीर के प्रति पाठकों और शेष भारत में पैदा होती विरक्ति के वातावरण में यह सामग्री पाठकों के भीतर उस हिस्से के प्रति एक अनुराग उत्पन्न करती है। दस खंडों और पांच स्थायी स्तंभों के साथ यह पत्रिका एक गहन समुद्र मंथन के साथ जिन पंद्रह रत्नों के साथ अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होती है वे सब अपने में बेजोड़ हैं। प्रोफेसर रजनीश शुक्ल अपने स्तंभ ‘कीर्ति कलश’ में कहते हैं, “वस्तुतः कश्मीर की संस्कृति का अवबोध भारतीयता का अवबोध है। कश्मीरियत भारतीयता से अलग नहीं भारत की चिति है। यह कश्मीरियत विशिष्ट संस्कृति न होकर निरंतर संस्कार की सभ्यता है। भारत का स्वत्व है। जड़ता की सभ्यता के विरुद्ध ज्ञानात्मक समाज एवं मूल्यात्मक विज्ञान की प्रतिष्ठा है।’’
इसी संकलन के महत्वपूर्ण आलेख में वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार जवाहरलाल कौल कश्मीरियत को अपने अनुभव के आधार पर समाजशास्त्रीय ढंग से परिभाषित करते हैं, “ कश्मीरियत मूल रूप से राजनीतिक कम, सास्कृतिक-सामाजिक स्थिति अधिक है, जिसे कश्मीर और राज्य के बाहर के पृथकतावादी नेताओं को अपने वास्तविक रूप से विलग करने में लगभग एक शताब्दी का समय लगा। …..लेकिन इसके अंकुर छह सौ वर्ष पहले कश्मीर में बहने वाली एक सांस्कृतिक धारा के कारण फूटे थे। नाम तब तक कश्मीरियत नहीं पड़ा था।’’
इस भावना की व्याख्या करते हुए कौल साहब बताते हैं कि, “यह प्रेम, सद्भावना, अध्यात्म, दर्शन और ज्ञान का ऐसा आंदोलन था जिसमें पीड़ा सहना तो स्वीकार था लेकिन पीड़ा देना स्वीकार नहीं था। इसे भारत के अन्य प्रदेशों में भक्ति आंदोलन कहा गया लेकिन कश्मीर में तब कोई विशेष नाम नहीं दिया गया।’’ दरअसल कश्मीर के लोग मुसलमान तो हो गए थे लेकिन जो कोई ध्यान से देखता वो यही कहता कि भीतर से वे अभी भी हिंदू हैं। “यह सच है कि कश्मीर की अधिकतर आबादी को धर्मांतरण करना पड़ा लेकिन कश्मीरियत का सांस्कृतिक आधार समाप्त नहीं हुआ।वह लोक मन में अनेक रूपों में विद्यमान रहा। लल्लेश्वरी ने कोई पंथ संवाद या संगठन नहीं चलाया, वे समाज को झकझोर कर इस संसार से चली गईं, लेकिन नुंद ऋषि की परंपरा उनके पश्चात भी जारी रही। उनके जाने के बाद उनके शिष्यों के चार आश्रम विभिन्न स्थानों पर बने, जो कई पीढ़ियों तक नुंद ऋषि की परंपरा का विस्तार करते रहे। इनमें अधिकतर ऋषि न केवल शाकाहारी थे बल्कि इन स्थानों में ऋषियों और पूर्वजों का भारतीय तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता था।’’
यह संकलन एक ओर वर्तमान संदर्भ में कश्मीर को विशिष्ट दर्जा देने के वाले अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए को हटाए जाने के बाद की गई कार्रवाई के अच्छे परिणामों को प्रस्तुत करता है, दूसरी ओर इस्लाम के आने से पहले की वहां की शैव, बौद्ध और दूसरी दार्शनिक और सांस्कृतिक धाराओं का वर्णन करता है तो तीसरी ओर इस्लाम को मानने वाले शासकों और कवियों रचनाकारों की विरासत का विरासत वर्णन करता है। समन्वय संपादक कृपाशंकर चौबे अपने स्तंभ ‘आरंभिक’ में लिखते हैं, “संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक पारित कर पांच भाषाओं- कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी को जम्मू-कश्मीर की राजभाषा बना दिया गया है। इससे अब तक उपेक्षित रहीं कश्मीरी डोगरी जैसी भाषाओं को पहली बार न्याय मिला है।’’ संस्कृत साहित्य में कश्मीर के योगदान की चर्चा करते हुए प्रोफेसर चौबे लिखते हैं, “संस्कृत साहित्य के आचार्य मुक्ताकण, शिवस्वामी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र बिल्हण, कल्हण, सोमदेव, गुणाढ्य, अभिनवगुप्त, उत्पल, कैयट, मम्मट, मंख, जगद्धर भट्ट इसी धरती के थे। संस्कृत साहित्य में उनकी देन अप्रतिम है।’’
इस अंक में एक ओर कश्मीरी पंडितों के निर्वासन की गहरी पीड़ा है तो दूसरी ओर महामाहेश्वर अभिनवगुप्त के शैव दर्शन और उनके विविध योगदान का विशद वर्णन है तो उसके नीचे एक धारा आदि कवयित्री लल्लेश्वरी के वाखों की है तो साथ में फारसी, उर्दू और कश्मीरी लेखकों और कवियों के रचनाओं की है। अग्निशेखर के काव्य संकलन `जलता पुल’ की एक कविता `ओ ललद्यद’ में कवि लल्लेश्वरी का आह्वान कुछ इस प्रकार करता है –
आज फिर पिला दे अपना दूध
वे पी रहे हैं हमारा खून
और हम
खून के आंसू
देखो सरक रही है हमारे ऊपर से
काले गिद्धों की परछाइयां
तैर रही हैं ये छायाएं
आंगन आंगन
गली-चौबारों, छतों
सड़कों स्कूलों
खेतों, जंगलों
तीर्थों, उत्सवों के ऊपर से
और कुछ पर्यावरणविदों को चिंता है
कि संसार में कम होते जा रहे हैं गिद्ध
अग्निशेखर, लल्लेश्वरी से ही नहीं संवाद करते। वे आचार्य अभिनवगुप्त से भी प्रश्न करते हैं।
हे महापूर्वज!
इन चिथड़े तंबू घरों में हम निर्वासित
हर शाम जलाते रतनदीप
और तन्मय हो पढ़ते
तुम्हारा भैरव स्त्रोत
हे महापूर्वज!
क्या सुन रहे हो इस पल
मेरे बगल के तंबू से आ रही
जीनोसाइड की शिकार
एक कश्मीरी बुढ़िया की पोपली आवाज में
इन नारकीय दिनों में भी
बची हुई आस्था
इसी तरह फारूख नाजिकी की एक कविता कश्मीर में मची मारकाट का वर्णन अपने ढंग से करती है –
मेरे हाथों से मेरी चिता बन गई
मेरे कंधों पर मेरी अर्थी उठी
पालकों की नोक से
दिनों के पृष्ठों पर
मेरे रक्त से मेरा नाम लिखा गया
और मैं चुप रहा
……………………
मेरे सरसब्ज जंगल उजाड़े गए
मेरी झीलों में अजगर बसाए गए
हारी पर्वत की इज्जत लूटी गई
मृत्यु के मकबरे सजाए गए
और मैं चुप रहा।
वैसे तो संकलन का हर खंड अपने में रोचक और समृद्ध है लेकिन साहित्य वाले खंड में अभिनवगुप्त पर लिखे गए चार लेख उनकी महत्ता का स्मरण दिलाते हैं। पहला लेख क्षमा कौल का है जिसका शीर्षक है— महामाहेश्वर अभिनवगुप्त। दूसरा लेख मयंक शेखर का है जिसका शीर्षक है— अभिवनगुप्त का सौंदर्यशास्त्रीय अवदान। तीसरा लेख उदय प्रताप सिंह ने उनके ध्वनि और रस के सिद्धांत में योगदान पर लिखा है और चौथा लेख जयप्रकाश सिंह का है जिन्होंने उन्हें संवाद परंपरा के प्रतिमान के रूप में देखा है। क्षमा कौल लिखती हैं, “महामाहेश्वर भगवान अभिनवगुप्त ने बहुत से ग्रंथ लिखे जिसमें श्रीतंत्रालोक का आकार सबसे बड़ा है तथा इसकी श्रेष्ठता भी उतनी ही है। जयरथ राजानक द्वारा लिखे गए भाष्य समेत यह आठ पुस्तकों का एक विशाल ग्रंथ है। यह पुस्तक भी शिव और पार्वती के बीच संवाद पद्धति में लिखी गई है।’’
अभिनवगुप्त के योगदान की चर्चा करते हुए मयंक शेखर लिखते हैं कि उन्होंने 42 ग्रंथों का प्रणयन किया। अपनी कृतियों के आधार पर वे आगमशास्त्र, नाट्यशास्त्र और भक्तिशास्त्र के व्याख्याता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य मयंक शेखर का आलेख गहन शोध के उपरांत लिखा गया है।
फारसी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी साहित्य में कश्मीर के योगदान की चर्चा के साथ ही हिंदी साहित्य में कश्मीर को योगदान की भी चर्चा है। प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने मास्टर जिंदा कौल, नीलकंठ शर्मा, दीनानाथ नादिम, हरिकृष्ण कौल, अग्निशेखर, क्षमा कौल, दुर्गाप्रसाद काचरू, मीराकांत, चंद्रकांता, रजनी पाथरे राजदान, दिलीप कुमार कौल, गौरीशंकर रैणा जैसे कई साहित्यकारों के हिंदी साहित्य में योगदान का जिक्र किया है। वे कहते हैं कि वैसे तो निर्वासन पर कई उपन्यास हैं लेकिन क्षमाकौल का उपन्यास ‘दर्दपुर’ दो विशेष कारणों से तात्पर्यपूर्ण बन जाता है। इसे एक निर्वासित कश्मीरी पंडित ने लिखा है। दूसरे इसे लिखने वाली एक स्त्री है।
सन 1990 के दिसंबर महीने में कश्मीरी पंडितों के भगाए जाने पर केंद्रित आशील कौल की कहानी वे अड़तालीस घंटे धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में यकीन करनेवाले एक संपादक के विस्थापन के दर्द को बयान करती है। किस तरह से एक नामी-गिरामी और पहुंच वाला व्यक्ति भागकर जम्मू के विस्थापितों के शिविरों में शरण लेता है और वहां भी लोग उसे यह कहकर भगाते हैं कि आपने हमें ढांढस बँधाए रखा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और समय रहते आगाह नहीं किया।
लेकिन विमर्श खंड में संकलित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का लेख सांस्कृतिक संघर्ष के विविध पक्ष रखने के बहाने कश्मीर के इतिहास को समेटकर रख देता है। यह लगभग एक हजार साल के टकराव और विवाद का इतिहास है। इसमें बीसवीं सदी के विवाद के साथ आज ताजिकिस्तान में तैमूरलंग को राष्ट्रनायक घोषित करने की घटना का भी जिक्र है। वे कश्मीर के प्रसिद्ध कहानीकार अवतार कृष्ण कहानी छाया में यह सवाल उठाते हैं कि क्या हम कश्मीरियों को तैमूर को अमीर तैमूर कहना चाहिए या तैमूरलंग? यह विमर्श भी धर्मांतरण से बने मुसलमानों और धर्मांतरण न करने वाले कश्मीरी पंडितों के बीच मचे घमासान के लिए आक्रमणकारी शक्तियों को तो दोषी मानता ही है लेकिन भारत पाक विभाजन को भी बहुत हद तक जिम्मेदार मानता है।
भारत की अन्य नौ भाषाओं कश्मीर पर क्या लिखा जा रहा है इसकी भी अच्छी प्रस्तुति है और विशेषांक के विषय से अलग बृषभ प्रसाद जैन का आलेख अपनी हिंदी नागरी सुधारिए बहुत मूल्यवान है। विनोबा, स्वामी विवेकानंद और ह्वेनसांग की कश्मीर यात्रा का भी अच्छा वर्णन है। कश्मीर की संगीत परंपरा, वहां की कला, स्थापत्य, नाटकों के इतिहास पर केंद्रित सामग्री भी स्तरीय है।
लेकिन जो चीज खटकती है वो यह कि महात्मा गांधी के नाम से स्थापित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से निकलने वाली पत्रिका में महात्मा गांधी की कश्मीर यात्रा का जिक्र नहीं है और न ही कश्मीर पर उनके विचारों को उद्धृत किया गया। महात्मा गांधी भारत के विभाजन और उसकी स्वतंत्रता से ठीक पहले जुलाई 1947 में श्रीनगर जाते हैं। वे कहते हैं कि कश्मीर कहां रहेगा इसका फैसला कोई राजा महाराजा नहीं करेगा बल्कि यहां के मुसलमान, हिंदू बौद्ध और सिख करेंगे। उनकी बड़ी सभा होती है और वे कश्मीर के भारत से जुड़ने का वातावरण निर्मित करके आते हैं। आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण भी कश्मीर के मामलों में सक्रिय थे। उनके योगदान पर भी चर्चा होनी चाहिए। मुश्किल यही है कि संघ परिवार जेपी को सिर्फ चौहत्तर के संदर्भ में ही याद करता है।
इस संकलन में अगर साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा ‘आतिशे-चिनार’ का अंश भी दिया जाता तो इसका वजन और भी होता। ‘आतिशे-चिनार’ को साहित्य अकादेमी का उर्दू श्रेणी का पुरस्कार मिल चुका है। संयोग से विश्वविद्यालय के ‘हिंदी समय’ पर उस पुस्तक की एक अच्छी समीक्षा भी मौजूद है। रोचक बात यह है कि पहले यह रचना विश्वविद्यालयों में पढ़ायी जाती थी लेकिन अब आतंकियों के दबाव के चलते हटा दी गई है। इस संकलन में कहीं उन कारणों को भी शामिल किया जाना चाहिए था जिनके नाते कश्मीर में आतंकवाद और विद्रोह की स्थितियां तैयार हुईं। निश्चित तौर पर उसके पीछे कश्मीर में धांधली से कराए जा रहे चुनावों का बड़ा योगदान है। वहां एक ओर अनुच्छेद 370 के बहाने दी गई स्वायत्तता एक मजाक बन कर रह गई थी तो दूसरी ओर चुनाव धांधली हो गए थे। वहां पांच अगस्त 2019 को पाबंदियां लगाकर जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो लोगों को तमाम नागरिक सुविधाओं से वंचित किया गया। उसपर भी काफी साहित्य लिखा गया है। हुजैफा पंडित का संकलन ‘हरा है यादों का रंग’, बशीर दादा का संकलन ‘हजारों इंकलाब आए’ भी वहां के लोगों का स्वर है।
लेकिन शायद यह किसी भी सरकारी संस्थान की मजबूरी है और उसकी सीमाएं भी। इसमें पिछले तीस वर्षों के इतिहास पर कश्मीरी पंडितों का नजरिया हावी है। अगर कुलदीप अग्निहोत्री के लेख में शेर बकरा संघर्ष का जिक्र न होता तो कश्मीर के इतिहास का वह जरूरी पक्ष नदारद था जो शेख अब्दुल्ला ने जागीदारों और मुल्ला मौलवियों से संघर्ष के दौरान मुस्लिम कांफ्रेंस से नेशनल कांफ्रेंस बनाते समय रचा था।
प्रूफ वगैरह की कुछ गलतियों के बावजूद बहुवचन का यह अंक कश्मीर से संबंधित साहित्य और संस्कृति के अध्येता के लिए मूल्यवान और संग्रहणीय है। इस अंक के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और उसके कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल साधुवाद के पात्र हैं।
बहुवचन – भारतीय साहित्य में कश्मीर, अंक-64-65-66. जनवरी-सितंबर, पृष्ठ संख्या-508. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, प्रभात प्रकाशन। मूल्य -225 रु.।