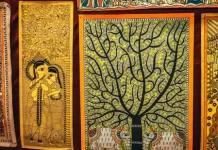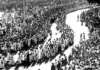(दिल्ली में हर साल 1 जनवरी को कुछ समाजवादी बुद्धिजीवी और ऐक्टिविस्ट मिलन कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें देश के मौजूदा हालात पर चर्चा होती है और समाजवादी हस्तक्षेप की संभावनाओं पर भी। एक सोशलिस्ट मेनिफेस्टो तैयार करने और जारी करने का खयाल 2018 में ऐसे ही मिलन कार्यक्रम में उभरा था और इसपर सहमति बनते ही सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप का गठन किया गया और फिर मसौदा समिति का। विचार-विमर्श तथा सलाह-मशिवरे में अनेक समाजवादी बौद्धिकों और कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी रही। मसौदा तैयार हुआ और 17 मई 2018 को, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर, नयी दिल्ली में मावलंकर हॉल में हुए एक सम्मेलन में ‘सोशलिस्ट मेनिफेस्टो ग्रुप’ और ‘वी द सोशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस’की ओर से, ‘1934 में घोषित सीएसपी कार्यक्रम के मौलिक सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए’ जारी किया गया। मौजूदा हालातऔर चुनौतियों के मद्देनजर इस घोषणापत्र को हम किस्तवार प्रकाशित कर रहे हैं।)
सामाजिक क्षेत्र में खर्च में कमी
एक ओर जहां सरकार, अमीरों को सबसिडी के रूप में लाखों करोड़ रुपये स्थानांतरित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ, सरकार अपने सामाजिक क्षेत्र के व्यय को कम रही है और दावा कर रही है कि वित्तीय राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है और राजकोषीय घाटे को कम करने की जरूरत है। लेकिन अगर वास्तव में सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के बारे में गंभीर होती, तो कॉरपोरेट घरानों को दी गयी बेमतलब की सबसिडी को कम करके यह आसानी से ऐसा कर सकती थी! जाहिर है कि ‘राजकोषीय घाटे में कमी’ का सिद्धांत कमजोर है और इसी बहाने सरकार कल्याणकारी योजनाओं में खर्च को कम करना चाहती है। यह वही नीति है जो विश्व बैंक चाहता है, ताकि इन सामाजिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा सके और निगमों को उनके लाभ के लिए सौंप दिया जा सके। केंद्र में लगातार सरकारें इस ‘आर्थिक सुधार’ को परिश्रमपूर्वक कार्यान्वित कर रही हैं। मोदी सरकार ने केंद्र के सामाजिक क्षेत्र के व्यय में विनाशकारी परिणामों के साथ और भी कठोर कटौती की है। हम सबसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में मोदी शासन के तहत सरकारी खर्च की स्थिति के बारे में अब यहां संक्षेप में चर्चा करते हैं-
1- शिक्षा
- भारत के संविधान में भारत को एक “संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणरज्य’’ का नागरिक बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता बतायी गयी है और जो सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप, समतावादी, बहुलवादी और प्रबुद्ध समाज को बनाए रखने में मदद करेगी।
- संविधान एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को वांछनीय मानता है जो विषमता, सामाजिक-आर्थिक स्तरीकरण, पितृसत्ता, धर्म-सांस्कृतिक या भाषाई आधिपत्य, भेदभाव और / या सामाजिक चिंताओं को दूर करने की भावना को मजबूत करती है।
ऊपर के वर्णन के अनुसार गुणवत्तापरक शिक्षा, निजी शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि निजी क्षेत्र केवल लाभ की चिंता करते हैं। वे समता/ज्ञान/एकता/न्याय की भावना को बढ़ावा देने में रूचि नहीं रखते हैं। एक अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित शिक्षा प्रणाली द्वारा ही प्रदान की जा सकती है।
हालांकि, भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पिछले तीन दशकों से, एक के बाद एक आयी सभी सरकारों ने विश्व बैंक द्वारा तय आर्थिक सुधारों के अनुरूप देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली का निजीकरण किया है। इसके लिए सरकार द्वारा अपनायी गयी रणनीति सरल है : धीरे-धीरे सरकारी शिक्षा प्रणाली को धन के अभाव में रखें, शिक्षकों द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता को खराब होने दें, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बिगड़ने दें; इसके बाद माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी शिक्षा प्रणाली से वापस लेना शुरू कर देंगे; निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए मांग उठने लगेगी; जो लोग वहन कर सकते हैं वे अपने बच्चों को इन निजी शैक्षणिक संस्थानों में भेज देंगे।
आज, तीन दशकों बाद, यह स्पष्ट है कि विश्व बैंक सरकारी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करने के अपने उद्देश्य से भी कहीं अधिक सफल रहा है।
स्कूली शिक्षा : देश में स्कूली शिक्षा की स्थिति इतनी निराशाजनक है कि यह वास्तव में राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए और मीडिया का मुख्य समाचार बनना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने से पहले 40 फीसद से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं। और जो बच्चे स्कूलों में जाते भी हैं, उनके लिए अधिकांश स्कूलों में स्थितियां बस भयानक हैं :
- देश के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में, एक ही शिक्षक एक ही कमरे में एक ही समय में दो या तीन अलग-अलग कक्षाएं पढ़ा रहे हैं।
- देश के प्राथमिक विद्यालयों में सभी नियमित शिक्षकों में से लगभग 20 फीसद पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं; एक ओर 14 फीसद शिक्षक ठेका के आधार पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक तिहाई पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं।
- लगभग एक तिहाई स्कूलों में उपयोग करने योग्य शौचालय की सुविधा नहीं है, और 40 फीसद स्कूलों में बिजली नहीं है।
- देशभर के स्कूलों में लगभग दस लाख शैक्षणिक पद रिक्त हैं (प्राथमिक विद्यालयों में 9,000,000 और माध्यमिक विद्यालयों में 1,00,000 पद), जो शैक्षिणक पदों का लगभग पांचवां हिस्सा है।
ऐसी निराशाजनक स्थितियों में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि कक्षा 5 के 50 फीसद छात्र पाठ पढ़ने में असमर्थ हैं या कक्षा 2 का गणित नहीं बना सकते हैं।
दूसरी तरफ, सक्षम वर्गों के लिए, शैक्षणिक और अतिरिक्त पाठ्यचर्या सुविधाओं के साथ अलग-अलग गुणवत्ता के निजी स्कूलों की एक विस्तृत शृंखला है, जिसमें प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक या और अधिक तक फीस होती है।
ऐसी भेदभावपूर्ण स्कूल शिक्षा प्रणाली के कारण, कक्षा एक में नामांकित बच्चों में से केवल 15-17 फीसद कक्षा 12वीं को पास कर पाते हैं। हाशिये पर रखनेवाले वर्गों के लिए स्थिति बदतर है : एससी के केवल 8 फीसद और एसटी के 6 फीसद लगभग 10-11 फीसद ओबीसी और करीब 9 फीसद मुस्लिम बच्चे ही कक्षा 12वीं पास कर पाते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि लगभग 92 फीसद दलितों और 94 फीसद जनजातीय और 90 फीसद ओबीसी कभी भी सामाजिक न्याय एजेंडा के तहत आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं बनते हैं।
उच्च शिक्षा : उच्च शिक्षा का निजीकरण अधिक तेज गति से हो रहा है। आधे से अधिक उच्च शैक्षिक नामांकन पहले से ही निजी शैक्षिक संस्थानों में हैं। चूंकि ये सभी लाभकारी संस्थान हैं, बहुत कम छात्र अपनी फीस वहन कर सकते हैं। हालांकि, सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में भी शिक्षा महंगी हो रही हैं। चूंकि सरकार इन संस्थानों को अनुदान कम कर रही है, और उन्हें सभी प्रकार के बहाने का उपयोग करके छात्र शुल्क बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नतीजतन, सरकारी वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में भी अध्ययन करना गरीब परिवारों के छात्रों के लिए अवहनीय होता जा रहा है। यही कारण है कि भारत के सकल नामांकन अनुपात या जीईआर, जो युवा आबादी के प्रतिशत अनुपात के रूप में उच्च शैक्षिक संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या को इंगित करता है, विकसित देशों की तुलना में काफी नीचे है- भारत के लिए जीईआर केवल 20 है, जबकि विकसित देशों में यह 60 से ऊपर है। कई देशों में 70 से ऊपर जीईआर है।
मोदी सरकार और शिक्षा : इस भयानक स्थिति के बावजूद, निश्चिन्त भाजपा सरकार शिक्षा बजट को और भी कम करती जा रही है। वित्तमंत्री जेटली ने खुद के द्वारा पेश किये गये पांच बजटों में स्कूली शिक्षा के लिए बजट आवंटन में इतनी तेजी से कटौती की है कि मामूली शर्तों में भी 2018-19 के बजट (50,000 करोड़ रुपये) में आवंटन वित्तीय वर्ष 2014-15 के (55,115 करोड़ रुपये) वास्तविक व्यय से कम है। वास्तव में, प्रतिवर्ष 8 फीसद की मुद्रास्फीति मानते हुए 2018-19 में स्कूली शिक्षा पर व्यय 2014-15 (सीएजीआर) में वास्तविक व्यय से 33 फीसद अधिक होना चाहिए।
जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, 2018-19 में बजट आवंटन 2014-15 (वास्तविक) में आवंटन से 7 फीसद (सीएजीआर) कम है। इसके अलावा, इसके भीतर उच्च शैक्षणिक खर्च कम हो गया है, आवंटन का एक प्रमुख हिस्सा आईआईटी और आईआईएम जैसे उत्कृष्टता के तथाकथित संस्थानों के लिए है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए आवंटन, जो देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों का नियामक है और 10,000 से अधिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करता है, केवल तीन वर्षों में आधे तक गिर गया है : इसे 2015-16 आरई में 9,315 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे; 2018-19 में यह घटकर 4,723 करोड़ रुपये हो गया है।
नरेंद्र मोदी और भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान शिक्षा (केंद्र + राज्य संयुक्त) पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 फीसद करने का वादा किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 मानता है कि यह वास्तव में मोदी शासन में गिर गया है, 2012-13 में जीडीपी का 3.1 फीसद से 2017-18 बीई में गिरकर 2.7 फीसद रह गया है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.