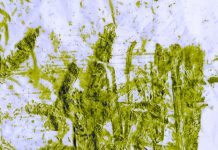(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा का आज जन्मदिन है। यह सुखद संयोग है कि इसी मौके पर उनकी रचनावली आठ भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। नब्बे पार के सच्चिदा जी के शतायु होने की शुभकामना के साथ उनका एक लेख प्रस्तुत है।)

भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभावों की चर्चा तो पिछले दिनों काफी होती रही है लेकिन इसके राजनीतिक प्रभावों पर कम ही विचार हुआ है, हालांकि यह उतना ही महत्त्वपूर्ण है। भूमंडलीकरण की राजनीति ने पिछले तीन सौ साल से विकसित हो रही लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरी तरह उलटने का काम किया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर। जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो हमारा आशय यूरोप में सत्रहवीं शताब्दी से विकसित हुई जनता की प्रभुसत्ता की उस अवधारणा से होता है जो आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था की जनक बनी। इसी का अंतरराष्ट्रीय पक्ष था राष्ट्रीय आजादी के आंदोलनों का जन्म और पश्चिमी देशों द्वारा गुलाम बनाये गये देशों में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की स्थापना। भूमंडलीकरण जनता की दोनों तरह की प्रभुसत्ता को अप्रासंगिक बनाता जा रहा है।
यूरोप में व्यापार और उद्योग-धंधों में लगे लोगों ने जिन्हें बुर्जुआ कहा जाता था, प्रारंभ में लोकतांत्रिक सत्ता के विकास में प्रमुख योगदान किया। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में इग्लैंड में पार्लियामेंट के अधिकारों को लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी। फिर 1789 की फ्रांस की क्रांति के पहले जब वहां के राजा ने ‘स्टेट्स जनरल’ बुलाया तो इसी वर्ग के प्रतिनिधियों ने राजा की अवज्ञा कर अपने को नेशनल एसेंबली के रूप में घोषित किया और यहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। यह वर्ग लोकतंत्र का उग्र पक्षधर बनकर आगे आया। स्थानीय सामंती बंधनों को तोड़ने का इसका आग्रह मूलतः व्यापार और उद्योग के निर्बाध विकास को सुनिश्चित करने के लिए था। इसी क्रम में कुछ मूल्यों के इर्द-गिर्द राष्ट्रीय अस्मिता-बोध और राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर जनता की प्रभुसत्ता की अवधारणा पैदा हुई।
जब तक व्यापार और उद्यम को स्थानीय सामंती सीमाओं से मुक्त करने की बात थी तब तक तो इस प्रक्रिया में कोई अंतर्विरोध नहीं दिखाई दिया। स्वतंत्र व्यापार एक सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकृत रहा लेकिन जब औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर फैलने लगी तो एक अंतर्विरोध दिखाई देने लगा। ब्रिटेन, जहां औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे होने के कारण स्वतंत्र भारत का लाभ उठा रहा था और इसलिए इसका पक्षधर था। लेकिन दूसरे देश जैसे जर्मनी और अमरीका, जो इस होड़ में बाद में शामिल हुए, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते थे इसलिए राष्ट्रीय उद्यमों की संरक्षण की नीति को लेकर चले। इनमें राष्ट्रीय सरकारें अपने उद्यमों को संरक्षण देती थीं। अमरीका में तो राष्ट्रीय उद्यमों को समर्थन देने की नीति 1930 तक चलती रही और परोक्ष रूप से (जैसे कोटा लागू कर) कुछ क्षेत्रों में आज भी चल रही है। द्वितीय विश्वयुद्ध के काल तक उन्मुक्त बाजार के सिद्धांत के साथ-साथ राष्ट्रीय सरकारों की इस जवाबदेही को भी स्वीकार किया जाता था कि वे उद्यमों को बचाये रखने और इनमें लगे श्रमिकों की हित-रक्षा की जवाबदेही लें।
उन्नीसवीं शताब्दी से राष्ट्रीय सरकारों के दायित्व में एक और आयाम जुड़ गया था। जैसे-जैसे औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग का प्रभुत्व समाज में बढ़ने लगा, यह महसूस किया गया कि इनमें लगे श्रमिकों और समाज के उपभोक्ताओं की हित रक्षा के लिए सरकारों का हस्तक्षेप जरूरी है। सत्ता पर जनता के प्रतिनिधियों के बढ़ते दबाव का यह सीधा परिणाम था। मजदूरों के आंदोलन तो सभी उद्योग-धंधों को जनता के नियंत्रण में लाने की मांग करने लगे। इसी के इर्द-गिर्द विभिन्न तरह के समाजवादी आंदोलन का विकास हुआ।
उपभोक्ताओं को बचाने के लिए इजारेदारियों को नियंत्रित करने की नीतियां सरकारों द्वारा अपनायी गयीं ताकि इजारेदारी का फायदा उठा उद्योगपति उपभोक्ताओं से मनमानी कीमत न वसूलें। इस तरह बीसवीं शताब्दी के मध्य तक यानी द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत के कुछ साल बाद तक दो शक्तियों के बीच किसी तरह का संतुलन बनाने का प्रयास होता रहा- पहली औद्योगिक व्यापारिक शक्ति, और दूसरी, जनता के पक्ष का विविध अनुपात में प्रतिनिधित्व करनेवाली प्रभुतासंपन्न राष्ट्रीय सरकारों की शक्ति, फिर भी इस काल में अकसर औद्योगिक शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक मान कर इनके हितों को सर्वोपरि राष्ट्र हित की तरह भी बढ़ाया जाता था। इन दोनों का सबसे सबल एकीकरण फासीवादी सरकारों की कॉरपोरेट स्टेट की अवधारणा में हुआ। वे इनके हितों को बढ़ाने के मकसद से दूसरे देशों पर आधिपत्य के लिए युद्ध को एक जायज माध्यम मानते थे। इस काल में राष्ट्रहित को सर्वोपरि हित मानना कोई खास विवाद का विषय नहीं था।
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से स्थिति में एक गुणात्मक बदलाव आया है। 1944 में ब्रेटनवुड्स में विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और इसी प्रक्रिया के तहत बाद में विश्व व्यापार संगठन आदि के अस्तित्व में आने से उन्मुक्त बाजार व्यवस्था ने एक नया रूप लिया। हालांकि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीका अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के बल पर संसार के चौधरी के रूप में उभरा, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असली ताकत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में आयी। यह बात अलग है कि इनमें ज्यादा और शक्तिशाली कंपनियां अमरीका की ही थीं। इससे स्वतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित और अमरीका के हित प्रायः एक बन जाते हैं।
इनमें कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आय तो दुनिया के अधिकांश देशों की राष्ट्रीय आय से अधिक है। इनके उत्पादन और व्यापार का क्षेत्र भी विश्वव्यापी है। अकसर इनका निवेश राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर होता है। ये प्रायः उन्हीं देशों में निवेश करती हैं जहां संसाधनों और सस्ते श्रम की बहुलता होती है, हालांकि आधुनिकतम उद्योगों के लायक कुशल श्रम औद्योगिक देशों में ही उपलब्ध हो सकते हैं। राष्ट्रीय सरकारों को वे अपने व्यापारिक हितों के अनुकूल नीतियां बनाने के लिए प्रभावित कर सकती हैं। चूंकि राष्ट्रीय आय और रोजगार दोनों ही ऐसे उद्योगों के फैलाव पर निर्भर माने जाते हैं, इसलिए सरकारों की मजबूरी हो जाती है कि वे इन कंपनियों को यथासंभव सहायता दें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा में समेकित हो ज्यादा प्रभावी रूप से काम करने के लिए ही अमरीका और जापान के विशाल उत्पादन और आय के मुकाबले के लिए यूरोप के एकीकरण की पहल हुई।
लेकिन इस एकीकरण का प्रभाव यह हुआ है कि यूरोपीय यूनियन के भीतर के किसी भी राष्ट्र की जनता के हाथ में यह अधिकार नहीं रह गया है कि वे अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों को बदल सकें। आर्थिक नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी यूरोपियन कमीशन की है जो काफी हद तक स्वायत्त है और अगर उसपर थोड़ा नियंत्रण है तो यूरोपीय संसद का है जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभाओं की तरह प्रभुतासंपन्न नहीं है। अतः अब नीतियां मूलतः यूरोप के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही बनायी जाती हैं।
इस तरह आम लोगों के हाथों से प्रभुसत्ता खिसकती जा रही है। हमारे अपने देश में भी भाजपा के तमाम स्वदेशी के नारों के बावजूद नीतियां विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के निर्देशों के तहत बनायी जाती हैं। इस तरह दिल्ली के शासन में देशी से ज्यादा विदेशी हितों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। आज दुनिया धनतंत्र की आदर्श स्थिति की ओर बढ़ रही है जिसमें अति धनाढ्य समूह अर्थव्यवस्था और राज्य-व्यवस्था राज्य दोनों को चला रहे हैं।
विशाल कंपनियों के उत्पादन और विनिमय के अंतरराष्ट्रीय हो जाने से अब दूसरे देशों पर प्रत्यक्ष सैनिक अधिकार की बात अप्रासंगिक बन गयी है। अब उनपर नियंत्रण के माध्यम आर्थिक-व्यापारिक हो गये हैं। इसके लिए ऊपर वर्णित तीन संस्थाएं यानी विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व व्यापार संगठन कारगर औजार हैं। सीधा या परोक्ष सैनिक हस्तक्षेप कुछ बुनियादी महत्त्व के प्राकृतिक साधनों, जैसे पेट्रोलियम के स्रोतों पर नियंत्रण के लिए ही होता है, जैसा पश्चिम एशिया या अफ्रीका के कुछ देशों में हुआ है। शायद ऐसा हथियारी हस्तक्षेप उन देशों में भी ही हो सकता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से अपने को काट कर आत्मनिर्भर आर्थिक ढांचा बनाएं।
हथियारों का विशाल मात्रा में उत्पादन और विक्रय अब मूलतः हथियार उद्योग से मिलनेवाले भारी मुनाफे के लिए ही होते हैं। इसलिए हम यह विडंबनापूर्ण स्थिति पाते हैं कि स्वीडन जैसा देश जो युद्धों में प्रायः तटस्थ रहा है, एक महत्त्वपूर्ण हथियार निर्माता है। इसी से हथियार बनानेवाले देशों का इस बात में निहित स्वार्थ है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हथियारी होड़ चलती रहे।
एक महत्त्वपूर्ण बदलाव मजदूर वर्ग की दृष्टि में आया है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जहां व्यापारी वर्ग अपने हितों को राष्ट्रीय सत्ता के साथ जोड़ रहा था वहां मजदूर वर्ग अपनी दृष्टि में अंतरराष्ट्रीय था और सारी दुनिया के मजदूरों के हित के साथ अपना हित जोड़ रहा था। नयी विश्व व्यवस्था के उदय के साथ पूंजी और मजदूरों की दृष्टि बिल्कुल उलट गयी है। पूंजी अब पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय हो गयी है क्योंकि आज इसकी सत्ता सीमाहीन है। इसका असर यह हो रहा है कि मजदूरों की दृष्टि संकुचित होती जा रही है। वे भयभीत हैं कि पूंजी सस्ते श्रम की तलाश में पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ओर भागेगी। इससे उनकी रोजगार की संभावना घटेगी। इसी कारण सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक के समय अमरीका के मजदूर संगठनों ने पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में श्रम मानकों को लागू करने का सवाल उग्र प्रदर्शन करके उठाया। इस तरह कुल मिलाकर भूमंडलीकरण की दिशा श्रमिकों की एकता के बिखराव, जनाधिकारों के क्षरण और लोक जीवन को विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में लाने की है।