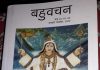— हिमांशु जोशी —
लेखक ने अपनी किताब की ‘भूमिका’ लिखने के लिए वरिष्ठ लेखक देवेंद्र मेवाड़ी को चुना है। देवेंद्र भूमिका में ही यह पूरी तरह स्पष्ट करने में सफल रहे हैं कि किताब हमें पहाड़ की सुंदरता के साथ-साथ पहाड़ की समस्याओं से भी परिचित कराएगी।
जैसे भूमिका में उन्होंने पहाड़ निवासी दिनेश दानू की यह बात लिखी है “आप लोग पहाड़ों को देखते हैं और हम इनमें रहते हैं। मूलभूत सुविधाओं से अनछुए ये पहाड़ आपको दिखने में सुंदर लगेंगे ही पर जब आपको इनमें ही रहना हो तब आपका यह विचार, विचार ही रह सकता है।
‘अपनी बात’ में लेखक ने व्यक्ति के जीवन में यात्राओं के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। यह किताब लेखक द्वारा उत्तराखंड में की गयी दस यात्राओं का संकलन है। लेखक के शब्दों में किताब का उद्देश्य उत्तराखंड की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक तस्वीर को सामने लाना है।
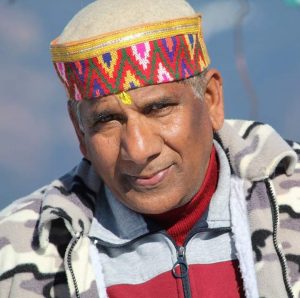
लेखक ने किताब की शुरुआत शिव की परण्यस्थली-मध्यमहेश्वर की यात्रा से की है, इसे पढ़ते हुए पाठक को लगता है कि वह भी लेखक के साथ पहाड़ की यात्रा पर है।
लेखक ने यात्रा के दौरान उनके सम्पर्क में रहे लोगों की बातों को ठीक वैसे ही लिख डाला है जैसे उन लोगों ने बोला है, जैसे लेखक को जगत नाम के खच्चर वाले ने हाथ पकड़कर कहा “वन टू थ्री, तुम भी फ्री हम भी फ्री इसलिए बैठो।”
किताब पढ़ते हुए आपको ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को देखने के साथ (जो रंगीन भी लग सकती थीं) बहुत से साहित्य के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी जो लेखक को किसी जगह को देख याद आते रहते हैं, कभी वह राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं को याद करते हैं तो कभी चंद्रकुंवर बर्त्वाल की कविताओं को।
बारिश की ‘दणमण’ जैसे पहाड़ी शब्दों का प्रयोग भी किया गया पर इनका मतलब समझने में आपको कोई परेशानी नही होगी और आप इन्हें प्रकृति की तरह ही आत्मसात कर लेंगे।
“प्रकृति ने जितनी सुंदर जगह यहाँ दी है उतना ही कुरूप व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार यहाँ का शासन-प्रशासन है” जैसी पंक्तियाँ सरकारी व्यवस्थाओं पर चोट मारती है।
किताब पढ़ते हुए यह भी महसूस होता है कि अगर उत्तराखंड यात्रा के दौरान आप यह किताब अपने साथ रखें तो आपको रास्ता पूछने के लिए शायद ही किसी की जरूरत पड़े।
कुत्ते और मुर्गे की बातचीत जबरदस्ती ठुँसी हुई लगती है।
गुजरात मॉडल सफल रहा हो या नहीं, पर कैन्यूर गाँव का मॉडल उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी गाँवों के लिए मॉडल बन सकता है।
शराब के खिलाफ नारों के साथ ही उसकी व्यवस्था करनेवाला वाकया हमें खुद पर लजाने का मौका तो देता है।
लेखक का रानीखेत में गोदाम बन चुके अपने कॉलेज के बारे में बात करना यह याद दिलाता है कि हमने अपने पुरातत्त्व भवनों का कितना ध्यान रखा है। लेखक ने किताब में उत्तराखंड के इतिहास से भी पर्दा उठाया है जैसे तिलाड़ीसेरा कांड शायद जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ा था पर अपने ही लोगों के द्वारा किये जाने की वज़ह से इतिहास के इस काले अध्याय के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती।
किताब को आगे पढ़ते हुए हम पौंटी गाँव के बारे में जानते हैं जहाँ के लोग सड़क, बिजली, जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी अपने में मगन हैं पर ऐसे गाँवों में इलाज के अभाव में दम तोड़ते लोगों की कहानी और स्कूलों की दुर्दशा मन विचलित करती हैं।
हिमाचल और उत्तराखंड में ‘विकास’ का इतना अंतर क्यों है इसकी वजह भी किताब समझाती है।
लेखक और उनके साथियों का पुंग से मोलिखर्क तक अँधेरे में जानवरों की गुर्राहट के बीच का सफर पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी कहानी चल रही हो।
ऊनी वस्त्रों का कारोबार बहुत से गाँवों में अच्छा चलता था जो रेडीमेड आने के बाद समाप्त हो गया है, पहाड़ी गाँवों की यह दुर्दशा समझ आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी अपनाने पर ज़ोर क्यों दिया था। पर अब इस बारे में सोचे कौन!
कुछ जगह लेखक ने पहाड़ की सुंदरता का सजीव प्रसारण किया है तो प्रकाश राम के ब्रिगेडियर बनने की कहानी आपको किताब पढ़ते मुस्कुराने का मौका भी देती है। लेखक ने यात्राओं को उनके समयानुसार क्रम से नहीं लगाया है पर यह आपको यह अखरेगा नहीं। सुंदरढुंगा इलाके में पर्यटकों ने प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया उसे पढ़ना जरूरी है। देवाधिदेव केदारनाथ की 2019 में की गयी यात्रा के दौरान लेखक 2013 आपदा के प्रभावों से पाठकों को रूबरू कराते हैं।
काँवड़ियों में शामिल कुछ लोगों की नशा करने की आदत पर लेखक ने व्यंग्य किया है तो स्कूल न पढ़ने वाले ‘दिल बहादुर’ से लेखक का नज़रें न मिला पाना तंत्र की नाकामी के बीच हमारी भी कुछ न कर सकने की मजबूरी पर हमें धिक्कारता है।
कोसी से रानीखेत की जमीन पूँजीपतियों के हाथों में आने की बात प्रदेश में भू-कानून की आवश्यकता याद दिलाती है।
3 अक्टूबर 2020 को लिखा ‘तुंगनाथ के उतुंग शिखर पर’ वृत्तांत किताब का आखिरी हिस्सा है, लगातार दस घण्टे किताब पढ़ते रहने के बाद भी मैंने इसे पढ़ते उबाऊ महसूस नही किया। मन करता है लेखक से मिल कर कहूँ कि ऐसे ही उत्तराखंड के बचे हुए कोनों में पहुँच वहाँ की खूबसूरती और समस्याओं से हमें परिचित कराते जाओ।
किताब पढ़ने के बाद आप लेखक का उत्तराखंड की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक तस्वीर को सामने लाने का जो उद्देश्य है उसे समझेंगे और यह भी चाहेंगे कि इसे दिल्ली में बैठे उत्तराखंड की सत्ता चला रहे केंद्र के दरबारियों के हाथों में पकड़ा देना चाहिए और कहना चाहिए कि असली पहाड़ देखना है तो ‘चले साथ पहाड़’!
किताब – चले साथ पहाड़
लेखक – अरुण कुकसाल
मूल्य – 240
प्रकाशक – सम्भावना प्रकाशन
लिंक –
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.