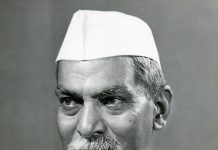(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
भारत और उपभोक्तावादी संस्कृति
विकसित पूँजीवादी देशों में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उपभोक्तावादी संस्कृति उत्पादन प्रक्रिया को बिना पूँजीवादी मूल्यों और ढाँचे को तोड़े चालू रखने और विकसित करने में सहायक होती है। लेकिन दुनिया के गरीब देशों में इस संस्कृति का असर इसके ठीक विपरीत होता है। भारत जैसे गरीब देशो में जहाँ साम्राज्यवादी संपर्क से परंपरागत उत्पादन का ढाँचा टूट गया है और लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए उत्पादन के तेज विकास की जरूरत है, वहाँ उपभोक्तावाद के असर से विकास की संभावनाएँ कुंठित हो गई हैं। पश्चिमी देशों के संपर्क से इन देशों में एक नया अभिजातवर्ग पैदा हो गया है जिसने इस उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना लिया है। इस वर्ग में भी उन वस्तुओं की भूख जग गई है जो पश्चिम के विकसित समाज में मध्यमवर्ग और कुशल मजदूरों के एक हिस्से को उपलब्ध होने लगी हैं। इन वस्तुओं की उपलब्धि से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोत्तरी हो जाती है। अतः इस अभिजातवर्ग में और इसकी देखा-देखी इससे नीचे के मध्यम और निम्न-मध्यमवर्ग में भी मोटरकार, एयरकंडीशन मशीन, फ्रिज और विभिन्न तरह के सामान और प्रसाधनों को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा जग गई है। हमारे देश में इसके दो सामाजिक परिणाम हुए हैं। पहला, चूँकि यही वर्ग देश की राजनीति में शीर्ष स्थानों पर है, देश के सीमित साधनों का उपयोग धड़ल्ले से लोगों की आम आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करने के बजाय वैसे उद्योगों और सुविधाओं के विकास के लिए हो रहा है जिनसे इस वर्ग की उपभोक्तावादी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। चूँकि उत्पादन का यह क्षेत्र अतिविकसित तकनीकी का और पूँजी प्रधान है, इन उद्योगों के विकास से विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है। मशीन, तकनीक और गैरजरूरी वस्तुओं के आयात पर हमारे सीमित विदेशी मुद्राकोष का क्षय होता है, और हमारा सबसे विशाल आर्थिक साधन जिसके उपभोग से देश का तेज विकास संभव था- यानी हमारी श्रमशक्ति बेकार पड़ी रह जाती है। जिन क्षेत्रों मे देश का विशाल जनसमुदाय उत्पादन में योगदान दे सकता है उनकी अवहेलना के कारण आम लोगों के जीवन-स्तर का या तो विकास नहीं हो पाता या वह नीचे गिरता है।
दूसरा, चूँकि उपभोक्तावाद व्यापक गरीबी के बीच खर्चीली वस्तुओं की भूख जगाता है, उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। चूँकि अभिजातवर्ग में वस्तुओं का उपार्जन ही प्रतिष्ठा का आधार है, चाहे इन वस्तुओं को कैसे भी उपार्जित किया जाए, भ्रष्टाचार को खुली छूट मिल जाती है। कम आयवाले अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग कर जल्दी से जल्दी धनी बन जाना चाहते हैं ताकि अनावश्यक सामान इकट्ठा कर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें। इसी का एक वीभत्स परिणाम दहेज को लेकर हो रहा औरतों पर अत्याचार भी है। बड़ी संख्या में मध्यमवर्ग के नौजवान और उनके माता-पिता, जो अपनी आय के बल पर शान बढ़ानेवाली वस्तुओं को नहीं खरीद सकते, दहेज के माध्यम से इस लालसा को मिटाने का सुयोग देखते हैं। इन वस्तुओं का भूत उनके सिर पर ऐसा सवार होता है कि उनमें राक्षसी प्रवृत्ति जग जाती है और वे बेसहारा बहुओं पर तरह-तरह का अत्याचार करने या उनकी हत्या करने तक से नहीं हिचकते। बहुओं की बढ़ रही हत्याएँ इस संस्कृति का सीधा परिणाम हैं। अपहरण जैसे अपराधों के पीछे भी कुछ ऐसी ही भावना काम करती है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का तो यह मूल कारण है। राजनीतिक लोगों के हाथ में अधिकार तो बहुत होते हैं, लेकिन जायज ढंग से धन उपार्जन करने की गुंजाइश कम होती है। चूँकि उनकी प्रतिष्ठा उनके रहन-सहन के स्तर पर निर्भर करती है, उनके लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर धन इकट्ठा करने का लोभ संवरण करना मुश्किल हो जाता है।
इस तरह समाज में जिनके पास धन व पद है और भ्रष्टाचार के अवसर हैं, उनके और आम लोगों के जीवन-स्तरों के बीच की खाई बढ़ती जाती है। इससे भी शासक और शासितों के बीच का संवाद-सूत्र टूटता है। सत्ताधारी लोग आम लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं और उत्पादन की दिशा अधिकाधिक अभिजातवर्ग की आवश्यकताओं से निर्धारित होने लगती है। इधर आम जरूरतों की वस्तुओं के अभाव में लोगों का असंतोष उमड़ता है तथा आंदोलन एवं उथल-पुथल की भूमिका तैयार होती है। इस स्थिति से उबरने के लिए शासकवर्ग अधिनायकवादी तरीकों से जनआंदोलनों से निपटना चाहता है। गरीब दुनिया के अधिकतर देशों में राजनीति का ऐसा ही आधार बन रहा है जिसमें संपन्न अल्पसंख्यक लोग छल और आतंक के द्वारा आम लोगों के हित के खिलाफ शासन चलाते हैं।
भारत के गाँवों में जो थोड़ा-बहुत स्थानीय आर्थिक आधार था उसको भी इस संस्कृति ने नष्ट किया है। भारतीय गाँवों की परंपरागत अर्थव्यवस्था काफी हद तक स्वावलंबी थी और गाँव की सामूहिक सेवाओं, जैसे सिंचाई के साधन, यातायात या जरूरतमंदों की सहायता आदि की व्यवस्था गाँव के लोग खुद कर लेते थे। यह व्यवस्था जड़ और जर्जर जरूर हो गई थी और ग्रामीण समाज मे काफी गैरबराबरी भी थी, फिर भी सामूहिकता का एक भाव था। हाल तक गाँवों में पैसेवालों की प्रतिष्ठा इस बात से होती थी कि वे सार्वजनिक कामों, जैसे कुँआ, तालाब आदि खुदवाने, सड़क मरम्मत करवाने, स्कूल और औषधालय आदि खुलवाने पर धन खर्च करें। इन पर काफी खर्च होता था और आजादी के पहले इस तरह की सेवा-व्यवस्था प्रायः ग्रामीण लोगो के ऐसे अनुदान से ही होती थी। यह संभव इस लिए होता था क्योंकि गाँवों के अंदर धनी लोगों की भी निजी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं और वे अपने धन का व्यय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ऐसे कामों पर करते थे। इसी कारण पश्चिमी अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों की हमेशा यह शिकायत रहती थी कि भारतीय गाँवों के उपभोग का स्तर बहुत नीचा है, जो उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। इन लोगों की दृष्टि में औद्योगिक विकास की प्रथम शर्त थी अंतरराष्ट्रीय बाजार और विनिमय में शामिल हो जाना।
उपभोक्तावादी संस्कृति ने गाँवों की अर्थव्यवस्था के इस पहलू को समाप्त कर दिया है। अब धीरे-धीरे गाँवों में भी संपन्न लोग उन वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं जो उपभोक्तावादी संस्कृति की देन हैं। चूँकि गाँव के संपन्न लोगों की संपन्नता भी सीमित ही होती है अब उनका सारा अतिरिक्त धन जो पहले सामाजिक कार्यों में खर्च होता था वह अब निजी तामझाम पर खर्च होने लगा है और लोग गाँव के छोटे से छोटे सामूहिक सेवा कार्य के लिए सरकारी सूत्रों पर आश्रित होने लगे हैं। इसके अलावा जो भी थोड़ा साधन गाँवों के भीतर से उनके विकास के लिए प्राप्त हो सकता था, अब उद्योगपतियों की तिजोरियों में जा रहा है। इससे गाँवों की गरीबी, दैन्य और दरिद्रता में बदलती जा रही है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.