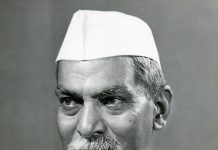(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
यह पुस्तिका आज से लगभग तीस वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। इस बीच दुनिया में बहुत उथल-पुथल और बदलाव आए हैं। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में जो मूल अवधारणा व्यक्त की गई है उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं लगती। उपभोक्तावादी संस्कृति आधुनिक औद्योगीकरण के साथ विकसित हुई है और इसको बल भी देती रही है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया को आकर्षक बनाने में इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया से पैदा सामाजिक अंतर्विरोधों को इसने और भी तीव्र किया है। सोवियत रूस और माओ के चीन, दोनों में समता का आदर्श ध्वस्त हो गया और तथाकथित साम्यवादी व्यवस्थाएँ खत्म हो गई। इनकी जगह निर्मम पूँजीवादी व्यवस्थाएँ कायम हुईं। इस प्रक्रिया के पीछे उपभोक्तावादी तामझाम की आकांक्षा का हावी होना भी एक कारक था। उपभोग की नई संभावनाओं की ललक उत्पादन और वितरण की किसी व्यवस्था को स्थिर नहीं होने देती। इस तरह महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्विता समतावादी मूल्यों पर हावी हो जाती है। तथाकथित कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं के ध्वस्त होने के दूसरे कारण भी गिनाए जा सकते हैं, लेकिन उपभोक्तावाद के दबाव में समता के आदर्शों का लोप भी एक प्रमुख कारण था।
भोग की लालसा एक स्वाभाविक रुझान है जो सभी पारंपरिक समाजों में रही है। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था को कायम रखने और इसे त्वरण देने का एक अनिवार्य उपकरण है। इसमे वयक्तिक स्तर पर कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। यह औद्योगिक व्यवस्था द्वारा प्रायोजित उपकरण है जिसे व्यक्ति आत्मसात कर निजी आकांक्षा में बदल लेता है।
अर्थ जगत में स्वयंसिद्ध सी प्रचलित बातें जैसे-‘उपभोक्ताओं की पसंद का सर्वोपरि होना’ या ‘उपभोक्ताओं के लोकतंत्र’ की जो बात बार-बार दुहराई जाती है वह शायद हम लोगों के समय का सबसे बड़ा भ्रम है। कहीं भी उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन लोगों की पसंद के हिसाब से नहीं होता। कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थों के परे आम आदमी में नए उत्पादों की कोई कल्पना नहीं होती। यह कहावत कि ‘आवश्यकता आविष्कार की जननी है’ किसी ऐसे अतीत की बात है जो हमारी जानकारी में नहीं है। वर्तमान काल में जबसे हम आधुनिक औद्योगिक सभ्यता से रूबरू हैं, स्थिति बिलकुल उल्टी है। आवश्यकताओं का आविष्कार किया जाता है और तब उन्हें लोगों की जरूरत बताया जाता है। सबसे ताजा उदाहरण मोबाइल फोन का है। इसकी जरूरत तो दूर, इसकी कल्पना भी आज से पचास साल पहले किसने की थी! पर आज लगभग घर-घर इसका प्रसार हो चुका है। इसके कार्यक्षेत्र का लगभग रोज फैलाव हो रहा है। इसके साथ कैमरा से लेकर कंप्यूटर तक के काम जोड़े जा रहे हैं और नए उपकरण तैयार हो रहे हैं। इनमें प्रत्येक का पहले आविष्कार हो जाता है और बाद में विज्ञापित कर लोगों के पास इन्हें पहुँचाया जाता है। अब यह लोगों की आवश्यकता बन जाती है। आविष्कार पहले और आवश्यकता बाद में आती है। लोगों के लिए नए आविष्कारों को आवश्यकता बनाने में आधुनिक विज्ञापन की अहम भूमिका होती है। धीरे-धीरे फैशन बनकर वे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज बनार्ड शॉ ने कहीं व्यंग्य में लिखा है कि अगर नाक फैशन बन जाए तो धीरे-धीरे लोगों की नाक ‘पंच’ (एक कॉमिक चरित्र) की तरह लंबी होने लगेगी।
मुझे अपने बचपन की याद है। उस समय हमारे यहाँ चाय पीनेवाले लोग शहरों में भी इक्के-दुक्के ही थे। कोई न इसका स्वाद जानता था और न गुण-अवगुण । लेकिन उसी समय बड़े-बड़े होर्डिंग लगने लगते थे- ‘सताती है हमको न मिहनत न सुस्ती, गरम चाय पीने से आती है फुर्ती।’ साथ-साथ लोगों को न सिर्फ घूम-घूम कर मुफ्त चाय पिलाई जाती थी बल्कि मुफ्त इसकी पुड़िया भी दी जाती थी। अब होर्डिंग गायब हैं लेकिन सुबह-सुबह, गाँव-गाँव गरीब और अमीर सभी घरों में चाय पी जाने लगी है। स्पष्ट है, यहाँ उपभोक्ता की पसंद बनाई गई है; चाय उपभोक्ता की पसंद की वजह से बाजार में नहीं आई।
लोगों को गैरजरूरी चीजों का आदी बनाने में आज ‘मॉल’ संस्कृति का विशेष हाथ है। अब गली-गली और घर-घर घूमकर नई वस्तुओं को पाने की ललक नहीं पैदा की जाती बल्कि लोग ही वैसी जगह पहुँचते हैं जहाँ तरह-तरह से आकर्षित करनेवाली वस्तुओं को सजधज के साथ लुभानेवाली अदा में उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। शायद यहाँ ‘गली-गली गो-रस फिरे मदिरा बैठ बिकाय’ के विपरीत व्यंजनों और व्यसनों का भेद मिटाकर साथ-साथ ही व्यसनों को व्यंजनों की तरह परोसा जाता है। सजावट और सेटिंग से जरूरी एवं गैरजरूरी सभी वस्तुएँ समान रूप से आकर्षित करती हैं। पहले लोगों में जैसा आकर्षण मेलों का होता था वैसा ही आकर्षण अब हर मौसम और हर महीनें में ‘मॉल’ का होता है, जहाँ जश्न भी है और हर किस्म का माल भी।
दरअसल अन्य जीवों की तरह मनुष्य भी निश्चित जीवनचक्र से बँधा होता है, और पोषण से लेकर प्रजनन तक का जीवनक्रम दिन, रात और विविध ऋतुओं के हिसाब से निर्धारित होता है। स्थान की भिन्नता और पोषक तत्वों की उपलब्धता के हिसाब से पेड़-पौधों और पड़ोस के पशुओं के साथ भी मनुष्य का एक निश्चित संबंध कायम होता है। इस तरह एक व्यापक कर्मकांड का ताना-बाना बुना होता है जिसकी भावनात्मक पकड़ इतनी जबरदस्त होती है कि इसका अतिक्रमणन सिर्फ समुदाय के लिए निंदनीय बन जाता है बल्कि स्वयं मनुष्य के भीतर एक अपराधबोध, पश्चाताप और भय पैदा करता है। परिस्थितियों के दबाव में ये परंपराजन्य वर्जनाएँ तभी टूटती हैं जब जीवन की नई जरूरतों के लिए इन्हें तोड़ना अस्तित्व का सवाल बन जाता है। अतीत में ऐसी जरूरतें पैदा हुईं एकाएक ऋतुओं के बदलाव, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं से। बाद में सभ्यता के उदय के साथ दिग्विजय को निकले महाबलियों के आक्रमणों से लोगों को बार-बार विस्थापित हो परिवेश बदलना पड़ा। इस दबाव में लोगों को जरूर अपने रहन-सहन एवं वेशभूषा को बदलने की मजबूरी हुई। लेकिन कालक्रम में फिर सब कुछ नए रीति-रिवाजों में स्थिर होता गया।
कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनकी आधुनिक सभ्यता बनाने में बड़ी भूमिका रही है, प्रारंभ में खिलौने और मनोरंजन बनी रही। मसलन चुंबक की जानकारी चीन में प्राचीन काल से थी पर सदियों बाद यूरोपीय जहाजियों ने इसका उपयोग कंपास बनाने में किया, जब वे महीनों लंबी समुद्री यात्राओं पर निकलने लगे थे। इसी तरह बारूद का ज्ञान चीनियों को प्राचीन काल में था पर वे इसका इस्तेमाल आतिशबाजी के लिए करते थे। यूरोपीय लोगों ने सदियों बाद तोप और तमंचों के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। सभ्यता के उदय के साथ विशाल पैमाने पर आक्रमण और नरसंहार की भूख तेज हुई। रुग्ण मानसिकता से पैदा इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सदियों से लगातार युद्ध आयुधों में सुधार और नए-नए आविष्कार होते रहे हैं।
पूँजीवादी व्यवस्था ने आवश्यकता से आविष्कार वाले क्रम को पूरी तरह उलट दिया है। पूँजीवाद में उत्पादन का एकमात्र लक्ष्य उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेच मुनाफा कमाना होता है। मुनाफे की मात्रा सदा उत्पादन और इसके उत्पादों की बिक्री से जुड़ी होती है। अगर लोगों की जरूरतें सीमित हों तो आबादी की बाढ़ के एक स्तर पर ये स्थिर हो सीमित हो जाएँगी। इससे उत्पादन पर एक सीमा लग जाएगी। यह पूँजीवादी व्यवस्था के ठहराव और इसकी मौत का संकेत होगा। इस ठहराव को तोड़ने का सरल उपाय है नई आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति की वस्तुओं का आविष्कार। आवश्यकताओं का आविष्कार पूँजीवादी व्यवस्था की मजबूरी बन जाता है। अगर रोज नए आविष्कारों से लोगों में नई जरूरतें पैदा की जा सकें तो उत्पादन पर कभी विराम नहीं लगेगा।
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नित्य नए उत्पादों को बाजार में लाकर पूँजीवाद अपने बाजार के संकट से निजात पा सकेगा। लेकिन क्या अनंत काल तक? यह संभावना दो कारणों से खारिज होती है- (1) पूँजीवाद में बाजार के मूल संकट पर विभिन्न बिंदुओं में मार्क्सवादी अर्थशास्त्रियों ने विचार किया है। उनके अनुसार इसके संकट का मूल कारण है उत्पादित वस्तुओं को खरीदने की क्रयशक्ति के एक हिस्से का सदा बाजार के लिए अनुपलब्ध होना। उनके अनुसार इसका कारण यह है कि उत्पादन में लगाए गए मजदूरों के श्रम की पूरी कीमत उन्हें नहीं दी जाती। इससे उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए जरूरी क्रयशक्ति का टोटा पड़ जाता है। इस विषय पर अनेक मार्क्सवादी चिंतकों ने विचार व्यक्त किया है और उन्होंने इसी अंतर्विरोध से पूँजीवाद के ध्वस्त होने की भविष्यवाणी की है। अभी तक इसके ध्वस्त नहीं होने का कारण एक बाहरी क्षेत्र ‘साम्राज्य’, ‘उपनिवेश’ आदि से क्रयशक्ति की उपलब्धता बतलाया गया है।
उपभोग और ऐयाशी की वस्तुओं की चाहे जितनी भी विविधता हो या उनका विस्तार हो अंततः उन्हें खरीदने की शक्ति तो किन्हीं हाथों में होनी ही चाहिए। अगर इसका टोटा होता है तो फिर संकट आएगा। अगर यह संकट अब तक टलता आया है तो इसका कारण यह हो सकता है कि अब तक बाजार या निवेश की दृष्टि से संसार के सभी कोने इसकी पहुँच में नहीं आए हैं और किसी बाहरी क्षेत्र से इसे राहत मिलती रही है। फिर भी सीमित रूप से बाजार के संकट का अंदेशा तो अर्थ-जगत पर बना ही रहा है।
1929-30 की मंदी से भी ‘न्यू डील’ की नीति से अमेरिकी व्यवस्था आंशिक रूप से ही उबर पाई थी। यह पूरी तरह उबरी द्वितीय विश्वयुद्ध से ही जब युद्ध की घोर बर्बादी ने विशाल बाजार उपलब्ध कराया। (2) दरअसल वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था के संकट का इससे बड़ा और मूल कारण जिसे उपभोक्तावादी संस्कृति और गहराती है वह है उत्पादन के लिए संसाधनों की सीमा। हमारी धरती एक सीमित नक्षत्र है और इसी सीमित नक्षत्र से उत्पादों के लिए असीमित संसाधनों की उपलब्धि असंभव है। जीवाश्म ईधनों- जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सारे स्रोत धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं, यह ईधन की लगातार बढ़ती कीमतों में प्रतिबिंबित है। अभी भारत के उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र देश में कोयले की घटती उपलब्धता के कारण विदेशो में कोयला खदानों को खरीदने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विभिन्न देशों में पैर फैलाने की आपाधापी है। इरान, इराक आदि के साथ बड़ी औद्योगिक शक्तियों की टकराहट का यह एक मूल कारण है। इससे उत्पादन के विस्तार का एक अलंघ्य सीमा तो लग ही जाती है।
जनमानस को जरूर एक समय तक उत्पादन के नए चमत्कारों से उलझाकर भ्रम में रखा जा सकता है। तत्काल बाजार के लुभानेवाले आकर्षणों मे आदमी आनेवाले या आसन्न संकटों की तरफ से लापरवाह जरूर हो जाता है। लेकिन इससे हम संसाधनों के अभाव की सीमा को टाल नहीं सकते। उत्पादन का जितना ही विस्तार होता है यह सीमा उतना ही पास आती जाती है। आत्मनियंत्रण ही एकमात्र उपाय है जिससे हम इस सीमा को दूर तक टाल सकते हैं।
अगर सीमाएँ हों भी तो आदमी सीमाओं के अतिक्रमण की कोशिश तो सदा से करता रहा है? इस संदर्भ में एक मूल प्रश्न उठाया जाता है- सुख की हमारी कल्पना क्या है? क्या सुख की कल्पना से भौतिक सुविधाओं को खारिज किया जा सकता है? क्या शारीरिक श्रम में कमी वांछनीय नहीं है?
शायद यह प्रश्न पुरातन काल से जबसे सभ्यता की शुरुआत हुई और पशुओं और दूसरे मनुष्यों पर काम का बोझ डाल कुछ लोगों के लिए आरामतलबी और शान-शौकत की जिंदगी संभव होने लगी, मानव समाज के सामने रहा है। श्रममुक्त आरामतलबी का रुझान औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों से शायद ज्यादा प्रबल होने लगा। उन्नीवीं सदी के प्रथम चरण में लिखे गए अपने विश्वविख्यात नाटक ‘फॉस्ट’ में जर्मन लेखक गोयथे ने ‘श्रमरहित ऐयाशी’ और ‘श्रमसाध्य सुरुचिपूर्ण जीवन’ की दो स्थितियों के बीच चुनाव का सीधा विकल्प प्रस्तुत किया है। नाटक के मुख्य नायक फॉस्ट ने समृद्धि और सुख के चिर जीवन की कामना से अपनी आत्मा को मेफिस्टोफिल्स (शैतान) के हवाले कर दिया है। मेफिस्टोफिल्स, फॉस्ट को अपने को परिवर्तित कर चिर-यौवन पाने के लिए डायनों द्वारा प्रस्तुत रसायनों की प्रक्रिया से गुजरने की सलाह देता है। लेकिन फॉस्ट प्रस्तुत प्रक्रिया के प्रति वितृष्णा जाहिर करता है। इसके जवाब में मोफिस्टोफिल्स कहता है- “ठीक है, एक तरकीब बिना डायन, सोना और जादू के अपनाई जा सकती है। अपनी भावनाओं को संयमित और सीमित दायरे में रखो। अपने को सादे आहार पर जीवित रखो। अपने मवेशियों के साथ रहो और स्वयं उनके मल को खाद के रूप में उस भूमि पर फैलाओं जहाँ से तुम अपना पोषण पाते हो। विश्वास करो, यह सबसे अच्छा तरीका है जिससे तुम अस्सी साल से अधिक तक अपने को युवा रख सकते हो।”
फॉस्ट का जवाब है- “मैं इसका अभ्यस्त नहीं हूँ। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं कुदाल लेकर जमीन की खुदाई करूँ। मेरे लिए सादगी के शुष्क जीवन की कोई अपील नहीं है।”
मेफिस्टोफिल्स कहता है- “वैसी हालत में मैं समझता हूँ कि डायन का रास्ता ही विकल्प है।”
उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ की यह दुनिया आज ज्यादा दारुण हो आदमी को आक्रांत कर रही है। आराम का जो लुभावना जीवन, गांधी के शब्दों में यह ‘शैतानी सभ्यता’ हासिल करा रही है अधिक आकर्षक और देखने में अधिक सहल भी है। लेकिन इसे हासिल करने का रास्ता झूठ, प्रपंच एवं हत्या का और उन सभी मानवीय मर्यादाओं और भावनाओं को नष्ट करने का है जिसका विवरण गोयथे के इस कालजयी नाटक में मिलता है। लेकिन यह नाटक आज निजी जीवन से बढ़कर सामूहिक रूप से विश्व स्तर पर मंचित हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों की सुख-सुविधा के लिए कुछ करोड़ लोग विश्वयुद्धों में और दूसरे कुछ करोड़ लोग छोटे-मोटे स्थानीय और गृहयुद्धों में मरते है और उनसे भी बड़ी तादाद में लोग अकाल, कुपोषण और विषाक्त हो रहे जल और भोजन से पैदा बीमारियों से असमय तड़प-तड़पकर मरते रहते हैं। इस सभ्यता से जिन्हें सहज और सुखद जीवन प्राप्त हो रहा है उनके लिए ये सब त्रासदियाँ महज आँकड़े हैं जो रूटिन के तहत संयुक्त राष्ट्रसंघ की संस्थाओं द्वारा संकलित और प्रसारित होते रहते हैं। ये आँकड़े निर्लिप्त होते हैं। इनमें न सड़ रही लाशों की दुर्गंध होती है, न घायल और बीमार लोगों के तड़पने की पीड़ा। हम अखबार के पन्ने पर ये आँकड़े देखते हैं और फिर पन्ना पलटते हैं और उसकी पीठ पर लुभानेवाले विज्ञापनों की दुनिया में अपनी संभावनाओं की कल्पना में डूब जाते हैं। हमारी त्रासदी यह है कि हमारा पूरा प्रचारतंत्र और जीवन की प्रस्तुतियाँ समस्या के एक ही पहलू को मन पर अंकित करती है। विडंबना यह है कि तर्क और विज्ञान के इस युग मे हम सुख और उपभोग (उपभोक्तावादी अर्थ में) का भेद करना भूल गए हैं। कार्य (वर्क) मशीनों का काम है या आँख से ओझल उन अर्धमानवों का जो दूर-दराज दुर्गम स्थानों पर खदानों में जहरीले और रेडियोधर्मी धूलों को फेफड़ों में भरते और असमय मरते रहते हैं। सभ्य मानव का काम है चटखारों से उदीप्त वासनाओं की तृप्ति। आज से आधी शताब्दी से अधिक पहले प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने ब्रिटेन के कोयला खदानों के श्रमिकों की तुलना ‘कैरियोटिड’ (यूनानी स्थापत्य में कंधों पर भवनों का बोझ उठानेवाली मानव मूर्तियाँ) से की थी। दुनिया के दूर-दराज अंचलों में या हमारी आँखों से ओझल यह सब हमारी चेतना से निर्वासित है क्योंकि इससे ‘आनंद’ में खलल पहुँचता है।
अगर शारीरिक श्रम इतना दुखद है तो लोग फिर बिना जरूरत पर्वतारोहण के कठोर श्रम का स्वेच्छा से वरण क्यों करते हैं? ओलंपिक या दूसरे कष्टसाध्य खेलों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? शायद सभी दूसरे जीवों की तरह श्रम और आराम के बीच संतुलन हमारी आनुवंशिक आवश्यकता है। दोनों में से किसी की अति या अभाव दुखदायी हो सकता है। हमारी नई पूँजीवादी औद्योगिक सभ्यता इस असंतुलन को पराकाष्ठा पर पहुँचाकर एक सिरे पर मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग फैलाती है तो दूसरे सिरे पर डायरिया, तपेदिक और काम के अत्यधिक बोझ से हरारत और मृत्यु। और अंत में खेल भी मनोरंजन की जगह व्यवसाय और मुनाफे का स्रोत बनता जा रहा है। इससे जुड़े विज्ञापनों से अरबों की कमाई होने लगती है। पहले मनोरंजन के लिए तीतर और मुर्गे लड़ाए जाते थे। फिर घुड़दौड़ आई जिस पर दाँव लगा कर जुआबाजी शुरू हुई और अब क्रिकेट आया है जो वास्तव में ‘क्रिकेट’ न रह कर अरबों के विज्ञापनों का धंधा बन गया है। इससे भी आगे बढ़कर – जैसे रोम में सर्कसों में मनुष्य और जानवरों को लड़ाने के खेल से नागरिकों को रिझाया जाता था, वैसा ही अब क्रिकेट में हो रहा है जिससे नागरिकों को जीवन की मूल समस्याओं के प्रति उदासीन बनाया जा रहा है। इस तरह श्रम की नैसर्गिक जरूरत को निरुद्देश्य क्रीड़ा के व्यवसाय में बदला गया है। परिवेश की भिन्नता से शारीरिक श्रम यातना की जगह आनंद का स्रोत भी हो सकता है जैसा श्रमसाध्य खेलों में होता है।
अंतिम रूप से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ संघर्ष व्यक्ति के स्तर पर होगा या व्यवस्था बदलने की नीति के स्तर पर होगा।
चूँकि उपभोक्तावादी संस्कृति को आदमी वैयक्तिक स्तर पर भी आत्मसात करता है और उस परिवेश से बी घिरा है जिससे उस पर उपभोक्तावादी दबाव बनता है, इससे निजात पाने का संघर्ष भी दोनों स्तरों पर होगा। लेकिन सबसे जरूरी है चेतना के स्तर पर इसके जादू से मुक्त होना। एक बात तो साफ दिखाई देती है कि इस संस्कृति को आधार मिला है वर्तमान पूँजीवादी औद्योगिक व्यवस्था से। इसलिए इसके खिलाफ मूल संघर्ष तो इस व्यवस्था से ही होगा। लेकिन निजी स्तर पर भी इसके मोह से मुक्त होने का प्रयास जरूरी होगा- वैसा ही जैसा स्वदेशी की लड़ाई राजनीतिक और वैयक्तिक रहन-सहन एवं लिबास दोनों के स्तर पर लड़ी गई थी। संसाधनों के सिकुड़ते आधार और पर्यावरण संकट से वर्तमान पूँजीवादी औद्योगिक व्यवस्था की सीमाएँ अब साफ उभरने लगी हैं। इससे आनेवाले दिनों में इसके खिलाफ संघर्ष आसान होता जाएगा। हालाँकि उन विकसित देशों में जहाँ उन्होंने परिवेश को अपनी उपभोक्तावादी जरूरतों के हिसाब से काफी बदल दिया है यह प्रयास बहुत ही दुखदायी हो सकता है। लेकिन जब अस्तित्व दाँव पर लग जाएगा तो मजबूरन व्यवस्था को बदलना ही होगा।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.