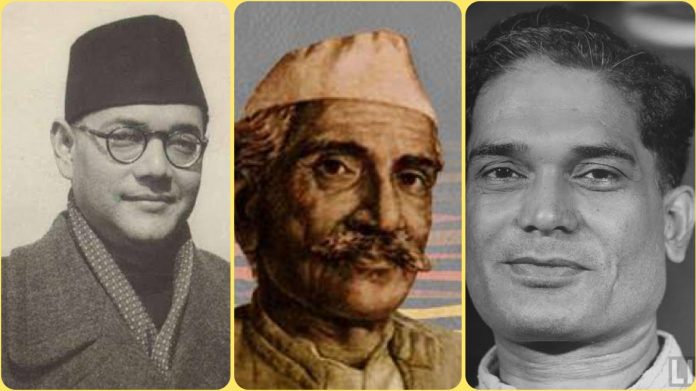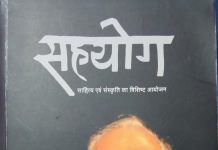— प्रोफेसर राजकुमार जैन —
(छठी किस्त)
सोशलिस्टों के लिए यह एक विकट स्थिति थी कि वो ना तो गाँधी को छोड़ना चाहते थे और न ही सुभाष बाबू को और न ही कांग्रेस का विभाजन उन्हें मंज़ूर था। सोशलिस्टों ने दोनों पक्षों, जो अब दक्षिण बनाम वामपंथ से बदलकर गाँधीवादियों बनाम सुभाषवादियों बन गया था, में एकता स्थापित करने का प्रयास किया।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जयप्रकाश नारायण ने त्रिपुरी अधिवेशन में ‘नेशनल डिमांड’ प्रस्ताव पेश किया जिसके बारे में उनका विचार था कि इसमें बोस तथा दक्षिणपंथियों के बीच समझौता हो सकेगा, जिसका समर्थन आचार्य नरेन्द्रदेव तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, इस पर अपनी सहमति जताई। जो इस प्रकार था– “कांग्रेस पिछली आधी सदी से भारत की जनता को जागृत करने में लगी हुई है तथा भारतवासियों की आजादी की तमन्ना का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले 20 वर्षों से यह जनता की इच्छानुसार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में जुटी हुई है। देश की आज़ादी के लिए यह अनेक प्रकार के त्याग व दमन को सहने के बावजूद यह लंबे समय से संघर्ष में जुटी हुई है। बढ़ते हुए जन समर्थन के कारण (कांग्रेस) बदली हुई परिस्थितियों में इसने आज़ादी प्राप्त करने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में स्थापित करने के उद्देश्य से कई नये कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया है। गर्वमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट को अस्वीकार कर पूर्ण संकल्प के साथ कांग्रेस घोषित करती है कि इस ‘फैडरल एक्ट’ का संपूर्ण विरोध तथा इसको किसी भी रूप में लागू होने का कड़ा विरोध करेगी।”
प्रस्ताव में अंग्रेज़ सरकार से माँग की गयी कि वे अविलंब भारत को आज़ादी प्रदान करें। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप न हो। देश के विभिन्न कांग्रेस संगठनों, कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों तथा विशेषकर किसानों का आह्वान करती है कि वे इन विघटनकारी शक्तियों जो देश में सांप्रदायिकता तथा अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं, का मुकाबला प्रांतीय सरकारों तथा विधायिकाओं के बाहर संगठन को मज़बूत करके करें ताकि वो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति बन जाए तथा प्रस्ताव के अंत में कांग्रेस से यह आग्रह किया गया कि वो सिविल नाफमानी की तैयारी करें।
जयप्रकाश द्वारा नेशनल डिमांड प्रस्ताव को पेश करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना तथा संघर्ष के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करना था। परंतु सुभाष बोस के बड़े भाई शरत बोस ने आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में केवल लफ्फाजी है केवल लफ्फाजी, इसमें कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। उनकी इस आलोचना से सोशलिस्टों द्वारा एकता के लिए किया जा रहा प्रयास निष्फल हो गया।
सोशलिस्टों ने सुभाषवादियों तथा गाँधीवादियों में समझौता कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया। विषय समिति में उन्होंने कई संशोधन पेश किये, इन संशोधनों में, सुभाष बोस की भर्त्सना वाले अंश को निकालने तथा केवल गाँधी की इच्छानुसार कार्यसमिति बने, केवल गाँधी ही कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं को हटाना भी शामिल था। ताकि पंत प्रस्ताव को निरस्त किया जा सके परंतु रूढ़िवादी नेता कांग्रेस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सोशलिस्टों को लग रहा था कि अगर पंत प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं तो इसका मतलब होगा कि इन रूढ़िवादियों को पूर्ण समर्थन। अगर विरोध करेंगे तो गाँधी के प्रति अविश्वास, नतीजे के रूप में कांग्रेस की टूट। इससे निराश होकर सोशलिस्टों ने पंत प्रस्ताव पर तटस्थ रहने का निर्णय कर लिया।
आज़ादी के संघर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भूमिका के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो पंत प्रस्ताव पर तटस्थ रहना, यही एक ऐसा विवादास्पद विषय था जिस पर पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह, पार्टी को तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा था, पार्टी में इस पर तीव्र प्रतिक्रिया थी, पार्टी के अधिकतर नौजवान कार्यकर्ता इस निर्णय के खिलाफ थे। उनका मानना था कि त्रिपुरी में अध्यक्ष पद के चुनाव में सोशलिस्टों ने सुभाष बाबू का समर्थन किया था। विषय समिति में भी पंत प्रस्ताव का विरोध किया तो मूल प्रस्ताव पर हम तटस्थ क्यों रहे? सुभाष समर्थकों तथा विशेष रूप से कम्युनिस्टों ने इसकी कड़ी आलोचना की। सुभाष बोस के समर्थक सोशलिस्टों पर विश्वासघात का खुला आरोप लगाने लगे, इसी वजह से बंगाल में सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ गयी, कम्युनिस्टों ने झूठ-मूठ की हवा फैलाकर बंगाल में अपने आप को मजबूत कर लिया।
स्वयं सुभाष बोस ने अपने एक लेख में कहा– “सन् 1939 के जनवरी महीने में वामपंथी धड़ा या प्रगतिशील तत्त्व मेरे अध्यक्ष बनने में सहायक थे। संख्या की दृष्टि से इन लोगों का कांग्रेस में बहुमत था। लेकिन एक कमी थी। वे गाँधी पक्ष (दक्षिणपंथी) की तरह एक नेतृत्व के अंदर संगठित नहीं थे। उस समय तक कोई ग्रुप या पार्टी ऐसी नहीं थी जिसे संपूर्ण वामपंथी पक्ष का विश्वास प्राप्त हो। यद्यपि उस समय वामपंथ की सबसे महत्त्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, लेकिन उसका प्रभाव सीमित था। इसके अलावा जब गाँधी पक्ष और मुझमें लड़ाई शुरू हुई तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अनिश्चय में पड़ गयी। अत: एक संगठित और अनुशासित वामपक्ष के अभाव में मेरे लिए गाँधी पक्ष से लड़ना असंभव हो गया।”
सुभाष बाबू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के शुरू से ही समर्थक थे, त्रिपुरी के निर्णय से उन्हें ठेस पहुँची। विडंबना यह थी कि रूढ़िवादी कांग्रेसी जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कांग्रेस के अंदर रहकर काम करने का हमेशा विरोध करते थे। इसके विपरीत सुभाष बाबू ने सोशलिस्टों का हमेशा समर्थन किया। त्रिपुरी कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा : “कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। मैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। लेकिन मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि शुरू से ही इसके सामान्य सिद्धांतों और नीतियों से मैं सहमत रहा हूँ।प्रथमत: वामपंथी तत्त्वों को एक पार्टी में संगठित करना वांछनीय है। दूसरे, किसी वामपंथी ब्लाक का तभी कोई मतलब है जब उसका चरित्र समाजवादी हो। कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्हें ऐसे ब्लाक (कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी) को पार्टी कहने पर आपत्ति है, लेकिन मेरे विचार से ऐसे ब्लाक को आप ग्रुप, लीग या पार्टी क्या कहते हैं, एकदम नगण्य बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर कोई वामपंथी ब्लाक समाजवादी कार्यक्रम अपना सकता है। वैसी अवस्था में उसे निश्चित तौर पर हम ग्रुप लीग या पार्टी कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या उसी तरह की दूसरी पार्टी की भूमिका वामपंथी ग्रुप की तरह होनी चाहिए। समाजवाद हमारे लिए तात्कालिक समस्या नहीं है, फिर भी समाजवादी प्रचार समाजवाद में विश्वास रखने और उसके लिए लड़नेवाली मात्र कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टी द्वारा ही संचालित किया जा सकता है।”
सुभाष बाबू ने अपने एक लेख में विस्तार से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्रिया-कलाप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा– “सन् 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उदय देश में प्रगतिशील या वामपंथी शक्तियों के पुनरुत्थान का निश्चित संकेत था। इसके साथ ही किसानों, छात्रों और कुछ हद तक कामगारों में असाधारण जागृति पैदा हुई। पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा नामक एक केंद्रित अखिल भारतीय किसान संगठन उभरा। इसके सबसे प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती थे। इस अवधि में अखिल भारतीय स्टूडेंट्स फेडरेशन के नेतृत्व में छात्र आंदोलन भी केंद्रित हुआ। सन् 1934 से 1938 के बीच कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनने का सर्वोत्तम अवसर था, लेकिन वह इसमें फेल हो गयी। शुरू से ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य का अभाव था। यह क्रांतिकारी आंदोलन का अगुवा बनने के बदले अधिकतर कांग्रेस के अंदर संसदीय विरोध का काम करती रही। सितंबर 1939 के बाद इस पार्टी के नेताओं को गाँधी और नेहरू ने अपने पक्ष में कर लिया, जिससे उसका भविष्य खत्म हो गया।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी द्वारा पंत प्रस्ताव पर तटस्थ रहने पर सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई, इस बारे में 31 मार्च 1939 को सुभाष बोस ने गाँधीजी के साथ निजी पत्रव्यवहार में लिखा कि सी.एस.पी. के कैडर में विभाजन हो गया है। पार्टी की कई प्रांतीय यूनिटों ने पार्टी के नेताओं की नीतियों के खिलाफ़ बगावत कर दी है। इनके बड़े नेता अभी कुछ भी कहें, परंतु वो दिन दूर नहीं जब इस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ आ जाएँगे, अगर आपको मेरी बात में कोई संदेह लगता है, तो इसको देखने के लिए कुछ इंतज़ार करना है।….बहुत सारे कार्यकर्ता केवल नैतिकता तथा अनुशासन के कारण चुप हैं।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर गाँधी-सुभाष प्रकरण को लेकर निरंतर हमले हो रहे थे, पार्टी प्रस्ताव पर तटस्थ क्यों रहीं? इसका स्पष्टीकरण देते हुए जयप्रकाश नारायण ने कहा “हमारी पार्टी ने इस हक़ीक़त को समझ लिया था कि कांग्रेस का नेतृत्व रूढ़िवादी कांग्रेसियों के हाथ में था, तथा वे ही आज़ादी की ललक चाहनेवाले लोगों की नुमाइंदगी करते थे। जनता पर सबसे ज्यादा उनका ही असर है। आज़ादी का आंदोलन एक नाजुक मोड़ पर है, कांग्रेस में एकता बनाए रखना, सबसे ज़रूरी है। पुराने कांग्रेसियों में ज्यादातर नेता उम्रदराज थे यदि उन्हें और पाँच वर्ष काम करने दिया जाए, कांग्रेस तथा मुल्क में एक अच्छा शक्ति संतुलन बन जाएगा। जैसा कि हमेशा होता आया है पुराने लोगों के बाद नये लोगों को मौका मिलता ही है। हमारी पार्टी ने सुभाषचंद्र बोस को वोट दिया था। हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमारा वोट वाम-पक्ष बनाम दक्षिणपंथ के आधार पर आधारित नहीं था। हमने सुभाष बोस को इसलिए वोट दिया क्योंकि हमने उनके मुकाबले खड़े श्री पट्टाभि सीतारामैया की तुलना में बोस को पसंद किया था। हमें यह आशा कभी नहीं थी कि यह कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न कर देगा। हमारी पार्टी किसी भी झगड़े में न पड़ी है, और न ही पड़ेगी। झगड़े से कभी एकता स्थापित नहीं होती। इसको टाला जा सकता था तथा समझौता हो सकता था। हमारी पार्टी ने इसको रोकने की कोशिश की। हम सुभाष बाबू के पास गए तथा उनसे कहा कि वे एक वक्तव्य जारी कर दें। उन्होंने यह किया भी परंतु वह संतोषजनक नहीं था। हमने दक्षिणपंथियों से भी बात की परंतु हमको निराशा मिली। हम इस निर्णय पर पहुँचे कि जब तक कांग्रेस की कार्यसमिति गाँधीजी की इच्छानुसार नहीं बनती तब तक एकता स्थापित नहीं हो सकती। प्रस्ताव में कई ऐसी बातें थीं, जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर दोनों पक्षों ने सहयोग दिया होता तो ही किसी समझौते पर पहुँचा जा सकता था। हम इस झगड़े में शामिल होना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। हमारे इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई। परंतु इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भावनाओं में बहकर तर्क, दलील बेकार हो जाते हैं। अध्यक्ष के चुनाव तथा पंत जी के प्रस्ताव के समय परिस्थितियाँ बिल्कुल बदली हुई थीं। स्वाभाविक था कि पार्टी के पास एक ही रास्ता (तटस्थ) था तथा उसी को हमने चुना।
आचार्य नरेन्द्रदेव ने जुलाई 1939 में दिल्ली सोशलिस्ट कांग्रेस में अध्यक्षता करते हुए अपने भाषण में त्रिपुरी में पार्टी द्वारा लिये गए निर्णय के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि वामपक्ष कमजोर तथा विभाजित था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी अगर प्रस्ताव के विरोध में मतदान करती तब भी पंत प्रस्ताव को पराजित नहीं किया जा सकता था। तथ्य यह है कि विषय कमेटी में भी पंत प्रस्ताव पास हो गया, हालाँकि बहुत कम मतों से। हालाँकि सोशलिस्ट पंत प्रस्ताव पर तटस्थ थे, परंतु उन्होंने सुभाष बाबू और कांग्रेस में एका कराने का पूर्ण प्रयत्न किया।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.