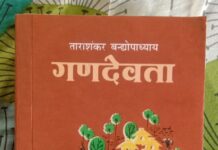— किशन पटनायक —
चुनाव होता है राजनीतिक सत्ता-केंद्रों के लिए। संसद, विधानसभा, पंचायत– ये सब राजनीतिक सत्ता-केंद्र हैं। उनके समानान्तर समाज के अंदर बहुत सारे शक्ति-केंद्र होते हैं। समाज का शक्ति-केंद्र वही है जहाँ से बहुत सारे लोगों या समूहों को नियंत्रित तथा प्रभावित किया जाता है। जहाँ धन एकत्रित है वहाँ एक शक्ति-केंद्र है, जहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है वहाँ भी एक शक्ति-केंद्र, है क्योंकि वहाँ से लोगों के मन, कार्य और आचरण को प्रभावित किया जा सकता है। नौकरशाही ऐसी संस्था है जिसमें धन का भी तत्त्व होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी। हिंसा जहाँ एकत्रित है वहाँ भी एक शक्ति-केंद्र है। नौकरशाही के अलावा माफिया भी वह बिंदु है जहाँ सामाजिक हिंसा केंद्रित हैं। जब बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के चुनाव होगा तो सौ फीसदी नतीजा इन शक्ति-केंद्रों की मर्जी के मुताबिक होगा।
राजनीतिक दल और प्रचार माध्यम जब खुद एक-एक शक्ति-केंद्र बन जाते हैं तब उनके हस्तक्षेप से नतीजे बदल सकते हैं और धन, हिंसा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के विपरीत लोगों की राय जा सकती है। हरेक आधुनिक राष्ट्र में राजनीतिक दलों और प्रचार माध्यमों की अपनी शक्ति बनी हुई है। इस तरह समाज के अनेक शक्ति-केंद्र हो जाते हैं। सामाजिक शक्ति के रूप में जाति का अलग केंद्र है। धर्म का अलग शक्ति-केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा राष्ट्र, राज्य, जिला, गाँव आदि भिन्न-भिन्न स्तरों में अनेक शक्ति-केंद्र हो सकते हैं।
जब तक इन शक्ति-केंद्रों को राजनीतिक उद्देश्य से संचालित नहीं किया जाता तब तक इसका प्रभाव चुनाव पर नहीं होगा, लेकिन इनमें से अधिकांश शक्ति-केंद्रों का राजनीतिकरण हो चुका है। 1960 तक उत्तर प्रदेश-बिहार में पिछड़ी जातियों का राजनीतिकरण विशेष ढंग से नहीं हुआ था। अभी तक ओड़िशा या बंगाल में पिछड़ी जातियों का राजनीतिकरण नहीं हुआ है। माफिया या राजनीतिकरण भी हाल की घटना है। यानी बहुत सारे नए शक्ति-केंद्रों का उदय पिछले दशकों में हुआ।
राजनीतिक सत्ता कानूनीतौर पर सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, कारण राज्य की यह कानूनी क्षमता है कि किसी भी सामाजिक शक्ति को कमजोर और पंगु बना दे। राज्य चाहेगा तो धनी वर्ग के धन के परिणाम को कम कर सकता है और मंदिर की पूजा को भी बंद करवा सकता है या जातियों में शादी पर भी पाबंदी लगा सकता है। इसलिए सामाजिक शक्तियों की यह इच्छा रहती है कि राज्य-सत्ता में उनका प्रभावी प्रतिनिधित्व रहे। जिसकी सामाजिक शक्ति या प्रतिष्ठा जितनी अधिक है उसकी उतनी अधिक गरज रहती है कि सत्ता-केंद्रों पर उसका कब्जा हो। इसलिए धन के हिसाब से पूँजीपतियों का और जातियों के हिसाब से सामाजिक तौर पर उच्चजातियों का सर्वाधिक आग्रह रहता है कि सत्ता-केंद्रों पर उनका नियंत्रण रहे। इसका मतलब हुआ कि समाज में जिसकी शक्ति जितनी अधिक है राजनीति में उसका आग्रह उतना अधिक होता है।
जब कोई नया समूह अपनी शक्ति को संगठित कर राजनीति या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो पहले के शक्तिशाली समूह इसको अनुचित समझते हैं। अगर बंगाल की पिछड़ी जातियाँ अपना एक शक्ति केंद्र बनाकर राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी तो बंगाल के ब्राह्मण-कायस्थ इस पर जरूर एतराज करेंगे।
राजतंत्र में राजा न सिर्फ राजसत्ता का अधिकारी होता था बल्कि इसपर भी ध्यान देता था कि समाज के अंदर जितने सामाजिक व सांस्कृतिक समूह हैं उनका भी संरक्षक बना रहे ताकि कोई सामाजिक शक्ति-केंद्र उसकी सार्वभौम सत्ता को चुनौती न दे। उसी तरह आधुनिक समाज में पूँजीवादी वर्ग न सिर्फ चुनाव के दिनों में अपने अनुकूल राजनीतिक दलों को जिताता है बल्कि उससे भी ज्यादा उसकी चेष्टा यह रहती है कि समाज में जो प्रभावी समूह यानी शक्ति-केंद्र है उन सब पर उसका नियंत्रण रहे। राजनीतिक दल, जातीय संगठन, प्रचार माध्यम, नाटक, संगीत, क्रिकेट- हरेक प्रभावशाली केंद्र में वह अपनी पैठ रखता है ताकि जब जरूरत हो उनका राजनीतिकरण कर सके। इसलिए पूँजीपति न सिर्फ राजनीतिक दलों को पैसा देता है बल्कि बुद्धिजीवियों से लेकर क्रिकेट खिलाड़ी तक सबको अपने ऊपर निर्भर बनाकर रखता है।
जितने भी शक्ति-केंद्र चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उन सारे शक्ति-केंद्रों को पूँजीपति वर्ग अपनी संचालन परिधि में रखता है। जिला या ग्रामीण स्तर का जो व्यापारी होता है वह अपने स्तर का एक शक्ति-केंद्र है, लेकिन वह पहले से राष्ट्रीय स्तर के पूँजीपति से जुड़ा रहता है। इसलिए अपने इलाके की राजनीति को अपने स्वार्थ के हिसाब से मोड़ देते समय वह इसका खयाल रखता है कि उसके इलाके की राजनीति पूँजीपतियों के विरुद्ध न हो जाए। इसी तरह विभिन्न शक्ति-केंद्रों का आपसी समन्वय बन जाता है।
जब से पिछड़ी जातियों का शक्ति-केंद्र बनने लगा है तब से धनी वर्गों का ध्यान उधर भी गया है और पिछड़े नेताओं को अपने साथ रखने की कोशिश हुई है। कुछ उद्योगपतियों का मुलायम सिंह-प्रेम इसी दिशा में एक कदम है ताकि पिछड़ों और दलितों की राजनीति ब्राह्मणों के विरुद्ध हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन पूँजीपतियों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है कि दलितों, पिछड़ों, औरतों और पिछड़े इलाकों की राजनीतिक चेतना विगत दो दशकों में काफी संगठित हुई है, उनका मतदान भी बढ़ा है, लेकिन देश की राजनीति का कोई भी हिस्सा आज पूँजीवाद विरोधी नहीं है।
जब तक देशी पूँजीपति भारत की राजनीति पर हावी थे तब तक तो राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पूँजीवाद विरोधी था, लेकिन जब से अंतरराष्ट्रीय पूँजीवाद का जोरदार प्रवेश हुआ है तब से राजनीति में पूँजीवाद का विरोध महत्त्वहीन हो गया है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय पूँजीवाद ने देश की राजनीति पर अपना पूर्ण नियंत्रण पा लिया है– न सिर्फ राजनीति पर बल्कि संस्कृति, शिक्षा और खेल पर भी, ताकि इन बिंदुओं से राजनीति का कोई दूसरा मोड़ न शुरू हो जाए।
क्रिकेट खिलाड़ी सोचेगा : मेरा राजनीति से क्या वास्ता? मैं तो पैसे के लिए खेल रहा हूँ और दूसरों का मनोरंजन कर रहा हूँ। होता यह है कि जिसके पैसे से वह खेलता है, जाने-अनजाने उसी की राजनीति का वह अंग बनता है। चुनाव में आने के पहले वह राजनीति का हिस्सा बन चुका रहता है। इसी तरह सारे शक्ति-केंद्रों का जाने-अनजाने राजनीतिकरण हो रहा है। जिसको चुनाव में पड़ना है उसको विभिन्न शक्ति-केंद्रों में सक्रिय होना पड़ता है या नये शक्ति-केंद्रों का निर्माण करना पड़ता है।
सत्ता-केंद्रों का चुनाव हो रहा है। अगर शक्ति-केंद्रों के द्वारा राजनीति नियंत्रित होती है, तो चुनाव को समझने के लिए शक्ति-केंद्रों का अध्ययन जरूरी है। किन शक्ति-केंद्रों का कितना और कैसा राजनीतिकरण हुआ है?नये-पुराने शक्ति-केंद्रों के प्रभाव और व्यापकता में कितनी घट-बढ़ हो रही है?
एक समय था जब श्रमिक संगठनों की शक्ति का इस्तेमाल पूँजीवाद विरोधी राजनीति के द्वारा होता था। अभी कोई बड़ा श्रमिक संगठन नहीं है जो क्रांतिकारी राजनीति का पक्षधर हो। तीस साल पहले समाजवादी और साम्यवादी पार्टियाँ क्रांतिकारी राजनीति का शक्ति-केंद्र थीं तो प्रचार माध्यम का एक हिस्सा, बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा, संस्कृति का एक हिस्सा, संगठित किसानों और विद्यार्थियों का एक हिस्सा उसी राजनीति का पक्षधर हो गया था। यहाँ तक कि नौकरशाही का भी एक हिस्सा निजीकरण का विरोधी हो गया था। ये सारे शक्ति-केंद्र या तो ध्वस्त हो चुके हैं, या फिर उनकी राजनीतिक दिशा बदल चुकी है। उनका इस्तेमाल एक भिन्न राजनीति के द्वारा हो रहा है।
सवाल उठता है कि चुनाव के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन, विषमता को कम करना तथा धनी वर्गों के अत्यधिक प्रभाव का विनाश कैसे हो सकता है?
भारत की मौजूदा परिस्थिति में चुनाव से इसकी उम्मीद करना कठिन है, यह संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव का नतीजा गैर-राजनीतिक सज्जन-समूहों का नहीं, एक लंबे अरसे की राजनीति का परिणाम होता है। 1991 से जो राजनीति चली है, राजनीतिक दिशाओं का जो परिवर्तन पिछले एक दशक में होता रहा है, चुनावों में उसका ही परिणाम निकलेगा। इसमें विषमता के विरुद्ध, धनी समूहों के अतिशय प्रभाव के विरुद्ध, महँगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई राजनीति नहीं है, गाँव की गिरती हैसियत को बचाने की कोई राजनीति नहीं है। इन उद्देश्यों का चुनाव परिणाम तब निकलेगा जब इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर कोई प्रभावी राजनीति पैदा होगी। यह राजनीति समाज के विभिन्न शक्ति-केंद्रों में घुसपैठ करेगी अर्थात् किसानों को, विद्यार्थियों को, दलितों, पिछड़ों और नारी आंदोलन को समाजवादी उद्देश्यों के लिए नए सिरे से प्रेरित करेगी। वह अपना एक प्रचार माध्यम बनाएगी, अपनी एक सांस्कृतिक धारा तथा अपनी एक वैचारिक धारा नए मुहावरे के सहारे बनाएगी।
जन आंदोलनों को अपनी राजनीति घोषित करनी होगी। कोई संगठन, कोई जन आंदोलन खुद चुनाव लड़े या न लड़े, उसकी अपनी राजनीति जाहिर करनी पड़ेगी।
राजनीति पर पूँजी के नियंत्रण पर हमला अमरीका में बाद में होगा, भारत जैसे विकासशील देशों में पहले होगा। विश्व-व्यवस्था में परिवर्तन की अगुआई विकसित राष्ट्र नहीं कर पाएँगे, पिछड़े-गरीब मुल्क करेंगे।
(अप्रैल 1996)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.