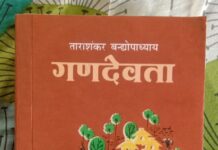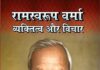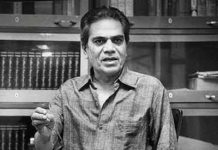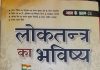— संजय गौतम —
उन्नीसवीं बारिश सुपरिचित कथाकार शर्मिला जालान का दूसरा उपन्यास है। उनका पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ करीब बीस वर्ष पहले ‘शादी से पेश्तर’। किताब के रूप में वह पहली किताब थी, हालांकि उन्होंने तब तक कई कहानियां लिख डाली थीं। उसके बाद उनका कहानी संग्रह आया ‘बूढ़ा चॉंद’ (2008) फिर लंबे अंतराल के बाद कहानियों का संग्रह ‘राग विराग तथा अन्य कहानियां’ (2018) तथा ‘मॉं, मार्च और मृत्यु’ (2019) और अब यह उपन्यास ‘उन्नीसवीं बारिश’। उपन्यास की कथावस्तु उनके मन में कितने समय तक खदबदाती रही है, इसका पता इस बात से भी लगता है कि इसी शीर्षक से उनकी लंबी कहानी ‘मॉं, मार्च और मृत्यु’ में भी प्रकाशित है। पात्रों के नाम अलग हैं, लेकिन कहानी का केंद्रीय भाव वही है, जो इस उपन्यास का है। यह कथावस्तु उनके मन को इतने आयामों में मथती रही कि एक लंबी कहानी लिखने के बाद भी संवेदना का मंथन जारी रहा और उसे विस्तार से समूची विसंगतियों के साथ व्यक्त करने के लिए उन्होंने उपन्यास का ताना-बाना बुना और अपने मन की छटपटाहट को बखूबी व्यक्त करने का प्रयास किया, हालॉंकि कभी भी पूरी तरह व्यक्त कहॉं हो पाता है!
कई बार लगता है कि लेखक पूरे जीवन अपने मन को ही लिखता रहता है, बस वे चीजें बदल जाती हैं, जिनके ऊपर उसके मन का प्रक्षेपण होता है और चीजें बदल जाने से प्रक्षेपण का रंग जितना बदलता है, उतना ही चीजों की रंगत भी, उसी रंग और रंगत को पकड़ने की कोशिश में ही लेखक का जीवन रीतता भी है, बीतता भी है। इस उपन्यास में भी जिस ‘चारुलता’ के ‘मन’ की कहानी है, वह मन लेखिका का ही तो है। इसीलिए चारुलता के मन को हम शर्मिला जालान की कहानी यात्रा की शुरुआत से देख सकते हैं, चारुलता के मन को हम उनके पहले उपन्यास में भी गहराई से महसूस सकते हैं।
चारुलता का जो मन है, वह बहुत ही मासूम, मुलायम लेकिन चौकन्ना है। वह मासूमियत से, मुलायमियत से लेकिन चौकन्नेपन से दुनिया को देखता है, दार्शनिक अंदाज में नहीं, सरल सहज दृष्टि से, लेकिन उसका सहज आत्मबोध ऐसा है कि चालाकियों को, काईंयापन को, अटपटेपन को मुस्कराते हुए, बेपरवाही से पकड़ लेता है। पाठक को चकित करता है, फिर आगे बढ़ जाता है।

चारुलता का मन स्त्री-देह लुब्धकों के मन को पहचान लेता है, और ऐसे लोगों से भयानक नफरत करता है, चाहे वह प्रेमी हो या कोई और सगा-संबंधी हो। यह खूब बात करना चाहता है, दुनिया में सभी से बात करना चाहता है, मनुष्य समाज से ही नहीं, पशु पक्षियों, पेड़-पौधों, घर-मकानों, सड़कों-गलियों से भी बात करना चाहता है, उनका हालचाल लेना चाहता है, लेकिन संबंधों के दैहिक आयाम की संभावना मात्र से ही उसके मन के भीतर उड़ती हुई तितलियॉं मरने लगती हैं।
चारुलता हिमांशु से मिलकर भी नहीं मिल पाती है। चारुलता के भीतर भी एक चारुलता है, जो हिमांशु से मिलते हुए भी मिलती नहीं है, वह जिस हिमांशु से मिलना चाहती है, जिसके बारे में जानना चाहती है, वह जिसे अपने बचपन की स्मृतियॉं सुनाना चाहती है, वह हिमांशु, हिमांशु के भीतर नहीं है। इसलिए उपन्यास की उन्नीस वर्षीय चारुलता तेईस वर्षीय हिमांशु के साथ बातचीत करते हुए भी मिल नहीं पाती है। चारुलता के जीवन में नीरू दीदी हैं, माँ हैं, बाबा हैं। अपने माता-पिता की वह इकलौती संतान है। पढ़ाई-लिखाई करके पत्रिका संपादन के कार्य से जुड़ जाती है। माँ के साथ कोलकता में रहती है। बाबा बनारस में बैंक में ऊँचे पद पर हैं।
जैसे चारुलता के भीतर दो मन है, उसी तरह सभी पात्रों के भीतर दो मन है। चारुलता किसी को भी सिर्फ ऊपर-ऊपर से नहीं देखती, वह सबके भीतर झाँकना चाहती है, झाँक कर देखती है तो जो दिखता है, वह होता नहीं है। बाबा भी जो दिख रहे हैं, वे नहीं हैं, उनके भीतर बहुत सी बातें हैं जो प्रथमत: अदृश्य हैं। उनका बनारस का जीवन रहस्यमय रहते हुए भी रहस्य नहीं रह जाता, जैसे-जैसे खुलता है चारुलता का मन उदास होता जाता है। बाबा जब कोलकाता लौट आते हैं, तब भी जीवन सामान्य नहीं हो पाता, वह अपनी संपत्ति के वारिस के लिए भतीजे को गोद लेते हैं। पितृसत्तात्मक सोच ही है कि न तो वह चारुलता को पर्याप्त समझते हैं, न पत्नी के भतीजे को गोद लेने पर विचार करते हैं।
इस कथा में न आदि है न उत्कर्ष न अंत। यह कथा ऐसे चित्रपट की तरह है, जिस पर संवेदना की सघन लहरें आती हैं, जाती हैं, और अपना चित्र उकेरती चली जाती हैं। कोई भी पात्र न पूरी तरह दोषी नजर आता है, न निर्दोष। लेखिका ने सभी पात्रों के अपने-अपने आकाश को निर्लिप्त भाव को देखा है। नीरू दीदी की पीड़ा, माँ की पीड़ा, चारुलता की पीड़ा की लहरें उपन्यास में तरंगों की तरह फैलती रहती हैं। माँ का संसार तो अनबोलते मानुष का संसार है, जिसका दर्द सिर्फ उसकी निस्संग गतिविधियों, आवाजों और आँखों में ही व्यक्त होता है।
उपन्यास के प्रमुख पात्र चारुलता, नीरू साहित्य से जुड़े हैं, स्वयं भी रचनाएं करते हैं। रवींद्रनाथ के साहित्य से आत्मीयता है, इसलिए साहित्य में आवाजाही चलती रहती है। कहीं डायरी शैली का उपयोग हैं तो कहीं पत्र शैली का। चारुलता स्वरचित छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से अपनी उलझनों को सामने लाती है तो नीरू दीदी की नोट की गयी कविताओं से उनके जीवन का द्वंद्व सामने आता है। नीरू दीदी की छोटी बहन की शादी हो गयी, लेकिन वह अपने बाबा की सेवा में ही लगी रह गयीं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती आदि कवियों की कविताओं से उनके मन की उलझनों को, परिवेश को सामने लाया गया है। उपन्यास के पूरे मानस को व्यक्त करने के लिए ‘गीतांजलि’ के गीत प्रारंभ में और बीच में दिए गए हैं।
पात्रों के मन की यात्रा करता हुआ यह उपन्यास जीवन-जगत के यथार्थ से दूर नहीं है। हिमांशु, रक्तिम दा, बाबा, स्वामी अवधेशानंद के माध्यम से पिछले बीस-तीस वर्षों में बनी और बन रही दुनिया का यथार्थ उपन्यास में बहता चला आता है। इसमें वैश्वीकरण का यथार्थ भी है, बाजार का यथार्थ भी और राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ताओं का यथार्थ भी।
शर्मिला जालान महिला लेखन की प्रतीति से संबंद्ध लेखिका नहीं हैं, इसलिए उनके लेखन को सिर्फ महिला लेखन की परंपरा में देखना उचित नहीं होगा। उनके भीतर समग्र साहित्य परंपरा है, लेकिन प्रवाह के रूप में। वस्तु या विन्यास के स्तर पर इसका मूर्त रूप खोजना भी ठीक नहीं है। उनकी अपनी शैली है, जिसे हम बातूनी शैली भी कह सकते हैं। उनके पात्र खूब बात करना चाहते हैं, तरह-तरह की बातें, तरह-तरह के लोगों से बातें, दुनिया को देखने-समझने वाली बातें, जिज्ञासु- उत्सुक आँखों से कहने और सुनने वाली बातें। इन बातों के बीच में ही किस्से का रस बहता रहता है और जीवन की कड़ियॉं खुलती रहती हैं। एक लेखिका के रूप में उन्हें इस बात का गहरा सलीका है कि कौन सी सूचना कब देनी है और कब तक उसे पात्र के मन में दबाए रखना है और कौन सी सूचना नहीं देनी है, उसे बस भंगिमाओं से व्यक्त करना है। इसी गहरे बोध के कारण उनकी किस्सारसाई में रस बना रहता है और पाठक जगह-जगह पर चमत्कृत-विस्मित होता है।
हर किताब की परंपरा खोजने की भी एक परंपरा है और परंपरा निर्धारित करने की भी परंपरा है। कहानी या उपन्यास है तो प्रेमचंद की परंपरा की है या जयशंकर प्रसाद की परंपरा की या फिर प्रगतिवादी लेखन की परंपरा है या कलावादी की। कविता है तो कबीर की परंपरा है या तुलसीदास की, अज्ञेय की है या मुक्तिबोध की। क्या किसी लेखक में किसी एक की परंपरा संभव है। निर्मल वर्मा याद आ रहे हैं, बच्चे के जन्म लेने पर अक्सर यह कहा जाता है कि बच्चे की नाक अमुक पर गयी है, आँख अमुक पर गयी है। यानी उसका हर अंग खास तौर पर आँख-नाक माँ-बाबा, दादा–दादी, नाना-नानी, बुआ आदि पर जाता है, लेकिन जिसे चीन्हा नहीं जा सकता क्या उसमें सभी का अंश नहीं रहता है। बच्चे में सभी का अंश रहते हुए भी उसकी निजता होती है, और उसी से वह पहचाना जाता है। किताब की भी ऐसी ही हालत है। अपने साहित्य और समाज में गहरे धॅंसे हुए लेखक की किताब में सारी दीवारें ढह जाती हैं। उसे कलावाद या प्रगतिवाद जैसे किसी साँचे में बिठाना मुश्किल होता है। इस किताब के साथ भी यह मुश्किल बनी हुई है।
इसकी कथा भी सरल रेखीय नहीं है। कौन सी चमकती हुई बात कहाँ पर आयी है, इसे याद रख पाना मुश्किल है, क्योंकि घटनाएं एक क्रम से घटित नहीं हैं। स्मृति-प्रवाह में आती जाती रहती हैं। इस स्मृति-प्रवाह में ऐसे कथन और ऐसी भंगिमाएं आती हैं जो मन के किसी कोने में दर्ज हो जाती हैं–‘हिमांशु जैसा है उसके वैसा होने के पीछे सदियों की शक्ति लगी हुई है। बाबा जैसे हैं, उनके होने के पीछे भी सदियों के संस्कार हैं। बाबा और हिमांशु पांच तत्त्व नहीं हैं जो चिता पर लेटाने के बाद भस्म बन जाते हैं। वे वह हैं जिन्हें देखे ‘छल’ की माया समझ में आती है। वे ‘छल’ भी नहीं। वह अपने जीवन का डर है। वह अपनी सुरक्षा का भाव। अपने को बचाना। अपने स्व को बचाना। अपने अहं को बचाना। पर चारु सिर्फ पांच तत्त्व नहीं जो भस्म बन जाए और चिता पर जलकर विलीन हो जाए व्योम में’। (पृ.151)
इन्हीं मानसिक जकड़नों की जड़ से फूटे हुए कल्ले हैं बाबा, हिमांशु और समरेश भी। इसीलिए चारु का मन किसी से नहीं मिल पाता न बाबा से, न हिमांशु से न समरेश से। समरेश के प्रति उसके मन में एक विश्वास पनपा था, लेकिन वह भी जरा सी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाया। टूट गया उससे भी मन। चारु अकेले रह गयी। ‘यह सच था कि उन दिनों समरेश ने उसे बदला था। वह कुछ और ही देखने-सुनने और समझने लगी थी, उसे लगा था दोनों एक-दूसरे के भीतर से आलोकित हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ हुई घटना वह उस पर यकीन नहीं कर पाती। वह अंदर तक हिल गयी थी। निराशा के अलावा उसके अंदर कोई भय समा गया था, जिसके तले दु:स्वप्न थे। (पृ-211)
चारुलता के ‘मन में जीवन की पवित्र सी कल्पना है। असंभव सी चाहना। वह चाहना यथार्थ में खंडित होती रहती। (213)
चारुलता के मन की कहानी इसी नियति की ओर पहुंचती है, लेकिन इस पहुंचने की यात्रा में, चारु सबके मन की थाह लगाती है। तीन खंडों तथा विभिन्न शीर्षकों एवं उपशीर्षकों के अंतर्गत लिखे गए इस उपन्यास में सभी प्रमुख पात्रों के ‘आकाश’ की तलाश है, सभी के आकाश की रंगत को पहचाना गया है, सभी के आकाश के रंग की विभिन्न छवियों को शब्द दिए गए हैं। रक्तिम दा जैसे समाज के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता की स्मृति से अपनी चिंताओं के हल्केपन को भी उजागर कर दिया गया है, ‘अक्सर हमें लगता है हम लौट जाएं। हम लहूलुहान होते हैं। थकने लगते हैं। हमारे में और रक्तिम दा में यही अंतर है। हम रात दिन खुद से घिरे रहते हैं। वे खुद के साथ दूसरों की भी चिंता करते हैं।’ नीरू दीदी की बातों से रक्तिम दा का पूरा व्यक्तित्व उभर आता है और व्यक्तिगत सुख-दुख की चिंता करने वालों की सीमाएं भी।
उपन्यास की कहानी बताने का कोई खास अर्थ इसलिए नहीं है कि इसकी संवेदना घटनाओं के क्रम में नहीं है, बल्कि मूर्त-अमूर्त भाव से शब्दों की सतह में छिपी हुई है। यहाँ मन का विश्लेषण नहीं, मन का विरेचन है। भावक के हृदय से शांत भाव से इससे गुजरने पर कई स्थलों पर यह मन में उथल-पुथल मचाएगी और अपने आसपास को देखने का नया आत्मबोध पैदा करेगी। किसी कृति का इससे बेहतर और क्या कार्य हो सकता है।
किताब- उन्नीसवीं बारिश
लेखिका- शर्मिला जालान
प्रकाशक- सेतु प्रकाशन, सी-21, सेक्टर 65, नोएडा
संपर्क नं. 8130745954
मूल्य- 260.00 रूपए मात्र
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.