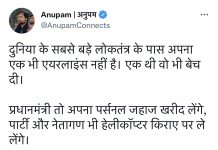— थंबु कानागासाबाइ —
संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संगठन है जिसका काम है अपने सदस्य-राष्ट्रों को साथ लेकर साझा चुनौतियों का सामना करना, साझा जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, स्थायी विश्व शांति के लिए सामूहिक कार्रवाई करना।
संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य मकसद है विश्व शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इस समय 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र के सभी मुख्य संगठनों में सुरक्षा परिषद सबसे बुनियादी संगठन है जिसके पाँच स्थायी सदस्य हैं- अमरीका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इसके अलावा दस सदस्य (देश) बारी-बारी से सुरक्षा परिषद में शामिल होते रहते हैं जिनका चयन क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मद्देनजर किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र (चार्टर) के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करना सदस्य-देशों के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की बाबत ऐसी अनिवार्यता नहीं है जब तक सुरक्षा परिषद पर उन पर अपनी मुहर न लगा दे। अलबत्ता संयुक्त राष्ट्र गौर करने और कदम उठाने के लिए सुरक्षा परिषद को अपनी सिफारिशें और सुझाव दे सकता है।
संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है उम्र, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किये बगैर मानव अधिकारों तथा बुनियादी आजादियों का संरक्षण करना और उनका लिहाज करने के लिए प्रोत्साहित करना, सदस्य-राष्ट्रों इस बात के लिए वचनबद्ध कराना कि इन अधिकारों की रक्षा की खातिर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू करने के लिए वे साझा तौर पर और अलग से भी कार्रवाई करेंगे।
हालांकि व्यवहार में मानव अधिकारों के हनन पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने बूते, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के बिना पर्याप्त कदम नहीं उठा सकती। सुरक्षा परिषद ने 1948 से, जब वह वजूद में आयी, अब तक 2400 से ज्यादा प्रस्ताव पास कर चुकी है। सुरक्षा परिषद को यह अख्तियार है कि वह संयुक्त राष्ट्र के किसी अनुच्छेद का ऐसा उल्लंघन किये जाने पर, जिससे शांति को खतरा हो, जिससे शांति भंग होती हो या जो आक्रमणकारी कार्रवाई हो, वैसा करनेवाले देश के खिलाफ अपने प्रस्तावों के जरिए आर्थिक, राजनीतिक और/या राजनयिक प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद सैन्य कार्रवाई समेत शांति स्थापना की कार्रवाई के लिए अधिकृत कर सकती है, जैसा कि 1991 में इराक के खिलाफ किया गया था, जिसने अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला करके उसपर कब्जा कर लिया था।
अगर किसी देश के नेताओं और/या फौजी अफसरों पर युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, जनसंहार आदि के आरोप हों, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी – इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट) में मुकदमा चलाने के लिए सिफारिश करने का अधिकार है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रस्ताव नं. 1706 (जिसे R2P – राइट टु रिस्पांसिबिलिटी कहा जाता है) के जरिए यह अधिकार है कि वह सशस्त्र टकराव के क्षेत्र में नागरिकों को बचाने और जनसंहार, युद्ध अपराध, नस्ली सफाये और मानवता के विरुद्ध अपराध आदि को रोकने के लिए एहतियाती कार्रवाई कर सकती है।
तो लब्बोलुआब यह कि विश्व शांति बनाये रखना, मानवाधिकारों का हनन रोकना और दोषियों को दंडित करना सिर्फ सुरक्षा परिषद के पंद्रह सदस्यों पर निर्भर करता है, खासकर पाँच स्थायी सदस्यों पर, जिन्हें वीटो (निषेधाधिकार) की शक्ति प्राप्त है, जिसके जरिए वे किसी भी प्रस्ताव को पलीता लगा सकते हैं भले उस प्रस्ताव को बाकी चौदह सदस्यों का समर्थन हासिल हो।
एक स्थायी सदस्य जब किसी प्रस्ताव को वीटो कर देता है, भले उस प्रस्ताव को बाकी सभी चौदह सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो, तो यह और कुछ नहीं बल्कि अन्य सदस्यों का अपमान और अनादर है, जिसे प्रायः अधिकार का दुरुपयोग कहा गया है। वीटो की शक्ति का बेजा इस्तेमाल महाशक्तियाँ यह धमकी देकर करती रहती हैं कि वीटो नहीं होगा तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं होगा।
फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर पाँच महाशक्तियों का कब्जा है जिनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा वीटो के इस्तेमाल का हालिया उदाहरण वह है जब यरुशलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के अपने फैसले पर वह सुरक्षा परिषद में अलग-थलग पड़ गया था। इस मामले में वीटो का इस्तेमाल करके अमरीका ने विश्व जनमत को ठेंगे पर रख दिया। संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा वित्तीय अंशदान अमरीका का है, लगभग 22.1 फीसद। इस कारण भी संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही और कार्यक्रमों पर उसका दबदबा रहता है।
अगर कोई संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के पिछले पचास साल का इतिहास उठाकर देखे तो निराशाजनक और नाकामियों से भरी तस्वीर ही उभरेगी।
कुछ नाकामियाँ नीचे बतायी जा रही हैं जिन्हें शुरू में ही रोका जा सकता था मगर जिन्हें भयावह परिणति तक पहुँचने दिया गया-
# बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान जनसंहार;
# कंबोडिया में पोल पोट शासन के द्वारा जनसंहार;
# 1994 में रवांडा में जनसंहार, जिसमें हजारों तुत्सी लोग हुतुस लोगों के हाथों मारे गये;
# 1995 में स्रेब्रेनिका में जनसंहार, जिसमें सर्बों ने मुसलिमों की हत्याएँ कीं;
# सोमालिया और सूडान में गृहयुद्ध, जिसमें हजारों विद्रोही सरकारी फौजों और आतंकवादियों के द्वारा, शासकों की सरपरस्ती में मारे गये।
श्रीलंका में 2006 से 18 मई 2009 तक जनसंहार जैसा जो युद्ध चला, उस दरम्यान वैश्विक संस्थाओं- संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद- की नाकामी इक्कीसवीं सदी में सबसे शर्मनाक नाकामियों में से एक है।
‘टोरंटो स्टार’ (कनाडा) ने उस नाकामी पर लिखा था-
“2009 में श्रीलंका में गृहयुद्ध के आखिरी महीने में जब 40,000 तमिल मार दिये गये, संयुक्त राष्ट्र ने एक औपचारिक बैठक तक नहीं की, न सुरक्षा परिषद की न महासभा की। और न ही अपने मानवाधिकार परिषद की।
“श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र ने कायरता भरी खामोशी अख्तियार कर ली थी और निगाहें दूसरी तरफ कर लीं, जिससे युद्ध-अपराधियों का हौसला बढ़ गया कि वे अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम दे सकें।
यह सिलसिलेवार नाकामी बहुत भयावह है, जबकि माना यह जा रहा था कि संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में स्रेब्रेनिका में हुए जनसंहार से यह सबक लिया होगा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा।”
‘स्टार’ के स्तंभकार रोजी डिमानो की टिप्पणी थी- “श्रीलंका के मामले में संयुक्त राष्ट्र विशेष रूप से बहरा, गूँगा और अंधा हो गया था।”
संयुक्त राष्ट्र को कहीं बेहतर पता रहा होगा कि श्रीलंका में गृहयुद्ध के अंतिम और चरम खूनी दौर में क्या हो रहा था, पर इसने उस सूचना को दबा दिया या हल्का बना दिया और नागरिकों की रक्षा के अपने मूल उद्देश्य में बुरी तरह विफल रहा।
सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय श्रीलंका के अधिकारियों की धौंसपट्टी में आ गये, जो 9/11 के बाद दुश्मन को हराने के लिए ‘मुँह बंद रखने की प्रभावी विश्व-व्यवस्था’ का लाभ उठा रहे थे। जनसंहार निरोधक परियोजना सूचकांक (जेनोसाइट प्रिवेंशन प्रोजेक्ट इंडेक्स) 2008 ने श्रीलंका को उन आठ देशों में रखा था जहाँ जनसंहार और बड़े पैमाने पर अत्य़ाचार की आशंका थी।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान-की-मून, जो श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान खामोश और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे थे, उन्होंने सितंबर 2016 में श्रीलंका का दौरा किया और अपने दफ्तर की नाकामी पर काफी अफसोस जताया। “1994 में रवांडा में कुछ बहुत भयानक हुआ था, यह जनसंहार था, दस लाख से ज्यादा लोग मारे गये थे। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपनी जवाबदेही कबूल की। हमने बार-बार कहा, ‘फिर ऐसा नहीं होगा’, लेकिन एक ही साल बाद स्रेब्रेनिका में फिर वही हुआ। हमने श्रीलंका में फिर वही किया।”
जले पर नमक छिड़कते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मई 2009 में एक प्रस्ताव में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) का सफाया करके गहयुद्ध का अंत करने के लिए तारीफ की। अलबत्ता मानवाधिकारों पर तमाचा जड़नेवाले और जनसंहार को सही ठहराने वाले इस प्रस्ताव की काफी निंदा हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने तथ्यों और आँकड़ों की बाबत अनजान रहने तथा श्रीलंकाई अधिकारियों की भ्रमित करनेवाली बातों के प्रभाव में आ जाने की बात स्वीकार की।
कुछ कानूनी टिप्पणीकारों ने यहाँ तक संकेत किया है कि संयुक्त राष्ट्र की नाकामी दरअसल मिलीभगत थी जिससे श्रीलंका सरकार को युद्ध के दौरान युद्ध को जारी रखने का प्रोत्साहन मिला।
संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की नाकामी मौजूदा परिस्थितियों में भी, पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में भी जारी है। रोहिंग्याओं की नागरिकता छीन लगी गयी है और लगभग सारे मानवाधिकारों से वंचित ये लोग राज्य-विहीन हो गये हैं।
रोहिंग्याओं की अपनी भाषा है, अपना धर्म, अपनी संस्कृति। वे एक जातीय समुदाय हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का संरक्षण मिलना ही चाहिए और संयुक्त राष्ट्र को म्यांमार के अधिकारियों तथा सुरक्षा बलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी ही चाहिए जिन्होंने रोहिंग्याओं को उनके रखाइन प्रांत से जबर्दस्ती भागने और पड़ोस के गरीब मुल्क बांग्लादेश में शरण लेने पर मजबूर किया है।
यूक्रेन पर रूस का बर्बर आक्रमण और सीमा का उल्लंघन, निरी बहानेबाजी और सुरक्षा संबंधी निराधार खतरे की बिना पर एक छोटे लोकतांत्रिक देश को पंगु बना देना और क्षत-विक्षत कर देना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली महाशक्ति की धौंस को ही दिखाता है।
यह और भी दुखद है कि अन्य लोकतांत्रिक देश और महाशक्तियाँ खामोश हैं, संयुक्त राष्ट्र भी रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही पर मूकदर्शक और लाचार नजर आता है जिसकी स्थापना ही अपने सदस्य-राष्ट्रों के बीच शांति व सुरक्षा कायम रखने के मकसद से की गयी थी।
लिहाजा, यह कहना सही है कि बेगुनाहों की रक्षा करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मुँह बंद रखने और मूकदर्शक की भूमिका में रहना ही बेहतर समझा है ताकि रूस कहीं भड़क कर उनकी सुरक्षा और उनके हितों को नुकसान न पहुँचाए।
(लेखक कोलंबो विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर रह चुके हैं।)
countercurrents.org से साभार
अनुवाद : राजेन्द्र राजन
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.