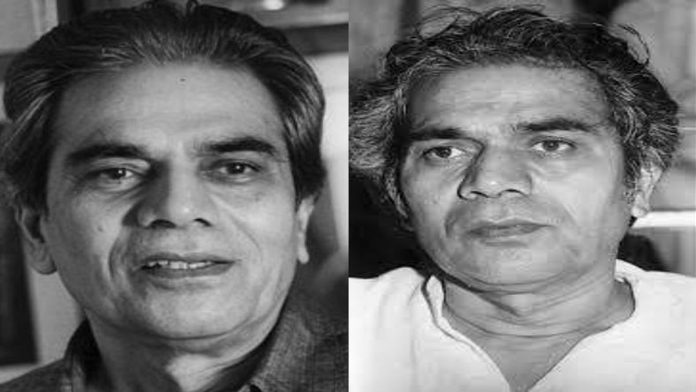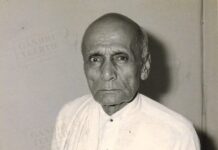— अरुण कुमार त्रिपाठी —
सन 2022 में मधु लिमये पर लिखना और उन्हें याद करना कोई आसान नहीं है क्योंकि इस दौर में न तो मधु लिमये जैसा नेता कहीं दिखाई पड़ रहा है और न ही उन्हें समझने वाले लोग दिख रहे हैं। मधु लिमये सिर्फ एक संघर्षशील समाजवादी योद्धा ही नहीं थे। वे एक चिंतक भी थे। अगर यह पूछा जाए कि वे किस मिट्टी के बने थे तो कहा जा सकता है कि उनमें डॉ राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेन्द्रदेव तीनों के तत्त्व थे। उनमें राममनोहर लोहिया जैसे एक प्रखर विपक्षी सांसद के गुण थे, जयप्रकाश नारायण जैसी त्यागवृत्ति थी तो आचार्य नरेन्द्रदेव जैसी लेखकीय कुशलता थी। वे संगीत प्रेमी भी थे। कुमार गंधर्व के लिए उनमें गजब की दीवानगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन, गोवा आंदोलन और बाद में आपातकाल विरोधी आंदोलन में जेल जाने में उन्होंने जो वीरता दिखाई वह अपने समाजवादी पुरखों से कहीं कम नहीं थी। वे चार बार लोकसभा के सदस्य रहे लेकिन उस राज्य से नहीं चुने गये जहाँ उऩका जन्म हुआ और जिस संस्कृति में वे रचे-बसे थे। उन्होंने बांका और मुंगेर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। संसद में वे 1964 में पहुँचे और डॉ लोहिया 1963 में पहुँचे थे। जबकि किशन पटनायक 1962 में चुनकर आए थे। इन प्रखर समाजवादियों ने मिलकर संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को जिंदा कर दिया।
मधु लिमये पर जनता पार्टी को तोड़ने का आरोप लगता है। उस समय वह आरोप उन पर इस तरह से चस्पाँ हो गया था कि वे खलनायक बन गए थे। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे तमाम संगठनों की गतिविधियों को देखकर लगता है कि वे तो सचमुच नायक थे। संघ की दोहरी सदस्यता के सवाल पर जनता पार्टी तोड़ना और फिर कांग्रेस की वापसी का रास्ता साफ करना यह तो कुछ समय के लिए संघ को सत्ता से बाहर रखने का ही एक प्रयास था। इस तरह मधु लिमये ने डॉ. राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की उन गलतियों को सुधारने का प्रयास ही किया जिसके चलते संघ परिवार को स्वीकार्यता मिली और वह इतना शक्तिशाली हो गया।
अपने निधन (8 जनवरी, 1995) से पहले मधु लिमये ने हिंदुस्तान टाइम्स में जो लेख लिखा था वह कांग्रेस की अहमियत को रेखांकित करनेवाला था। वे देश के सेकुलर ढाँचे के लिए चिंतित थे और उसे बचाने में कांग्रेस का अहम योगदान मान रहे थे। लेकिन 2022 में जब भारतीय राजनीति बुरी तरह फासीवाद की तरफ जा रही है तो मधु लिमये के कुछ ग्रंथों का पुनर्पाठ किया जाना चाहिए। उनमें स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा, बर्थ ऑफ नान कांग्रेसिज्म, सोशलिस्ट-कम्युनिस्ट इंटरैक्शन इन इंडिया जैसी किताबें महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अलावा मधु लिमये की महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, गोवा लिबरेशन मूवमेंट, जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट, रिलीजस बायगोट्री : ए थ्रेट टु अवर स्टेट, भी पढ़ी जानी चाहिए।
मधु लिमये का समाजवाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और दुनिया के मजदूर व किसान आंदोलन के साथ गर्भनाल का रिश्ता रखता था। स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा में उनके विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि वे 1857 से लेकर 1957 तक उभरे भारतीय राष्ट्रवाद को कितनी बारीकी से देखते हैं और उसके आवश्यक सूत्रों को पकड़ते हैं। राष्ट्र शब्द कैसे आया और इसे लोगों ने अपने-अपने इलाकों में किस प्रकार व्याख्यायित किया इसको भी मधु लिमये ने स्पष्ट किया है। महाराष्ट्र के लिए उसका अर्थ कुछ और था, बंगाल के लिए कुछ और था और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और था। जिन्ना के लिए अलग था, नेहरू के लिए अलग था, गांधी के लिए अलग था। लेकिन भारत की साझी विरासत का जो रूप 1857 में दिखा, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने उसे ही आगे बढ़ाने का काम किया। यह बात अलग है कि 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भी वह विरासत खंडित हो गयी।
मधु लिमये का दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ गैर-कांग्रेसवाद पर है। जॉर्ज फर्नांडीज और मधु लिमये ने किस प्रकार जनसंघ को गैर-कांग्रेसवाद का हिस्सा बनाने का विरोध किया था और डॉ. लोहिया उसपर अड़े रहे इसकी कहानी रोचक और इतिहास-सचेत दृष्टि को रेखांकित करनेवाली है। मधु लिमये यह भी स्पष्ट करते हैं कि जयप्रकाश नारायण संसदीय राजनीति से वैराग्य लेने के बाद जब फिर उसमें संपूर्ण क्रांति में लौटते हैं तो वे सबको मिलाकर चलने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पवित्र घोषित करने और दलविहीन लोकतंत्र का जो विचार प्रस्तुत करते हैं वह कितना अव्यावहारिक है, इस बात को लोहिया और जयप्रकाश वाले लेख में बहुत खुलकर व्यक्त करते हैं। जयप्रकाश और लोहिया की भिन्नताओं को रेखांकित करते हुए मधु लिमये यह भी दिखाते हैं कि उनके भीतर पारस्परिक सम्मान और एकता की भी संभावनाएँ रही हैं।
जब जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं तो मधु लिमये उनसे कहते हैं कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। तब वे कहते हैं यह तो तुम लोगों का काम है। इस पर जब मधु लिमये कहते हैं कि आपकी संपूर्ण क्रांति तो वास्तव में डॉ लोहिया की सप्तक्रांति ही है तो इसे जयप्रकाश नारायण स्वीकार करते हैं। समाजवादी आंदोलन के बारे में मधु जी की यह टिप्पणी बेहद सटीक है। उन्होंने कहा था कि गांधी ने देश को चलाने के लिए नेहरू और पटेल जैसी दो बैलों की जोड़ी पकड़ ली थी और उनके कंधों पर देश की गाड़ी रख दी थी। आज समाजवादी आंदोलन के लिए भी किसी वैसे गांधी की जरूरत थी जो जयप्रकाश और लोहिया के कंधों पर आंदोलन का जुआ रख दे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी आंदोलन को वैसा गांधी मिला नहीं।
गांधीजी को समझने के लिए मधु लिमये की टिप्पणी भी बहुत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जीवन के प्रारंभ में किस प्रकार समाजवादी, सुभाष बाबू की ओर आकर्षित थे और गांधी से थोड़े खिंचे रहते थे लेकिन बाद में गांधी के आदर्श और व्यवहार दोनों ने समाजवादियों को मुरीद कर लिया। मधु लिमये ने गांधी को बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार तब देखा था जब वे भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर रहे थे। रात के समय पहले हिंदी और बाद में अंग्रेजी में दिए गए गांधी के उस भाषण ने उनके मानस पर गहरा प्रभाव डाला और वे भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े।
30 जनवरी, 1948 को जब एक धर्मान्ध व्यक्ति ने तीन गोलियाँ दाग कर तीन गोलियाँ दाग कर गांधीजी की हत्या की तब मधु लिमये रोम में थे। वे अंतरराष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लेने नवंबर में ही बेल्जियम चले गये थे फिर भ्रमण के लिए रोम पहुँचे। वहाँ का अखबार देखकर वे समझ नहीं पाये कि गांधी को क्या हुआ है। क्योंकि वहाँ की भाषा वे जानते नहीं थे। उन्होंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी जाननेवाले वेटर से खबर पढ़वाई और तब उन्हें यकीन हुआ कि कल शाम ही गांधी की हत्या कर दी गयी। तब उन्हें लगा जैसे गांधी सचमुच उनसे कुछ कह रहे हैं। इस स्वगत को उन्होंने कुछ इस तरह व्यक्त किया :
गांधी कह रहे हैं कि मेरे नौजवान दोस्तो, अगर तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो तो मुझे बुतों में कैद मत करना। उन सिद्धांतों के अनुसार काम करना मुझे प्रिय रहे हैं। हे राम, ओ दिव्य सुगंध की साँस। यद्यपि पीड़ा मुझे जलाए दे रही है, मैं तुम्हारी आनंदमयी उपस्थिति महसूस कर रहा हूँ।
मधु लिमये जैसे प्रतिबद्ध और आंदोलन से लेकर संसदीय राजनीति में सक्रिय रहनेवाले और बेहद विचारशील समाजवादी आज नहीं हैं। उनके सभी गुणों का समन्वय दुर्लभ है। वे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सुरों के साधक थे।
हालांकि वे दमे के मरीज थे और इन्हीं मूल्यों को साधते हुए उनका दम निकला। वे सुर आज दुनिया में दबते जा रहे हैं लेकिन मानवता का संगीत उन सुरों के बिना निकलेगा नहीं। अगर किसी ने निकालने का प्रयास भी किया तो या तो वह अमानवीय या बेहद बेढंगा और बेसुरा हो जाएगा। मधु जी सचमुच विभिन्न गुणों का माधुर्य लिये हुए थे। उनके सभी गुणों को साधना बहुत कठिन है। लेकिन उनके एक-एक गुण को लेकर तो विभिन्न लोग काम कर ही सकते हैं। उनके जन्म शताब्दी वर्ष और आजादी के अमृत महोत्सव में यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.