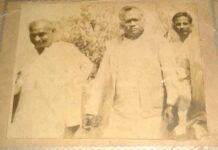सन 1857 के विद्रोह को अत्यधिक सख्ती और खूबी के साथ दबाने में सर जॉन लारेंस (अंग्रेज अफसर) अग्रणी था। इस विद्रोह के बारे में उसने ‘ट्रिवेल्यन’ के नाम से विद्रोह काल के दौरान कई पत्र लिखे। इन पत्रों के पठन से अंग्रेजों की मनःस्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। लारेंस कहता है : “एक अर्से से सेना की स्थिति असंतोषजनक थी। सेना ने एक लंबे समय से अपनी ताकत को देखा था, पहचाना था। लगातार हम हिंदुस्तानी सेना का विस्तार करते जा रहे थे, मगर यूरोपियन पलटनों की संख्या हमने उसके साथ-साथ नहीं बढ़ाई….अधिकतर सिपाही पूरबिये थे। बंगाल आर्मी एक महान किस्म का भ्रातृसंघ बन गयी थी जहाँ सभी सदस्य सहचिंतन और समान आचार-व्यवहार के लिए तत्पर थे….इसलिए हमें यूरोपियन पलटनों की तादाद बढ़ाकर कम-से-कम दुगुनी कर देना चाहिए। हिंदुस्तानी सैनिकों की संख्या जितनी निहायत आवश्यक हो उतने तक ही महदूद रखी जाए।” (सर जॉन लारेंस की जीवनी :द्वितीय खण्ड, पृ. 289-90)
दूसरे पत्र में जॉन लारेंस ने विद्रोह के दौरान उत्तर भारत और मध्य भारत की हालत का वर्णन किया है। अंग्रेजी हुकूमत के अस्तित्व के लिए जो खतरा उत्पन्न हो गया था उसका उल्लेख करते हुए लारेंस ने लिखा- “आज 60 हजार सिपाही हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन यूरोपियन सैनिकों की संख्या तेजी से नहीं बढ़ाने से नए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर साल ब्रिटेन से 20 हजार गोरे सैनिक भारत भेजे जाएं अन्यथा हम लोग हुकूमत को नहीं बचा पाएंगे। इस समय दिल्ली से पेशावर तक सिर्फ दस हजार गोरे सिपाही मौजूद हैं। साथ ही उनके 18 हजार हिंदुस्तानी सैनिकों पर (यानी गैर-पंजाबी सैनिकों पर) नजर भी रखनी है। अगर पंजाबी और गोरी पलटनों में अनबन हो जाए तो गोरे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना मुश्किल हो जाएगा। मुझे इस बात का डर है कि कहीं पंजाबी सैनिक हमारी यह कमजोरी भांप न जाएं और अपने लिए सुअवसर पैदा हुआ है, ऐसा न मानने लग जाएं। अगर कहीं ऐसा हो गया तो हमारा क्या हश्र होगा।” (उपरोक्त पृ.296)
इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि पंजाबियों पर भी सर जॉन लारेंस को विश्वास नहीं था। ये पंजाबी सैनिक भी उलट सकते हैं, ऐसा उसे हमेशा डर रहता था। इन सिपाहियों का आपसी भाईचारा उसे भयभीत किये रहता था।
भारतीय सेना के ढाँचे के बारे में जॉन लारेंस लिखता है : “इंग्लैण्ड में कुछ लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा हिंदुस्तान में जातीयता की मान्यता दी गयी है, प्रतिष्ठा प्रदान की जा रही है और उसके दुष्परिणामों को भुलाया जा रहा है। लेकिन सत्य यह है कि बंगाल आर्मी के अलावा और जगह इस तरह की स्थिति नहीं है। यह बात सत्य है कि बंगाल आर्मी में अवध और बिहार के ब्राह्मणों और राजपूतों की बड़े पैमाने पर भरती होती रही है। लेकिन उसके कई कारण रहे हैं। सैनिकी परंपरा और शारीरिक दृष्टि से उनको सबसे अधिक उपयुक्त समझा गया था। नैतिक दृष्टि से भी उनको योग्य पाया गया था। सबसे बड़ा कारण यह था कि परंपरा से उनके पुरखे भी हमारी सेना में काम कर रहे थे। इसीलिए इन भूभागों से सिपाहियों की अत्यधिक भर्ती हुई थी। हमारे अफसरों के मन पर भी उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी थी कि समाज के दूसरे वर्गों के लोगों को भर्ती करने के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। चूंकि ये लोग एक ही प्रदेश से आते थे, एक ही बोली बोलते थे, अतः उनके आपस में गहरे रिश्ते थे। चूंकि उनमें खून का रिश्ता और सामंजस्य था इसलिए ये सैनिक भाइयों की तरह सोचते थे, काम करते थे। पूरी बंगाल आर्मी एक भ्रातृसंघ जैसी थी। इन गलतियों को आगे चलकर हमें सुधारना होगा।”(उपरोक्त, पृ. 317-318)
हिंदुस्तानी सेनाओं के एक सचित्र इतिहास के लेखक मैकमून ने भी कहा है :“1857 में बंगाल आर्मी की संख्या 1 लाख 37 हजार थी जिसमें से 20 हजार घुड़-सेना थी। इनमें से बहुत ज्यादा पूरबिये थे, यानी पूर्वी भारत के लोग, जैसे अवध के राजपूत, ब्राह्मण आदि। बंगाल आर्मी में मुसलमानों की संख्या भी नगण्य रही थी। सिक्ख राज्य समाप्त होने के बाद सिक्खों का भी उसमें शुमार हो गया था। ये विभिन्न वर्गों के लोग आपस में घुलमिल गए थे। पलटनों का निर्माण वंश, जाति और धर्म आदि के आधार पर नहीं था।”(मैकमून : द आर्मीज ऑफ इण्डिया, पृ.84)
सर जॉन लारेंस को दिए जाने वाले सम्मान और पदवियों के बारे में सर फ्रेडरिक करी ने उनको एक पत्र लिखा था। उसके जवाब में अपनी चिंता से लारेंस नें उसे अवगत कराया : “भगवान की कृपा से पंजाब की जनता न केवल शांत और संतोषी थी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादार भी। अगर पंजाब में भी विद्रोह फैल जाता तो हमारा क्या हश्र होता? सारे अंग्रेज मौत के घाट उतर जाते और इंग्लैण्ड पूर्व में अपनी सत्ता को बचा नहीं पाता। इस समय पंजाबी सैनिकों की संख्या 80 हजार तक पहुंच गयी है। एक भी दुर्व्यवहार का उदाहरण उनमें नहीं पाया गया है। उन्होंने पूरी तरह अंग्रेजों का साथ दिया है। अंग्रेजों को इस बात को कृतज्ञयतापूर्ण स्मरण करना चाहिए।”(सर जॉन लारेंस की जीवनी, पृ.335)
कृतज्ञता के साथ अविश्वास भी कम मात्रा में नहीं था। इसी अविश्वास के कारण सिक्खों को भी वे तोपखाने से अलग रखना चाहते थे। धार्मिक भेद-भावों, भाषिक भेद-भावों को उकसा कर ही अंग्रेजी हुकूमत स्थायी बनी रह सकती थी। कुछ समय बाद जॉन लारेंस ने ही लार्ड कैनिंग से कहा : “पंजाबी सैनिकों का व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी संख्या अत्यधिक है। सारे बुद्धिमान हिंदुस्तानी इस बात को समझते हैं। इस विद्रोह के बाद पंजाबी भी इस पर सोचने लगेंगे। तोपखाने में उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन उसे और भी घटा देना चाहिए… हमारे लिए यह तसल्ली की बात है कि पंजाबी सैनिकों में कई वंश, जाति और मजहब के लोग हैं। सिक्खों के पुराने वर्चस्व को याद करके पठान उनसे कटते हैं। जहां तक सिक्खों का सवाल है, वे मुसलमानों के द्वेष रखते हैं। इन दरारों के बावजूद हमें इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भविष्य में कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो सकती हैं कि ये सब एकजुट हो जाएं।” (उपरोक्त, पृ.350)
1857 का विद्रोह शुरू होते ही अंग्रेजों ने सबसे पहला अगर कोई काम किया तो वह था हथियारों के संबंध में कानून जारी करना। आर्म्स एक्ट जारी करना। इस कानून के तहत सभी नागरिकों को आदेश दिया गया कि वे अपने सभी हथियार सरकारी रजिस्टर में दर्ज कारायें। हथियारों को दर्ज नहीं कराना या उनको छिपाकर रखना जुर्म माना गया और उसके लिए दण्ड तथा जेल दोनों किस्म की सजाएँ रखी गयीं। यह सजा छह महीने तक की दी जा सकती थी। साथ-ही-साथ पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेटों को हथियारों की तलाशी लेने का भी अधिकार दिया गया।
एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है कि जब हथियारों को जमा कराने का यह आदेश जारी किया गया तो एक बहुत ही हृदयविदारक दृश्य उपस्थित हो गया। पुराने बुजुर्ग मराठा पटेल अपने हथियार लेकर आने लगे जो न जाने कितनी पीढ़ियों से उनके पास जमा थे। ये सुंदर बनावट के मेच लाक्स थे, उत्कृष्ट किस्म की तलवारें थीं जिनके ऊपर बढ़िया किस्म की नक्काशी का काम किया गया था, या इन तलवारों को रखने के लिए बनाए गए खूबसूरत म्यान थे। इन म्यानों पर भी रत्न और सोना लगा हुआ था। तलवारें भी उत्कृष्ट किस्म के फौलाद की बनी हुई थीं। उनकी मूठों पर सोने और चांदी का नक्काशी का काम किया हुआ था और कुछ मूठें तो रत्नजड़ित भी थीं। अजीब किस्म के खंजर थे। उसी तरह के भाले और गदाएँ आदि सारे आयुधों को ले-ले कर वे आगे आते थे।
इन हथियारों के पीछे कितना गौरवशाली इतिहास था। इनके मालिकों ने अपने पुरखों की अमानत के रूप में उनकी रक्षा की थी। यह बात सही है कि इस कानून का “मानवीयतापूर्ण” पालन किया गया था लेकिन उत्तरी भारत में विद्रोह फैलने की खबरें जब आने लगीं तो हम लोगों (अंग्रेजों) के बीच में भी “कहीं यहाँ भी बगावत शुरू हो जाए”, जैसी चर्चा शुरू हो गयी थी। जो अच्छे किस्म के हथियार थे, उनकों लोहारों द्वारा अधिकारियों के समक्ष तुड़वा दिया गया और उनके टुकड़े होते देखकर रोने लगे। जो नौजवान थे, उनकी आँखों में मैंने विद्वेष की नयी छटा देखी। निःसंदेह वे अपने मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति द्वेष के नए अंकुर समाए वापस चले गए। लेकिन इसका किसी के पास क्या इलाज था? वे लोग इसे अपना दुर्भाग्य या किस्मत कहकर दुखी होते हुए वापस लौट जाते थे।
इसी कानून (आर्म्स ऐक्ट) की तमाम राष्ट्रीय नेताओं और गांधीजी ने आगे चलकर बड़े कड़े शब्दों में आलोचना की थी और कहा था कि हिंदुस्तान को दुर्बल तथा कमजोर बनानेवाला यह कानून अंग्रेज सरकार को वापिस लेना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों में लगातार इस आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पास होते थे।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.