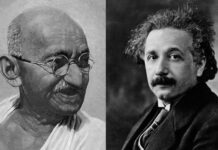पाकिस्तान के निर्माण के बाद वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त हो गयी। प्रारंभ में पाकिस्तान के प्रशासन में हिंदुस्तान से जो लोग गए थे, जैसे मुस्लिम लीगी नेता, बड़े-बड़े व्यापारी और पूंजीपति, उन्हीं का वहां दबदबा हो गया। लेकिन जिन्ना साहब और लियाकत अली की मृत्यु के बाद पाकिस्तान के नेतृत्व में एक परिवर्तन आने लगा। शुरू से ही पाकिस्तान की थल सेना का आधिक्य होने के कारण उसका प्रभाव प्रशासन में धीरे-धीरे बढ़ने लगा। पाकिस्तान में चूंकि संसदीय संस्थाओं की कोई गहरी परंपरा नहीं थी और कोई कांग्रेस जैसा शक्तिशाली दल नहीं था इसलिए कुछ वर्षों के अंदर सत्ताधारी मुस्लिम लीग का विघटन हो गया और उसके साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की भी अवनति। अंत में सारी सत्ता सेना के हाथ में चली गयी।
जब पाकिस्तान में सैनिकी प्रशासन हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में जबरन एकता लाने के प्रयास शुरू किए। जब पाकिस्तान की स्थापना हुई थी तो समूचे आई.सी.एस. अधिकारी वर्ग में सिर्फ एक बंगाली मुसलमान था। तीनों सेनाओं के 2117 अधिकारियों में सिर्फ 81 पूर्वी पाकिस्तान के थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की आबादी पश्चिमी पाकिस्तान की कुल आबादी से अधिक थी। पाकिस्तान का प्रशासन जब पूरी तरह सेना के हाथों में चला गया तो पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता महसूस करने लगी कि पाकिस्तान के भविष्य के निर्माण में उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस तरह जब वे अपने ‘स्वराज्य’ के अधिकारों से वंचित होने लगे तो पाकिस्तान के प्रति उनकी आस्था भी कम होने लगी। पाकिस्तान के प्रशासक भूल गए कि पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान से आए हुए शरणार्थियों की ही मादरी भाषा उर्दू थी बाकी न पश्चिम के किसी आदमी की मादरी जुबान उर्दू थी, और न पूर्वी पाकिस्तान में रहनेवाले बंगालियों की।
जैसे-जैसे इस्लाम के नाम पर सेना के अधिकारी और पंजाब के नौकरशाह पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर अपने निर्णय थोपने लगे, वैसे-वैसे पश्चिमी पाकिस्तान के उर्दू अभिमुख भौगोलिक राष्ट्रवाद के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान का भौगोलिक भाषिक राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरने लगा। अर्थात् एक ओर इस्लाम का नारा, पाकिस्तानी भौगोलिक निष्ठा और उर्दू तथा दूसरी ओर बंगाली भाषा और पूर्वी बंगाल की प्रादेशिक भावना के बीच जबरदस्त संघर्ष पैदा हो गया। शेख मुजीबुर्रहमान की छह माँगें इसी बात की परिचायक थीं कि अब पूर्वी पाकिस्तान की जनता पश्चिमी पाकिस्तान के अधिराज्य में रहने के लिए तैयार नहीं है। यदि पाकिस्तान की हुकूमत में चुनावी बहुमत के आधार पर बंगालियों को नेतृत्व सौंपा जाता तो शायद पाकिस्तान का विघटन कुछ समय के लिए रुक जाता। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बंगलाभाषी लोगों का नेतृत्व कदापि नहीं स्वीकारते। छह सूत्री माँग के ठुकराए जाने पर जिस तरह बंगाल के लोगों ने याहयाशाही के खिलाफ विद्रोह किया, उसी तरह यदि शेख मुजीबुर्रहमान प्रधानमंत्री बनते तो शायद पश्चिमी पाकिस्तान की जनता और सेना भी विद्रोह करके पश्चिमी पाकिस्तान की आजादी की घोषणा कर देती। जो भी हो, इन दो इलाकों का ‘एक राष्ट्र और एक राज्य’ के अंदर निर्वाह होना दिन-प्रति-दिन मुश्किल हो गया। नतीजा यह हुआ कि जहां एक-राष्ट्रीयत्व को द्विराष्ट्र के सिद्धांत ने काटा वहां इस्लामी राष्ट्रवाद को काटने के लिए बंगाली राष्ट्रवाद का पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं का नारा पर्याप्त साबित हुआ। पहले ‘एक राष्ट्रीयता’ की जगह ‘दो राष्ट्रीयताओं’ का निर्माण हुआ, बाद में ‘दो राष्ट्रों’की जगह ‘तीसरे राष्ट्र’ का सृजन हो गया। इस तरह वहां न केवल राष्ट्रीयता ही हास्यास्पद बन गयी बल्कि और कितने राष्ट्र तथा उनके प्रभुसत्तासंपन्न राज्य बनते हैं, यह देखना है।
वास्तव में अब समय आ गया है कि पाकिस्तान, बंगलादेश, और भारत के लोग अपनी पुरानी गलतियों पर पुनर्विचार करें। इसका यह मतलब नहीं है कि द्विराष्ट्रीयता की निरर्थकता को देखते हुए अब बंगलादेश और पाकिस्तान के लोग एक-राष्ट्रीयत्व के सिद्धांत को दिल से स्वीकारेंगे और एक-राष्ट्रीयत्व के आधार पर एक संयुक्त राज्य कायम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नजदीक भविष्य में ऐसा होना मेरी राय में नामुमकिन है। यह जरूरी नहीं है कि एक-राष्ट्रीयत्व का यानी पुराने हिंदुस्तान की भौगोलिक एकता को कबूल करने का अवश्यंभावी परिपाक ‘एक राज्य’ का निर्माण है।
आज जर्मन राष्ट्र तीन हिस्सों में बँटा हुआ है। आस्ट्रिया (आस्ट्रिया भी जर्मन राष्ट्र का ही एक अंग है), पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। निकट भविष्य में इन तीन जर्मनियों का एकीकरण प्रायः असंभव सा है। जहां तक आस्ट्रिया का सवाल है, 1955 की आस्ट्रियन संधि में यह एक प्रावधान है कि आस्ट्रिया आइंदा से जर्मनी के साथ, चाहे राजनीतिक रूप में या आर्थिक रूप में, एकता साधने का कभी प्रयास नहीं करेगा। निःसंदेह आस्ट्रिया द्वारा इस संधि की यह शर्त तोड़ी जाएगी तो रूस आस्ट्रिया के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाएगा।
अगर जर्मन राष्ट्र में तीन स्वतंत्र, सार्वभौम और प्रभुसत्तासंपन्न राज्य रह सकते हैं और आपस में मित्रता के संबंध और रिश्ते कायम करने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं तो क्या पुराने संयुक्त हिंदुस्तान के अंदर से ये जो तीन स्वतंत्र सार्वभौम राज्य बन गए हैं, क्या ये तीनों अपनी सार्वभौमिकता को न छोड़ते हुए, अपनी भौगोलिक समानता, और समान इतिहास, समान व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को दृष्टिगत रखकर आपस में भाईचारे और मित्रता के रिश्ते स्थापित नहीं कर सकते?
पाकिस्तान के लोग चाहे जितने भी इस्लामी क्यों न बनें, किसी भी हालत में वे इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि वे ईरानी नहीं हैं। न ही वे चाहने पर भी अरब बन सकते हैं। आज भौगोलिक राष्ट्रीयत्व की कल्पना वैश्विक इस्लाम के ऊपर हावी होने लगी है, पैन इस्लामिज्म कोरा दिवास्वप्न साबित हो रहा है।
जब सर मोहम्मद इकबाल से पूछा गया था कि पहले आप एक-राष्ट्रवादी थे, बाद में आप एक-राष्ट्रीयता के विरुद्ध हो गए तो इसका क्या कारण है? इसके जवाब में इकबाल ने कहा था कि “राष्ट्रीयता की कल्पना बुनियादी तौर पर इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम और राष्ट्रीयता एकसाथ नहीं चल सकते।” तब उनसे सवाल किया गया कि क्या इसका यह मतलब है कि पैन इस्लामी संघ के वे समर्थक हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ‘मैं पैन इस्लामी राज्य का समर्थक नहीं हूँ। पैन इस्लामवाद एक कल्पना-विलास मात्र है और उसको कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।’ (रिकंस्ट्रक्शन आफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम : मोहम्मद इकबाल)
इकबाल साहब का कहना है कि “अब दुबारा एक इस्लामी राज्य और खिलाफत स्थापित होना संभव नहीं है। यह व्यावहारिक भी नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि अलग-अलग मुस्लिम राष्ट्र होंगे, वे सार्वभौम भी रहेंगे, लेकिन साथ-ही-साथ कामनवेल्थ बनाकर एक-दूसरे के नजदीक आने का प्रयास करेंगे।”
मेरी राय में सर मोहम्मद इकबाल का मुस्लिम अंतरराष्ट्रीय कामनवेल्थ का सुझाव उनकी बुद्धि की कपोल-कल्पना मात्र है। आज वास्तविकता क्या है?वास्तविकता यह है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय संघ के पक्ष में कोई भावना आज मुस्लिम जगत में नहीं है। ईरान और इराक के बीच घमासान लड़ाई चल रही है और जहां तक अरब देशों का सवाल है, फिलीस्तीन के सवाल पर भी वे एक-दूसरे से मिलकर कोई प्रभावशाली कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। अक्सर वे अरब राष्ट्र की एकता के आदर्श की बात करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी भौगोलिक सार्वभौमिकता और अपने अलग अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
इस परिप्रेक्ष्य में लेकिन जिन्ना साहब के विचार ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। अपने एक भाषण में पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हुए (पाकिस्तान की स्थापना से पहले) जिन्ना साहब ने कहा था : “मुस्लिम जगत विभिन्न और स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गया है। इसमें से कोई भी राष्ट्र या राज्य अपने ऊपर दूसरे का स्वामित्व कबूल नहीं करेगा, चाहे यह अरब राष्ट्र की एकता के नाम पर हो अथवा इस्लाम के नाम पर।” ऐसी स्थिति में सर मोहम्मद इकबाल की कामनवेल्थ, पैन इस्लामावाद का विश्वव्यापी राज्य जैसी कल्पनाएं धरातल पर उतरती प्रतीत नहीं होतीं। वह एक निर्गुण, निराकार स्वप्न के रूप में ही रहेंगी, बल्कि इसको कार्यान्वित कर सगुण रूप देना असंभव है।
पीछे हमने जिन्ना साहब द्वारा प्रस्तुत मांगों के बारे में पढ़ा। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व ने इन सूत्रों को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस ने जिन्ना साहब के इन सभी सूत्रों को कबूल कर लिया था। जहां तक स्वतंत्र मतदाता सूची और स्वतंत्र चुनाव क्षेत्रों का सवाल था, यह सहूलियत पहले ही मुसलमानों द्वारा हासिल की जा चुकी थी। जहां तक सिंध को अलग प्रांत के रूप में स्वीकारने की बात थी, उसमें भी आपत्तिजनक कुछ नहीं था। आसानी से कांग्रेस पार्टी इसको कबूल कर सकती थी। अंग्रेजों ने 1935 के संवैधानिक कानून में इसको स्वीकार भी किया था। रही शेष अधिकारों की बात कि वे प्रांतों को सौंपे जाएं, उसके बारे में भी आगे चलकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया। 8 अगस्त 1942 को पास किए गए अपने प्रस्ताव में कि शेष अधिकार प्रांतों के हाथों में रहेंगे की बात को उन्होंने कबूल कर लिया था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सन् 1928-29 में कांग्रेस पार्टी ने जब इन मांगों को स्वीकार नहीं किया था तो उसके पीछे एम.आर.जयकर और मुंजे जैसे कुछ कट्टरपंथी हिंदू नेताओं का विरोध था।
बाद में घटी घटनाओं की रोशनी में जब इन सूत्रों पर हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि यदि उस समय आरंभ में ही कांग्रेस पार्टी ने इन चौदह सूत्रों को मंजूर कर लिया होता तो शायद हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द और समझौता कायम करने में हमें सफलता मिल जाती। लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में निश्चित रूप से भी कुछ कहना संभव नहीं है। कारण इसका कि दूसरा पक्ष भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। क्योंकि जब भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का नेतृत्व एक-दूसरे के नजदीक आने लगता था तो इतने में ब्रिटिश सरकार अपनी टाँग अड़ा देती थी। कांग्रेस मुसलमानों की जिन माँगों को मंजूर करने के लिए तैयार हो जाती थी, उससे कुछ अधिक ही ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को दे देती थी जिससे समझौते की बात टूट जाती थी।