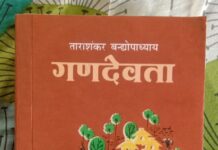— संजय गौतम —
प्रख्यात लेखक, अनुवादक, संपादक अमृतराय की जन्मशती के अवसर पर लमही का विशेषांक प्रकाशित हुआ था, जिससे अमृतराय को समझने में साहित्य की नई पीढ़ी को मदद मिली थी। ‘लमही’ ने इसी परिप्रेक्ष्य में ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चा’ पर केंद्रित विशेषांक प्रकाशित किया है। इस अंक से साहित्य में संयुक्त मोर्चा को लेकर 1950-51 में ‘हंस’ में चली बहस के बारे में तो पता चलता ही है, उस समय के साहित्यिक विवादों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। राहुल सांकृत्यायन के साथ ही अन्य साहित्यकारों पर डॉ. रामविलास शर्मा का प्रहार और फिर अमृतराय का जवाब सामने आता है।
इस पूरे प्रकरण पर अमृतराय ने 1951 में ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चा’ नामक लगभग दो सौ पृष्ठ की पुस्तक लिखी। यह एक ऐतिहासिक विमर्श की किताब है। तब से साहित्यकारों का संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत समय-समय पर महसूस की जाती रही है, बातचीत चलती रही है, लेकिन आज तक मोर्चा क्या ठीक से कोई साझा कार्यक्रम तक नहीं बन पाया और न ही उस पर लेखकों का समूह चल पाया।
ताजा संदर्भ 11 दिसंबर 2021 को प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच की ओर से इलाहाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम का है, जिसमें ‘समकालीन जनमत’ के प्रधान संपादक रामजी राय ने ‘साहित्य संस्कृति में आज के संयुक्त मोर्चे’ के विषय में दस प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को ‘लमही’ के संपादक विजय राय ने अपने संपादकीय में ज्यों का त्यों उद्धृत किया है। प्रस्ताव में ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ की आज की चुनौतियों के साथ ही पूंजीवाद, नवउदारवाद इत्यादि का जिक्र किया गया है; पारिस्थितियों, पर्यावरण, लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं का जिक्र किया गया है और इन सभी की खातिर कार्य करने के लिए संयुक्त मोर्चे की जरूरत को बताया गया है। संपादकीय में इसकी जरूरत को बताते हुए विजय राय लिखते हैं- “चौथे पांचवें दशक में जिस तरह साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकजुटता की दरकार थी, ठीक उसी तरह आज सांप्रदायिकता और कथित राष्ट्रवाद के खिलाफ जनपक्षधर रचनाकारों और लेखक संगठनों की ओर से संयुक्त मोर्चा की निहायत जरूरत है।” (पृ.5)
इस अंक में अमृतराय की किताब ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चा’ के परिप्रेक्ष्य में आज संयुक्त मोर्चा की जरूरत, उसकी बाधाओं-उलझनों के बारे में राजाराम भादू, डॉ. मृत्युंजय सिंह, हीरालाल नागर, उषा वेरागकर आठले, आशुतोष कुमार, शशिभूषण मिश्र, कुमार वीरेंद्र, वंदना चौबे, डॉ. सिद्धार्थशंकर राय, ब्रजेश, अरुणाभ सौरभ, अंकिता तिवारी, कुमार मंगलम, नीरज कुमार मिश्र, नरेंद्र अनिकेत, जनार्दन, शीतांशु, आनंद पांडेय जैसे साहित्य-संस्कृति की समस्याओं से गहरे जुड़े लेखकों ने अपने विचार रखे हैं। विशेष लेख में दूधनाथ सिंह का आलेख ‘संयुक्त मोर्चा का अपराजेय योद्धा,’ राजेद्र कुमार का आलेख ‘प्रगतिशील विचार सरणियां और अमृतराय का अपना विवेक’, शंभुनाथ का आलेख ‘शिविरों के परे भी सच है’ दिया गया है।

संपादकीय में वीर भारत तलवार का पत्र दिया गया है। वह उस दौर को याद करते हुए लिखते हैं, ‘अपनी जमीनी और गहरी प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने ऐसी दृष्टि अर्जित की थी कि वैचारिक अतियों और राजनीतिक संकीर्णता की सीमाओं से बाहर निकलकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध अधिक से अधिक लेखकों को एकजुट करना चाहिए।’
दूधनाथ सिंह ने अपने लेख में लिखा है, ‘लेकिन मैंने जब सन् 91 के आसपास यह किताब (विचारधारा और साहित्य) पढ़ी तो मेरे मन में बहुत सारी दूसरी बातें उठ रही थीं। अमृतराय के दिमाग में अभी भी ‘वामपंथी संकीर्णतावाद’ का प्रेतनृत्य चल रहा था। दरअसल मुझे लगता है, उन्हें कभी इससे मुक्ति नहीं मिली। जबकि इस बीच स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी में तीन फाड़ हो चुके थे। (पृ.104) दूधनाथ जी आगे लिखते हैं- ‘संयुक्त मोर्चा की वकालत ही शिविरबद्धता के खिलाफ एक सीधा मोर्चा था।’
दरअसल अमृतराय साहित्य में संकीर्णतावाद के खिलाफ थे, इस मामले में डॉ. रामविलास शर्मा से उनके गहरे मतभेद थे, जिन्हें प्रकट करने के लिए ही उन्होंने ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चा’ का प्रकाशन किया। वह लिखते हैं–‘साहित्य की सामाजिक सोद्देश्यता और साहित्यकार की पक्षधरता को संकीर्ण ढंग से परिभाषित करना साहित्य के लिए और प्रगतिशील जनवादी साहित्य आंदोलन के लिए अनिष्टकारी ही नहीं है, मार्क्स एंगेल्स के प्रति भी अन्याय है।’ यही नहीं वह किसी भी प्रकार की शिविरबद्धता के खिलाफ थे। या कहें, शिविरबद्धता उनकी प्रकृति में नहीं थीं, ‘सामुदायिक चिंतन प्रकृत्या शिविरबद्धता मांगता है और मेरा मन जैसा कुछ बना था, वैसी शिविरबद्धता मेरे लिए कभी संभव नहीं हो पायी।’ वह विवेक को ही अपना सबसे बड़ा सहचर मानते थे। इस परिप्रेक्ष्य में राजेंद्र कुमार के आलेख में विस्तार से विचार किया गया है।
सवाल उठता है कि क्या आज साहित्य का संयुक्त मोर्चा बन सकता है। रामजी राय के प्रस्ताव को कितनी गंभीरता से लिया गया या साहित्यिक संगठन आगे उस प्रस्ताव पर कितना चल सके। इसका विस्तार से लेखा-जोखा मिल जाता है कुमार वीरेंद्र के आलेख में। उन्होंने उस पृष्ठभूमि की भी विस्तार से चर्चा की है, जिसमें ‘साहित्य का संयुक्त मोर्चा’ किताब लिखी गई और आज के परिवेश की भी। उन्होंने बताया है कि तीनों लेखक संगठन यानी जसम, जलेस और प्रलेस द्वारा साझा कार्यक्रम किए गए, लेकिन आगे चलकर सभी के मतभेद भी सामने आए। संजीव के पचहत्तरवें वर्ष के आयोजन के बाद जो विवाद उभरा वह गौरतलब है। उन्होंने शत्रु की आलोचना और मित्र की आलोचना भाषा और दृष्टि के प्रकरण को भी याद किया है। उन्होंने एकता के परिप्रेक्ष्य में प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष विभूतिनारायण राय के विचार जानने चाहे तो उन्होंने जवाब दिया तीनों प्रमुख लेखक संगठन किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं। जब तीनों राजनीतिक पार्टियां ही एक नहीं हो पा रही हैं तो तीनों लेखक संगठन एक कैसे हो सकेंगे। इसी तरह जब जन संस्कृति मंच के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार से मोर्चे की बाधाओं के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था- जिन मतभेदों के कारण लेखक संगठनों की शाखाएं प्रशाखाएं बनी थीं, वे मतभेद हल कर लिये गए हों, ऐसा नहीं दीखता है। राजेंद्र कुमार इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हैं कि नए लेखक संगठनों से जुड़ना ही नहीं चाहते। वे कहते हैं कि सभी प्रतिबद्ध लेखक अपने-अपने संगठन में रहते हुए भी वर्तमान बुनियादी समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाते रहें।
इस तरह बात साफ हो जाती है कि आज भी सभी लेखकों की तो छोड़ दें साहित्य के तीन संगठनों- जसम, जलेस और प्रलेस- के बीच भी एका होने में मुश्किलें हैं, क्योंकि ये तीनों अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। गौर करना होगा कि इन लेखक संगठनों के बाहर भी बहुत से लेखक हैं, जो सार्थक रच रहे हैं और साहित्य के स्तर पर मौजूदा समस्याओं से जूझ रहें है। आज बड़ा सवाल है कि क्या लेखकों के बीच परस्पर गहरा संवाद है?
इस सवाल की तह में जाएंगे तो कई तरह के सवाल उठते जाएंगे। राजनीति, विचारधारा और साहित्य के सवालों पर गंभीर विचार करना होगा। साहित्य को किसी राजनीतिक संगठन का पिछलग्गू होना चाहिए या अपनी आवाज की स्वायत्तता हासिल करनी चाहिए। विचारधारा आरोपित होनी चाहिए या संवेदना के भीतर से उपजनी चाहिए। क्या साहित्य किसी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध होकर, उसकी रणनीति में शामिल होकर जनविश्वास हासिल कर सकता है? क्या राजनीतिक दल और राजनीतिक विचारधारा दोनों एक ही चीज है? रणनीति एक तात्कालिक चीज है, जबकि साहित्यिक विचारधारा दीर्घकालिक है।
इस अंक को पढ़ते हुए ये सवाल उठेंगे। लेखकों को सोचना होगा कि आज के राजनीतिक कोलाहल में उनकी आवाज कैसे सुनी जाए। इसके लिए केवल सत्ता का प्रतिरोध ही नहीं बल्कि जनता की सोच को बदलने के दीर्घकालिक मोर्चे पर भी कार्य करना होगा। जनदबाव से ही सत्ता अपना चरित्र बदलने पर विवश होती है।
इस अंक से यदि यह बहस आगे बढ़े और साहित्यकारों के बीच एका का रास्ता बने तो सुखद एवं सार्थक होगा।
पत्रिका – लमही
संपादक – विजय राय
मूल्य – रु.100 मात्र notnul पर उपलब्ध
ईमेल – [email protected]
मोबा. – 9454501011
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.