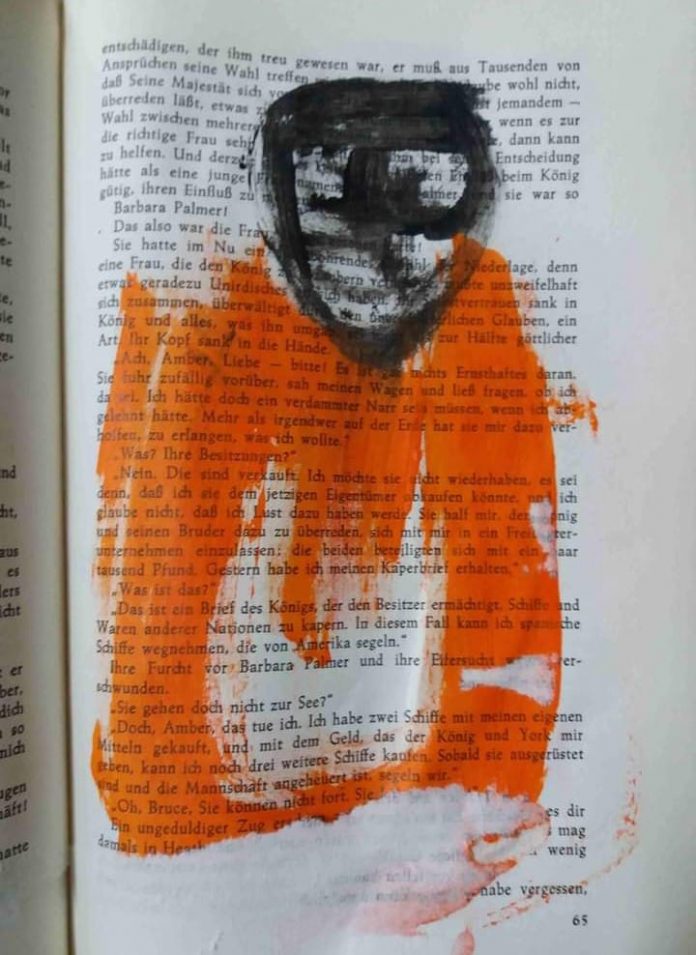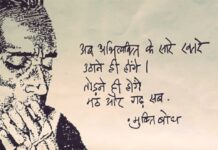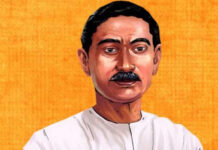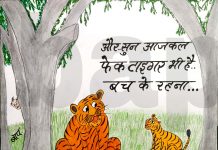— राम जन्म पाठक —
यह ऐसा प्रश्न है जो हर लेखक से पूछा जाता है। बाहरी लोग लेखक से उतना नहीं पूछते, जितना एक लेखक खुद से पूछता है। कथा-शिल्पी शशिभूषण द्विवेदी ने एक बार राजेंद्र यादव से पूछा कि हम लिखते क्यों हैं? राजेंद्र यादव ने उत्तर न देकर प्रतिप्रश्न कर दिया, ”आखिर हम जीते क्यों हैं?”
क्या लिखना, जीना है? और अगर जीने को लेकर कोई उत्तर नहीं है तो भला लिखने को लेकर कैसे हो सकता है। फिराक साहब का शेर है- ”मौत का भी इलाज हो शायद/ जिंदगी का कोई इलाज नहीं।” तो क्या लिखना भी एक लाइलाज बीमारी है, जिंदगी की तरह। और तुम्हारे लिखने से क्या कुछ उखरता-सपरता भी है, कोई पत्ता खड़कता भी है या ऐसे ही कागद-कारे किए जा रहे हो !
और फिर इतना विपुल लेखन। इतना सारा प्रकाशन। इतने सारे लेखक। पुराने और नए। और अब तो छपने का संकट भी खतम। फेसबुक, ब्लॉग। सोशल साइटें। जहां चाहो, वहां लिखो। जितना चाहो, उतना लिखो। लेकिन सब मिलकर भी इस ”चलती-चाकी” का कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम कौन-सा तीर मार लोगे? शायर कहता है- हजारों खिज्र ( महापुरुष) पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। मगर अफसोस है कि आदमी अब तक भटकता है।
यह सब कुछ हमें पता है। तब फिर वह कौन-सा पहरेदार है, जो आपको सीटी मार कर सोते से जगाता है और धकेल देता है, ‘चलो, लिखो।’? और आप आज्ञाकारी बच्चे की तरह कूद-फांद करने लगते हैं। चले जाइए उन अहर्निश चलने वाले सेमिनारों, गोष्ठियों, कक्षाओं में, जहां प्रबुद्ध वक्तागण आपको हतोत्साहित करते हैं कि लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो आप अपनी नींद क्यों खराब किए हैं श्रीमन। आप भी जाकर सोइए। लेकिन वे हैं कि अपनी उपेक्षा और उपहास की शैली से आपको हलाक करते रहेंगे।
उनका प्रश्न है कि तुम कौन-से वेदव्यास और वाल्मीकि हो, कोई तुम्हें क्यों पढ़े?
कोई पढ़े या न पढ़े। कोई समझे या न समझे। कोई माने या न माने। इतना तो तय है कि अर्द्धवज्रासन में बैठा, मुंह में कलम दबाए हर लेखक अपनी लेखन-मुद्रा में वेदव्यास-वाल्मीकि, होमर-मिल्टन, टॉल्सटॉय-शेक्सपीयर, तुलसी-सूर, कबीर-रहीम से कम नहीं होता है। अगर वह खुद को उस ऊंचाई पर न रखे तो लिख ही नहीं सकता। भले ही उसकी रचना दो कौड़ी की हो।
भारत जैसे देश में, जहां कि बहुसंख्यक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है और निरक्षर है, और अनगिनत कठिनाइयों से सराबोर है, लेखक होने का अर्थ क्या है? गरीबी रेखा से नीचे का मतलब कि निर्धनता, बीमारी, विस्थापन, रौरव नरक। दुखों की मायानगरी। भूख और गंदगी का हाहाकार। छटपटाते-मरते लोग। हत्या, दमन, लूटमार, खींचाखांची यानी कुंभीपाक। तबाही का जलजला। ऐस में आप कैसे लिखें?
आप सोचते हैं कि आपके लिखने से पीर-पर्वत कुछ पिघलेगा और कोई मुक्तिदायिनी गंगा निकलेगी। तो फिर लिखने की शर्त क्या होगी ? क्या किसी हाट-बाजार में ऐसी कोई पुस्तिका बिकती है जो आपको लिखना सिखा दे? किसी दवाई की दुकान पर कोई कैप्सूल? क्या इसकी कोई आचार संहिता है, जो एक लेखक को रास्ता दिखा दे? जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो कि लेखक को नशा नहीं करना चाहिए या सवेरे उठकर नहाना चाहिए या सेक्स नहीं करना चाहिए। या मीट-मटन नहीं खाना चाहिए। ऐसी कोई निर्देशावली कहीं है क्या? जैसे कि निराला अपनी एक कविता में गांधीजी से पूछते हैं, ”बापू, गर तुम मुर्गी खाते?” वैसा कुछ। क्या सचमुच लेखक होने की कोई कसौटी है या उसकी कोई नैतिकता है। कोई बाहरी नियमन, कोई बंदिश?
इतना तो तय है कि लेखन, कोई ऐशो-आराम की चीज नहीं है।
आखिर वह कौन-सी चीज है जो एक लेखक को लेखक बनाती है। क्या सिर्फ शब्दों की चटाई तैयार करते जाना या लिख-लिखकर चट्टे लगाना या साल-दर-साल किताबों के अंबार लगाना? तो फिर क्या? हरिवंशराय ‘बच्चन’ जी कुछ मददगार हो सकते हैं- ”पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी।…पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी।”
यह निशानी ही बताती है कि प्रथमतया तो इसका यही विधान है कि इसका कोई विधान ही नहीं है। और द्वितीयत: इस उपहारस्वरूप मिली स्वतत्रंता का दुरुपयोग अगर आप करेंगे तो तीनों लोकों में आपके लिए कोई जगह ही नहीं होगी। यही है वह जगह कि इसमें आपके माता-पिता, सखा-सहोदर, भाई-बंधु, दोस्त-प्रेमिका कोई मदद नहीं कर सकता। इस अंधेरेपन से आपको खुद ही निपटना है। और खराब रचना के लिए कोई बहाना नहीं है।
लिखना कोई शगल नहीं है। यहां भी एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। उठता हाहाकार जिधर है, उसी तरफ अपना भी घर है। जो कवि के इस संकेत को पहचान लेगा, वही लेखक बन पाएगा। यही वह सूत्र है, जिसे मुक्तिबोध ने खोजा है, ”बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम !” कबीर ने ऐसे ही लोगों को हांक लगाई होगी- जो घर फूंके आपनो तो चले हमारे साथ। लिखना, घर-फूंक तमाशा देखना है। सबको अपने लेखन की कीमत चुकानी होती है। फैज़ अहमद फैज़ ने चुकाई थी। जेल गए थे। नागार्जुन ने भी चुकाई थी। इस समय भारतीय समाज का लेखक बहुत डरा हुआ है। क्या वह वही लिख रहा है, जो वह लिखना चाहता है? क्या किसी ने उसकी घांटी पकड़ रखी है? जब कोई लेखक नहीं बोल रहा है तो कम से कम एक किसान नेता को ही धन्यवाद कहना चाहिए, जो कम से कम बोलता तो है कि, ”कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है।’
तो पक्ष चुनना ही लेखन है। पक्ष किसका? मैथिलीशरण गुप्त की काव्यपंक्ति है- ”रक्षक पर भक्षक को वारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे!” यहीं एक लेखक, विधाता के समकक्ष खड़ा होता है। अगर कोई लेखक गूंगों की वाणी नहीं बन सकता, नेत्रहीनों का नेत्र नहीं बन सकता, तो फिर वह भाटों की तरह विरुदावली गाने वालों की पांत में ही गिना जाएगा। जो अपने समय की क्रूरताओं, बदमाशियों और अत्याचारों के खिलाफ लेखनी नहीं चलाएगा, वह आज नहीं तो कल राख ही होगा। उसे न भारी-भरकम पुरस्कार बचा सकेंगे, न पुस्तक मेले, न पंचसितारों के सेमिनार, न विश्वविद्यालयों की मुदर्रिसी।
क्या आप अब भी लेखक बनना चाहते हैं !
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.