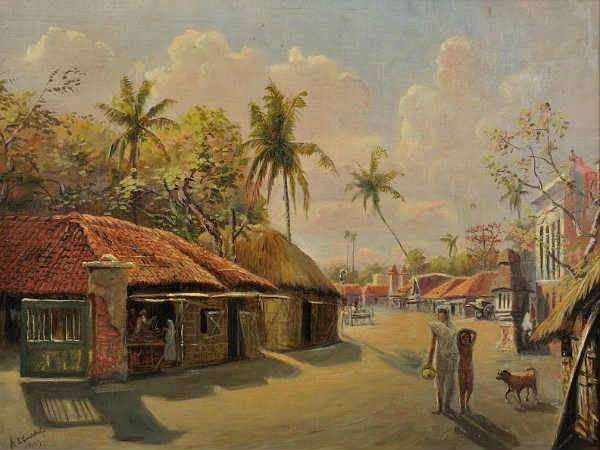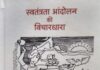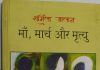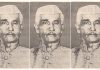— किशन पटनायक —
यह लेख देवीप्रसाद मौर्य की पुस्तक ‘क्रांति के पहले’ (प्रकाशक- गंगा प्रसाद तिवारी, चौखंभा प्रकाशन, 9/5 जवाहर मार्ग, इंदौर, मध्यप्रदेश) के प्राक्कथन के रूप में लिखा गया था।
मुझे कभी-कभी विद्वानों की लिखी पुस्तकों के लिए आमुख या दो शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो मैं असमंजस में पड़ जाता हूं। अपने ऊपर एक संदेह होता है कि मेरी जो थोड़ी-बहुत राजनैतिक बुद्धिजीवी होने की प्रतिष्ठा है, उसकी वजह से मुझे यह गंभीर काम सौंपा जा रहा है। जबकि पांडुलिपि का लेखक मुझसे अधिक जानकारी रखता है, उसका गहरा अध्ययन है और स्पष्ट तथा सशक्त भाषा में अपनी बातों को लिखता है, उस पर मैं जो लिखूंगा वह सतही हो जाएगा। फिर भी यह लोभ संवरण नहीं किया जाता है कि इस किताब के साथ-साथ मुझे भी कुछ कहने का और प्रसिद्धि का हिस्सेदार बनने का मौका मिल जाएगा।
क्रांति के ऐतिहासिक-सामाजिक संदर्भ का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करना इस पुस्तक का ध्येय है। इतनी समग्रता में क्रांति के संदर्भ की चर्चा एक लंबे अरसे से नहीं हो रही है। वामपंथी साहित्य में इसका अभाव होने लगा है। भारतीय साम्यवादी आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में रजनी पामदत्त नामक ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेता ने ‘इंडिया टुडे’ नामक किताब लिखी थी जो पुरानी पड़ जाने पर भी अभी तक सब प्रकार के कम्युनिस्टों के लिए भारत को समझाने का एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। डा. देवीप्रसाद की किताब का पैमाना भी उसी प्रकार का है। पामदत्त का विश्लेषण आर्थिक-राजनैतिक था, प्रस्तुत निबंध के विश्लेषण मुख्यतः ऐतिहासिक-सामाजिक हैं। विषय क्षेत्र की व्यापाकता आज के पाठक को उत्साहित नहीं करती है, लेकिन प्रस्तुत पूरी किताब में से अगर एक ही अध्याय ‘हिंदुस्तानी समाज’ कोई पढ़ने के लिए छांट ले तो भी यह एक सार्थक कृति प्रतीत होगी और हो सकता है कि उसके बाद पुस्तक के अन्य अंशों के प्रति पाठक का आकर्षण बढ़े। भारतीय इतिहास को समझने के लिए पिछले दिनों जो भी प्रगतिशील अध्ययन हुए हैं उनसे उभरे तथ्यों को संवारते हुए इस अध्याय में एक ऐतिहासिक दृष्टि प्रस्तुत की गई है जो बहुप्रचलित होनी चाहिए। इतिहास की पाठ्य पुस्तकें भी इसी ढांचे पर लिखी जानी चाहिए।
भारतीय इतिहास की इस दृष्टि को प्रचलित करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि प्रभावशाली सामाजिक वर्गों के अहं को इससे ठेस पहुंचती है। भारतीय इतिहास को अंग्रेज शासकों ने इस तरह लिखा कि वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद और देशी नौकरशाहों के अनुकूल हो। आजादी के बाद नौकरशाही के सामाजिक आधार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है।
राजनीति में भले शूद्रों का महत्त्वपूर्ण अनुप्रवेश हुआ हो, लेकिन नौकरशाही, शिक्षा-व्यवस्था, व्यापार-उद्योग, यहां तक कि ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट नेतृत्व का भी सामाजिक आधार एक जैसा है और अपरिवर्तित है। इसलिए पुराने ढंग से लिखे गए इतिहास को अभी भी उनका समर्थन प्राप्त है।
हाल में भारत के इतिहास लेखन के संदर्भ में एक बहुत ही छोटे अंश को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। उपयोगी होते हुए भी यह विवाद राजनैतिक ही था। मुसलमान राजत्व और मुसलमान शासकों के चरित्र, नीयत और देशप्रेम के सवाल को अगर हम प्राचीन इतिहास (मुसलमान पूर्व) से काटकर देखेंगे तो उसके बारे में संतुलित दृष्टिकोण और सही नतीजे नहीं निकल पाएंगे। एक पक्ष अपने राजनैतिक कारण से कहता है कि मुसलमान दुष्ट था, दूसरा पक्ष अपने राजनैतिक कारणों से कहता है कि मुसलमान निर्दोष था।
अगर प्राचीन इतिहास के सारे तथ्यों को लिखा जाएगा और उसी कड़ी में मुसलमान आक्रमणकारियों की बात भी लिखी जाएगी तो राजनैतिक पक्षपात की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि जितना दुष्ट मुसलमान हमलावर था उतने ही दुष्ट उसके पहले के सारे हमलावर थे–शक, हूण और आर्य भी। दिक्कत इसलिए होती है कि इन पुराने हमलावरों की बर्बरता का विशद वर्णन इतिहास पुस्तकों में होता नहीं है। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकारों को यह बताना था कि उनके आने के पहले जो राज प्रशासन था वह बहुत बुरा था, अंग्रेजों ने उसे हटाकर एक कल्याणकारी राज की प्रतिष्ठा की। अंग्रेजों के पहले भारत के प्रमुख भागों पर मुसलमान राज था, इसलिए मुसलमानों की बुराई और अंग्रेजों की अच्छाई पर इतिहास पुस्तकों का ध्यान केंद्रित हो गया। अंग्रेजी राज में नौकरशाही पर हिंदू द्विजों का कब्जा था, इसलिए उनको भी यह अच्छा लगा।
आसानी से उपलब्ध कुछ तथ्यों को लेकर प्राचीन इतिहास लिखा गया जो बहुत ही संक्षिप्त और सतही रूप में पाठ्य पुस्तकों में पेश किया जाता है। उसके अनुसार मगध, थानेश्वर, उज्जैन, चोल आदि के कुछ राजवंशों को गिना देना और यात्रियों के विवरण के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति की झलकियां दे देना भारत का इतिहास है। राजनैतिक कारणों से प्रेरित होकर कुछ प्रगतिशील लोग चाहते हैं कि मुसलमान कालीन इतिहास को नए सिरे से लिखा जाए। यह असंभव है क्योंकि इस प्रकार का लेखन सही इतिहास नहीं होगा। जब तक प्राचीन इतिहास को ठीक ढंग से नहीं लिखा जाता है और उसकी कड़ी से जोड़कर मुसलमान काल को नहीं समझा जाता तब तक कोई सार्थक इतिहास नहीं बन पाएगा। अगर इतिहास के जरिए हम अपनी जनता को, उनके रक्त, मस्तिष्क और स्थिति को समझना चाहते हैं तो प्राचीन इतिहास को नए सिरे से जनता के इतिहास के तौर पर लिखना होगा। यह कैसे लिखा जा सकता है उसका एक ढांचा इस पुस्तक के एक चर्चित अध्याय में है।
भारतीय संस्कृति और समाज का मौलिक गुण ‘वर्णसंकर’ है। उसकी ताकत और कमजोरी दोनों इसी में निहित है। जिन समाजों में वर्णसंकर प्रक्रिया स्वाभाविक, सहज और स्वस्थ गति से चली, देश की मिट्टी, हवा और परंपरा को मान्यता देकर नए तत्त्वों को मिलाने की कोशिश हुई, उन दिनों एक मजबूत राज्य भी पैदा हुआ- सांस्कृतिक प्रभाव दूर-दूर तक फैला। इसके विपरीत जब-जब सामाजिक मिश्रण की गति को रोकने की कोशिश हुई, या बाहरी तत्त्वों ने अपने को लादने की कोशिश की, तब वर्णसंकर का मतलब ‘अनेकता में एकता’ न होकर ‘एक से अनेक’ और अनमेल अनेकता हो जाता है।
आर्य भी लंबे समय तक भारत की तत्कालीन लोकसंस्कृति से अलग नहीं रह सके। अपने वेद उपनिषद की बुद्धि से लैस होकर प्रचलित अनार्य संस्कृति को अपनाने का जो महान कारगर और कौशल अपनाया, उससे एक बड़ा देश और भव्य संस्कृति विश्व के धरातल पर प्रकट हो गई, लेकिन उस तरीके में ऐसे तत्त्व थे जो कालक्रम में अब अभिशाप साबित हो रहे हैं। पुराण और जातिप्रथा आर्यों के वर्णसंकर अभियान की ही उपज है। उपनिषद की बातों को विश्वसनीय बनाने के लिए काले रंग के देवता के मुख से गीता नि:सृत कराना निश्चित रूप से एक चमत्कारी प्रयोग था। उसी प्रकार सबल अनार्यों को समकक्ष बनाकर और कमजोर तबकों को सेवक या दास के तौर पर अपनाने के लिए जो जातिप्रथा बनाई वह भी दुनिया का सबसे ज्यादा अपरिवर्तनीय सामाजिक ढांचा साबित हो रहा है।
मिश्रण हो तो गया, सामाजिक भी सांस्कृतिक भी, लेकिन अपने को केंद्र में रखने के लिए उद्देश्य से इसके लिए जो विषमतामूलक वंशानुक्रमिक ढांचा अपनाया गया वह कुछ समय के बाद अवरोध पैदा करने लगा। सबसे पहले बुद्ध ने इसकी चेतावनी दी। बौद्ध प्रभावित हिंदू समाज ही ने सारे भारत को राजनैतिक तौर पर एकत्रित किया और भारतीय संस्कृति को एशिया में फैलाया। शंकराचार्य ने हिंदू समाज के नेतृत्व में आत्मविश्वास जरूर पैदा किया, लेकिन सामाजिक गतिशीलता पैदा करने की ताकत बौद्ध प्रभाव के बाद फिर कहीं से नहीं मिली।
जब मुसलमान हमलावर आए उनको न रोकने की, न पचाने की ताकत हिंदू समाज में थी, और ये हमलावर भी ऐसे ही थे कि अपने को लादने की कोशिश में उन्होंने समाज पर अपनी पकड़ खो डाली और अंततः ऐसे विदेशियों के हाथ देश को सौंप दिया जो हिंदुस्तान को अपनाना भी नहीं चाहते थे। हिंदुओं का पुरुषार्थ तो लुप्त हो चुका था, मुसलमान भी सही वर्णसंकर नीति न अपनाने के कारण, अपने धर्म को लादने की कोशिश में खुद कमजोर हो गए।
यूरोपीयकरण भी भारतीय समाज में गति पैदा करने में असमर्थ है क्योंकि भारतीय समाज को बदले बिना यह यूरोपीय मूल्यों को थोपना चाहता है। पुरानी विषमताओं को दूर किए बगैर नई पूंजीवादी विषमताएं पैदा करने की इसकी कोशिश तो हिंदुस्तानी समाज को नेस्तनाबूत कर इसकी संभावनाओं को भी खतम करने पर तुली हुई है। समझना यह जरूरी है कि समतामूलक ढांचे में ही भारतीय समाज का पुनर्जागरण हो सकता है।
हिंदुस्तानी समाज में एकता के बदले अनेकता बढ़ रही है। विषमतामूलक वर्णसंकर नीति का यह अंजाम कालक्रम में होना अनिवार्य था। इसकी काट के लिए एक समतामूलक वर्णसंकर नीति की जरूरत होगी, जिसके तहत नागा से लेकर सिख तक और भील से लेकर मुसलमान तक एक ही सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हो सकें। यह एक धार्मिक ढांचा नहीं हो सकता है, राष्ट्रीयता के ढांचे में ही यह संभव होगा। राष्ट्रीयता को यह सामाजिक अर्थ देने की कोशिश सिर्फ गांधीजी ने ही की थी। राष्ट्रीयता का सिर्फ यह नकारात्मक अर्थ होगा कि हमारा देश दूसरे देशों से अलग है, बल्कि राष्ट्रीयता का यह अर्थ होगा कि सामाजिक अनेकता और विषमता को पाटने वाला यह आंदोलन होगा। राष्ट्रीय आंदोलन की इस भूमिका को भारत के बुद्धिजीवियों की स्वीकृति न मिलने के कारण आजादी के बाद यह पहलू लुप्त हो गया और राष्ट्रीयता का अर्थ सिर्फ पाकिस्तान विरोध या चीन विरोध में सीमित रह गया है।
भारत के इतिहास और समाज को नए सिरे से अध्ययन करने की जरूरत को अब टाला नहीं जा सकता है। इतिहास के अध्ययन से अपने समाज के बारे में एक नया एहसास पैदा होगा, सामाजिक विषमता और अनेकता को मिटाने की जरूरत एक चुनौती के रूप में खड़ी होगी। इन प्रक्रियाओं के बगैर क्रांतिकारी राजनीति भी अधूरी और सतही रहेगी। ‘क्रांति के पहले’ शीर्षक की प्रासंगिकता यही है।
क्रांति के लिए क्रांतिकारियों का एक राजनैतिक संगठन तो आवश्यक है ही, लेकिन राष्ट्र और समाज के बारे में एक ऐतिहासिक समझ और चेतना पैदा किए बगैर राजनैतिक कार्यक्रमों का असर गहरा नहीं होता है। यानी राज्यक्रांति की पहल के पहले या साथ-साथ एक बौद्धिक तथा सांस्कृतिक क्रांति चाहिए।
शायद क्रांति के इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है। हम इस बात को नादानी से छुपाते हैं क्योंकि कम्युनिस्टों ने प्रचार कर रखा है कि पहले आर्थिक क्रांति होगी, बाद में उसकी संस्कृति पैदा होगी। अगर सांस्कृतिक क्रांति भी होगी तो बाद में ही होगी। अगर इतिहास में खोजें तो आधुनिक विश्व में जो भी साम्यवादी राष्ट्रीय या औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं, उनके पहले एक बौद्धिक उथल-पुथल उस राष्ट्र के समाज में हुई है। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली हो सके, उसके पहले एक साहित्यिक क्रांति हुई। तोलस्तोय, दोस्तोवस्की आदि महान साहित्यिकों ने रूसी नौजवानों और बुद्धिजीवियों के मानस को अगर नहीं झकझोरा होता तो क्या क्रांति को इतना समर्थन रूसी समाज में मिल जाता? यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई उसको संभव बनाने के लिए उसके पहले धर्म सुधार आंदोलन और बौद्धिक पुनर्जागरण हुए। भारत में एक राष्ट्रीय क्रांति हुई, उसके अग्रदूत के रूप में दयानन्द, विवेकानन्द, ब्रह्मसमाज आदि सामाजिक आंदोलन हुए। ऐसा मानना मार्क्सवादी ऐतिहासिक सिद्धांत के विपरीत नहीं होगा।
अगर भौतिकता को प्राथमिकता दी जाए, मस्तिष्क को उसकी उपज माना जाए, तब भी इस प्रतिपादन के अनुसार ही, भौतिक जगत या आर्थिक ढांचे में जिस वक्त परिवर्तन की जरूरत, स्थिति या तनाव पैदा होगा उसी वक्त से मानसिक संवेदना और बौद्धिक प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अतः क्रांति पहले दिमाग में आएगी, बाद में राजनैतिक कार्यक्रमों के द्वारा उसको उतारा जाएगा। राजनैतिक क्रांति खुद एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति की उपज है। बौद्धिक या सांस्कृतिक क्रांति भी उसी सामाजिक स्थिति की उपज है, अतः यह पूर्वगामी होगी या साथ-साथ चलेगी।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.