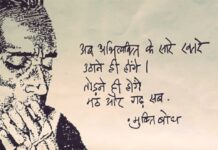— राम जन्म पाठक —
अक्सर रात के तीन-चार बजे नींद उचट जाती है। ‘कुरआन’ में नींद को छोटी मौत कहा गया है। तो क्या मैं छोटी मौत से बाहर आ गया हूं? मैं सोचता हूं बत्ती जला दूं। फिर सोचता हूं, क्या फायदा। महानगरीय जीवन में यही वक्त है जब लोग घोड़ा बेचकर सोते हैं। सड़क पर वाहनों की आवाजाही और उनका शोर, धम्म-घम्म की आवाजें आती रहती हैं। फिर बत्ती जला देता हूं। बाथरूम जाता हूं। कमरे में आकर कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। कहीं मन नहीं लगता। मोबाइल में मौजूद वीडियो-क्लिपों में इतना अनंत दोहराव है कि देख-देखकर ऊब गया हूं। वही जावेद उर्फी, अवध ओझा, और ‘देख रहा है न विनोद’ की अनगिनत बार देखी गई दृश्यावलियां।
अश्लील कारोबार की अश्लील तस्वीरों से पटा पड़ा संसार। पोर्नोग्राफी का अखंड समुद्री विस्तार। न चाहते हुए भी तुम्हारे सामने ऐसे-ऐसे दृश्य आ जाते हैं कि अकेले में भी मन लिजालिजाहट से भर जाता है। यह अजंता, एलोरा और खजुराहो की कल्पनाओं से बची रही गई कौन-सी दृश्यावलियां हैं, जो मानव-मन रच रहा है। अश्लीलता का ऐसा जगमग और भिनभिनाता संसार, लगता है उलटी हो जाएगी। किसी दार्शनिक, विचारक, दानिश्वर ने हमें चेताया क्यों नहीं कि एक दिन अश्लीलता ही सबसे बड़ी कला हो जाएगी, और कट्टरता सबसे बड़ी राजनीति और झूठ सबसे बड़ा मूल्य!
कहीं किसी अखबार में मैंने एक दिन पढ़ा कि दुनिया में इंटरनेट-डाटा की जो समूची खपत है, उसमें से 85-86 फीसद सिर्फ पोर्नोग्राफी देखने में खर्च हो रहा है। तब तो ओशो ठीक ही कहता था कि संसार अपने ‘काम-किला’ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। पश्चिम के लोग तो फिर भी कुछ मुक्त हैं, लेकिन पूरब, और उसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप जकड़ा हुआ है। ये कौन लोग हैं, जो ऐसी फिल्मों के चिरपिपासु हैं?
मैं, मोबाइल फेंक देता हूं और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता हूं। कालोनी की सड़क पर। चारों तरफ सड़कों को अवैधरूप से कब्जा किए कारों की पांतें, रोशनी में नहाई सड़कें और जहां-तहां सोते-जागते कुत्ते। कालोनी नींद के आगोश में है। यह नोएडा का सेक्टर ग्यारह है। नोएडा के आलीशान इलाकों में एक। बड़ी-बड़ी कोठियां; दो सौ, तीन-सौ वर्गमीटर में बने सुंदर-सलोने-सुघर फ्लैट। नोएडा की सड़कें इलाहाबाद से लोहा लेती दीखती हैं। इलाहाबाद में सड़कें बहुत चौड़ी हैं। आजादी के बाद दो ही ऐसे शहर हैं जिन्हें नियोजित तरीके से बसाया गया है, चंडीगढ़ और नोएडा। बाकी शहर कबाड़खाना जैसे लगते हैं।
मेरे ठीक सामने राष्ट्रीय सहारा का मीडिया हाउस है। कभी यहां बहुत चहल-पहल रही होगी। दीवारों के पलस्तर झड़ गए हैं और वे मटमैली हो गई हैं। अंदर पता नहीं क्या चलता है, शायद अखबार अब भी निकलता है। शायद चैनल भी चलता हो। गेट पर इक्का-दुक्का गार्ड नजर आते हैं। सुब्रत राय के जेल जाने के बाद इस मीडिया हाउस की रही-सही मर्यादा भी चली गई है। कर्मचारियों का बकाया नहीं दिया जा रहा है। और भी बहुत कुछ। किसी बमबारी में उजड़े हुए चमन की तरह दिखता है यह मीडिया हाउस।
मुझे इलाहाबाद का ‘एनआइपी-अमृत प्रभात’ का परिसर याद आता है। उसके भी मालिक बंगाली थे और सहारा के भी। ऐसे ही मन में ख्याल आता है। क्या कोई साम्य है, पता नहीं। बिल्कुल नहीं। कहां महात्मा शिशिर घोष और कहां सुब्रत राय? ऐसे मीडिया हाउसों की पतनगाथाओं के राज़ कोई पोशीदा तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी इब्तिदा में ही इनकी इंतिहा दर्ज रहती है?
लेकिन एक साम्य तो है, बर्बादी का। और कर्मचारियों के बकाए का। उनके घरों के बुझते चूल्हों का। शादी के इंतजार में बड़ी होती बेटियों का। और बिना फीस चुकाए स्कूलों से लौटते बच्चों का। ऐसे मीडिया हाउसों के अधिग्रहण की कोई योजना है सरकार के पास? क्या वे थोक के भाव में जो रातोरात सड़क पर आ जाते हैं, भारत के नागरिक नहीं?
जाने दीजिए। ”किस-किस को याद कीजिए। किस-किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए।”
और इधर हाल यह है कि नींद आ ही नहीं रही है। मौत का मुअय्यन न भी होता तो भी नींद जरूरी है।
मैं पुकारता हूं, कालीचरन (गार्ड) को। मेरे ठीक सामने कॉलोनी का मेन गेट है। कालीचरन की पाली रात की रहती है। रात भर गाड़ियों के आवागमन के कारण गेट खोलना और बंद करना, यही उसका काम है। दो बजे के बाद आवाजाही कुछ टूटती है, तो ‘जोमैटो’ और खाना पहुंचाने वाले लड़के गेट खड़खड़ाते हैं। वह भुनभुनाता है, पता नहीं किसे तीन बजे रात को खवास (भूख) है। कालीचरन में अमीरों के प्रति अजीब-सी बदहवास नफरत है, जो निश्चय ही उनके अत्याचारों से उपजी होगी।
फिर, सोचता हूं, सोया है तो सोया ही रहने दो। किसी को तो नींद आ रही है। वही सही।
कालीचरन उठें तो लेकर नोएडा सेक्टर-22 के आलीशान स्टेडियम में जाऊं। सुबह की सैर को। थोड़ी हवाखोरी के लिए।
अभी तीन-चार घंटे का समय है। इसे कैसे बिताऊं? रेलवे स्टेशनों पर का इंतजार हम सब जानते हैं। ऊंघते-औंघाते, भागते-दौड़ते, घड़ी की सुइयां देखते कुछ खटर-पटर जरूरी है। मोबाइल उठाकर कुछ देखूं क्या? सोऊं? नींद नहीं आएगी। टहलूं? मन नहीं है।
फिर क्या करूं? समय का क्या है, बीत ही जाएगा।
——
मैं दिल्ली में नहीं, दिल्ली के सीमांत पर रहता हूं। इधर नोएडा, उधर दिल्ली। मेरा कार्यालय भी सीमांत पर है। सड़क इस पार नोएडा, उस पार दिल्ली। यह सीमांत शब्द भी अजीब है। मेरे पिता भी शायद सीमांत किसान हैं? क्या इस सीमांतता से पिंड छूटेगा हमारा? भारत के अस्सी प्रतिशत किसान सीमांत या मझोले हैं। भारतवासियों का भी यही हाल है। सत्तर फीसद आबादी बस दो जून की रोजी-रोटी के चक्कर में सुबह-शाम करती रहती है।
कालीचरन उठ गए हैं। उन्हें लेकर मैं सेक्टर-22 के स्टेडियम चला जाता हूं। वह मुझे रास्ते में बरजता है, ‘साहब, कार धीरे चलाया कीजिए।’ मैं अनसुना करता हूं। पता नहीं, मैं कहां से उसे ‘साहब’ लगता हूं। उसके भीतर पीढ़ियों की भरी हुई गरीबी है और उससे उपजा भय। इसलिए वह सुरक्षित संबोधन चुनता है, ताकि किसी को बुरा न लगे। स्टेडियम में मेरे ठीक बराबर चलता है। कंधे से कंधा मिलाकार, शाना-ब-शाना। लगता है कि हम दोनों एक जोड़ी बैल हों मानो, और किसी बैलगाड़ी के जुआठे में जुते हों। अगर आगे-पीछे हुए, गाड़ी पलट जाएगी?
वह स्टेडियम में कूदती-फांदती लड़कियों को देखता है। खाए-अघाए-मोटाए अधेड़ों और बूढ़ों को। नितंबिनी महिलाओं को। ये सब अपनी चर्बी गलाने आए हैं। कभी-कभी फब्ती कसता है, धीरे-से, “देख रहे हैं, साहब? गांवों में तो कोई स्टेडियम और पार्क नहीं होते। बदन पर चर्बी भी नहीं होती। सब हंड़ियाए, उजाड़, खंखड़। क्या स्टेडियम सिर्फ शहरी लक्जरी है?”
एक दिन उसने अजीब सवाल पूछा, ”साहब, दुनिया में सारी अच्छी चीजें बुरे लोगों के पास ही क्यों हैं?” मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, ”अच्छे मकान, अच्छी गाड़ियां, अच्छी महिलाएं, अच्छा खाना, अच्छी शराब..अच्छा बिस्तर…”
मैं थोड़ा गंभीर हो गया, ”तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?” कालीचरन ने कहा, ”और क्या, क्या मैं जानता नहीं हूं। हर कोठी का हाल मैं जानता हूं। सब घूस, काली कमाई, कामचोरी का पैसा है।”
कालीचरन ने मुझे सकते में डाल दिया है। मैं वापस लौटता हूं।
कार्ल मार्क्स को पलटता हूं, गांधी से पूछता हूं, टैगौर से। कहीं से कोई सदा नहीं आती !
मैं कालीचरन को क्या जवाब दूं !
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.