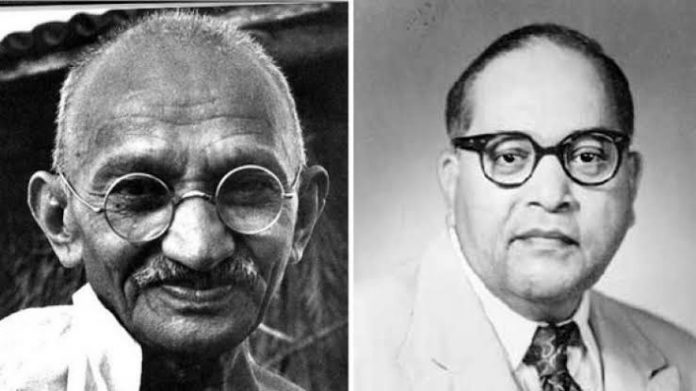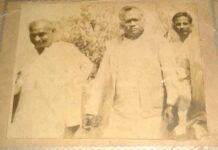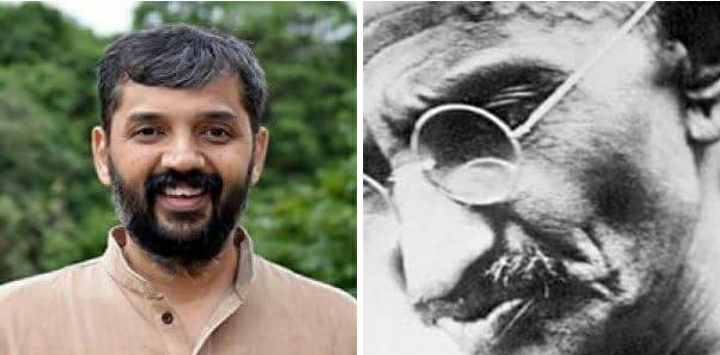— अरुण कुमार त्रिपाठी —
महात्मा गांधी और डा आंबेडकर के बीच दूसरा टकराव गोलमेज सम्मेलन के दौरान लंदन में हुआ। आंबेडकर लंदन 29अगस्त को पहुँच गए थे और गांधी के जाने की संभावना नहीं थी। लेकिन बाद में स्थितियाँ बदलीं और शिमला में वायसराय से मिलने के बाद गांधी 29 अगस्त को बंबई से निकलकर 12सितंबर को लंदन पहुँच गए। सम्मेलन 7 सितंबर को ही शुरू हो चुका था लेकिन महात्मा गांधी का पहला भाषण 15 सितंबर को हुआ। इसमें गांधीजी ने कहा, “कांग्रेस संस्था किसी एक जाति, धर्म या वर्ग के लोगों की प्रतिनिधि न होकर सब धर्मों की, जातियों की एकमेव प्रतिनिधि है। कांग्रेस ने दो मुख्य ध्येय तय किए हैं–अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम एकता। ऐसी संस्था ने मुझे एकमेव प्रतिनिधि के रूप में माँग रखने के लिए भेजा है। कांग्रेस मुसलमान वर्ग और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिनिधि है। संक्षेप में, वह सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्गों की एकमेव प्रतिनिधि है।”
जब गांधीजी ने कहा कि “मैं आपके सम्मुख यह दावा कर रहा हूँ कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश-हिंदुस्तान की ही नहीं, रियासती जनता के 85-95 प्रतिशत लोगों की भी प्रतिनिधि है’’ इस पर आंबेडकर का कहना था कि “जिन पाँच प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं करती, वे कौन हैं?’’ गांधीजी और डा आंबेडकर के बीच रियासतों के सवाल पर भी नोकझोंक हुई।
आंबेडकर ने रियासतदारों को संघराज्य में शामिल किए जाने से पहले उनकी शासन व्यवस्था में बहुमत की कद्र होने की शर्त रखी और इस तरह उनके विशेषाधिकार का विरोध किया। इस पर रियासतदार भड़क गए। गांधीजी इस टकराव को शांत करते हुए बोले, “व्यापक अर्थ में कहा जाए तो मेरी सहानुभूति डा आंबेडकर के मत के साथ है लेकिन वैचारिक दृष्टि से मैं गेविंग जोन्स और सर सुलतान अहमद के साथ सहमत हूँ।’’ चूँकि गेविंग और सुलतान दोनों ने रियासतदारों का समर्थन किया था इसलिए गांधीजी का ऐसा कहना डा आंबेडकर का विरोध ही करना था। आंबेडकर चाहते थे कि रियासतों के भीतर लोकतंत्र हो, एक प्रकार की जनक्रांति हो। जबकि गांधी की चिंता किसी भी तरह से अंग्रेजों के समक्ष उपस्थित भारत के सारे हिस्सेदारों को एक करने की थी। ऐसे में वे कभी किसी को खुश करते थे तो कभी किसी को। कभी किसी से भिड़ जाते थे तो कभी किसी को पुचकारते थे। यह परदेशियों से लड़ते हुए एक राष्ट्रीय नेता की मजबूरी थी जिसे बार-बार अपनों से भी लड़ना पड़ता था। वैसी मजबूरी आंबेडकर की कम दीखती है। या दीखती भी है तो कभी कभी। शायद यही कारण था कि गांधीजी ने रियासतदारों के पक्ष में बयान देते हुए कहा, “मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि रियासतदार अपनी रियासतों में क्या करें क्या न करें, इसके बारे में राय देने का हमें हक नहीं है।’’ (धनंजय कीर, डा बाबासाहेब आंबेडकर : जीवन चरित)
इसके बाद गांधीजी जातियों और संप्रदायों की जटिल समस्या की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, “हिंदू, मुसलमानों और सिखों के स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की समस्याओं पर विचार करके उसे स्वीकृति दी गई है। ऐतिहासिक कारण ध्यान में रखकर डा आंबेडकर का जो कहना है वह पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आया है। फिर भी अस्पृश्य वर्ग के कल्याण संबंधी बातें आगे पेश करने की जिम्मेदारी में कांग्रेस आंबेडकर के साथ सहयोग करेगी। लेकिन हिंदुस्तान में अन्य किसी वर्ग के कल्याण की जैसी कल्पना है वैसी ही कल्पना अस्पृश्य वर्ग के कल्याण की भी है। इसलिए भविष्य में किसी भी वर्ग के कल्याण के लिए उसे विशेष प्रतिनिधित्व देने का मैं कड़ा विरोध करूँगा।’’
गांधीजी के इस एलान पर आंबेडकर ने यही धारणा बनाई कि वे अस्पृश्यों के कल्याण के विरुद्ध एक प्रकार के युद्ध का एलान कर रहे हैं। लंदन में संविधान समिति की बैठक में संवाद बढ़ने के साथ गांधी के साथियों और आंबेडकर के बीच दूरी बढ़ती गई। एक संवाद में मदन मोहन मालवीय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर अगर आवश्यकतानुसार धन खर्च किया जाए तो अस्पृश्यता इतिहास का विषय बन जाएगी। इस पर आंबेडकर का सवाल था कि सुशिक्षित होने पर भी मैं अस्पृश्य क्यों गिना जाता हूँ? गलतफहमी के इन झोंकों के बीच अल्पसंख्यक समिति का कार्य आरंभ होने से पहले गांधी के बेटे देवदास गांधी ने आंबेडकर से भेंट की। उन्होंने गांधी और आंबेडकर की भेंट सरोजिनी नायडू के घर पर करवाई। आंबेडकर ने बातचीत की लेकिन उन्हें लगा कि गांधीजी अपना दिल खोल नहीं रहे हैं। उधर गांधीजी मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ मिलने की तैयारी कर रहे थे।
गांधी जी 1916 में हुए लखनऊ समझौते के तहत मुस्लिमों को तो विशेषाधिकार के तहत अलग सीटें दिए जाने को तैयार थे और ऐसी सहमति उन्होंने सिखों के लिए भी दे दी थी लेकिन दलितों या अस्पृश्यों के लिए वे अलग चुनाव क्षेत्र देने को तैयार थे। इसे वे हिंदू समाज में विभाजन के रूप में देखते थे और ऐसा होने पर यह भी सिद्ध होता था कि अस्पृश्यता एक हल न होनेवाली समस्या है। इसीलिए वे अपने को अस्पृश्य समाज का भी प्रतिनिधि मानकर प्रस्तुत कर रहे थे। अल्पसंख्यक वर्ग के साथ होनेवाले समझौते के बारे में आंबेडकर एक तरफ तो सहमति दे रहे थे तो दूसरी तरफ उसी को आधार बनाकर अस्पृश्य समाज के लिए भी वैसी ही रियायत माँग रहे थे। कभी कभी वे इसे प्रतिस्पर्धा का मुद्दा भी बनाते थे कि गांधीजी अस्पृश्य समाज के साथ भेदभाव करते हुए अल्पसंख्यकों को तवज्जो दे रहे हैं। इस विशेष या दोहरे मताधिकार का मतलब यह था कि एक चुनाव क्षेत्र में अस्पृश्य समाज को दो तरह के वोट देने का हक होगा। एक तो वह अपने समाज से खड़े प्रतिनिधि के लिए वोट करेगा और उसमें सामान्य वर्ग का कोई मतदाता वोट नहीं देगा। दूसरी तरफ वह सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि के लिए भी वोट देगा।
इस बीच मुसलमान नेताओं के साथ चलनेवाली गांधीजी की वार्ताओं पर आंबेडकर की टिप्पणी थी कि “इस तरह से यदि समझौता हो रहा है तो मुझे उसमें बाधा डालने की इच्छा नहीं है। तथापि मुझे इतना ही पूछना है कि उस समझौते के विचार-विमर्श में कोई अस्पृश्य प्रतिनिधि होगा या नहीं।” गांधीजी से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद आंबेडकर निश्चिन्त थे लेकिन वार्ताओं का रुख इस तरह बदलता गया कि आखिर में अल्पसंख्यक समिति के समक्ष गांधी ने स्वीकार किया कि जातीय समस्या के बारे में सर्वसम्मत समझौता प्राप्त करने में हम विफल रहे हैं इसलिए समिति का कामकाज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। आंबेडकर ने कहा कि गांधी ने करार भंग किया है। आंबेडकर ने इसे करार भंग माना। उन्होंने कहा कि अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि वे हैं। जबकि गांधी का कहना था कि उनकी प्रतिनिधि कांग्रेस है। आंबेडकर का कहना था कि अस्पृश्य वर्ग को आजादी की जल्दी नहीं है लेकिन अगर आजादी आ रही है तो वह किसी श्रेष्ठि वर्ग के हाथ में जाने के बजाय सभी के बीच में बँटनी चाहिए।
आंबेडकर 12 अक्तूबर को टाइम्स आफ इंडिया में लिखे अपने पत्र में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “मुसलमानों के साथ समझौता करते समय उनकी चौदह माँगों को स्वीकार करने के बारे में गांधीजी ने जो शर्त लगाई थी उनमें से एक शर्त यह भी थी कि अस्पृश्य वर्ग और अन्य छोटे अल्पसंख्यक वर्ग की माँगों का मुसलमान विरोध करें। ………………….यह नीति हमारी राय में महात्मा को शोभा नहीं देती। अस्पृश्यों के कट्टर दुश्मनों से यह कृत्य हो सकता था। अस्पृश्यों के बारे में गांधीजी की भूमिका मित्र की तो है ही नहीं, साफ साफ दुश्मन की भी नहीं है।”
इंग्लैंड और भारत के समाचारपत्रों ने इस घटना को गांधी-आंबेडकर विवाद के रूप में प्रस्तुत किया। उनका यह महत्त्वपूर्ण कोण था कि बाबासाहेब ने गांधीजी का विरोध किया है। आंबेडकर का आरोप था कि महात्मा गांधी एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं, उनके बोलचाल में दोहरापन है और वे अन्य प्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। “आंबेडकर का यह भी कहना था कि गांधीजी अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य कर रहे हैं लेकिन इस कार्य का मूलभाव मानवीयता नहीं दयाभाव है। अस्पृश्य किसी की दया नहीं चाहते। वे समानता का हक चाहते हैं। इधर भारत में अछूत गांधीजी पर चिढ़ गए थे और सवर्ण आंबेडकर पर। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि गांधीजी का विरोध करनेवाला यह युवक है कौन। गांधीजी के अंधभक्त बाबासाहेब को ‘देशद्रोही’, ‘भीमासुर’, ‘चार्वाक’, ‘आस्तीन का साँप’, ‘अंग्रेजों का बगलबच्चा’ जैसे दुर्वचनों से संबोधित कर रहे थे।”(डा भीमराव आंबेडकर : व्यक्तित्व विकास—डा सूर्यनारायण रणसुभे, पृष्ठ संख्या-49)।
गांधी को आंबेडकर का सवाल परेशान कर रहा था लेकिन उसी के साथ जहाँ वे अछूतों के साथ सवर्ण समाज की एकता कायम करने के लिए चिंतित थे वहीं वे इस बात से भी बेचैन थे कि पृथक निर्वाचन की पद्धति लागू होने के बाद अछूतों पर अत्याचार न हो। गांधी ने 31 अक्तूबर 1931 को कहा –
अछूत श्रेष्ठ वर्ग के शासन में हैं। वे श्रेष्ठ वर्ग उनका पूरी तरह से दमन कर सकते हैं या उन पर पूरी तरह से प्रतिशोध की कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि वे उनकी मर्जी पर हैं। मैं अपनी शर्म आपके समक्ष रख सकता हूँ लेकिन मैं उनके लिए संपूर्ण विनाश को कैसे आमंत्रित कर सकता हूँ? क्या मैं वैसे अपराध का दोषी नहीं बनूँगा?
(मोहनदास—-राजमोहन गांधी, पृष्ठ संख्या-360, पेंगुइन बुक्स)
उधर गांधी, आंबेडकर को भी अपनी तरफ खींचने में लगे थे और उन्होंने उन्हें खुश करने के लिए जो टिप्पणी की वह भारत का कोई भी सवर्ण नेता नहीं कर सकता था—
मेरे मन में आंबेडकर के लिए सर्वोच्च सम्मान है। उन्हें कटु होने का पूरा हक है। यह उनका संयम ही है कि वे हमारा सिर नहीं फोड़ दे रहे हैं। मेरे साथ यही स्थिति दक्षिण अफ्रीका प्रवास के आरंभिक दिनों में हुई थी। मैं जहाँ भी जाता था वहाँ हमें यूरोपीय रोष का सामना करना पड़ता था। इसलिए आंबेडकर द्वारा अपना गुस्सा निकालना स्वाभाविक ही है।
13 नवंबर को जो अल्पसंख्यक समझौता हुआ उसपर डा आंबेडकर और आगाखान के दस्तखत थे। उसमें मुस्लिमों, अछूतों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और भारत में रहनेवाले यूरोपीय लोगों की खातिर भारतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की माँग की गई। न सिर्फ इस समझौते ने गांधी की पूरी योजना को विफल कर दिया बल्कि कांग्रेस विरोधी अल्पसंख्यकों ने एक ऐसा मोर्चा बनाया जिसने गोलमेज सम्मेलन को गांधी की माँगों को स्वीकार करने से रोक दिया। गांधी ने कहा कि वे इससे ज्यादा अपमानित कभी नहीं हुए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी दलील और रणनीति तैयार कर ली थी। एक तरफ तो उन्होंने पृथक अछूत निर्वाचन क्षेत्र को एक भयावह किस्म का स्थायी विभाजन करार दिया वहीं अपनी भावना और योजना व्यक्त करते हुए कहा –
मैं भारत की आजादी पाने के लिए भी अछूतों का अहम हित बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं दावा करता हूँ कि निजी तौर पर अछूतों के व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा दावा है कि अगर जनमत संग्रह हुआ तो मैं उनके वोट हासिल करूँगा और चुनाव में जीत भी। आज हिंदू समाज सुधारकों का ऐसा संगठन है जो अस्पृश्यता का दाग मिटाने को तैयार है। सिख जैसे हैं वैसे हमेशा ही रहेंगे। वैसा मुसलमानों और यूरोपीयों के साथ भी है। क्या अछूत हमेशा अछूत ही रहेंगे।
गांधी का कहना था कि हर गाँव में जो विभाजन है उसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र और बढ़ाएगा। जो लोग अलग चुनाव क्षेत्र की माँग कर रहे हैं वे नहीं जानते कि आज का भारतीय समाज कैसे बना है। अपनी बात को उन्होंने एक घोषणा के साथ समाप्त किया –
मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूँ कि अगर इस फैसले पर विरोध करनेवाला मैं अकेला ही बचा तो मैं अपनी जान की कीमत पर इसका विरोध करूँगा।
दूसरे अर्थों में वे आमरण अनशन करेंगे। (मोहनदास—राजमोहन गांधी, पृष्ठ 361, पेंगुइन बुक्स)
गांधी ने ब्रिटिश नेताओं और उनके प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि गोलमेज सम्मेलन नाकाम रहा। बातचीत के माध्यम से स्वराज प्राप्त करने का रास्ता विफल हो चुका है और जंग होगी।
गांधी और आंबेडकर की यह लड़ाई यूरोप से देश तक फैल चुकी थी। भारत के दोनों नेताओं को तार भेजे जा रहे थे। कुछ अछूतों ने गांधी को भी तार भेजे थे लेकिन कहा जाता है कि आंबेडकर को भेजे गए तारों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी। एमसी राजा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अस्पृश्य परिषद का सम्मेलन संपन्न हुआ। परिषद ने आंबेडकर को समर्थन दिया। इधर देश में नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह तेज हुआ तो संघ और हिंदू महासभा के नेता वीएस मुंजे और विनायक दामोदर सावरकर ने गांधी का विरोध करते हुए आंबेडकर का समर्थन किया।
गांधी को लगता था कि अंग्रेज हिंदू समाज को विभाजित कर रहे हैं इसलिए उन्हें आजादी की लड़ाई के साथ उनसे इस मोर्चे पर टक्कर लेनी ही होगी। लेकिन साथ ही वे हिंदू समाज की छुआछूत भावना के विरुद्ध भी समाज को झटका देना चाहते थे। गांधी 28 दिसंबर 1931 को बंबई पहुँचे लेकिन उससे पहले नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके भाई गिरफ्तार हो चुके थे। चार जनवरी 1932 की अलसुबह गांधी को भी मुंबई के मणिभवन से गिरफ्तार कर लिया गया। वायसराय विलिंगटन ने तय कर रखा था कि इस बार कांग्रेस को खत्म कर देना है। कांग्रेस के इतिहासकारों के अनुसार 75,000 लोग गिरफ्तार हुए और चार लाख लोगों को लाठियों से पीटा गया।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.