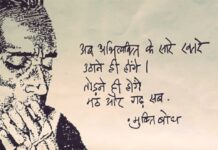— ध्रुव शुक्ल —
सुना है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी प्रधानमंत्री जी को हर साल पके हुए ताजे आम भेजती हैं। आम का नाम लेने से आम आदमी की याद आती है जो हर हाल में सबके साथ घुल-मिलकर जीवन को मीठा और रसपूर्ण बनाये रखने की कला जानता है। पर राजनीतिक दलों को कच्चा ‘आम’ पसंद है। उनकी राजनीति अभी तक लोकतंत्र में पके हुए ‘आम’ का स्वाद नहीं जान पायी और खु़द कच्ची रह गयी।
एक पके हुए आम को चखो और देखो तो लगता है कि प्रकृति उसे सर्वधर्म समभाव के फल की तरह ही पकाती है। वह अपने हरे छिलके के भीतर सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न भगवा रंग को पकाकर सबके लिए मिठास में बदल देता है। उसकी गुठली के भीतर उजला-सफेद चंद्रमा उगा दीखता है। उसे चखते हुए देश के तिरंगे झण्डे की याद आती है। कहते हैं कि मुगल बादशाह उत्तर भारत के आमों की किस्मों का पूरा ख़याल रखते थे। आम कई किस्म के खट-मिट्ठे स्वाद वाले होते हैं। उन्हें जात-पांत में बांटकर खाने से उनका स्वाद चला जाता है।
राजनीति सरसों के तेल जैसी हो गयी है। उसे कच्चे आम खाने की जल्दी मची रहती है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में ‘आम ‘को पूरा पकने नहीं देते। इससे पहले कि वह खुद लोकतंत्र की शाखा पर पककर अपनी स्वतंत्रता का पूरा स्वाद ले पाये, उसे कच्चा ही तोड़कर सत्ता की बरनी में अपने मन का अचार डाल लेते हैं। जिन राजनीतिक दलों के अचार और विचार में फफूंद लग जाती है वे अपनी खाली बरनियां लिए अगले पांच साल तक सत्ताधारी दल के ‘आम’ के अचार पर लार टपकाते रहते हैं।
जिस तरह आम आदमी के स्वभाव की, उसी तरह आमों की भी कई किस्में हैं और उनमें कई तरह की मिठास होती है। राजनीति पके हुए आमों की तरह आम आदमी के जीवन के विविध मीठे स्वादों को भूलती जा रही है। तभी तो राजनीति में खटास बढ़ती ही जा रही है। आमों की किस्मों में एक लंगड़ा आम भी होता है। ऐसा लगता कि ज़्यादातर नेता लंगड़ा आम खाकर किसी तरह अपने-अपने लंगड़े दलों को संभाले हुए हैं। कुछ दल तो लूले भी हैं, भले ही लूला आम नहीं होता। गूंगे,बहरे और अंधे आम भी नहीं होते। पर ‘आम’ जीवन के बीच अनकही, अनसुनी और अनदेखी की हवा चल रही है। लोकतंत्र के वृक्ष से अधपके आम टपक रहे हैं। पत्थर मारकर गिराये जा रहे हैं।
आमों पर कोयल बोल रही है। वोटरों की राजनीतिक बस्तियों से कौओं की कांव-कांव ही सुनायी दे रही है। राजनीतिक दलों के घोषणापत्र कच्चे आम की चटनी जैसे चटपटे तो लग रहे हैं पर उनमें विविध स्वाद वाला जीवन का मीठा आमरस नहीं छलक रहा।
—–
सरकार मसाला डोसा पकाने की विधि
आजमाइए और मजे से खाइए
सबसे पहले देश ही जनता को टुकड़ों में बांट लें। हिन्दू, मुसलमान, दलित, आदिवासी और पिछड़ी जनता के नाम पर उसके पांच टुकड़े तो कर ही लें। चाहें तो उनकी अलग-अलग ढेरियां बना लें, जैसे सब्जियों का थोक व्यापार करने वाले सब्जी मण्डी में आलू, प्याज, टमाटर, भिण्डी और बैंगन की ढेरियां लगाते हैं। वे आलू को प्याज में और प्याज को टमाटर में कभी लुढ़कने नहीं देते।
सब्जियां भले ही अलग-अलग भाव पर तौली जाती हों पर वे सांभर में उसी तरह हिल-मिल जाती हैं जैसे चुनाव जीतने के बाद हर जात-बिरादरी के फुटकर नेता। वे सत्ता की गली हुई दाल के सांभर रूपी स्वीमिंगपूल में तैरने लगते हैं और जनता ऐसे सूखने लगती है जैसे मैथी की भाजी। इसीलिए चुनाव के समय जनता को थोड़ी गीली रखें। उसे अपने संप्रदाय का भजन सुनाकर उस पर झूठी आशाओं का पानी ज़रूर छिड़कते रहें।
अपनी इच्छा के अनुसार टुकड़ों में बंटी हुई जनता से वोट झटक लेने के बाद आप अपने मन का सरकार मसाला डोसा और सांभर पकाने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। सांभर पकाने के लिए आपका यूनाइटेड प्रेशर कुकर बढ़िया होना चाहिए।
चुनाव जीतते ही गठबंधन के तवे पर एकजुटता के चुल्लू भर पानी का जोरदार किंचा मारिए और अपनी-अपनी खाली कटोरी के पेंदे से एक ऐसा गरमागरम संसदीय दल का नेता पूरे तवे पर फैलाइए जो अपनी आगोश में सारे आलुओं और प्याज को पहले ही ले सके। सबकी खाली कटोरी नारियल की चटनी से भर सके। सरकार मसाला डोसा में अल्पसंख्यक काजू और महिला आरक्षण की किशमिश भी दिखना चाहिए। उसमें किसा हुआ निर्दलीय नारियल भी ज़रूर होना चाहिए।
तो लीजिए बन गया — सरकार मसाला डोसा। अब उसकी रूमाल की तरह तहें बना लें और उसके चारों तरफ़ बैठकर उसे उसी तरह खायें जैसे मंत्रिमण्डल की बैठक में तले हुए काजू पर टूट पड़ते हैं। कभी-कभार अंदाज ठीक न रहने से सब्जियां ज़्यादा कट जाती हैं और वे सत्ता के सांभर में तैरने की आस लगाये रहती हैं। उनकी इच्छा होती है कि वे सत्ता का सलाद ही बन जायें।
सांभर एक ऐसा व्यंजन है जिसमें तैरती भांति-भांति की सब्जियां दलीय एकता के भ्रम में डाले रहती हैं। सरकार मसाला डोसा की बगल में कटोरी में भरा हुआ सांभर ऐसा दिखता है जैसे कोई निगम मण्डल हो। सत्ता की गली हुई दाल में तैरती सब्जियां उसमें ऐसे शोभती हैं जैसे निगम मण्डल की सदस्य बना दी गयी हैं। मनोनीत अध्यक्ष के रूप में बैंगन अलग चमकता है। अगर राजनीतिक मौसम के अनुरूप सदस्य अनुपस्थित हैं तो बैंगन की अध्यक्षता में उसके साथ अकेली लौकी ही सांभर के स्वीमिंगपूल में तैरती है।
आप एक बार में खूब सारा सांभर पका लें जिसमें डुबाकर पूरे पांच साल सरकार मसाला डोसा खाया जा सके। मजे से पकाइए। सत्ता तो वातानुकूलित होती है। वहां तो सड़े हुए को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इतना जरूर है कि सरकार मसाला डोसा पकाने के लिए जिस जनता को टुकड़ों में बांटा जाता है उसका जीवन उमस और बदबू से भरी सब्जी मण्डी जैसा हो जाता है।
राजनीति में जलेबीवाद का आगमन
जब नेता लोकहित के विचारों को त्यागकर केवल अपनी सत्ता की चिन्ता करने लगते हैं तभी राजनीति में जलेबीवाद की शुरुआत होती है। राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच अपने-अपने दलों की छोटी-बड़ी गुमटियां सजाकर केवल अपनी बातों के पनीले शीरे में डूबीं जलेबियां बनाने लगते हैं। उनमें राजनीति के सर्वोच्च जलेबीवादी प्रवर्तक से आगे निकलने की होड़ लगने लगती है। जलेबीवाद का प्रमुख सिद्धांत यह पाया गया है कि — एक ही प्रकार की राजनीतिक चाशनी में अपनी-अपनी जलेबियां डुबाकर हर हाल में सत्ता प्राप्त की जाये।
समाज में ऊंचे, मध्यम और पिछड़े वर्ग की तरह जलेबियां भी तीन प्रकार की होती हैं। उड़द की दाल से बनी और गायछाप रंग में रंगी इमरती घी से भरी गरम कड़ाही में अचानक किसी फूल-सी खिलकर तैरती हुई ऊपर आ जाती है। यह जलेबी ऊंचे राजनीतिक-सामाजिक और आर्थिक वर्गों को आजकल खूब पसंद है। गोरी मैदा में ख़मीर उठाकर कड़ाही में तैरती जलेबियां रोज़ सबेरे शहरी मध्यवर्ग के नाश्ते में जगह बनाये हुए हैं। देशी मावे से बनी कत्थई-काली जलेबियां गरीब गांवों के मेले-ठेलों में खूब बनती हैं। इन पर बैठे बर्र-चीटों को देखकर लगता है कि जैसे जलेबीवादी इनका खून चूस रहे हों।
सत्ता पाने के राजनीतिक जलेबीवाद ने इमरती को ऊंचा उठाकर गोरी और कत्थई-काली जलेबियों के बीच विभेद पैदा करके शहरी गोरी जलेबियों को इमरती के पक्ष में फुसला लिया है। गांवों की कत्थई-काली जलेबियां कभी इस दल के और कभी उस दल के पनीले शीरे में डूबती-उतराती रहती हैं । उन्हें जात-पांत के नाम पर खुलेआम चूसने वाले जलेबीवादी बर्र-चीटों से अब तक छुटकारा नहीं मिला। जलेबीवादी उन्हें इस भ्रम में डुबाये रहते हैं कि एक दिन काली-कत्थई जलेबियों को भी इमरती होना है।
राजनीति में आये इस जलेबीवाद पर विचार करते हुए यही लग रहा है कि जनता को इमरतियां खिलाने की झूठी आशाओं में भरमाकर केवल जलेबीदार बातें बनाना ही जलेबीवाद है। वे उस गुलाब जल की खुशबू से भरी मीठी जलेबियां कहीं नहीं हैं जिन्हें एक दिन जनता बराबरी से बैठकर खा सकेगी। सत्ता की इमरती पाने की इच्छा भी ऐसा जागतिक भ्रम है जिसकी चाहत में जलेबीवादी नेता एक-दूसरे को धकेलकर न जाने किस राजधानी की ओर दौड़े चले जा रहे हैं?
ईश्वर की मृत्यु, इतिहास का अंत और विचारों से विदाई की घोषणाएं तो बीसवीं सदी में हो गयी हैं। अब इक्कीसवीं सदी — साधनों की मृत्यु, धर्मों के पतन और परहित की विदाई के लिए जानी जायेगी। राजनीतिक जलेबीवाद इसलिए अपनी जड़ें जमा पा रहा है क्योंकि जलेबीवादियों की कुंदमति से उत्पन्न जीवन विरोधी कुतर्कों का प्रवर्तन सामाजिक जीवन में बढ़ती संवेदनात्मक लापरवाहियों से भरी भीड़ के बीच ही हो सकता है।
—–
अनसुनी-अनदेखी के साम्राज्य में
थक गये हैं शिल्पकार
पत्थरों को तराशकर
मिटा न पाये अब तक
अनसुनी-अनदेखी का साम्राज्य
कविताएं सुना रहे हैं कवि
तराशे गये पत्थरों को
जगा रहे हैं सदियों से
संगीतकार भैरवी गाकर
थक गये हैं लोग
बजा-बजाकर घण्टियां
क्यों लगता है सबको
पत्थर देख रहे हैं उनकी ओर
पत्थरों से टकराकर
वहीं झर जाते हैं शब्द
आंखें हो जाती हैं भारी
मुरझा जाती है मुस्कान
पत्थरों से झरती प्रपा
सदियों पहले सूख गयी
प्यासे खड़े हैं लोग
देवालय के बाहर
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.