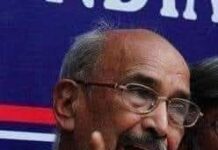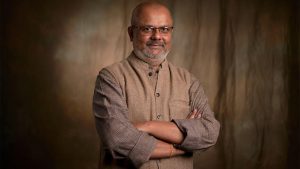
— रमेश शर्मा —
(यह लेख आईटीएम यूनिवर्सिटी, ग्वालियर में अनुपम मिश्र स्मृति व्याख्यान-3 पर आधारित है।)
धरती हम सब की धरोहर है, वह इसलिए कि इसी धरती पर हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ें फैली हुई हैं और इसलिए भी कि इन जड़ों की सशक्तता अथवा असशक्तता ही हमारे भविष्य का निर्णायक संकेतक है/होगा। इस धरती में मानवीय गतिविधियों का संक्षिप्त इतिहास, संभावनाओं और समस्याओं का जटिल घालमेल है– धरती के सीमित संसाधनों की अंधाधुंध लूट के चलते इन संसाधनों पर निर्भर रहने वाले मानव और दूसरे जीव-जंतुओं का पतन प्रारंभ होना इसका प्रथम प्रमाण है। इसीलिए आज इस धरती के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील होना, हम सबके समक्ष विकल्प नहीं बल्कि अपरिहार्य विवेकशीलता की कसौटी है।
विगत 400 बरसों के कालखंड में जल-जंगल और जमीन का साझा इतिहास – पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक काल में हुए साम्राज्यवादी विस्तार, विश्वयुद्ध और उसके बाद आए औद्योगिक काल, कल्याणकारी राज्यों के उदय और विकास की भूख – और फिर इन साझे संसाधनों के अराजक अधिग्रहणों के काल तक की यात्रा – कुल मिलाकर इस धरती की हमारी धरोहर अर्थात् साझे संसाधनों के पतन का अतीत और व्यतीत है।
इन साझे संसाधनों को बचाने का संघर्ष ही – अपने अर्थात् मानव जाति (और समग्र सजीवों) को कल के सुरक्षित भविष्य की उम्मीद देना है। और उस सुरक्षित भविष्य के लिए आज हमारा विवेकशील होना शायद पहली और अंतिम शर्त हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हुए हम विवेकशील होने का प्रयास करें।
संपन्नता का साम्राज्य
आज से लगभग 170 बरस पूर्व (वर्ष 1854 में) अमरीकी महाद्वीप के सुदूर पश्चिम क्षेत्र में अमरीकी साम्राज्य के विस्तार के लिए तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन ने मूलनिवासी ‘अमरीकी रेड इंडियंस’ के प्रमुख को प्रस्ताव दिया कि वे गोरे अमरीकी लोगों की नई बस्तियों के लिए रेड इंडियन्स से 1.5 लाख डॉलर के एवज में 20 लाख एकड़ भूमि खरीदना चाहते हैं। इसके जवाब में अमरीकी रेड इंडियंस के मुखिया, जिन्हें ‘सियेटल का प्रमुख’ भी कहा जाता था, ने ‘वाशिंगटन के प्रमुख’ अर्थात् अमरीकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन को विस्तार से उत्तर दिया।
इस ऐतिहासिक पत्र का सारांश है :
जिस धरती से जनमी यह काया
आखिर उस मातृभूमि का मूल्य कैसे लगाओगे ?
हम सौदा नहीं कर सकते
अपने अन्नदा धरती और पुरखा पहाड़ का
लेकिन यदि फिर भी लेना चाहते हो इसे
तो वचन दो
यह धरती – पेड़-पौधों में बसे देवता – नदियों की उन्मुक्तता
सौंपोगे अपने वंशजों को वैसे ही अलक्षित
जैसा आज हम तुम्हें दे रहे हैं
प्रेम करना इस वसुन्धरा से उतना ही – जितना ईश्वर का शाश्वत प्रेम है
हम सबके लिए
बाद के लगभग 100 बरसों के औपनिवेशिक कालखंड में लगभग 5 करोड़ 60 लाख रेड इंडियंस मूलनिवासियों का नरसंहार हुआ और उत्तर-मध्य व दक्षिण अमरीका में रक्तरंजित उपनिवेशों की स्थापना हुई। और फिर औपनिवेशिक साम्राज्यों के विस्तार के चलते संसाधनों की लूट का अध्याय प्रारंभ हुआ- जो आज भी जारी है।
उपनिवेशकाल
उपनिवेशकाल – शायद मानव सभ्यता के संक्षिप्त इतिहास का सबसे अराजक काल रहा है जब संसाधनों की लूट के साथ-साथ उन संसाधनों के संरक्षकों अर्थात् मूलनिवासियों को गुलाम बनाया गया। अपनी ही धरती पर फ्रेंच साम्राज्य के गुलाम सेनेगली हों अथवा ब्रितानिया साम्राज्य के गुलाम ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी हों अथवा पुर्तगाली साम्राज्य के समक्ष गुलाम बना दिये गये ब्राजीलियाई कबीले हों अथवा स्पेनी साम्राज्य के गुलाम कोलम्बियाई आदिवासी हों – वास्तव में वे तमाम समानताएँ अपने जल-जंगल- जमीन की स्वाधीनता और स्वशासन के लिए संघर्ष कर रहे उन मूलनिवासियों के कत्ल, गुलाम और विकलांग बना दिये गये उनकी पीढ़ियों, मिटा दी गयी उनकी संपन्न सभ्यताओं की विरासतों, मूक कर दिये गये उनके लोकगीतों और पूरी तरह से शब्दहीन कर दिये गये उनके प्रतिरोध के लोकगीतों और लोक कथाओं का लिखित-अलिखित, भूला-बिसरा, आधा-अधूरा और सुना-अनसुना इतिहास है।
विश्वविख्यात पुस्तक ‘चिरायु पृथ्वी’ बताती है कि ब्रितानिया हुकूमत द्वारा गुलाम देशों के संसाधनों के सरकारीकरण के लिए वर्ष 1770 से 1830 के मध्य ब्रिटिश संसद के द्वारा 3280 कानून पारित और लागू किये गये जिसका मकसद पूरी दुनिया में सामुदायिक संसाधनों की बाड़बंदी थी – जिसके परिणामस्वरूप दुनिया के लगभग 44 फीसदी जंगल और लगभग 53 फीसदी कृषिभूमि को, ब्रिटिश सरकार की मिलकियत घोषित कर दिया गया।
इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ मूलनिवासी, आदिवासी अपने ही जल-जंगल और जमीन पर लगान देनेवाले किसान, मजदूरी करनेवाले भूमिहीन और जंगलों में अतिक्रमणकर्ता घोषित कर दिये गये। 20वीं सदी के आते-आते अनुमानतः दुनिया के लगभग 80 फीसदी प्राकृतिक संसाधनों को दुनिया की 6 औपनिवेशिक शक्तियों के मध्य लूट-खसोट का केंद्र और बाद के बरसों में विश्वयुद्धों का कारण बनाया गया।
विश्वयुद्ध
आज दुनियाभर में 6 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर ‘युद्धों और हिंसक संघर्षों’ के कारण हुए प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने और उसे रोकने के लिए संगठित प्रयासों के स्मरण का दिवस मनाया जाता है। विश्व इतिहास प्रोजेक्ट के अनुसार औपनिवेशिक काल में संसाधनों की लूट में अपने यूरोपीय पड़ोसियों से पिछड़ने के कारण स्वरूप जर्मनी में प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से विश्वयुद्ध की शुरूआत की और फिर लगभग दो-तिहाई दुनिया इससे धुलस गयी। एक ऐसा भयावह युद्धकाल जिसमें सैनिकों की मौत अथवा हत्या की संख्या के आधार पर – नायक का फैसला नहीं, बल्कि संसाधनों की तबाही के लिए जवाबदेही के आधार पर- खलनायक का निर्णय होना चाहिए।
क्या आप जानते हैं कि विश्वयुद्धों के सबसे बड़े लाभार्थी कौन थे?ड्यू पोंट कंपनी जो बारूद अर्थात् डायनामाइट बनाती थी और जिसके खरीदार हरेक पक्ष थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार विश्वयुद्धों के दौरान ड्यू पोंट कंपनी को लगभग 1.5 बिलियन पौंड का मुनाफा हुआ था।
लेकिन विश्वयुद्ध खत्म होते ही ड्यू पोंट कंपनी के पास बड़ी चुनौती थी कि अथाह बारूद का क्या किया जाए? केमिकल इंजीनियर ने मिलकर बारूद से पहली बार नाइट्रेट का नया फार्मेशन अर्थात् यूरिया और सुपर फास्फेट बनाया जिसने कृषि को उद्योग में बदल दिया। जो बारूद किसी की जिन्दगी एक बार में समाप्त कर सकता था उसे धीमे जहर में बदल दिया गया और फिर इन रासायनिक उर्वरकों के चलते हरित क्रांति या हरित भ्रान्ति का नया दौर शुरू हुआ।
आज इस तथाकथित हरित क्रांति के अमानवीय दुष्परिणामों को पंजाब के भटिंडा से राजस्थान के बीकानेर तक चलने वाले कैंसर एक्सप्रेस की कहानियों में सुना-देखा जा सकता है। पंजाब का मालवा प्रान्त हरित क्रांति के दौर और उसके बाद खतरनाक सीमा तक खेती के नाम पर हुए रसायनों–उर्वरकों और दूसरी जहरीली दवाइयों के दुरुपयोग का एक अर्थ में तो ‘जिन्दा’ लेकिन शनैः-शनैः दम तोड़ता उदाहरण है।
औद्योगिक क्रांति
बीसवीं सदी और उसके साथ आए औद्योगिक क्रांति का नया दौर मूलतः मशीनों और रासायनिक और मेटालार्जिक तकनीकों के उपयोग-दुरुपयोग का था – जिसके चलते जनसंख्या, खाद्य उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़े और फिर विकास का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन इसी क्रम में खेती को उद्योग और उद्योग को विकास की विरासत मशीन में बदल दिया गया।
विश्वविख्यात पुस्तक ‘चिरायु पृथ्वी’ के अनुसार विगत 150 बरसों की औद्योगिक क्रांति और फिर हरित क्रांति के चलते आज लगभग 70 फीसदी घास के मैदान, 56 फीसदी जंगल, 40 फीसदी स्थानीय जलस्रोत पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं।
और फिर इन संसाधनों पर निर्भर रहनेवाले दुनिया की तथाकथित अविकसित तथा विकासशील देशों की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या को उनकी आजीविका और अधिकारों से वंचित करते हुए – हमने उन्हें हमेशा के लिए गरीबी के गर्त में धकेल दिया है। अर्थात् हमने सीखा कि – नई क्रांति के इस नये दौर में लोगों को गुलाम बनाने के अमानवीय कृत्य के बजाय संसाधनों की अंधाधुंध लूट और अधिग्रहण के माध्यम से उन्हें हमेशा के लिए गरीबी की गुमनामी में धकेला जा सकता है। और फिर यह भी सीखा कि उनके परमार्थ के लिए गरीबी उन्मूलन और विकास की नियमावली के तहत कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, उन्हें भ्रष्ट और जर्जर राज्यों पर स्थायी रूप से परजीवी (अथवा योजनाजीवी) बनाये रख सकती है। जहाँ उनकी हैसियत ‘अधिकार संपन्न नागरिक’ से अपघटित करके ‘अधिकार-विहीन लाभार्थी’ की कर दी जा सकती है। यह संसाधनों की लूट के नये तरीके और लुट चुके लोगों के परमार्थ हेतु जनतंत्र के नये फरमान और जर्जर राज्यों द्वारा संसाधनों की लूट के नये विधान हैं।
पर्यावरण
जब भी हम पर्यावरण के विषय में सोचते हैं अथवा कुछ कहना चाहते हैं तो जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधन ही हमारे दिमाग में आते हैं। आज भारत के संदर्भ में इन समाप्त होते संसाधनों और पर्यावरण की समीक्षा के साथ अपने साझा भविष्य का खुला आकलन आवश्यक है।
आज की आर्थिक दुनिया में सकल घरेलू उत्पादन अर्थात् जी.डी.पी. का बढ़ना ही विकास का प्रमुख पैमाना है – इसलिए आज के विकास और जीडीपी के मध्य शरीर और आत्मा का स्थापित संबंध है। यदि यह सही है तो पर्यावरण-अर्थशास्त्र के कुछ बुनियादी सिद्धांतों और उनके अर्थ और अनर्थ को समझना जरूरी हैं।
सैद्धांतिक रूप से जंगल में खड़े साल-सरई के पेड़ की जी.डी.पी. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक लगभग नगण्य होती है। लेकिन यदि जंगल के इस साल-सरई के पेड़ को काट दिया जाए और ट्रक से टिम्बर मार्ट में ले जाकर उसका फर्नीचर बना दिया जाए तो इसका जी.डी.पी. कई गुना बढ़ जाएगा।
सैद्धांतिक रूप से एक बहती हुई नदी का जी.डी.पी. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक लगभग नगण्य होता है। लेकिन यदि नदी में बाँध बना दिया जाए- उसका पानी उद्योगों को दिया जाए – उन उद्योगों के अपशिष्ट को नदी में फेंक दिया जाए और फिर नदी को साफ करने के लिए जल-शोधन संयंत्र लगा दिया जाए तो नदी का जी.डी.पी. लगभग दसों गुना हो जाएगा।
सैद्धांतिक रूप से धरती के नीचे दबे कोयले का जी.डी.पी. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक लगभग नगण्य होता है। लेकिन यदि धरती के नीचे दबे कोयले को निकालने के लिए जंगलों को काट दिया जाए और धरती का सीना चीरकर कोयले को निकालकर बिजली बनायी जाए और उस बिजली तथा ईंधन के जलने से हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उद्योगों में वायु शोधन यंत्र, घरों में एयर फिल्टर और एयर कंडीशन लगाया जाए तो जी.डी.पी. सैकड़ों गुना हो जाएगी।
अर्थात् इन उदाहरणों और उनके परिणामों से हम समझ सकते हैं कि मौजूदा विकास का अर्थ संसाधनों के रास्ते पूँजी की गतिशीलता है – श्रम की गतिशीलता नहीं, बल्कि मानवीय श्रम को मशीन; मशीन को कंप्यूटर; कंप्यूटर को रोबोटिक्स; रोबोटिक्स को आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस को न्यूरोमार्फिक कंप्यूटिंग से स्थापित-विस्थापित करते हुए हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जहाँ श्रम की समाप्त होती संभावनाएँ- बेरोजगारी के बाजार को जन्म दे रही हैं। श्रम के पराभव के नये दौर में गुलजार होते इस बाजार में किसी भी बेरोजगार की हैसियत एक ऐसे गुलाम की है जो अपने ही देश के लिए कोई संपत्ति साबित नहीं हो सकता।
(बाकी हिस्सा कल)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.